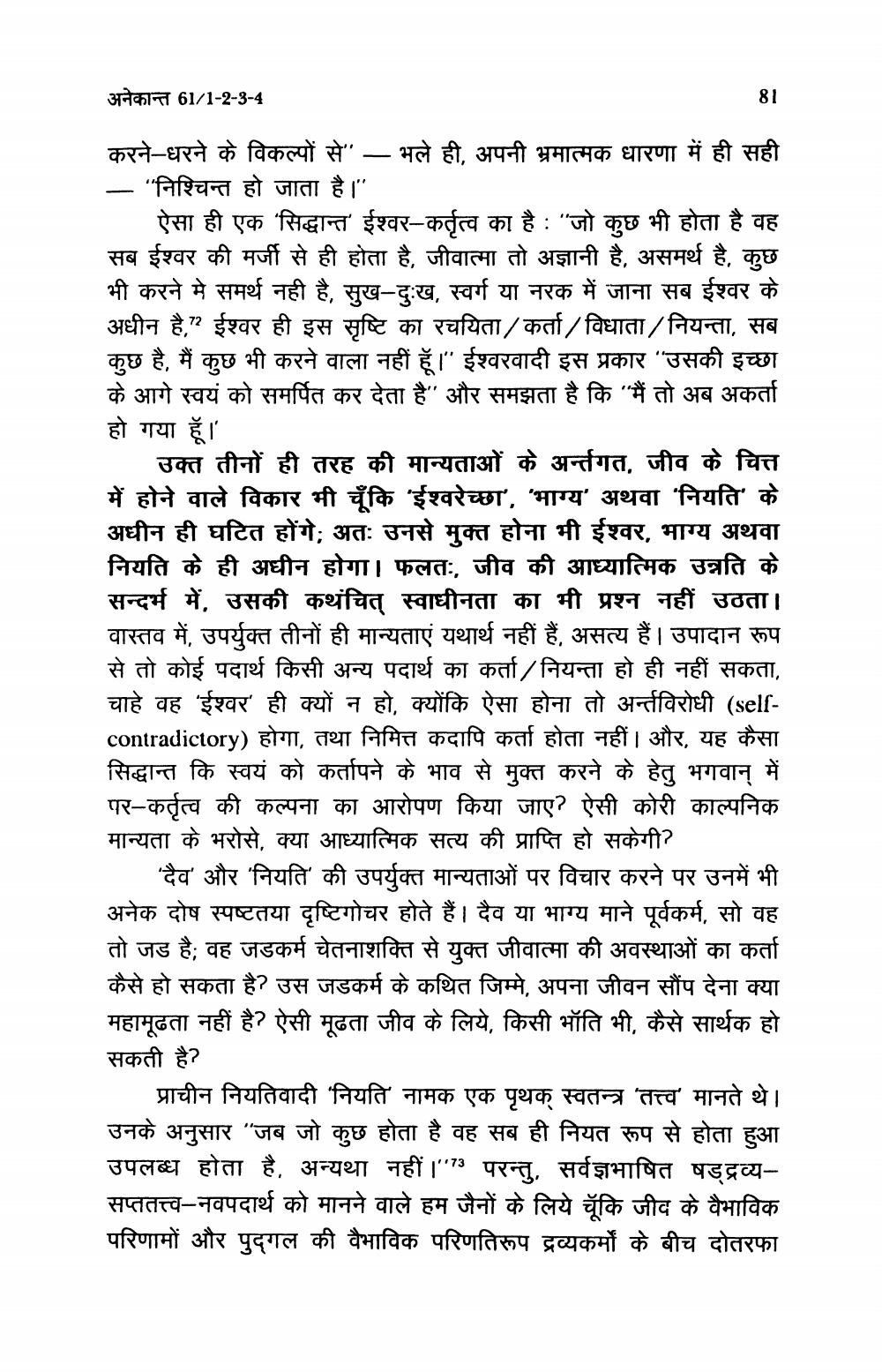________________
अनेकान्त 61/1-2-3-4
करने–धरने के विकल्पों से" - भले ही, अपनी भ्रमात्मक धारणा में ही सही - "निश्चिन्त हो जाता है।"
ऐसा ही एक 'सिद्धान्त' ईश्वर-कर्तृत्व का है : “जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है, जीवात्मा तो अज्ञानी है, असमर्थ है, कुछ भी करने में समर्थ नही है, सुख-दुःख, स्वर्ग या नरक में जाना सब ईश्वर के अधीन है,? ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता/कर्ता/विधाता/नियन्ता, सब कुछ है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ।" ईश्वरवादी इस प्रकार "उसकी इच्छा के आगे स्वयं को समर्पित कर देता है" और समझता है कि “मैं तो अब अकर्ता हो गया हूँ।
उक्त तीनों ही तरह की मान्यताओं के अर्न्तगत, जीव के चित्त में होने वाले विकार भी चूँकि 'ईश्वरेच्छा', 'भाग्य' अथवा 'नियति' के अधीन ही घटित होंगे; अतः उनसे मुक्त होना भी ईश्वर, भाग्य अथवा नियति के ही अधीन होगा। फलतः, जीव की आध्यात्मिक उन्नति के सन्दर्भ में, उसकी कथंचित् स्वाधीनता का भी प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में, उपर्युक्त तीनों ही मान्यताएं यथार्थ नहीं हैं, असत्य हैं। उपादान रूप से तो कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का कर्ता/नियन्ता हो ही नहीं सकता, चाहे वह 'ईश्वर' ही क्यों न हो, क्योंकि ऐसा होना तो अतविरोधी (selfcontradictory) होगा, तथा निमित्त कदापि कर्ता होता नहीं। और, यह कैसा सिद्धान्त कि स्वयं को कर्तापने के भाव से मुक्त करने के हेतु भगवान् में पर-कर्तृत्व की कल्पना का आरोपण किया जाए? ऐसी कोरी काल्पनिक मान्यता के भरोसे, क्या आध्यात्मिक सत्य की प्राप्ति हो सकेगी? ___'दैव' और 'नियति' की उपर्युक्त मान्यताओं पर विचार करने पर उनमें भी अनेक दोष स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। दैव या भाग्य माने पूर्वकर्म, सो वह तो जड है; वह जडकर्म चेतनाशक्ति से युक्त जीवात्मा की अवस्थाओं का कर्ता कैसे हो सकता है? उस जडकर्म के कथित जिम्मे, अपना जीवन सौंप देना क्या महामूढता नहीं है? ऐसी मूढता जीव के लिये, किसी भॉति भी, कैसे सार्थक हो सकती है?
प्राचीन नियतिवादी 'नियति' नामक एक पृथक् स्वतन्त्र 'तत्त्व' मानते थे। उनके अनुसार "जब जो कुछ होता है वह सब ही नियत रूप से होता हुआ उपलब्ध होता है, अन्यथा नहीं।'73 परन्तु, सर्वज्ञभाषित षड्द्रव्यसप्ततत्त्व-नवपदार्थ को मानने वाले हम जैनों के लिये चूंकि जीव के वैभाविक परिणामों और पुद्गल की वैभाविक परिणतिरूप द्रव्यकर्मों के बीच दोतरफा