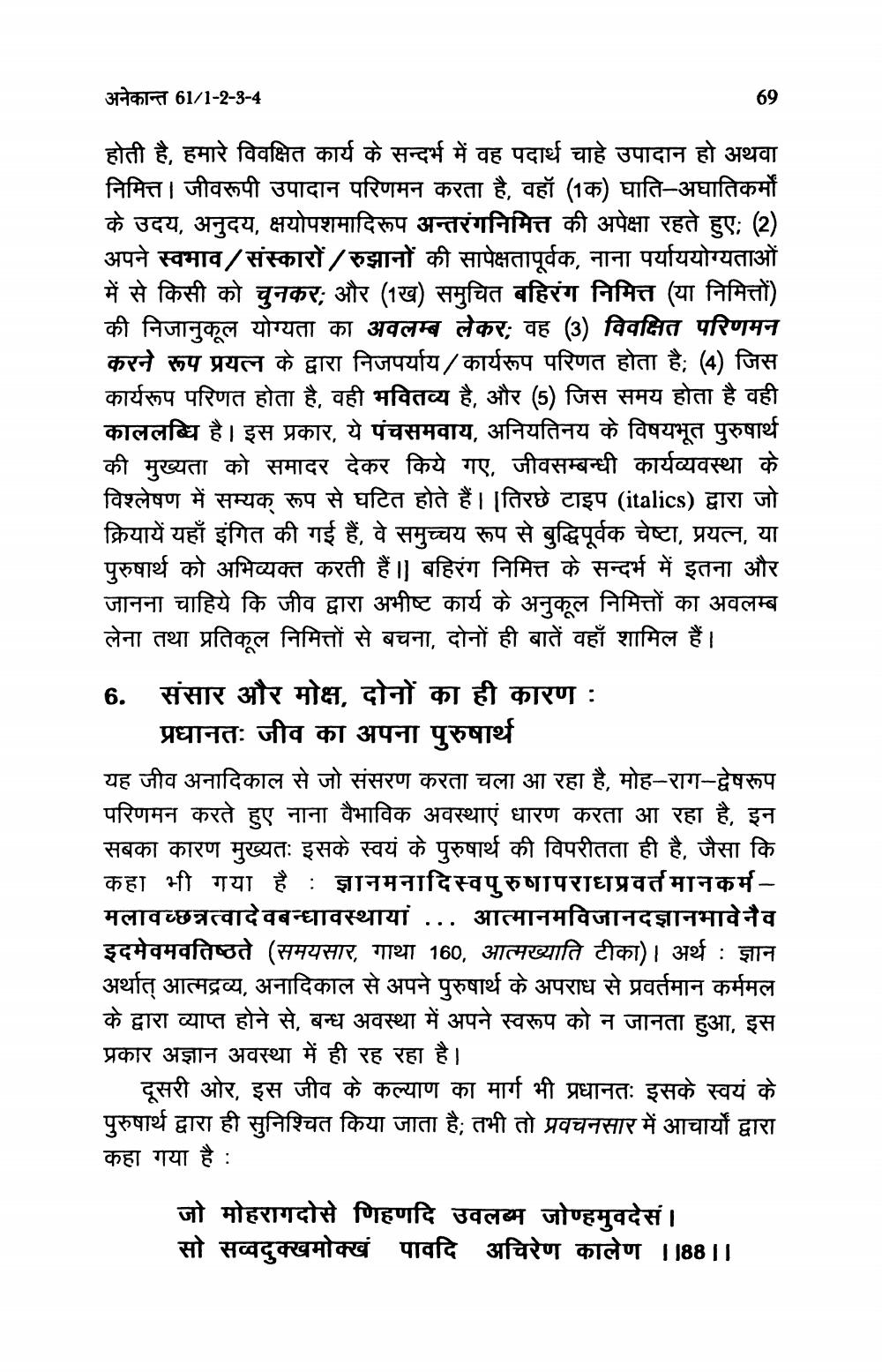________________
69
अनेकान्त 61/1-2-3-4 होती है, हमारे विवक्षित कार्य के सन्दर्भ में वह पदार्थ चाहे उपादान हो अथवा निमित्त । जीवरूपी उपादान परिणमन करता है, वहाँ (1क) घाति-अघातिकर्मों के उदय, अनुदय, क्षयोपशमादिरूप अन्तरंगनिमित्त की अपेक्षा रहते हुए; (2) अपने स्वभाव/संस्कारों/रुझानों की सापेक्षतापूर्वक, नाना पर्याययोग्यताओं में से किसी को चुनकर; और (ख) समुचित बहिरंग निमित्त (या निमित्तों) की निजानुकूल योग्यता का अवलम्ब लेकर; वह (3) विवक्षित परिणमन करने रूप प्रयत्न के द्वारा निजपर्याय/कार्यरूप परिणत होता है; (4) जिस कार्यरूप परिणत होता है, वही भवितव्य है, और (5) जिस समय होता है वही काललब्धि है। इस प्रकार, ये पंचसमवाय, अनियतिनय के विषयभूत पुरुषार्थ की मुख्यता को समादर देकर किये गए, जीवसम्बन्धी कार्यव्यवस्था के विश्लेषण में सम्यक् रूप से घटित होते हैं। [तिरछे टाइप (italics) द्वारा जो क्रियायें यहाँ इंगित की गई हैं, वे समुच्चय रूप से बुद्धिपूर्वक चेष्टा, प्रयत्न, या पुरुषार्थ को अभिव्यक्त करती हैं।] बहिरंग निमित्त के सन्दर्भ में इतना और जानना चाहिये कि जीव द्वारा अभीष्ट कार्य के अनुकूल निमित्तों का अवलम्ब लेना तथा प्रतिकूल निमित्तों से बचना, दोनों ही बातें वहाँ शामिल हैं। 6. संसार और मोक्ष, दोनों का ही कारण :
प्रधानतः जीव का अपना पुरुषार्थ यह जीव अनादिकाल से जो संसरण करता चला आ रहा है, मोह-राग-द्वेषरूप परिणमन करते हुए नाना वैभाविक अवस्थाएं धारण करता आ रहा है, इन सबका कारण मुख्यतः इसके स्वयं के पुरुषार्थ की विपरीतता ही है, जैसा कि कहा भी गया है : ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेवबन्धावस्थायां ... आत्मानमविजानदज्ञानभावेनैव इदमेवमवतिष्ठते (समयसार, गाथा 160, आत्मख्याति टीका)। अर्थ : ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्ममल के द्वारा व्याप्त होने से, बन्ध अवस्था में अपने स्वरूप को न जानता हुआ, इस प्रकार अज्ञान अवस्था में ही रह रहा है।
दूसरी ओर, इस जीव के कल्याण का मार्ग भी प्रधानतः इसके स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है; तभी तो प्रवचनसार में आचार्यों द्वारा कहा गया है :
जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्म जोण्हमुवदेसं। सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण |188 ||