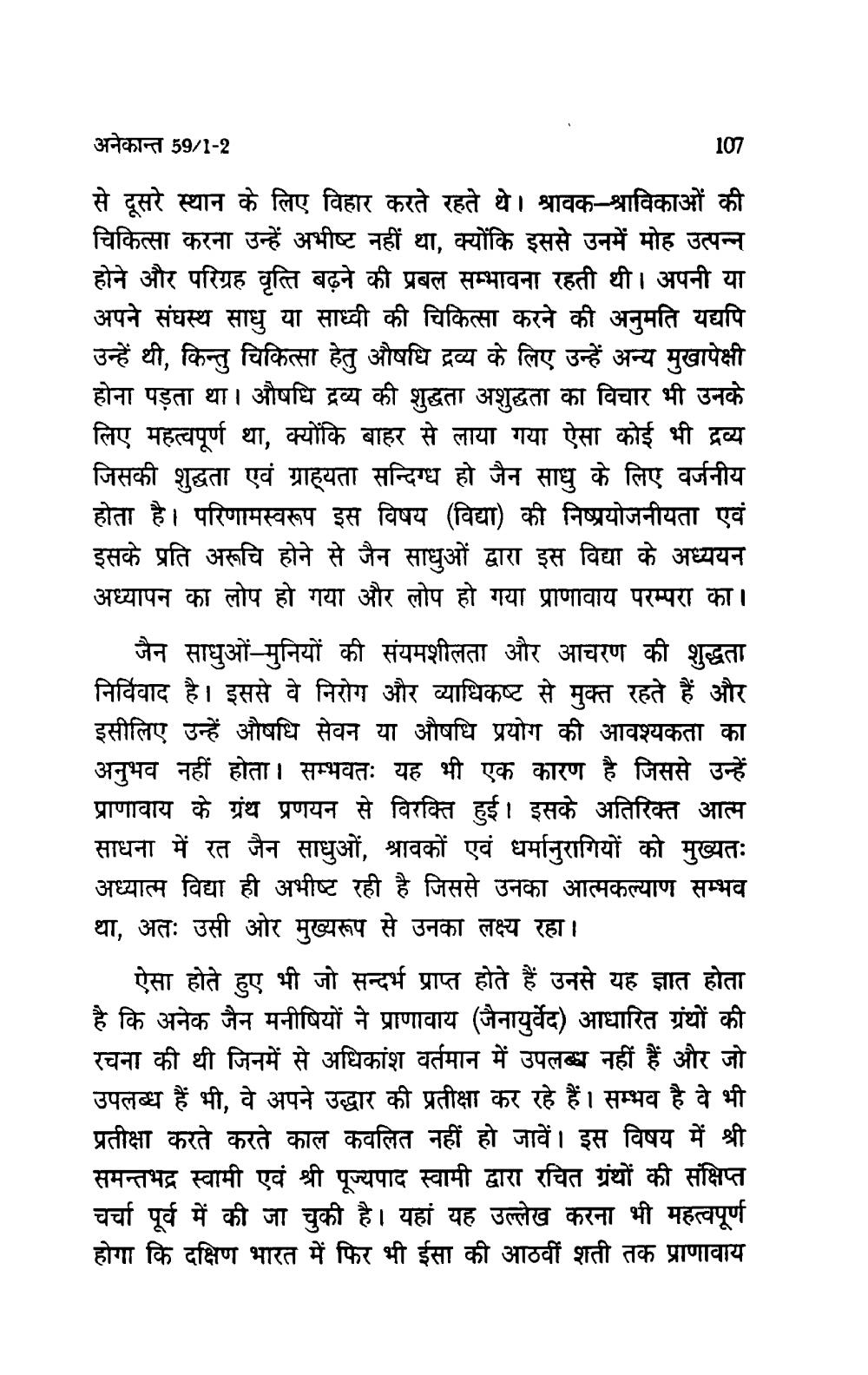________________
अनेकान्त 59/1-2
107
से दूसरे स्थान के लिए विहार करते रहते थे। श्रावक-श्राविकाओं की चिकित्सा करना उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि इससे उनमें मोह उत्पन्न होने और परिग्रह वृत्ति बढ़ने की प्रबल सम्भावना रहती थी। अपनी या अपने संघस्थ साधु या साध्वी की चिकित्सा करने की अनुमति यद्यपि उन्हें थी, किन्तु चिकित्सा हेतु औषधि द्रव्य के लिए उन्हें अन्य मुखापेक्षी होना पड़ता था। औषधि द्रव्य की शुद्धता अशुद्धता का विचार भी उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाहर से लाया गया ऐसा कोई भी द्रव्य जिसकी शुद्धता एवं ग्राह्यता सन्दिग्ध हो जैन साध के लिए वर्जनीय होता है। परिणामस्वरूप इस विषय (विद्या) की निष्प्रयोजनीयता एवं इसके प्रति अरूचि होने से जैन साधुओं द्वारा इस विद्या के अध्ययन अध्यापन का लोप हो गया और लोप हो गया प्राणावाय परम्परा का।
जैन साधुओं-मुनियों की संयमशीलता और आचरण की शुद्धता निर्विवाद है। इससे वे निरोग और व्याधिकष्ट से मुक्त रहते हैं और इसीलिए उन्हें औषधि सेवन या औषधि प्रयोग की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सम्भवतः यह भी एक कारण है जिससे उन्हें प्राणावाय के ग्रंथ प्रणयन से विरक्ति हुई। इसके अतिरिक्त आत्म साधना में रत जैन साधुओं, श्रावकों एवं धर्मानुरागियों को मुख्यतः अध्यात्म विद्या ही अभीष्ट रही है जिससे उनका आत्मकल्याण सम्भव था, अतः उसी ओर मुख्यरूप से उनका लक्ष्य रहा।
ऐसा होते हुए भी जो सन्दर्भ प्राप्त होते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि अनेक जैन मनीषियों ने प्राणावाय (जैनायुर्वेद) आधारित ग्रंथों की रचना की थी जिनमें से अधिकांश वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं और जो उपलब्ध हैं भी, वे अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्भव है वे भी प्रतीक्षा करते करते काल कवलित नहीं हो जावें। इस विषय में श्री समन्तभद्र स्वामी एवं श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ग्रंथों की संक्षिप्त चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि दक्षिण भारत में फिर भी ईसा की आठवीं शती तक प्राणावाय