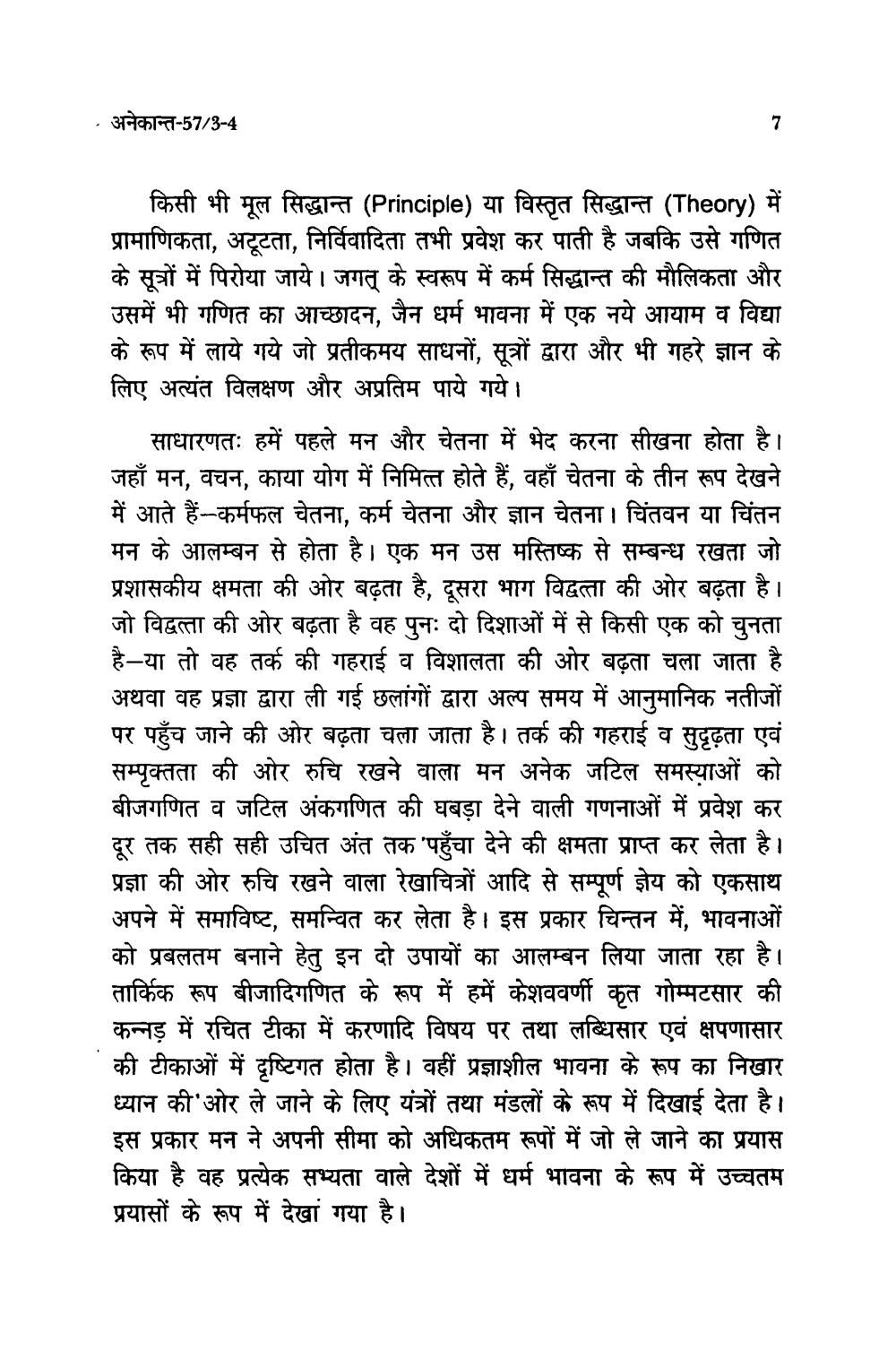________________
• अनेकान्त-57/3-4
किसी भी मूल सिद्धान्त (Principle) या विस्तृत सिद्धान्त (Theory) में प्रामाणिकता, अटूटता, निर्विवादिता तभी प्रवेश कर पाती है जबकि उसे गणित के सूत्रों में पिरोया जाये। जगत् के स्वरूप में कर्म सिद्धान्त की मौलिकता और उसमें भी गणित का आच्छादन, जैन धर्म भावना में एक नये आयाम व विद्या के रूप में लाये गये जो प्रतीकमय साधनों, सूत्रों द्वारा और भी गहरे ज्ञान के लिए अत्यंत विलक्षण और अप्रतिम पाये गये।
साधारणतः हमें पहले मन और चेतना में भेद करना सीखना होता है। जहाँ मन, वचन, काया योग में निमित्त होते हैं, वहाँ चेतना के तीन रूप देखने में आते हैं-कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। चितवन या चिंतन मन के आलम्बन से होता है। एक मन उस मस्तिष्क से सम्बन्ध रखता जो प्रशासकीय क्षमता की ओर बढ़ता है, दूसरा भाग विद्वत्ता की ओर बढ़ता है। जो विद्वत्ता की ओर बढ़ता है वह पुनः दो दिशाओं में से किसी एक को चुनता है-या तो वह तर्क की गहराई व विशालता की ओर बढ़ता चला जाता है अथवा वह प्रज्ञा द्वारा ली गई छलांगों द्वारा अल्प समय में आनुमानिक नतीजों पर पहुँच जाने की ओर बढ़ता चला जाता है। तर्क की गहराई व सुदृढ़ता एवं सम्पृक्तता की ओर रुचि रखने वाला मन अनेक जटिल समस्याओं को बीजगणित व जटिल अंकगणित की घबड़ा देने वाली गणनाओं में प्रवेश कर दूर तक सही सही उचित अंत तक पहुँचा देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा की ओर रुचि रखने वाला रेखाचित्रों आदि से सम्पूर्ण ज्ञेय को एकसाथ अपने में समाविष्ट, समन्वित कर लेता है। इस प्रकार चिन्तन में, भावनाओं को प्रबलतम बनाने हेतु इन दो उपायों का आलम्बन लिया जाता रहा है। तार्किक रूप बीजादिगणित के रूप में हमें केशववर्णी कृत गोम्मटसार की कन्नड़ में रचित टीका में करणादि विषय पर तथा लब्धिसार एवं क्षपणासार की टीकाओं में दृष्टिगत होता है। वहीं प्रज्ञाशील भावना के रूप का निखार ध्यान की ओर ले जाने के लिए यंत्रों तथा मंडलों के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार मन ने अपनी सीमा को अधिकतम रूपों में जो ले जाने का प्रयास किया है वह प्रत्येक सभ्यता वाले देशों में धर्म भावना के रूप में उच्चतम प्रयासों के रूप में देखा गया है।