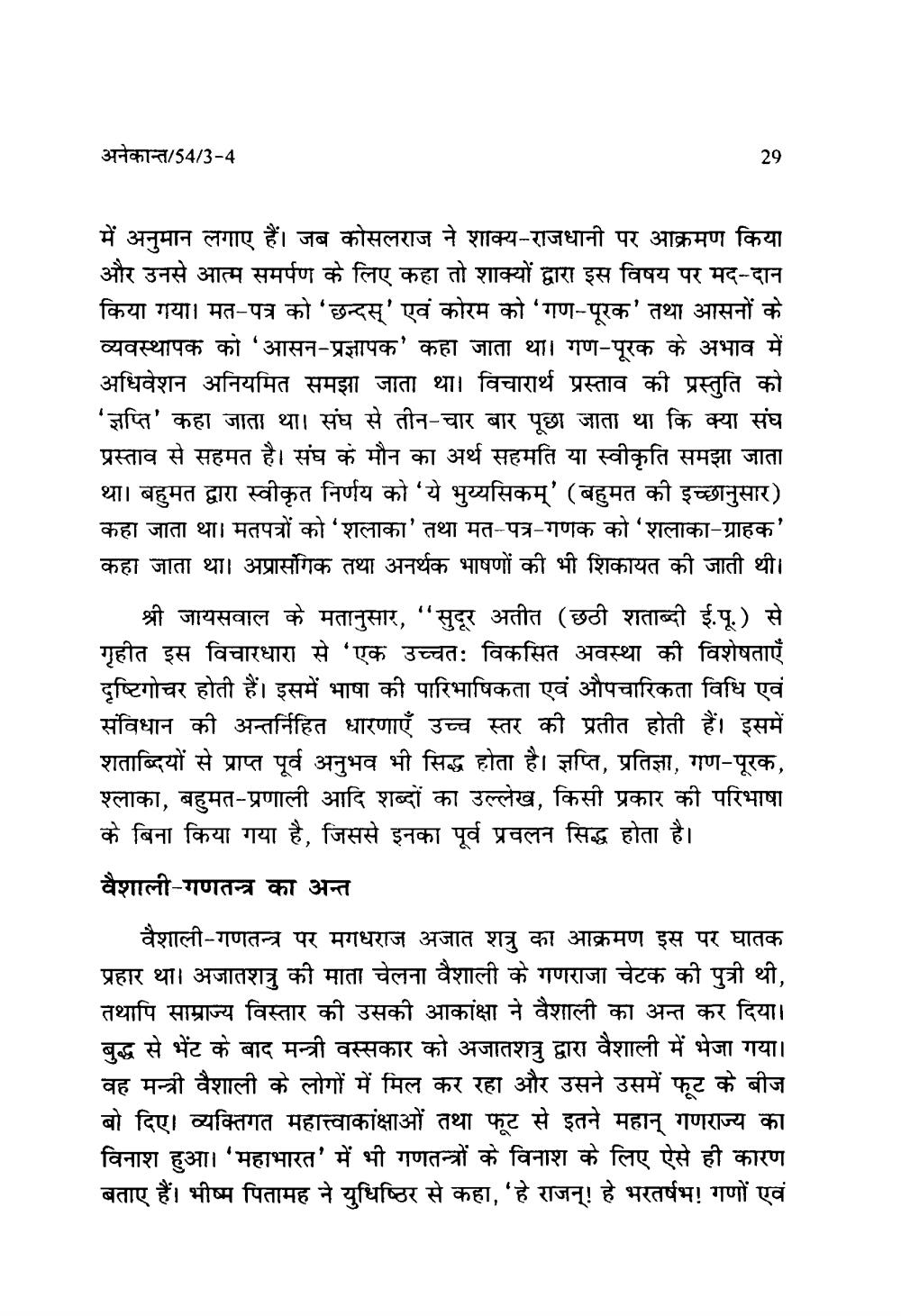________________
अनेकान्त/54/3-4
29
में अनुमान लगाए हैं। जब कोसलराज ने शाक्य-राजधानी पर आक्रमण किया
और उनसे आत्म समर्पण के लिए कहा तो शाक्यों द्वारा इस विषय पर मद-दान किया गया। मत-पत्र को 'छन्दस्' एवं कोरम को 'गण-पूरक' तथा आसनों के व्यवस्थापक को 'आसन-प्रज्ञापक' कहा जाता था। गण-पूरक के अभाव में अधिवेशन अनियमित समझा जाता था। विचारार्थ प्रस्ताव की प्रस्तुति को 'ज्ञप्ति' कहा जाता था। संघ से तीन-चार बार पूछा जाता था कि क्या संघ प्रस्ताव से सहमत है। संघ के मौन का अर्थ सहमति या स्वीकृति समझा जाता था। बहुमत द्वारा स्वीकृत निर्णय को 'ये भुय्यसिकम्' (बहुमत की इच्छानुसार) कहा जाता था। मतपत्रों को 'शलाका' तथा मत-पत्र-गणक को 'शलाका-ग्राहक' कहा जाता था। अप्रासंगिक तथा अनर्थक भाषणों की भी शिकायत की जाती थी।
श्री जायसवाल के मतानुसार, "सुदूर अतीत (छठी शताब्दी ई.पू.) से गृहीत इस विचारधारा से 'एक उच्चत: विकसित अवस्था की विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसमें भाषा की पारिभाषिकता एवं औपचारिकता विधि एवं संविधान की अन्तर्निहित धारणाएँ उच्च स्तर की प्रतीत होती हैं। इसमें शताब्दियों से प्राप्त पूर्व अनुभव भी सिद्ध होता है। ज्ञप्ति, प्रतिज्ञा, गण-पूरक, श्लाका, बहुमत-प्रणाली आदि शब्दों का उल्लेख, किसी प्रकार की परिभाषा के बिना किया गया है, जिससे इनका पूर्व प्रवलन सिद्ध होता है। वैशाली-गणतन्त्र का अन्त
वैशाली-गणतन्त्र पर मगधराज अजात शत्रु का आक्रमण इस पर घातक प्रहार था। अजातशत्रु की माता चेलना वैशाली के गणराजा चेटक की पुत्री थी, तथापि साम्राज्य विस्तार की उसकी आकांक्षा ने वैशाली का अन्त कर दिया। बुद्ध से भेंट के बाद मन्त्री वस्सकार को अजातशत्रु द्वारा वैशाली में भेजा गया। वह मन्त्री वैशाली के लोगों में मिल कर रहा और उसने उसमें फूट के बीज बो दिए। व्यक्तिगत महात्त्वाकांक्षाओं तथा फूट से इतने महान् गणराज्य का विनाश हुआ। 'महाभारत' में भी गणतन्त्रों के विनाश के लिए ऐसे ही कारण बताए हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, 'हे राजन्! हे भरतर्षभ! गणों एवं