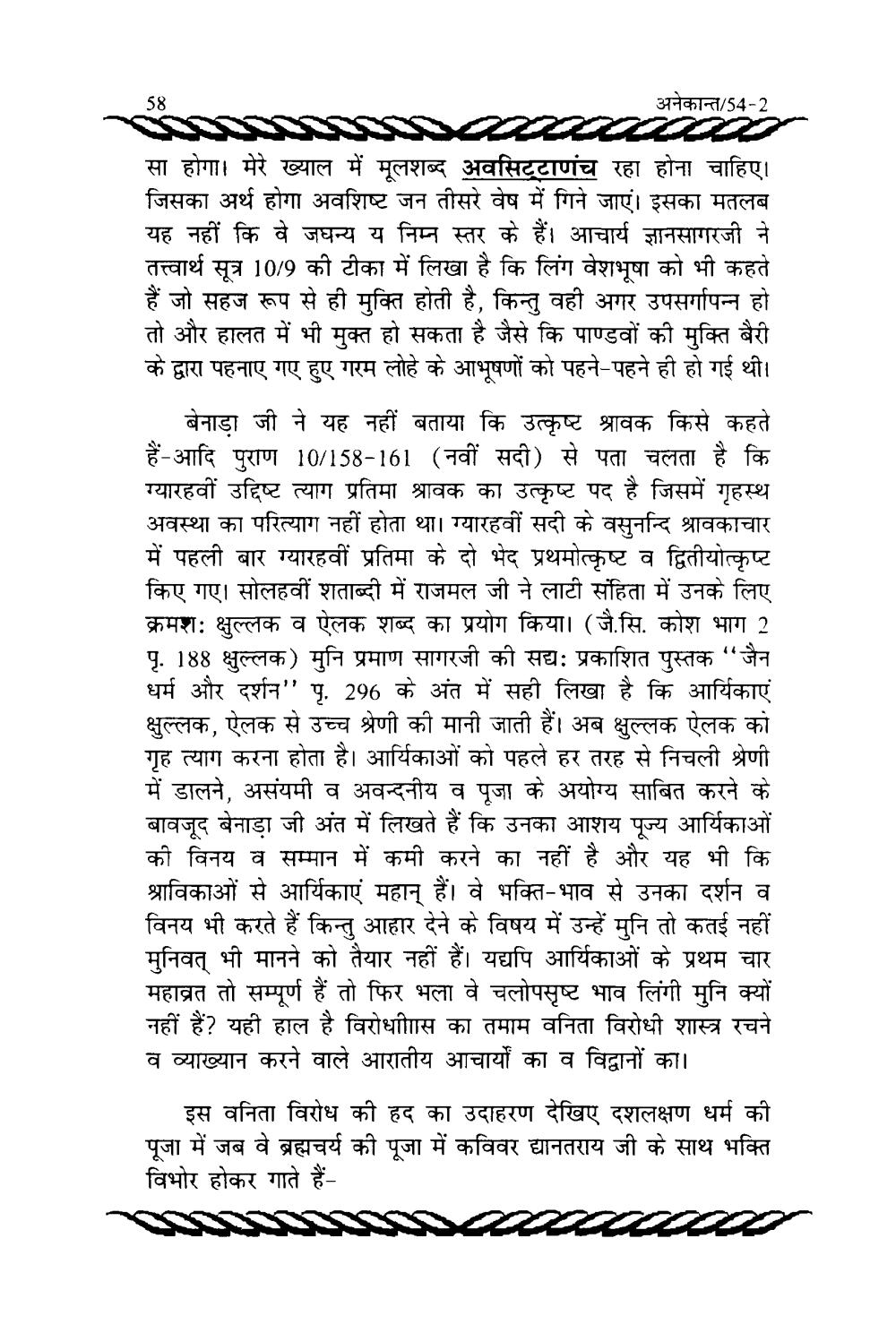________________
58
__ अनेकान्त/54-2
सा होगा। मेरे ख्याल में मूलशब्द अवसिटाणंच रहा होना चाहिए। जिसका अर्थ होगा अवशिष्ट जन तीसरे वेष में गिने जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि वे जघन्य य निम्न स्तर के हैं। आचार्य ज्ञानसागरजी ने तत्त्वार्थ सूत्र 10/9 की टीका में लिखा है कि लिंग वेशभूषा को भी कहते हैं जो सहज रूप से ही मुक्ति होती है, किन्तु वही अगर उपसर्गापन्न हो तो और हालत में भी मुक्त हो सकता है जैसे कि पाण्डवों की मक्ति बैरी के द्वारा पहनाए गए हुए गरम लोहे के आभूषणों को पहने-पहने ही हो गई थी।
बेनाड़ा जी ने यह नहीं बताया कि उत्कृष्ट श्रावक किसे कहते हैं-आदि पुराण 10/158-161 (नवीं सदी) से पता चलता है कि ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा श्रावक का उत्कृष्ट पद है जिसमें गृहस्थ अवस्था का परित्याग नहीं होता था। ग्यारहवीं सदी के वसुनन्दि श्रावकाचार में पहली बार ग्यारहवीं प्रतिमा के दो भेद प्रथमोत्कृष्ट व द्वितीयोत्कृष्ट किए गए। सोलहवीं शताब्दी में राजमल जी ने लाटी संहिता में उनके लिए क्रमश: क्षुल्लक व ऐलक शब्द का प्रयोग किया। (जै.सि. कोश भाग 2 पृ. 188 क्षुल्लक) मुनि प्रमाण सागरजी की सद्यः प्रकाशित पुस्तक "जैन धर्म और दर्शन" पृ. 296 के अंत में सही लिखा है कि आर्यिकाएं क्षुल्लक, ऐलक से उच्च श्रेणी की मानी जाती हैं। अब क्षुल्लक ऐलक को गृह त्याग करना होता है। आर्यिकाओं को पहले हर तरह से निचली श्रेणी में डालने, असंयमी व अवन्दनीय व पूजा के अयोग्य साबित करने के बावजूद बेनाड़ा जी अंत में लिखते हैं कि उनका आशय पूज्य आर्यिकाओं की विनय व सम्मान में कमी करने का नहीं है और यह भी कि श्राविकाओं से आर्यिकाएं महान् हैं। वे भक्ति-भाव से उनका दर्शन व विनय भी करते हैं किन्तु आहार देने के विषय में उन्हें मुनि तो कतई नहीं मुनिवत् भी मानने को तैयार नहीं हैं। यद्यपि आर्यिकाओं के प्रथम चार महाव्रत तो सम्पूर्ण हैं तो फिर भला वे चलोपसृष्ट भाव लिंगी मुनि क्यों नहीं हैं? यही हाल है विरोधास का तमाम वनिता विरोधी शास्त्र रचने व व्याख्यान करने वाले आरातीय आचार्यों का व विद्वानों का।
इस वनिता विरोध की हद का उदाहरण देखिए दशलक्षण धर्म की पूजा में जब वे ब्रह्मचर्य की पूजा में कविवर द्यानतराय जी के साथ भक्ति विभोर होकर गाते हैं