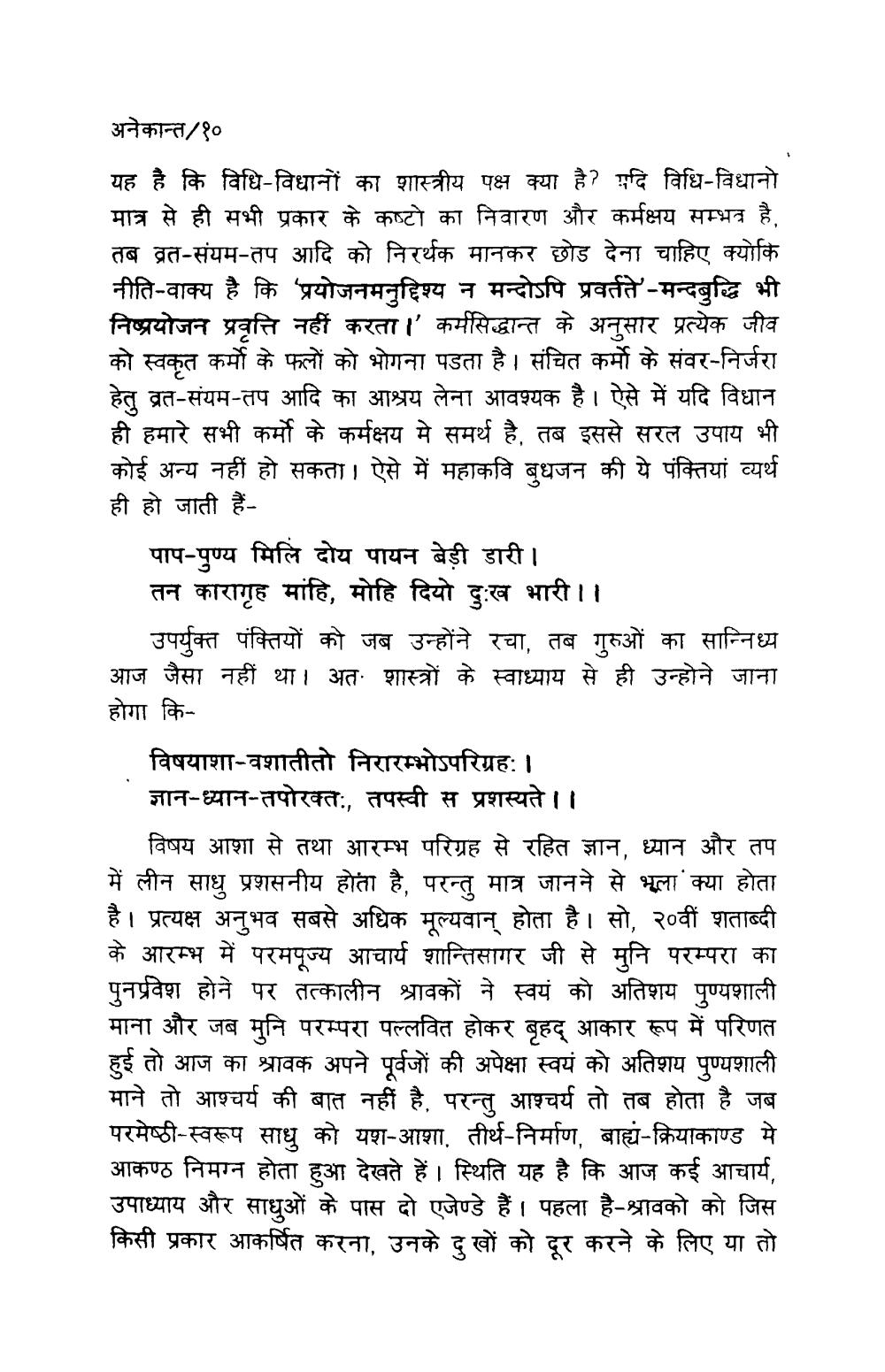________________
अनेकान्त/१० यह है कि विधि-विधानों का शास्त्रीय पक्ष क्या है? मदि विधि-विधानो मात्र से ही सभी प्रकार के कष्टो का निवारण और कर्मक्षय सम्भव है, तब व्रत-संयम-तप आदि को निरर्थक मानकर छोड देना चाहिए क्योकि नीति-वाक्य है कि प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते-मन्दबुद्धि भी निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं करता।' कर्मसिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव को स्वकृत कर्मो के फलों को भोगना पडता है। संचित कर्मो के संवर-निर्जरा हेतु व्रत-संयम-तप आदि का आश्रय लेना आवश्यक है। ऐसे में यदि विधान ही हमारे सभी कर्मो के कर्मक्षय मे समर्थ है, तब इससे सरल उपाय भी कोई अन्य नहीं हो सकता। ऐसे में महाकवि बुधजन की ये पंक्तियां व्यर्थ ही हो जाती हैं
पाप-पुण्य मिलि दोय पायन बेड़ी डारी। तन कारागृह माहि, मोहि दियो दुःख भारी।।
उपर्युक्त पंक्तियों को जब उन्होंने रचा, तब गुरुओं का सान्निध्य आज जैसा नहीं था। अतः शास्त्रों के स्वाध्याय से ही उन्होने जाना होगा कि
विषयाशा-वशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञान-ध्यान-तपोरक्त:, तपस्वी स प्रशस्यते ।।
विषय आशा से तथा आरम्भ परिग्रह से रहित ज्ञान, ध्यान और तप में लीन साधु प्रशसनीय होता है, परन्तु मात्र जानने से भूला क्या होता है। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अधिक मूल्यवान् होता है। सो, २०वीं शताब्दी के आरम्भ में परमपूज्य आचार्य शान्तिसागर जी से मुनि परम्परा का पुनप्रवश होने पर तत्कालीन श्रावकों ने स्वयं को अतिशय पुण्यशाली माना और जब मुनि परम्परा पल्लवित होकर बृहद् आकार रूप में परिणत हुई तो आज का श्रावक अपने पूर्वजों की अपेक्षा स्वयं को अतिशय पुण्यशाली माने तो आश्चर्य की बात नहीं है, परन्तु आश्चर्य तो तब होता है जब परमेष्ठी-स्वरूप साधु को यश-आशा. तीर्थ-निर्माण, बाह्य-क्रियाकाण्ड मे आकण्ठ निमग्न होता हुआ देखते हैं। स्थिति यह है कि आज कई आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के पास दो एजेण्डे हैं। पहला है-श्रावको को जिस किसी प्रकार आकर्षित करना, उनके दुखों को दूर करने के लिए या तो