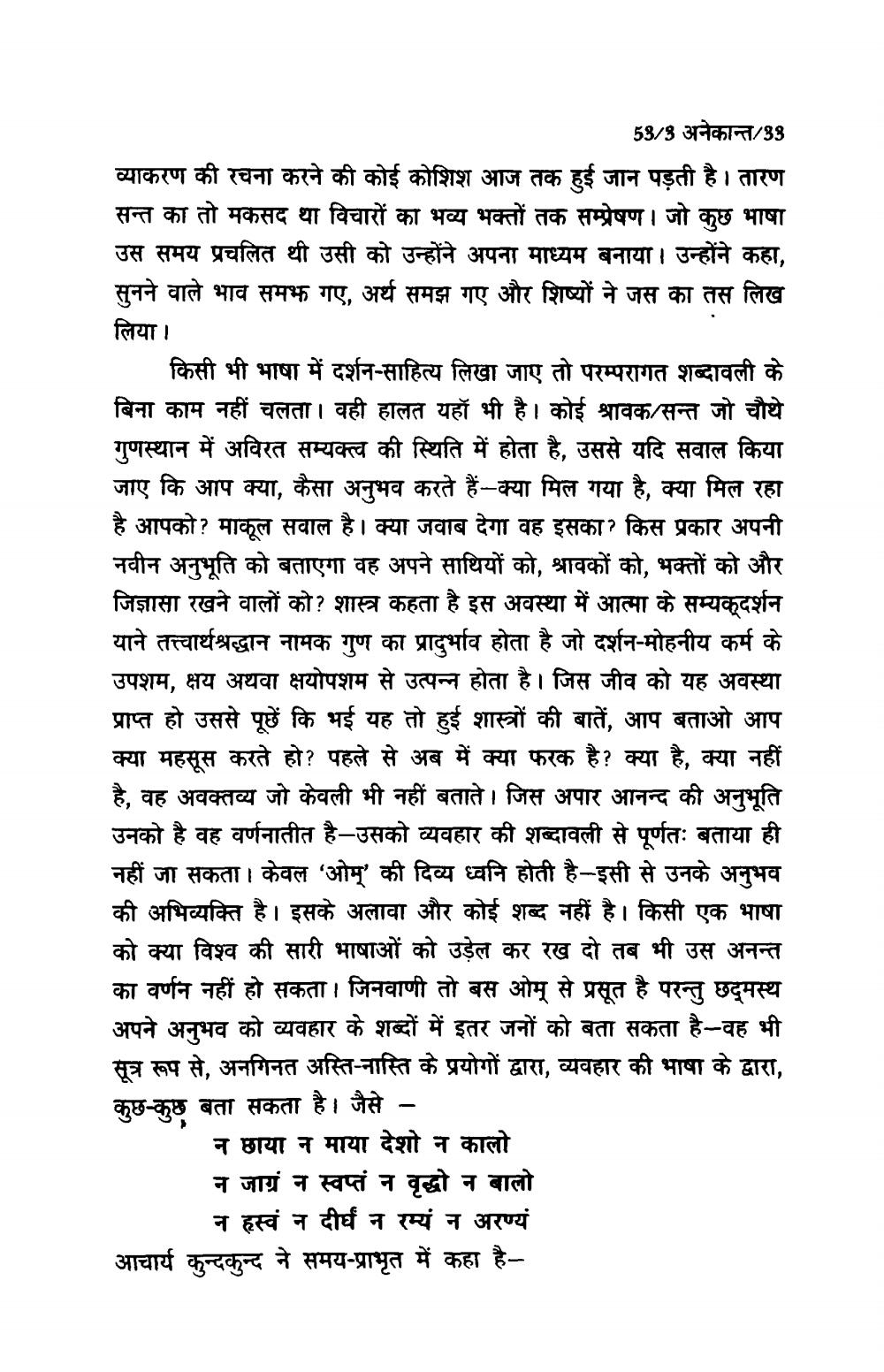________________
53/3 अनेकान्त/33 व्याकरण की रचना करने की कोई कोशिश आज तक हुई जान पड़ती है। तारण सन्त का तो मकसद था विचारों का भव्य भक्तों तक सम्प्रेषण। जो कुछ भाषा उस समय प्रचलित थी उसी को उन्होंने अपना माध्यम बनाया। उन्होंने कहा, सुनने वाले भाव समझ गए, अर्थ समझ गए और शिष्यों ने जस का तस लिख लिया।
किसी भी भाषा में दर्शन-साहित्य लिखा जाए तो परम्परागत शब्दावली के बिना काम नहीं चलता। वही हालत यहाँ भी है। कोई श्रावक/सन्त जो चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक्त्व की स्थिति में होता है, उससे यदि सवाल किया जाए कि आप क्या, कैसा अनुभव करते हैं-क्या मिल गया है, क्या मिल रहा है आपको? माकूल सवाल है। क्या जवाब देगा वह इसका? किस प्रकार अपनी नवीन अनुभूति को बताएगा वह अपने साथियों को, श्रावकों को, भक्तों को और जिज्ञासा रखने वालों को? शास्त्र कहता है इस अवस्था में आत्मा के सम्यकुदर्शन याने तत्त्वार्थश्रद्धान नामक गुण का प्रादुर्भाव होता है जो दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। जिस जीव को यह अवस्था प्राप्त हो उससे पूछे कि भई यह तो हुई शास्त्रों की बातें, आप बताओ आप क्या महसूस करते हो? पहले से अब में क्या फरक है? क्या है, क्या नहीं है, वह अवक्तव्य जो केवली भी नहीं बताते। जिस अपार आनन्द की अनुभूति उनको है वह वर्णनातीत है-उसको व्यवहार की शब्दावली से पूर्णतः बताया ही नहीं जा सकता। केवल 'ओम्' की दिव्य ध्वनि होती है-इसी से उनके अनुभव की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। किसी एक भाषा को क्या विश्व की सारी भाषाओं को उड़ेल कर रख दो तब भी उस अनन्त का वर्णन नहीं हो सकता। जिनवाणी तो बस ओम् से प्रसूत है परन्तु छद्मस्थ अपने अनुभव को व्यवहार के शब्दों में इतर जनों को बता सकता है-वह भी सूत्र रूप से, अनगिनत अस्ति-नास्ति के प्रयोगों द्वारा, व्यवहार की भाषा के द्वारा, कुछ-कुछ बता सकता है। जैसे -
न छाया न माया देशो न कालो न जाग्रं न स्वप्तं न वृद्धो न बालो
न हस्वं न दीर्घं न रम्यं न अरण्यं आचार्य कुन्दकुन्द ने समय-प्राभृत में कहा है