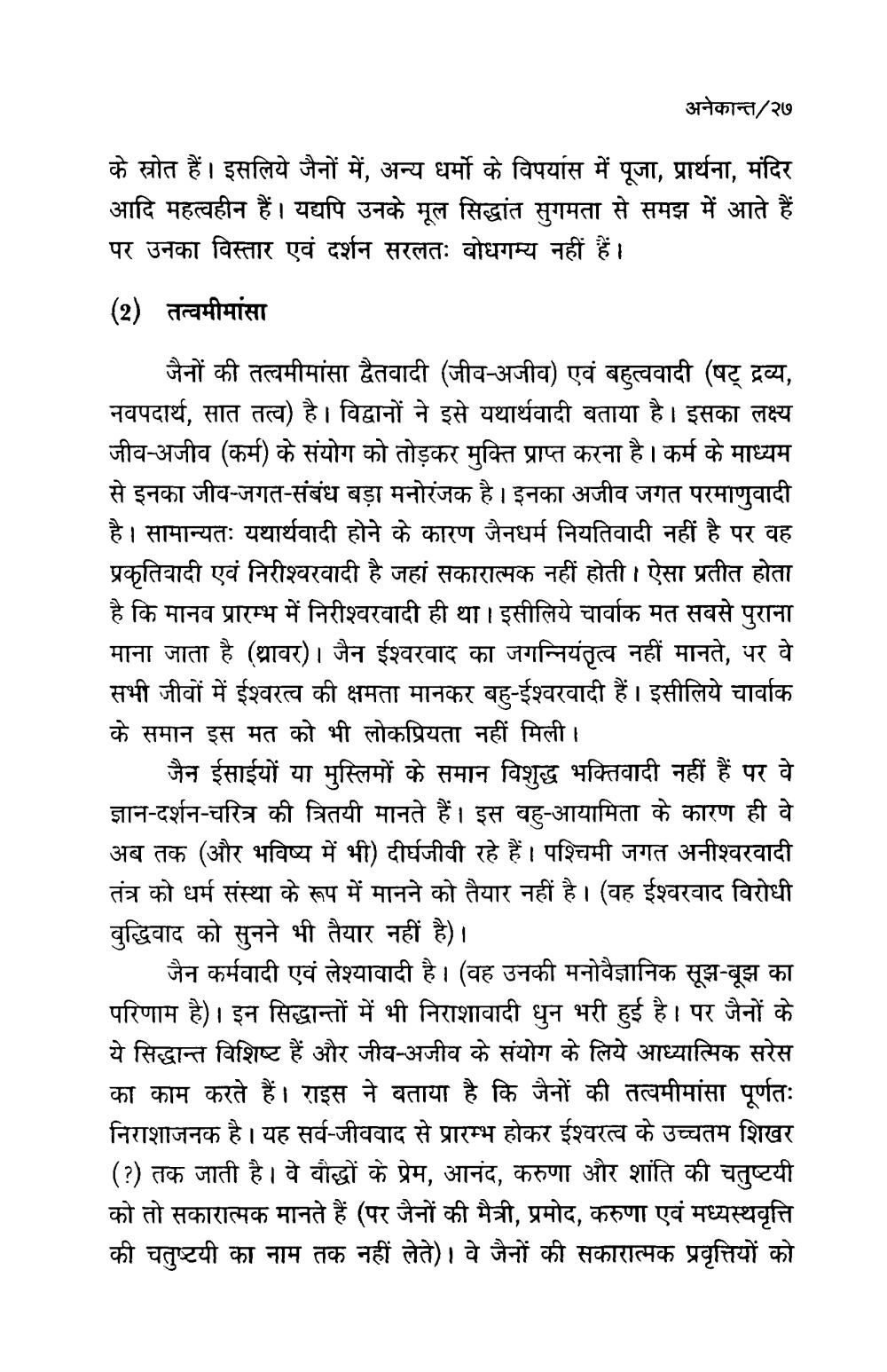________________
अनेकान्त/२७
के स्रोत हैं। इसलिये जैनों में, अन्य धर्मो के विपयांस में पूजा, प्रार्थना, मंदिर आदि महत्वहीन हैं। यद्यपि उनके मूल सिद्धांत सुगमता से समझ में आते हैं पर उनका विस्तार एवं दर्शन सरलतः बोधगम्य नहीं हैं।
(2) तत्वमीमांसा
जैनों की तत्वमीमांसा द्वैतवादी (जीव-अजीव) एवं बहुत्ववादी (षट् द्रव्य, नवपदार्थ, सात तत्व) है। विद्वानों ने इसे यथार्थवादी बताया है। इसका लक्ष्य जीव-अजीव (कर्म) के संयोग को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है। कर्म के माध्यम से इनका जीव-जगत-संबंध बड़ा मनोरंजक है। इनका अजीव जगत परमाणुवादी है। सामान्यतः यथार्थवादी होने के कारण जैनधर्म नियतिवादी नहीं है पर वह प्रकृतिवादी एवं निरीश्वरवादी है जहां सकारात्मक नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव प्रारम्भ में निरीश्वरवादी ही था। इसीलिये चार्वाक मत सबसे पुराना माना जाता है (थ्रावर)। जैन ईश्वरवाद का जगन्नियंतृत्व नहीं मानते, पर वे सभी जीवों में ईश्वरत्व की क्षमता मानकर बहु-ईश्वरवादी हैं। इसीलिये चार्वाक के समान इस मत को भी लोकप्रियता नहीं मिली।
जैन ईसाईयों या मुस्लिमों के समान विशुद्ध भक्तिवादी नहीं हैं पर वे ज्ञान-दर्शन-चरित्र की त्रितयी मानते हैं। इस बहु-आयामिता के कारण ही वे अब तक (और भविष्य में भी) दीर्घजीवी रहे हैं। पश्चिमी जगत अनीश्वरवादी तंत्र को धर्म संस्था के रूप में मानने को तैयार नहीं है। (वह ईश्वरवाद विरोधी बुद्धिवाद को सुनने भी तैयार नहीं है)।
जैन कर्मवादी एवं लेश्यावादी है। (वह उनकी मनोवैज्ञानिक सूझ-बूझ का परिणाम है)। इन सिद्धान्तों में भी निराशावादी धुन भरी हुई है। पर जैनों के ये सिद्धान्त विशिष्ट हैं और जीव-अजीव के संयोग के लिये आध्यात्मिक सरेस का काम करते हैं। राइस ने बताया है कि जैनों की तत्वमीमांसा पूर्णतः निराशाजनक है। यह सर्व-जीववाद से प्रारम्भ होकर ईश्वरत्व के उच्चतम शिखर (?) तक जाती है। वे बौद्धों के प्रेम, आनंद, करुणा और शांति की चतुष्टयी को तो सकारात्मक मानते हैं (पर जैनों की मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं मध्यस्थवृत्ति की चतुष्टयी का नाम तक नहीं लेते)। वे जैनों की सकारात्मक प्रवृत्तियों को