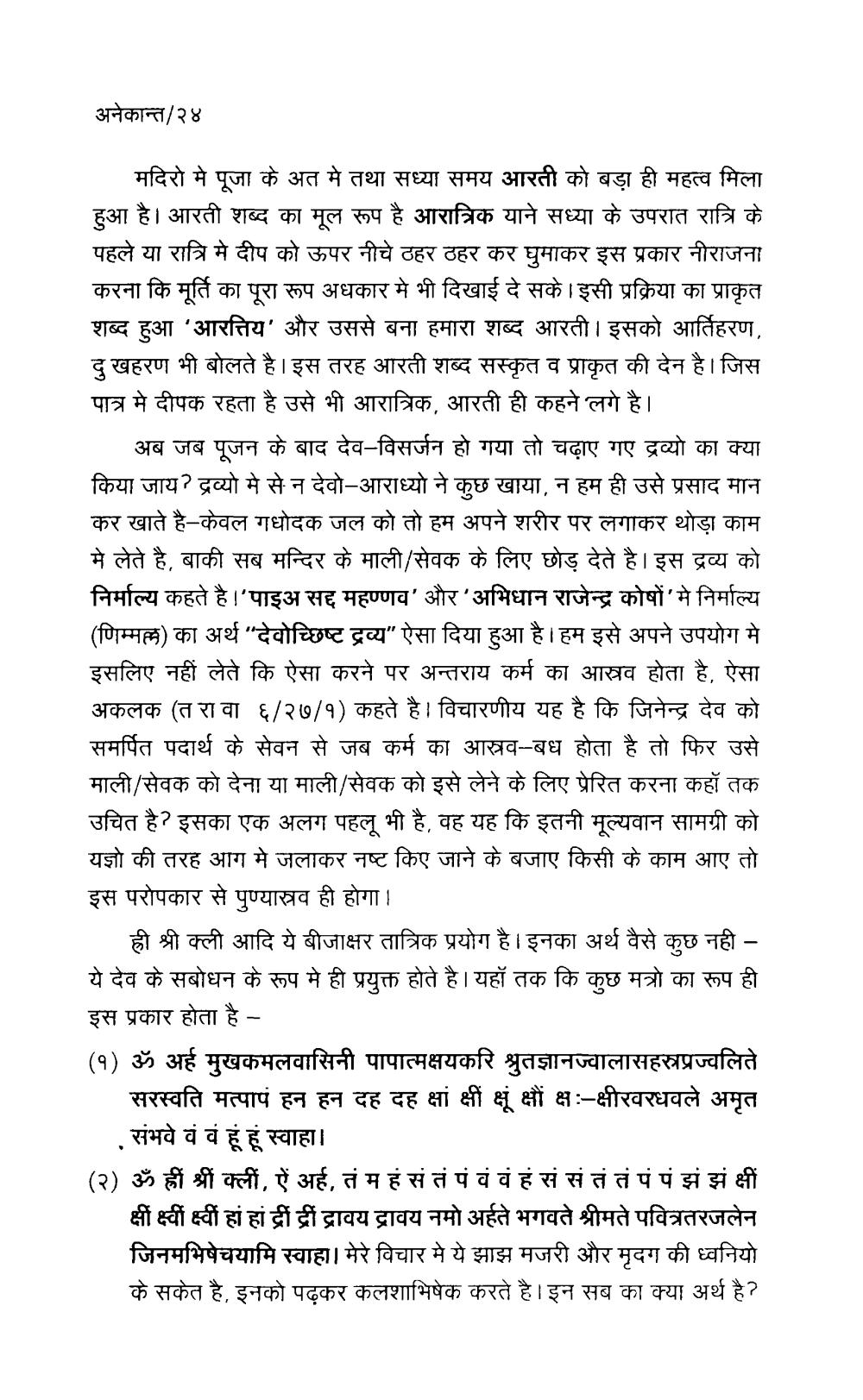________________
अनेकान्त/२४
मदिरो मे पूजा के अत मे तथा सध्या समय आरती को बड़ा ही महत्व मिला हुआ है। आरती शब्द का मूल रूप है आरात्रिक याने सध्या के उपरात रात्रि के पहले या रात्रि मे दीप को ऊपर नीचे ठहर ठहर कर घुमाकर इस प्रकार नीराजना करना कि मूर्ति का पूरा रूप अधकार मे भी दिखाई दे सके। इसी प्रक्रिया का प्राकृत शब्द हुआ 'आरत्तिय' और उससे बना हमारा शब्द आरती। इसको आर्तिहरण, दुखहरण भी बोलते है। इस तरह आरती शब्द सस्कृत व प्राकृत की देन है। जिस पात्र मे दीपक रहता है उसे भी आरात्रिक, आरती ही कहने लगे है।
अब जब पूजन के बाद देव-विसर्जन हो गया तो चढ़ाए गए द्रव्यो का क्या किया जाय? द्रव्यो मे से न देवो-आराध्यो ने कुछ खाया, न हम ही उसे प्रसाद मान कर खाते है केवल गधोदक जल को तो हम अपने शरीर पर लगाकर थोड़ा काम मे लेते है, बाकी सब मन्दिर के माली/सेवक के लिए छोड़ देते है। इस द्रव्य को निर्माल्य कहते है। 'पाइअ सद्द महण्णव' और 'अभिधान राजेन्द्र कोषों मे निर्माल्य (णिम्मल्ल) का अर्थ "देवोच्छिष्ट द्रव्य" ऐसा दिया हुआ है। हम इसे अपने उपयोग मे इसलिए नहीं लेते कि ऐसा करने पर अन्तराय कर्म का आस्रव होता है, ऐसा अकलक (त रा वा ६/२७/१) कहते है। विचारणीय यह है कि जिनेन्द्र देव को समर्पित पदार्थ के सेवन से जब कर्म का आस्रव-बध होता है तो फिर उसे माली/सेवक को देना या माली/सेवक को इसे लेने के लिए प्रेरित करना कहाँ तक उचित है? इसका एक अलग पहलू भी है, वह यह कि इतनी मूल्यवान सामग्री को यज्ञो की तरह आग मे जलाकर नष्ट किए जाने के बजाए किसी के काम आए तो इस परोपकार से पुण्यास्रव ही होगा।
ह्री श्री क्ली आदि ये बीजाक्षर तात्रिक प्रयोग है। इनका अर्थ वैसे कुछ नही - ये देव के सबोधन के रूप मे ही प्रयुक्त होते है। यहाँ तक कि कुछ मत्रो का रूप ही इस प्रकार होता है - (१) ॐ अर्ह मुखकमलवासिनी पापात्मक्षयकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते
सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं झू क्षौं क्ष:-क्षीरवरधवले अमृत
संभवे वं वं हूं हूं स्वाहा। (२) ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐं अर्ह, तं म हं संतं पं वं वं हं सं सं तं तं पं पं झं झंक्षी
क्षी क्ष्वी क्ष्वी हां हां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। मेरे विचार मे ये झाझ मजरी और मृदग की ध्वनियो के सकेत है, इनको पढ़कर कलशाभिषेक करते है। इन सब का क्या अर्थ है?