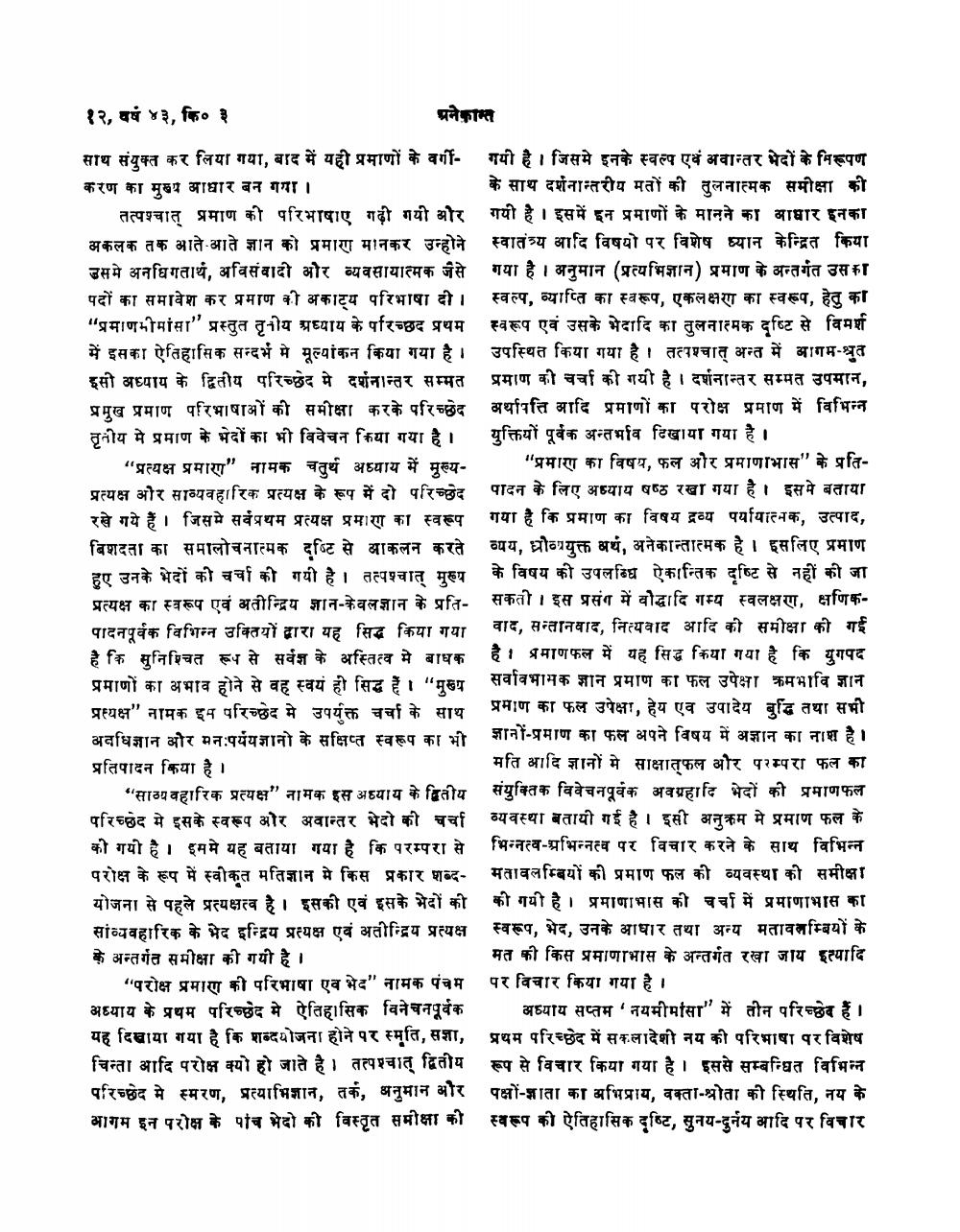________________
१२, वर्ष ४३, कि०३
अनेकान्त
साथ संयुक्त कर लिया गया, बाद में यही प्रमाणों के वर्गी- गयी है। जिसमे इनके स्वल्प एवं अवान्तर भेदों के मिरूपण करण का मुख्य आधार बन गया।
के साथ दर्शनान्तरीय मतों की तुलनात्मक समीक्षा की ___ तत्पश्चात् प्रमाण की परिभाषाए गढ़ी गयी और गयी है । इस में इन प्रमाणों के मानने का आधार इनका अकलक तक आते-आते ज्ञान को प्रमाण मानकर उन्होने स्वातंत्र्य आदि विषयो पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया उसमे अनधिगतार्थ, अविसंवादी और व्यवसायात्मक जैसे गया है । अनुमान (प्रत्यभिज्ञान) प्रमाण के अन्तर्गत उसका पदों का समावेश कर प्रमाण की अकाट्य परिभाषा दी। स्वल्प, व्याप्ति का स्वरूप, एकलक्षण का स्वरूप, हेतु का "प्रमाणमीमांसा" प्रस्तुत तृतीय अध्याय के परिच्छद प्रथम स्वरूप एवं उसके भेदादि का तुलनात्मक दृष्टि से विमर्श में इसका ऐतिहासिक सन्दर्भ मे मूल्यांकन किया गया है। उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात् अन्त में आगम-श्रुत इसी अध्याय के द्वितीय परिच्छेद मे दर्शनान्तर सम्मत प्रमाण की चर्चा की गयी है । दर्शनान्तर सम्मत उपमान, प्रमुख प्रमाण परिभाषाओं की समीक्षा करके परिच्छेद अर्थापति आदि प्रमाणों का परोक्ष प्रमाण में विभिन्न तृतीय मे प्रमाण के भेदों का भी विवेचन किया गया है। युक्तियों पूर्वक अन्तर्भाव दिखाया गया है।
"प्रत्यक्ष प्रमाण" नामक चतुर्थ अध्याय में मुख्य- "प्रमाग का विषय, फल और प्रमाणाभास" के प्रतिप्रत्यक्ष और साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में दो परिच्छेद पादन के लिए अध्याय षष्ठ रखा गया है। इसमे बताया रखे गये हैं। जिसमे सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप गया है कि प्रमाण का विषय द्रव्य पर्यायात्मक, उत्पाद, बिशदता का समालोचनात्मक दृष्टि से आकलन करते व्यय, ध्रौप्रयुक्त अर्थ, अनेकान्तात्मक है। इसलिए प्रमाण हुए उनके भेदों की चर्चा की गयी है। तत्पश्चात् मुख्य के विषय की उपलब्धि ऐकान्तिक दृष्टि से नहीं की जा प्रत्यक्ष का स्वरूप एवं अतीन्द्रिय ज्ञान-केवलज्ञान के प्रति- सकती। इस प्रसंग में बौद्धादि गम्य स्वलक्षण, क्षणिकपादनपूर्वक विभिन्न उक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया गया वाद, सन्तानवाद, नित्यवाद आदि की समीक्षा की गई है कि सुनिश्चित रूप से सर्वज्ञ के अस्तित्व मे बाधक है। प्रमाण फल में यह सिद्ध किया गया है कि युगपद प्रमाणों का अभाव होने से वह स्वयं ही सिद्ध हैं। "मुख्य सर्वावभामक ज्ञान प्रमाण का फल उपेक्षा क्रमभावि ज्ञान प्रत्यक्ष" नामक इस परिच्छेद मे उपर्युक्त चर्चा के साथ
प्रमाण का फल उपेक्षा, हेय एव उपादेय बुद्धि तथा सभी अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानो के सक्षिप्त स्वरूप का भी ज्ञाना-प्रमाण का फल अपने विषय में अज्ञान का नाश है। प्रतिपादन किया है।
मति आदि ज्ञानों साक्षात्फल और परम्परा फल का "साव्यवहारिक प्रत्यक्ष" नामक इस अध्याय के द्वितीय संयुक्तिक विवेचनपूर्वक अवग्रहादि भेदों को प्रमाणफल परिच्छेद मे इसके स्वरूप और अवान्तर भेदो की चर्चा व्यवस्था बतायी गई है। इसी अनुक्रम मे प्रमाण फल के की गयी है। इसमे यह बताया गया है कि परम्परा से भिन्नत्व-अभिन्नत्व पर विचार करने के साथ विभिन्न परोक्ष के रूप में स्वीकृत मतिज्ञान मे किस प्रकार शब्द- मतावलम्बियों की प्रमाण फल की व्यवस्था की समीक्षा योजना से पहले प्रत्यक्षत्व है। इसकी एवं इसके भेदों की की गयी है। प्रमाणाभास की चर्चा में प्रमाणाभास का सांव्यवहारिक के भेद इन्द्रिय प्रत्यक्ष एवं अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष __ स्वरूप, भेद, उनके आधार तथा अन्य मतावलम्बियों के के अन्तर्गत समीक्षा की गयी है।
मत को किस प्रमाणाभास के अन्तर्गत रखा जाय इत्यादि __ "परोक्ष प्रमाण की परिभाषा एव भेद" नामक पंचम पर विचार किया गया है। अध्याय के प्रथम परिच्छेद मे ऐतिहासिक विनेचनपूर्वक अध्याय सप्तम 'नयमीमांसा" में तीन परिच्छेद हैं। यह दिखाया गया है कि शब्दयोजना होने पर स्मृति, सज्ञा, प्रथम परिच्छेद में सकलादेशी नय की परिभाषा पर विशेष चिन्ता आदि परोक्ष क्यो हो जाते है। तत्पश्चात् द्वितीय रूप से विचार किया गया है। इससे सम्बन्धित विभिन्न परिच्छेद मे स्मरण, प्रत्याभिज्ञान, तर्क, अनुमान और पक्षों-ज्ञाता का अभिप्राय, वक्ता-श्रोता की स्थिति, नय के आगम इन परोक्ष के पांच भेदो की विस्तृत समीक्षा की स्वरूप की ऐतिहासिक दृष्टि, सुनय-दुर्नय आदि पर विचार