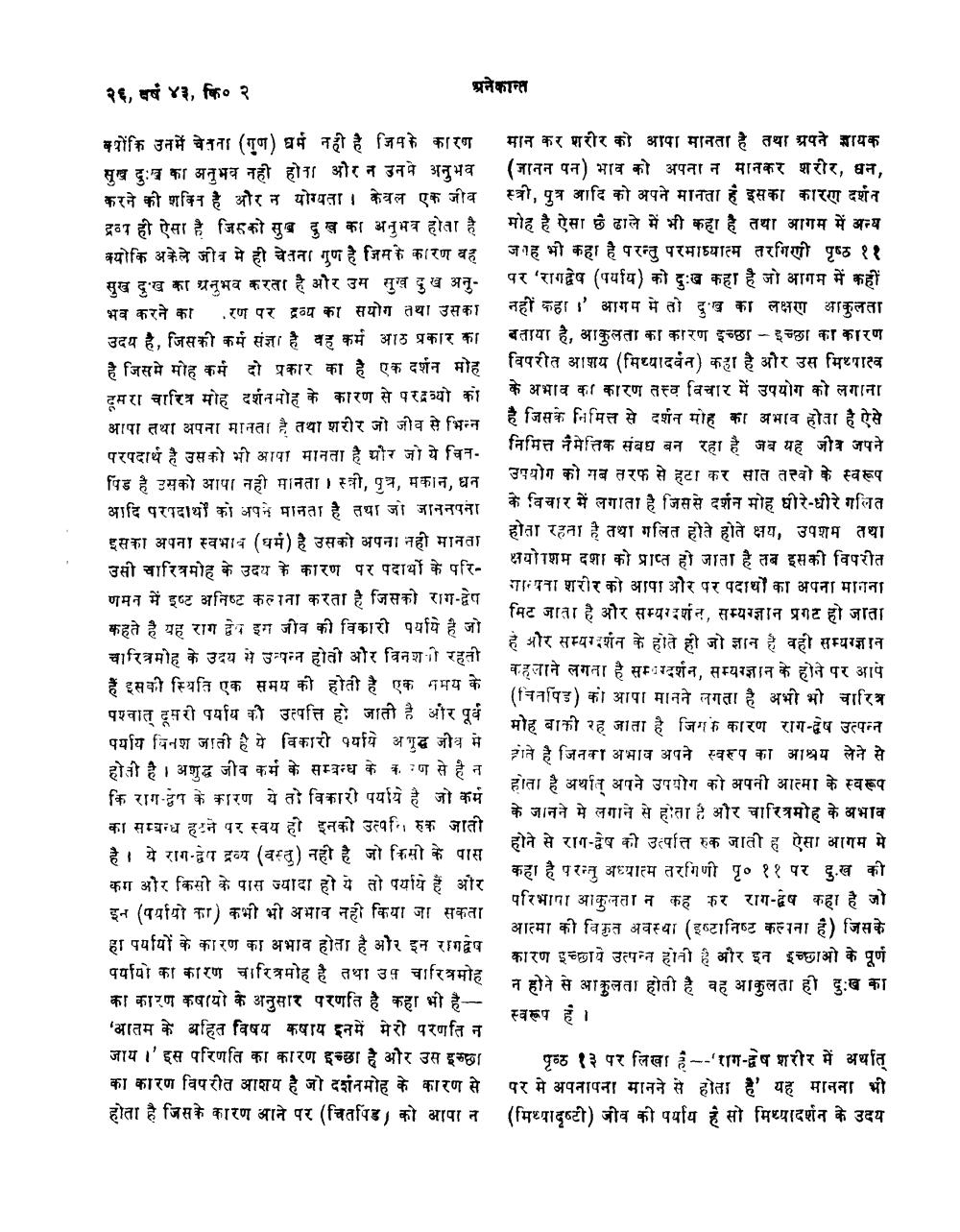________________
२९४३० २
क्योंकि उनमें चेतना (गुण) धर्म
होता
सुख दुःख का अनुभव नहीं करने की शक्ति है और न
श्रनेकान्त
नहीं है जिसके कारण और न उनने अनुभव केवल एक जीव अनुभव होता है जिसके कारण वह
योग्यता
सुख दुख अनु
द्रव्य ही ऐसा है जिसको सुख दुख का क्योंकि अकेले जीव में ही चेतना गुण है सुख दुःख का अनुभव करता है और उम भव करने का रण पर द्रव्य का सयोग तथा उसका उदय है, जिसकी कर्म संज्ञा है वह कर्म आठ प्रकार का है जिसमे मोह कर्म दो प्रकार का है एक दर्शन मोह दूसरा चारित्र मोह दर्शनमोह के कारण से परद्रव्यों को आपा तथा अपना मानता है तथा शरीर जो जीव से भिन्न परपदार्थ है उसको भी आपा मानता है और जो नि पिंड है उसको आप नहीं मानता स्त्री, पुत्र, मकान, धन आदि परपदार्थों को अपने मानता है तथा जो जाननपना इसका अपना स्वभाव (धर्म) है उसको अपना नही मानता उसी चारित्रमोह के उदय के कारण पर पदार्थों के परि णमन में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है जिसको राग-द्वेष कहते है यह राग व इस जीव की विकारी पर्याये है जो चारित्रमोह के उदय से उत्पन्न होती और विश रहती हैं इसकी स्थिति एक समय की होती है एक समय के पश्वात् दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है और पूर्व पर्याय निश जाती है ये विकारी अशुद्ध जीव मे होती है। अशुद्ध जीव कर्म के सम्बन्ध के कण से है न कि राग-द्वेग के कारण ये तो विकारी पर्याये है जो कर्म का सम्बन्ध हटने पर स्वयं ही इनकी उत्रुक जाती है । ये राग-द्वेष द्रव्य (वस्तु) नही है जो किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा हो ये तो पर्याये हैं और इन (पर्याय का कभी भी अभाव नहीं किया जा सकता हा पर्यायों के कारण का अभाव होता है और इन रागद्वेष पर्याय का कारण चारित्रमोह है तथा उन चारित्रमोह का कारण कषायो के अनुसार परणति है कहा भी है'आतम के अहित विषय कषाय इनमें मेरो परणति न जाय। इस परिणति का कारण इच्छा है और उस इच्छा का कारण विपरीत आशय है जो दर्शनमोह के कारण से होता है जिसके कारण आने पर (चितपिंड को आपा न
मान कर शरीर को आपा मानता है तथा अपने ज्ञायक (जानन पन ) भाव को अपना न मानकर शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि को अपने मानता है इसका कारण दर्शन मोह है ऐसा छै ढाले में भी कहा है तथा आगम में अन्य जगह भी कहा है परन्तु परमाध्यात्म तरगिणी पृष्ठ ११ पर 'रागद्वेष (पर्याय) को दुःख कहा है जो आगम में कहीं नहीं कहा।' आगम में तो दुःख का लक्षरण आकुलता बताया है, आकुलता का कारण इच्छा इच्छा का कारण विपरीत आशय ( मिथ्यादर्शन) कहा है और उस मिथ्यात्व के अभाव का कारण तत्त्व विचार में उपयोग को लगाना है जिसके निमित्त से दर्शन मोह का अभाव होता है ऐसे निमित्त नैतिक संबंध बन रहा है जब यह जीव अपने उपयोग को सब तरफ से हटा कर सात तत्वों के स्वरूप के विचार में लगाता है जिससे दर्शन मोह धीरे-धीरे गलित होता रहता है तथा गलित होते होते क्षय, उपशम तथा क्षयोपशम दशा को प्राप्त हो जाता है तब इसकी विपरीत मान्यता शरीर की आपा और पर पदार्थों का अपना मानना मिट जाता है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान प्रगट हो जाता है और सम्यग्दर्शन के होते ही जो ज्ञान है वही सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान के होने पर आप (पिड) की आपा मानने लगता है अभी भी चारित्र मोह बाकी रह जाता है जिसके कारण राग-द्वेष उत्पन्न होते है जिनका अभाव अपने स्वरूप का आश्रय लेने से होता है अर्थात् अपने उपयोग को अपनी आत्मा के स्वरूप के जानने में लगाने से होता है और चारित्रमोह के अभाव होने से राग-द्वेष की उत्पत्ति रुक जाती है ऐसा आगम मे कहा है परन्तु अध्यात्म तरगिणी पृ० ११ पर दुःख की परिभाषा आकुलता न कह कर राग-द्वेष कहा है जो आत्मा की विकृत अवस्था ( इष्टानिष्ट कलना है ) जिसके कारण इच्छा उत्पन्न होती है और इन इच्छाओ के पूर्ण न होने से आकुलता होती है वह आकुलता ही दुःख का स्वरूप हैं ।
पृष्ठ १३ परा-राग-द्वेष शरीर में अर्थात् पर मे अपनापना मानने से होता है यह मानना भी (मिपादृष्टी) जीव की पर्याय है सो मिथ्यादर्शन के उदय