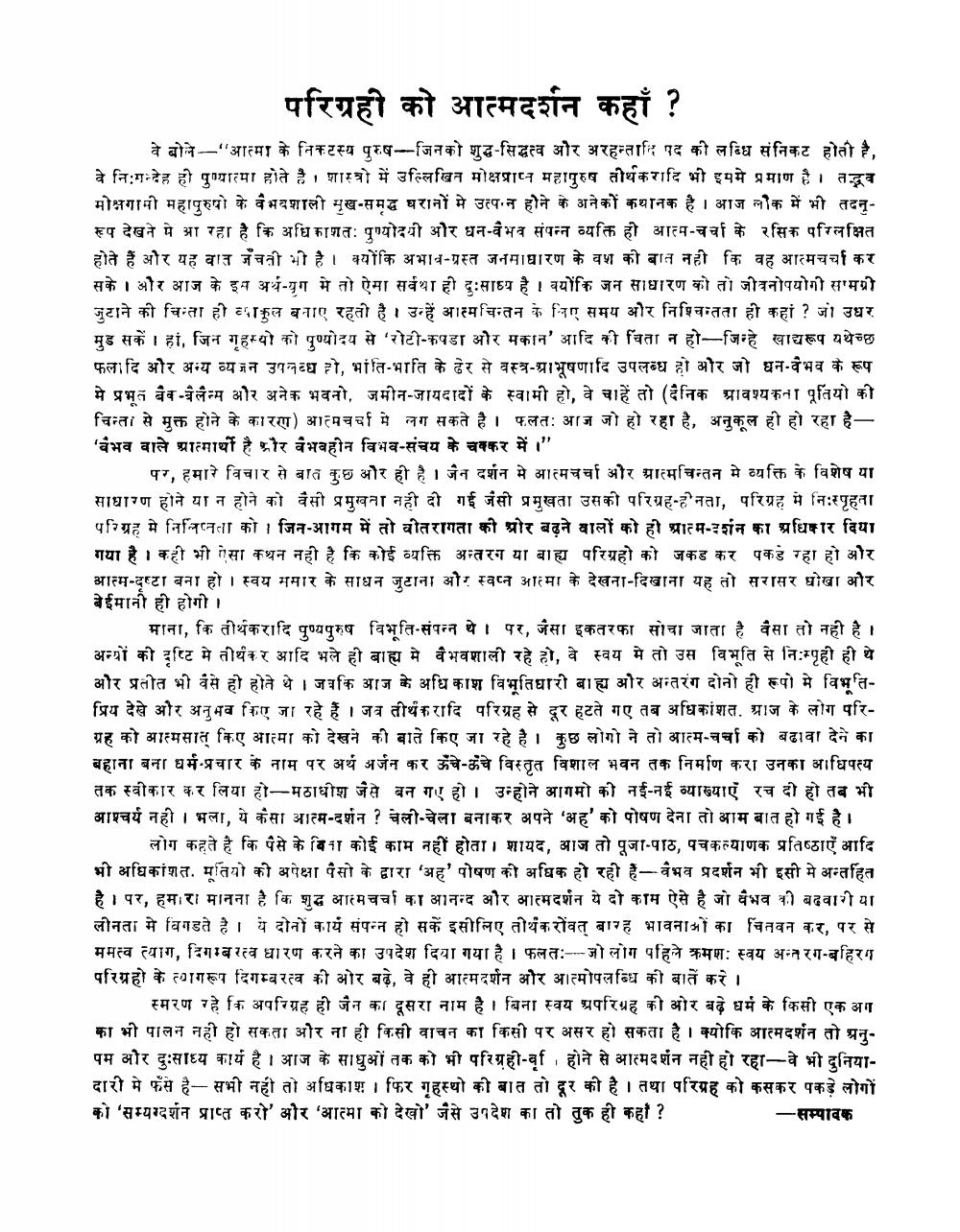________________
परिग्रही को आत्मदर्शन कहाँ ?
वे बोले -"आत्मा के निकटस्य पुरुष-जिन को शुद्ध-सिद्धत्व और अरहन्तादि पद की लब्धि संनिकट होती है, वे नि:गन्देह ही पुण्यात्मा होते है। शास्त्रो में उल्लिखित मोक्षप्राप्त महापुरुष तीर्थक रादि भी इसमे प्रमाण है। तद्भव मोक्षगामी महापुरुषो के वैभवशाली मुख-समद्ध घरानों मे उत्पन्न होने के अनेकों कथानक है । आज लोक में भी तदनुरूप देखने मे आ रहा है कि अधिकाशतः पुण्योदयी और धन-वैभव संपन्न व्यक्ति ही आत्म-चर्चा के रसिक परिलक्षित होते हैं और यह बात जंचती भी है। क्योंकि अभाव-ग्रस्त जनमाधारण के वश की बात नही कि वह आत्मचर्चा कर सके । और आज के इस अर्थ-युग मे तो ऐमा सर्वथा ही दुःसाध्य है । क्योंकि जन साधारण को तो जीवनोपयोगी सामग्री जुटाने की चिन्ता ही व्याकुल बनाए रहती है। उन्हें आत्मचिन्तन के लिए समय और निश्चिन्तता ही कहां? जो उधर मुड सकें। हां, जिन गृहस्यो को पुण्योदय से 'रोटी-कपडा और मकान' आदि की चिंता न हो-जिन्हे खाद्यरूप यथेच्छ फलादि और अन्य व्य जन उपलब्ध हो, भांति-भाति के ढेर से वस्त्र-ग्राभूषणादि उपलब्ध हो और जो धन-वैभव के रूप मे प्रभूत बैक-बैलैन्म और अनेक भवनो, जमीन-जायदादों के स्वामी हो, वे चाहें तो (दैनिक आवश्यकता पूर्तियो की चिन्ता से मुक्त होने के कारण) आत्मचर्चा में लग सकते है। फलत: आज जो हो रहा है, अनुकूल ही हो रहा है'वैभव वाले प्रात्माओं है और वैभवहीन विभव-संचय के चक्कर में।" ।
पर, हमारे विचार से बात कुछ और ही है । जैन दर्शन मे आत्मचर्चा और प्रात्मचिन्तन मे व्यक्ति के विशेष या साधारण होने या न होने को वैसी प्रमुखता नही दी गई जैसी प्रमुखता उसकी परिग्रह-हीनता, परिग्रह में नि:स्पृहता परिग्रह मे निलिप्तता को। जिन-आगम में तो वीतरागता की ओर बढ़ने वालों को ही प्रात्म-दर्शन का अधिकार दिया गया है । कही भी सा कथन नही है कि कोई व्यक्ति अन्तरग या बाह्य परिग्रहो को जकड कर पकडे रहा हो और आत्म-दृष्टा बना हो । स्वय ममार के साधन जुटाना और स्वप्न आत्मा के देखना-दिखाना यह तो सरासर धोखा और बेईमानी ही होगी।
माना, कि तीर्थकरादि पुण्यपुरुष विभूति-संपन्न थे। पर, जैसा इकतरफा सोचा जाता है वैसा तो नही है । अन्यों की दृष्टि मे तीर्थक र आदि भले ही बाह्य मे वैभवशाली रहे हो, वे स्वय मे तो उस विभूति से नि:स्पृही ही थे और प्रतीत भी वैसे ही होते थे। जबकि आज के अधि काश विभूतिधारी बाह्य और अन्तरंग दोनो ही रूपो मे विभूतिप्रिय देखे और अनुभव किए जा रहे हैं । जव तीर्थंकरादि परिग्रह से दूर हटते गए तब अधिकांशत. प्राज के लोग परिग्रह को आत्मसात् किए आत्मा को देखने की बाते किए जा रहे है। कुछ लोगो ने तो आत्म-चर्चा को बढावा देने का बहाना बना धर्म प्रचार के नाम पर अर्थ अर्जन कर ऊँचे-ऊँचे विस्तृत विशाल भवन तक निर्माण करा उनका आधिपत्य तक स्वीकार कर लिया हो-मठाधीश जैसे बन गए हो। उन्होने आगमो की नई-नई व्याख्याएँ रच दी हो तब भी आश्चर्य नही । भला, ये कैसा आत्म-दर्शन? चेली-चेला बनाकर अपने 'अह' को पोषण देना तो आम बात हो गई है।
लोग कहते है कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। शायद, आज तो पूजा-पाठ, पचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ आदि भी अधिकांशत. मूतियो की अपेक्षा पैसो के द्वारा 'अह' पोषण को अधिक हो रही है-वैभव प्रदर्शन भी इसी मे अन्तहित है। पर, हमारा मानना है कि शुद्ध आत्मचर्चा का आनन्द और आत्मदर्शन ये दो काम ऐसे है जो वैभव की बदवारी या लीनता मे विगडते है। ये दोनों कार्य संपन्न हो सकें इसीलिए तीर्थंकरोंवत् बारह भावनाओं का चितवन कर, पर से ममत्व त्याग, दिगम्बरत्व धारण करने का उपदेश दिया गया है । फलत:--- जो लोग पहिले क्रमश: स्वय अन्त रग-बहिरग परिग्रहो के त्यागरूप दिगम्ब रत्व की ओर बढ़े, वे ही आत्मदर्शन और आत्मोपलब्धि की बातें करे ।
स्मरण रहे कि अपरिग्रह ही जैन का दूसरा नाम है। बिना स्वय अपरिग्रह की ओर बढ़े धर्म के किसी एक आग का भी पालन नहीं हो सकता और ना ही किसी वाचन का किसी पर असर हो सकता है । क्योकि आत्मदर्शन तो अनुपम और दुःसाध्य कार्य है। आज के साधुओं तक को भी परिग्रही- । होने से आत्मदर्शन नहीं हो रहा-वे भी दुनियादारी मे फंसे है- सभी नही तो अधिकाश । फिर गृहस्थो की बात तो दूर की है । तथा परिग्रह को कसकर पकड़े लोगों को 'सम्यग्दर्शन प्राप्त करो' और 'आत्मा को देखो' जैसे उपदेश का तो तुक ही कहाँ ?
-सम्पादक