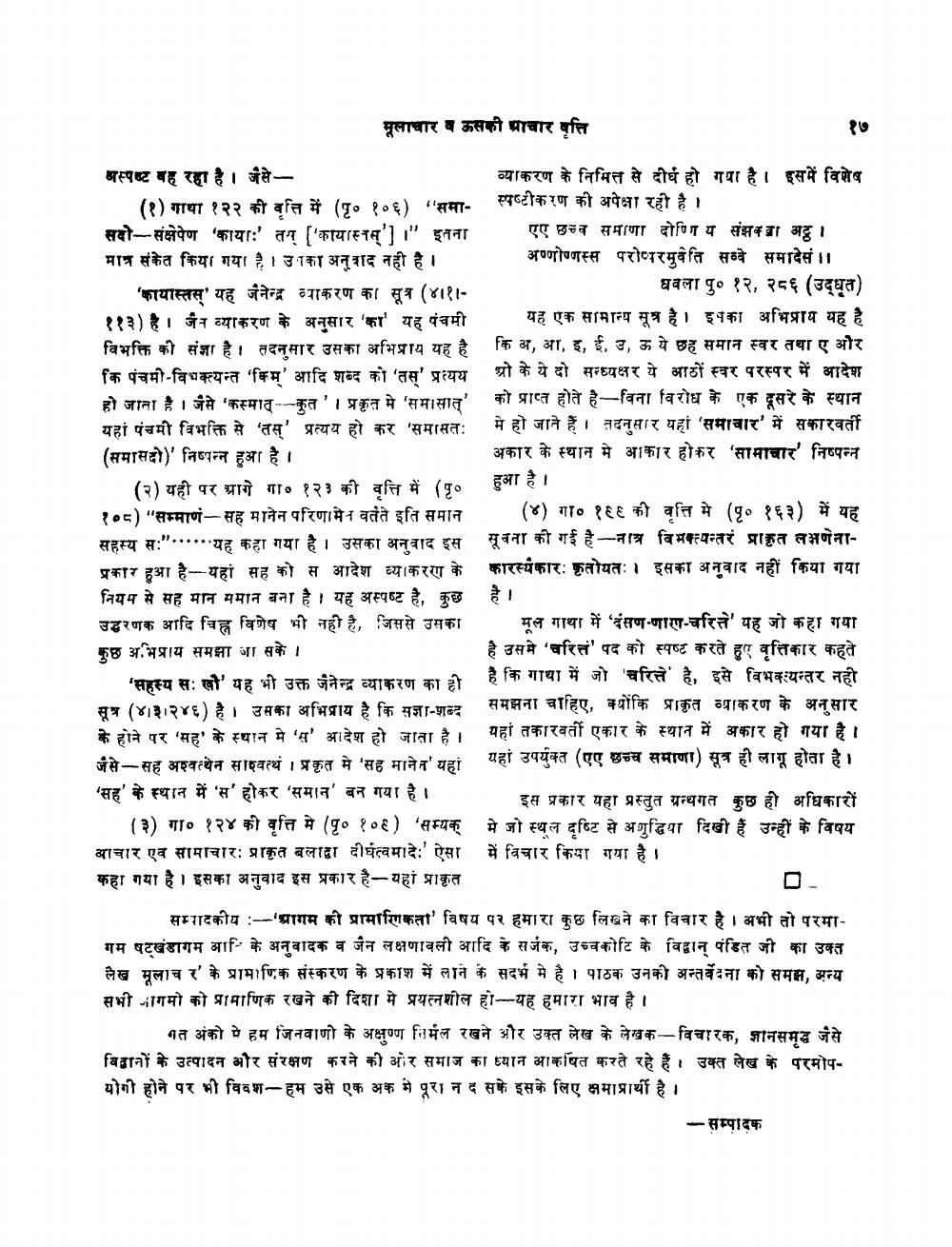________________
मूलाधार व ऊसकी प्राचार वृत्ति
अस्पष्ट बह रहा है। जैसे
व्याकरण के निमित्त से दीर्घ हो गया है। इसमें विशेष (१) गाथा १२२ की वृत्ति में (पृ० १०६) "समा
स्पष्टीकरण की अपेक्षा रही है। सदो-संक्षेपेण 'काया' तर 'कायास्नस्']।" इतना
एए छच्च समाणा दोणिय संझना अट्ठ। मात्र संकेत किया गया है। उनका अनुवाद नही है।
अण्णोण्णस्स परोपरमुवेति सव्वे समादेसं ।। 'कायास्तस्' यह जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र (४।१।
धवला पु० १२, २८६ (उद्धृत) ११३) है। जैन व्याकरण के अनुसार 'का' यह पंचमी यह एक सामान्य मूत्र है। इसका अभिप्राय यह है विभक्ति की संज्ञा है। सदनसार उसका अभिप्राय यह है कि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ ये छह समान स्वर तथा ए और कि पंचमी-विभक्त्यन्त 'किम्' आदि शब्द को 'तस' प्रत्यय प्रो के ये दो सन्ध्यक्षर ये आठों स्वर परस्पर में आदेश हो जाता है। जैसे 'कस्मात् कुत' । प्रकृत मे 'समासात्'
को प्राप्त होते है-विना विरोध के एक दूसरे के स्थान यहां पंचमी विभक्ति से 'तस्' प्रत्यय हो कर 'समासत: मे हो जाते हैं। तदनुसार यहाँ 'समाचार' में सकारवर्ती (समासदो)' निष्पन्न हुआ है।
अकार के स्थान मे आकार होकर 'सामाचार' निष्पन्न (२) यही पर आगे गा० १२३ की वृत्ति में (पृ० ।
हुआ है। १०८) "सम्माणं-सह मानेन परिणामेन वर्तते इति समान (४) गा० १६६ की वृत्ति मे (पृ० १६३) में यह सहस्य सः"....."यह कहा गया है। उसका अनुवाद इस सूचना की गई है-मात्र विमक्त्यन्तरं प्राकृत लक्षणेनाप्रकार हुआ है---यहां सह को स आदेश व्याकरण के कारस्यकारः कृतोयतः । इसका अनुवाद नहीं किया गया नियम से सह मान ममान बना है। यह अस्पष्ट है, कुछ है। उद्धरणक आदि चिह्न विणेष भी नहीं है, जिससे उसका मूल गाथा में 'दंसण-णार-चरित्ते' यह जो कहा गया कुछ अभिप्राय समझा जा सके।
है उसमे 'चरितं' पद को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार कहते 'सहस्य सः खो' यह भी उक्त जैनेन्द्र व्याकरण का ही है कि गाथा में जो 'चरित्ते' है, इसे विभक्त्यन्तर नही सूत्र (४।३।२४६) है। उसका अभिप्राय है कि सज्ञा-शब्द समझना चाहिए, क्योंकि प्राकृत व्याकरण के अनसार के होने पर 'सह' के स्थान में 'स' आदेश हो जाता है। यहां तकारवती एकार के स्थान में अकार हो गया है। जैसे-सह अश्वत्थेन साश्वत्थं । प्रकृत मे 'सह मानेन' यहां यहाँ उपयुक्त (एए छच्च समाणा) सूत्र ही लागू होता है। 'सह' के स्थान में 'स' होकर 'समान' बन गया है।
इस प्रकार यहा प्रस्तुत ग्रन्थगत कुछ ही अधिकारों (३) गा० १२४ की वृत्ति मे (पृ० १०६) 'सम्यक् मे जो स्थल दृष्टि से अशुद्धिया दिखी हैं उन्हीं के विषय आचार एव सामाचार: प्राकृत बलाद्वा दीर्घत्वमादेः' ऐसा में विचार किया गया है। कहा गया है। इसका अनुवाद इस प्रकार है-यहां प्राकृत
सम्पादकीय :--'प्रागम की प्रामाणिकता' विषय पर हमारा कुछ लिखने का विचार है । अभी तो परमागम षटखंडागम आनि के अनुवादक व जैन लक्षणावली आदि के सर्जक, उच्चकोटि के विद्वान पंडित जी का उक्त लेख मूलाच र' के प्रामाणिक संस्करण के प्रकाश में लाने के सदर्भ मे है । पाठक उनकी अन्तर्वेदना को समझ, अन्य सभी नागमो को प्रामाणिक रखने की दिशा मे प्रयत्नशील हो-यह हमारा भाव है।
त अंको से हम जिनवाणी के अक्षुण्ण निर्मल रखने और उक्त लेख के लेखक-विचारक, ज्ञानसमद्ध जैसे विद्वानों के उत्पादन और संरक्षण करने की और समाज का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। उक्त लेख के परमोपयोगी होने पर भी विवश-हम उसे एक अक मे पूरा न द सके इसके लिए क्षमाप्रार्थी है।
-सम्पादक