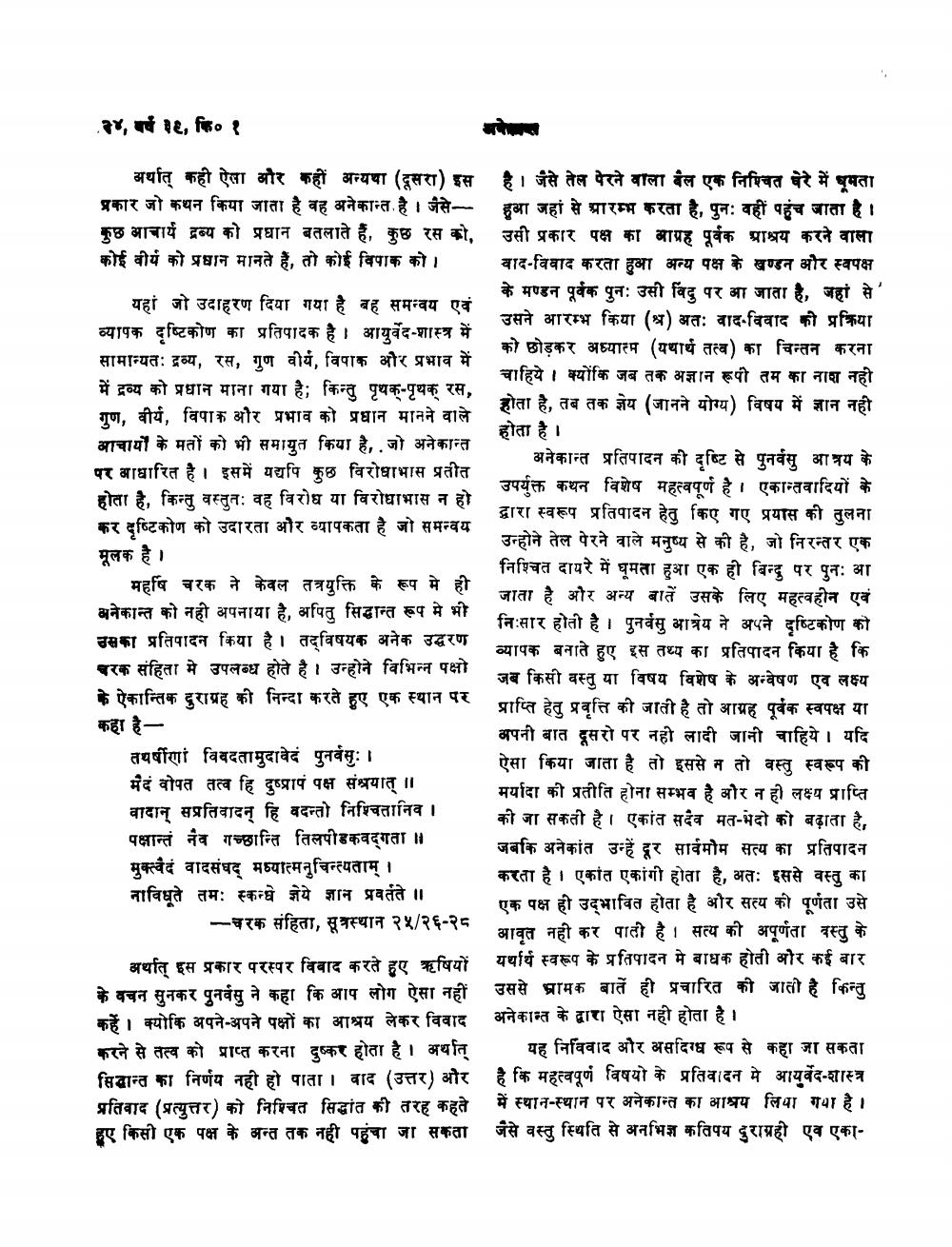________________
२४ वर्ष ३२ कि० १
अर्थात् कही ऐसा और कहीं अन्यथा ( दूसरा ) इस प्रकार जो कथन किया जाता है वह अनेकान्त है । जैसेकुछ आचार्य द्रव्य को प्रधान बतलाते हैं, कुछ रस को, कोई वीर्य को प्रधान मानते हैं, तो कोई विपाक को
-
यहां जो उदाहरण दिया गया है वह समन्वय एवं व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। आयुर्वेद-शास्त्र सामान्यतः द्रव्य, रस, गुण वीर्य, विपाक और प्रभाव में में द्रव्य को प्रधान माना गया है किन्तु पृथक्-पृथक् रस गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव को प्रधान मानने वाले आचार्यों के मतों को भी समायुत किया है, जो अनेकान्त पर आधारित है। इसमें यद्यपि कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है, किन्तु वस्तुतः वह विरोध या विरोधाभास न हो कर दृष्टिकोण को उदारता और व्यापकता है जो समन्वय मूलक है ।
महर्षि चरक ने केवल तत्रयुक्ति के रूप मे ही अनेकान्त को नही अपनाया है, अपितु सिद्धान्त रूप मे भी उसका प्रतिपादन किया है। तद्विषयक अनेक उद्धरण चरक संहिता मे उपलब्ध होते है । उन्होने विभिन्न पक्षो के ऐकान्तिक दुराग्रह की निन्दा करते हुए एक स्थान पर कहा है
तर्षीणां विवदतामुदावेदं पुनर्वसुः ।
मैदं वोपत तत्व हि दुष्प्रापं पक्ष संश्रयात् ॥ वादान् सप्रतिवादन् हि वदन्तो निश्चितानिव । पक्षान्तं नैव गच्छान्ति तिलपीडकवद्गता ॥ मुक्त्वेदं [वादसंपद् मध्यात्मनुचिन्त्यताम् । नाविधूते तमः स्कन्धे शेये ज्ञान प्रवर्तते ।।
चरक संहिता, सूत्रस्थान २५/२६-२८
अर्थात् इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए ऋषियों के वचन सुनकर पुनर्वसु ने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कहें। क्योंकि अपने-अपने पक्षों का आश्रय लेकर विवाद करने से तत्व को प्राप्त करना दुष्कर होता है । अर्थात् सिद्धान्त का निर्णय नही हो पाता बाद (उत्तर) और प्रतिवाद ( प्रत्युत्तर) को निश्चित सिद्धांत की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष के अन्त तक नहीं पहुंचा जा सकता
अपे
है। जैसे तेल पेरने वाला बैल एक निश्चित घेरे में घूमता हुआ जहां से आरम्भ करता है, पुनः वहीं पहुंच जाता है। उसी प्रकार पक्ष का आग्रह पूर्वक श्राश्रय करने वाला वाद-विवाद करता हुआ अन्य पक्ष के खण्डन और स्वपक्ष के मण्डन पूर्वक पुनः उसी बिंदु पर आ जाता है, जहां से उसने आरम्भ किया (ध) अतः वाद-विवाद की प्रक्रिया को छोड़कर अध्यात्म (यथार्थ तत्व) का चिन्तन करना चाहिये। क्योंकि जब तक अज्ञान रूपी तम का नाश नही होता है, तब तक ज्ञेय (जानने योग्य) विषय में ज्ञान नहीं होता है।
।
अनेकान्त प्रतिपादन की दृष्टि से पुनर्वसु आश्रय के उपर्युक्त कथन विशेष महत्वपूर्ण है। एकान्तवादियों के द्वारा स्वरूप प्रतिपादन हेतु किए गए प्रयास की तुलना उन्होंने तेल पेरने वाले मनुष्य से की है, जो निरन्तर एक निश्चित दायरे में घूमता हुआ एक ही बिन्दु पर पुनः आ जाता है और अन्य बातें उसके लिए महत्वहीन एवं निःसार होती है । पुनर्वसु आत्रेय ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि जब किसी वस्तु या विषय विशेष के अन्वेषण एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति की जाती है तो आग्रह पूर्वक स्वपक्ष या अपनी बात दूसरो पर नही लादी जानी चाहिये । यदि ऐसा किया जाता है तो इससे न तो वस्तु स्वरूप की मर्यादा की प्रतीति होना सम्भव है और न ही लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। एकांत सदैव मतभेदों को बढ़ाता है, जबकि अनेकांत उन्हें दूर सार्वमोम सत्य का प्रतिपादन करता है । एकांत एकांगी होता है, अतः इससे वस्तु का एक पक्ष ही उभावित होता है और सत्य की पूर्णता उसे आवृत नहीं कर पाती है सत्य की अपूर्णता वस्तु के यर्थार्थ स्वरूप के प्रतिपादन मे बाधक होती और कई बार उससे भ्रामक बातें ही प्रचारित की जाती है किन्तु अनेकान्त के द्वारा ऐसा नही होता है ।
यह निर्विवाद और असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण विषयों के प्रतिवादन मे आयुर्वेद-शास्त्र में स्थान-स्थान पर अनेकान्त का आश्रय लिया गया है । जैसे वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ कतिपय दुराग्रही एव एका