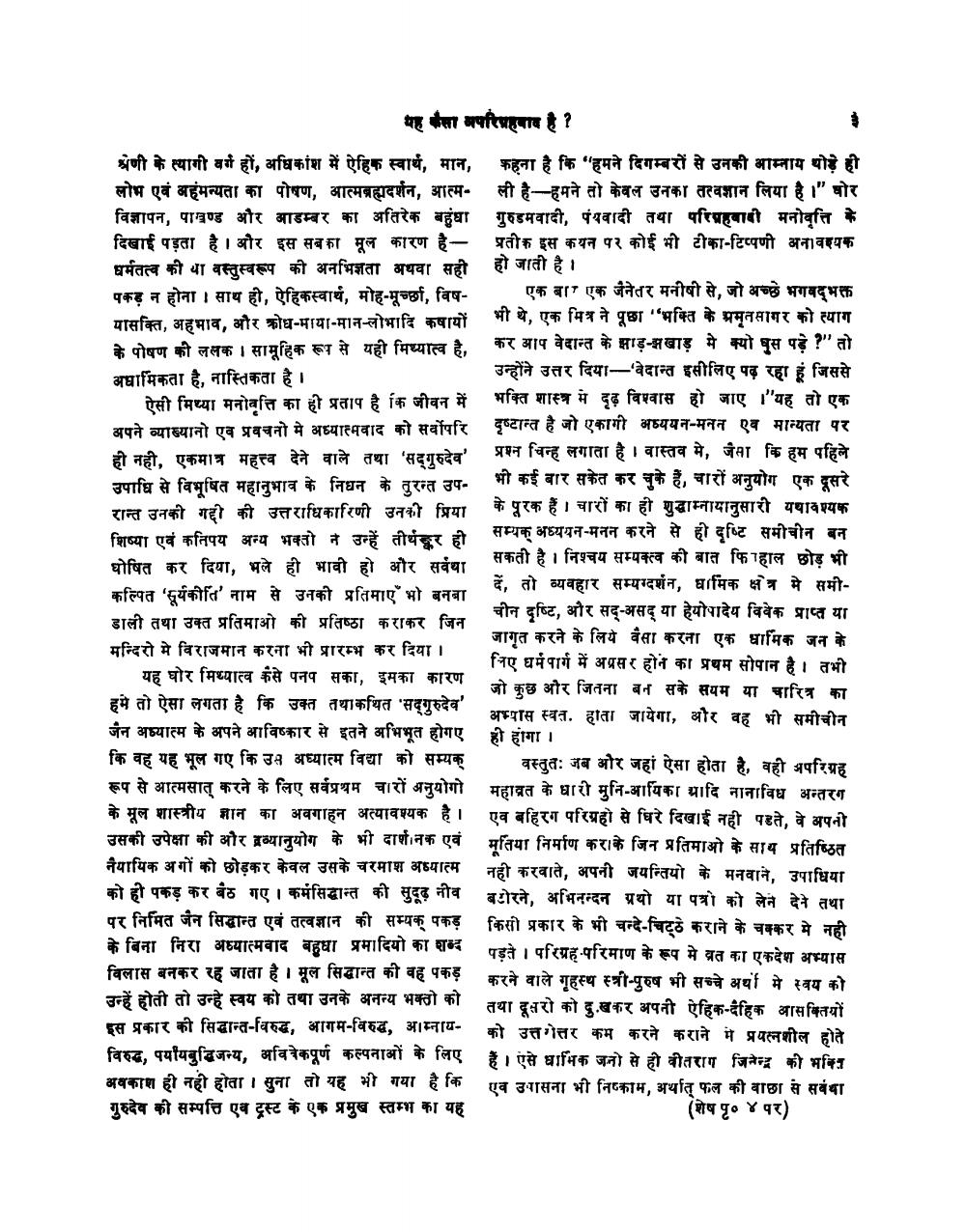________________
यह कैसा अपरिग्रहवाब है? श्रेणी के त्यागी वर्ग हों, अधिकांश में ऐहिक स्वार्थ, मान, कहना है कि "हमने दिगम्बरों से उनकी आम्नाय थोड़े ही लोभ एवं अहंमन्यता का पोषण, आत्मब्रह्मदर्शन, आत्म- ली है-हमने तो केवल उनका तत्वज्ञान लिया है।" घोर विज्ञापन, पाखण्ड और आडम्बर का अतिरेक बहुधा गुरुडमवादी, पंयवादी तथा परिग्रहवादी मनोवृत्ति के दिखाई पड़ता है। और इस सबका मूल कारण है- प्रतीक इस कयन पर कोई भी टीका-टिप्पणी अनावश्यक धर्मतत्व की या वस्तुस्वरूप की अनभिज्ञता अथवा सही हो जाती है। पकड़ न होना । साथ ही, ऐहिकस्वार्थ, मोह-मूर्छा, विष- एक बार एक जैनेतर मनीषी से, जो अच्छे भगवद्भक्त यासक्ति, अहभाव, और क्रोध-माया-मान-लोभादि कषायों भी थे, एक मित्र ने पूछा "भक्ति के अमृतसागर को त्याग के पोषण की ललक । सामूहिक रूप से यही मिथ्यात्व है, कर आप वेदान्त के झाड़-मखाड़ मे क्यो घुस पड़े?" तो अधार्मिकता है, नास्तिकता है।
उन्होंने उत्तर दिया-'वेदान्त इसीलिए पढ़ रहा हूं जिससे ऐसी मिथ्या मनोवृत्ति का ही प्रताप है कि जीवन में भक्ति शास्त्र में दृढ़ विश्वास हो जाए "यह तो एक अपने व्याख्यानो एव प्रवचनो मे अध्यात्मवाद को सर्वोपरि दृष्टान्त है जो एकागी अध्ययन-मनन एव मान्यता पर ही नही, एकमात्र महत्त्व देने वाले तथा 'सदगुरुदेव' प्रश्न चिन्ह लगाता है । वास्तव मे, जैसा कि हम पहिले उपाधि से विभूषित महानुभाव के निधन के तुरन्त उप
भी कई बार सकेत कर चुके हैं, चारों अनुयोग एक दूसरे रान्त उनकी गद्दी की उत्तराधिकारिणी उनकी प्रिया के पूरक हैं। चारों का ही शुद्धाम्नायानुसारी यथावश्यक शिष्या एवं कतिपय अन्य भक्तो ने उन्हें तीर्थकर ही
सम्यक् अध्ययन-मनन करने से ही दृष्टि समीचीन बन घोषित कर दिया, भले ही भावी हो और सर्वथा
सकती है । निश्चय सम्यक्त्व की बात फिाहाल छोड़ भी
दें, तो व्यवहार सम्यग्दर्शन, धार्मिक क्षेत्र मे समीकल्पित 'सूर्यकोति' नाम से उनकी प्रतिमाएं भो बनबा
चीन दृष्टि, और सद्-असद् या हेयोपादेय विवेक प्राप्त या डाली तथा उक्त प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा कराकर जिन
जागृत करने के लिये वैसा करना एक धार्मिक जन के मन्दिरो मे विराजमान करना भी प्रारम्भ कर दिया।
लिए धर्मपार्ग में अग्रसर होने का प्रथम सोपान है। तभी यह घोर मिथ्यात्व कैसे पनप सका, इसका कारण
जो कुछ और जितना बन सके सयम या चारित्र का हमे तो ऐसा लगता है कि उक्त तथाकथित 'सद्गुरुदेव'
अभ्यास स्वत. हाता जायेगा, और वह भी समीचीन जैन अध्यात्म के अपने आविष्कार से इतने अभिभूत होगए ही होगा। कि वह यह भूल गए कि उस अध्यात्म विद्या को सम्यक् वस्तुतः जब और जहां ऐसा होता है, वही अपरिग्रह रूप से आत्मसात् करने के लिए सर्वप्रथम चारों अनुयोगो महाव्रत के धारी मुनि-आर्यिका बादि नानाविध अन्तरग के मूल शास्त्रीय ज्ञान का अवगाहन अत्यावश्यक है। एव बहिरग परिग्रहो से घिरे दिखाई नही पडते, वे अपनी उसकी उपेक्षा की और द्रव्यानुयोग के भी दार्शनिक एवं मूर्तिया निर्माण कराके जिन प्रतिमाओ के साथ प्रतिष्ठित नैयायिक अगों को छोड़कर केवल उसके चरमाश अध्यात्म नही करवाते, अपनी जयन्तियो के मनवाने, उपाधिया को ही पकड़ कर बैठ गए। कर्मसिद्धान्त की सुदृढ़ नीव बटोरने, अभिनन्दन प्रथो या पत्रो को लेन देने तथा पर निर्मित जैन सिद्धान्त एवं तत्वज्ञान की सम्यक् पकड़ किसी प्रकार के भी चन्दे-चिट्ठे कराने के चक्कर मे नही के बिना निरा अध्यात्मवाद बहुधा प्रमादियो का शब्द
पड़ते । परिग्रह-परिमाण के रूप मे व्रत का एकदेश अभ्यास विलास बनकर रह जाता है। मूल सिद्धान्त की वह पकड़
करने वाले गृहस्थ स्त्री-पुरुष भी सच्चे अर्थो मे स्वय को उन्हें होती तो उन्हे स्वय को तथा उनके अनन्य भक्तो को
तथा दूसरो को दु.खकर अपनी ऐहिक-दैहिक आसक्तियों
तथा र इस प्रकार की सिद्धान्त-विरुद्ध, आगम-विरुद्ध, आम्नाय-
को उत्तगेत्तर कम करने कराने में प्रयत्नशील होते
को उत्तरोत्तर कम करने में विरुद्ध, पर्यायबुद्धिजन्य, अविवेकपूर्ण कल्पनाओं के लिए हैं। एसे धाभिक जनो से ही वीतराग जिनेन्द्र की भक्ति अवकाश ही नही होता। सुना तो यह भी गया है कि एव उपासना भी निष्काम, अर्थात् फल की वाछा से सर्वथा गुरुदेव की सम्पत्ति एव ट्रस्ट के एक प्रमुख स्तम्भ का यह
(शेष पृ० ४ पर)