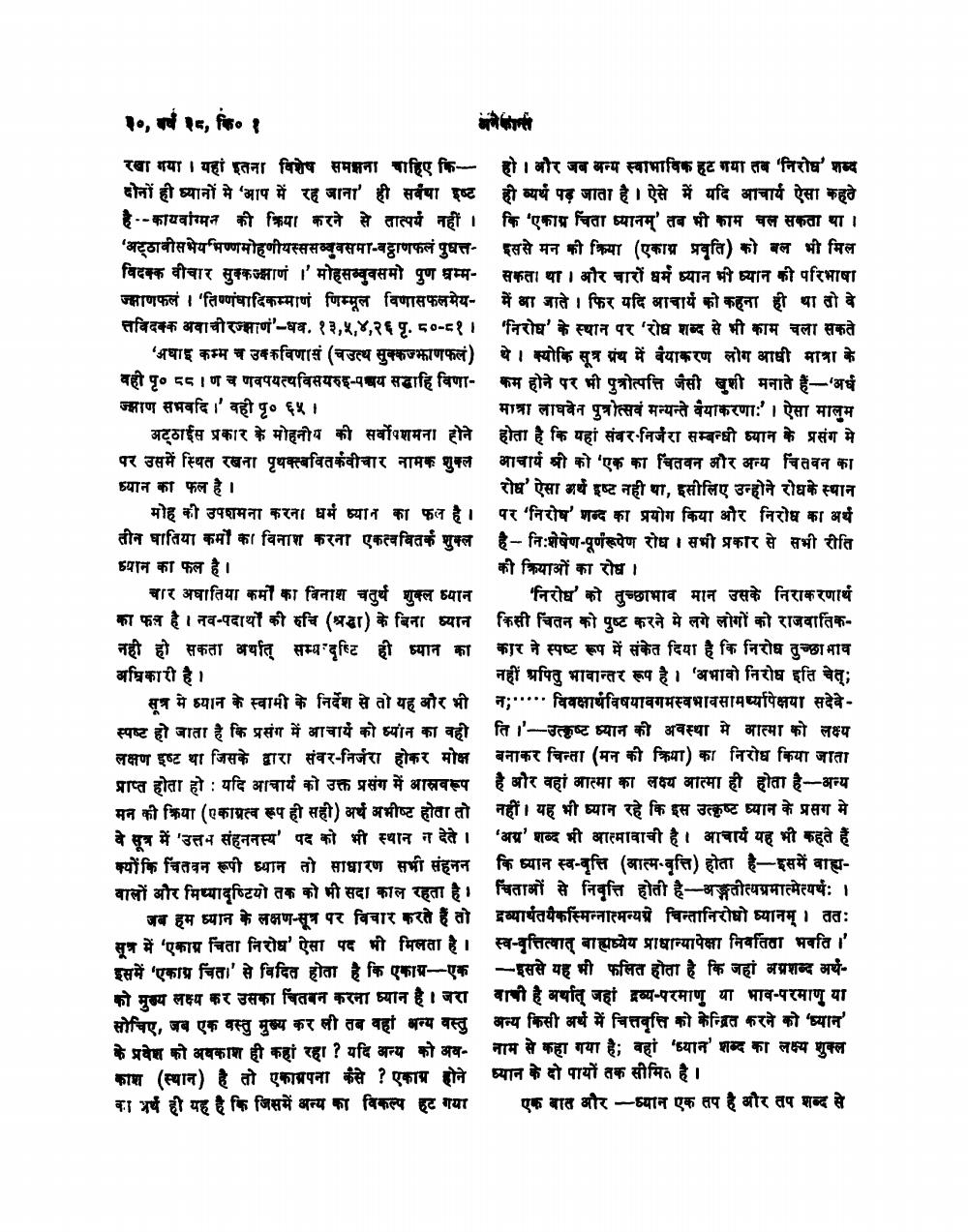________________
१० वर्ष १८ कि.. रखा गया। यहां इतना विशेष समझना चाहिए कि- हो। और जब अन्य स्वाभाविक हट गया तब 'निरोध' शब्द दोनों ही ध्यानों मे 'आप में रह जाना' ही सर्वथा इष्ट ही व्यर्थ पड़ जाता है। ऐसे में यदि आचार्य ऐसा कहते है.-कायवांग्मन की क्रिया करने से तात्पर्य नहीं। कि 'एकाग्र चिता ध्यानम्' तब भी काम चल सकता था। 'अट्ठावीसभेयभिण्णमोहणीयस्ससव्वुवसमा-बट्ठाणफलं पुषत्त- इससे मन की क्रिया (एकाग्र प्रवृति) को बल भी मिल विदक्क वीचार सुक्कज्माणं ।' मोहसम्वुवसमो पुण धम्म- सकता था। और चारों धर्म ध्यान भी ध्यान की परिभाषा ज्माणफलं । 'तिग्णधादिकम्माणं णिम्मूल विणासफलमेय- में आ जाते । फिर यदि आचार्य को कहना ही था तो वे तविदक्क अवाचीरमाणं'-धव. १३,५,४,२६ पृ.८०-८१। 'निरोध' के स्थान पर 'रोध शब्द से भी काम चला सकते
'अघाइ कम्म च उक्कविणासं (चउत्थ सुक्कज्झाणफलं) थे। क्योकि सूत्र ग्रंथ में वैयाकरण लोग आधी मात्रा के वही पृ० ८५ । ण च णवपयत्यविसयरुइ-पश्चय सदाहि विणा- कम होने पर भी पुत्रोत्पत्ति जैसी खुशी मनाते हैं-'अर्ध ज्झाण सभवदि।' वही पृ०६५।
मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः' । ऐसा मालम ___ अट्ठाईस प्रकार के मोहनीय की सर्वोपशमना होने होता है कि यहां संवर-निर्जरा सम्बन्धी ध्यान के प्रसंग मे पर उसमें स्थित रखना पृथक्त्ववितकवीचार नामक शुक्ल आचार्य श्री को 'एक का चितवन और अन्य चितवन का ध्यान का फल है।
रोध' ऐसा अर्थ इष्ट नही था, इसीलिए उन्होने रोधके स्थान मोह की उपशमना करना धर्म ध्यान का फल है। पर 'निरोष' शब्द का प्रयोग किया और निरोध का अर्थ तीन घातिया कर्मों का विनाश करना एकत्ववितर्क शुक्ल है-नि:शेषेण-पूर्णरूपेण रोध । सभी प्रकार से सभी रीति ध्यान का फल है।
की क्रियाओं का रोध। चार अघातिया कर्मों का विनाश चतुर्थ शुक्ल ध्यान निरोध' को तुच्छाभाव मान उसके निराकरणार्थ का फल है । नव-पदार्थों की रुचि (श्रद्धा) के बिना ध्यान किसी चिंतन को पुष्ट करने मे लगे लोगों को राजवार्तिकनही हो सकता अर्थात् सम्यग्दृष्टि ही ध्यान का कार ने स्पष्ट रूप में संकेत दिया है कि निरोध तुच्छाभाव अधिकारी है।
नहीं अपितु भावान्तर रूप है। 'अभावो निरोध इति चेत्; सूत्र में ध्यान के स्वामी के निर्देश से तो यह और भी ना...' विवक्षार्थविषयावगमस्वभावसामापेक्षया सदेवेस्पष्ट हो जाता है कि प्रसंग में आचार्य को ध्यान का वही ति।'-उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था मे आत्मा को लक्ष्य लक्षण इष्ट था जिसके द्वारा संवर-निर्जरा होकर मोक्ष बनाकर चिन्ता (मन की क्रिया) का निरोध किया जाता प्राप्त होता हो : यदि आचार्य को उक्त प्रसंग में आम्रवरूप है और वहां आत्मा का लक्ष्य आत्मा ही होता है-अन्य मन की क्रिया (एकाग्रत्व रूप ही सही) अर्थ अभीष्ट होता तो नहीं। यह भी ध्यान रहे कि इस उत्कृष्ट ध्यान के प्रसग मे वे सूत्र में 'उत्तम संहननस्य' पद को भी स्थान न देते। 'अय' शब्द भी आत्मावाची है। आचार्य यह भी कहते हैं क्योंकि चितवन रूपी ध्यान तो साधारण सभी संहनन कि ध्यान स्व-वृत्ति (आत्म-वृत्ति) होता है-इसमें वाह्यवालों और मिथ्यादृष्टियो तक को भी सदा काल रहता है। चिंताओं से निवृत्ति होती है-अङ्गतीत्यग्रमात्मेत्यर्थः ।
जब हम ध्यान के लक्षण-सूत्र पर विचार करते हैं तो द्रव्यातयकस्मिन्नात्मन्यग्रे चिन्तानिरोधो ध्यानम् । ततः सूत्र में 'एकाग्र चिता निरोध' ऐसा पद भी मिलता है। स्व-वृत्तित्वात् बाह्यध्येय प्राधान्यापेक्षा निवतिता भवति ।' इसमें 'एकाग्र चिता' से विदित होता है कि एकाग्र-एक -इससे यह भी फलित होता है कि जहां अग्रशब्द अर्थको मुख्य लक्ष्य कर उसका चितवन करना ध्यान है। जरा वाची है अर्थात् जहां द्रव्य-परमाणु या भाव-परमाणु या सोचिए, जब एक वस्तु मुख्य कर ली तब वहाँ अन्य वस्तु अन्य किसी अर्थ में चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने को 'ध्यान' के प्रवेश को अवकाश ही कहां रहा ? यदि अन्य को अव- नाम से कहा गया है। वहां 'ध्यान' शब्द का लक्ष्य शुक्ल काश (स्थान) है तो एकाग्रपना कैसे ? एकाग्र होने ध्यान के दो पायों तक सीमित है। का अर्थ ही यह है कि जिसमें अन्य का विकल्प हट गया एक बात और -ध्यान एक तप है और तप शब्द से