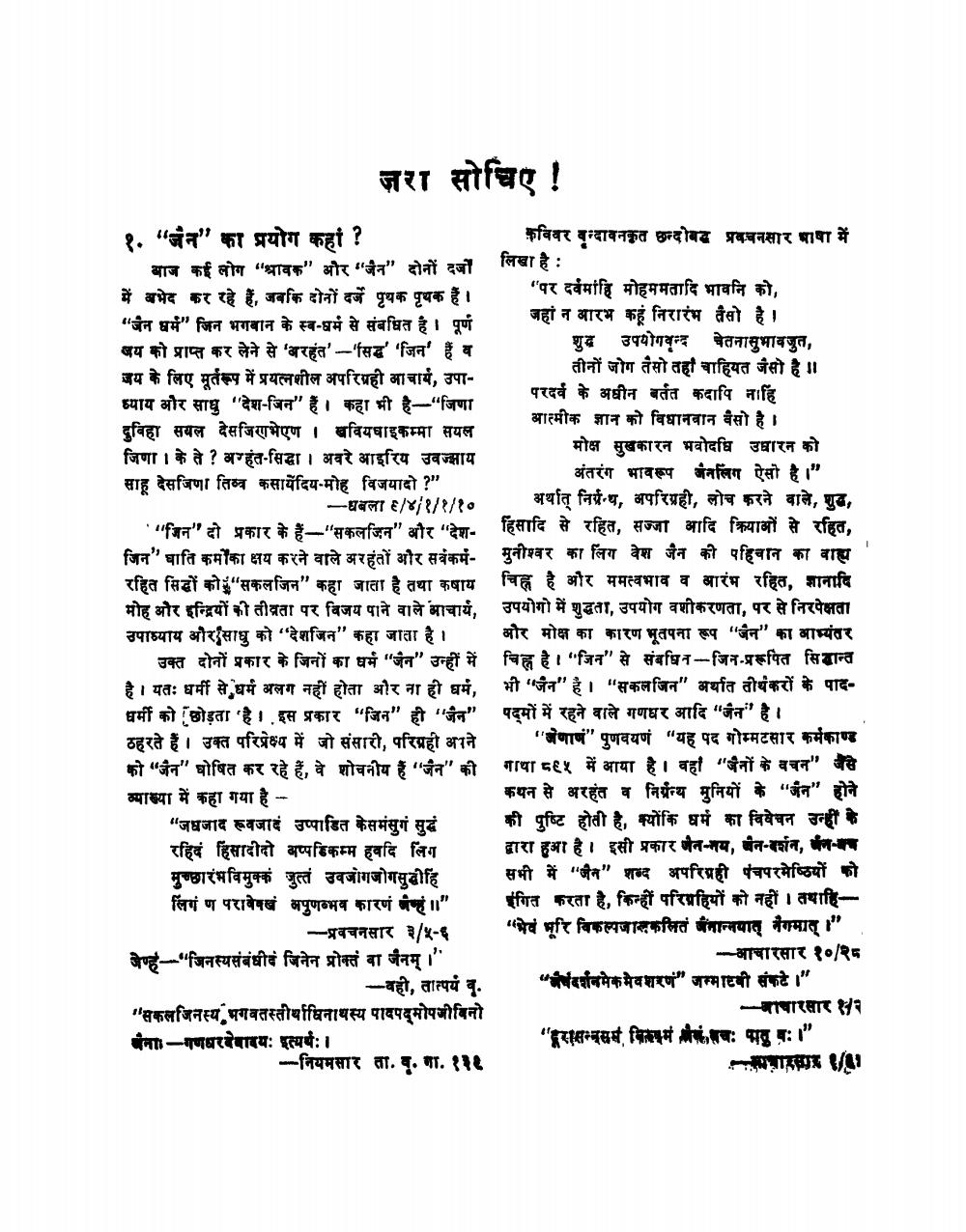________________
जरा सोधिए !
१. "जैन" का प्रयोग कहां ?
कविवर वृन्दावनकृत छन्दोबद्ध प्रवचनसार भाषा में ___बाज कई लोग "श्रावक" और "जैन" दोनों दो लिखा है : में बभेद कर रहे हैं, जबकि दोनों दर्जे पृथक पृथक हैं।
"पर दवमाहि मोहममतादि भावनि को, "जैन धर्म" जिन भगवान के स्व-धर्म से संबधित है। पूर्ण
जहां न आरभ कहूं निरारंभ तेसो है। जय को प्राप्त कर लेने से 'बरहंत' --सिद्ध' 'जिन' हैं व
शुद्ध उपयोगवन्द चेतनासुभावजुत, जय के लिए मूर्तरूप में प्रयत्नशील अपरिग्रही आचार्य, उपा
तीनों जोग तैसो तहाँ चाहियत जैसो है। ध्याय और साधु "देश-जिन" हैं। कहा भी है-"जिणा
परदर्व के अधीन बर्तत कदापि नाहिं दुबिहा सयल देसजिरणभेएण । खवियघाइकम्मा सयल
आत्मीक ज्ञान को विधानवान वैसो है। जिणा । के ते? अहंत-सिद्धा। अवरे आइरिय उवज्झाय
मोक्ष सुखकारन भवोदधि उधारन को साहू देसजिणा तिब्ब कसायेंदिय-मोह विजयादो?"
अंतरंग भावरूप अनलिंग ऐसो है।" -धबला ९/४/१/१/१०
र अर्थात् निम्र-थ, अपरिग्रही, लोच करने वाले, शुद्ध, "जिन" दो प्रकार के हैं-"सकलजिन" और "देश- हिंसादि से रहित, सज्जा आदि क्रियाओं से रहित, जिन" घाति कोका क्षय करने वाले अरहंतों और सर्वकर्म- मुनीश्वर का लिंग वेश जैन की पहिचान का वाह्य रहित सिद्धों को "सकलजिन" कहा जाता है तथा कषाय चिह्न है और ममत्वभाव व बारंभ रहित, ज्ञानादि मोह और इन्द्रियों की तीव्रता पर विजय पाने वाले माचार्य, उपयोगो में शुद्धता, उपयोग वशीकरणता, पर से निरपेक्षता उपाध्याय और साधु को "देशजिन" कहा जाता है। और मोक्ष का कारण भूतपना रूप "जैन" का आभ्यंतर
उक्त दोनों प्रकार के जिनों का धर्म "जैन" उन्हीं में चिह्न है । "जिन" से संबधिन-जिन-प्ररूपित सिद्धान्त है। यतः धर्मी से धर्म अलग नहीं होता और ना ही धर्म, भी "जैन" है। "सकलजिन" अर्थात तीर्थंकरों के पादधर्मी को छोड़ता है। इस प्रकार "जिन" ही "जैन" पद्मों में रहने वाले गणधर आदि "जैन" है। ठहरते हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में जो संसारी, परिग्रही अपने "जेणाणं" पुणवयणं "यह पद गोम्मटसार कर्मकाण्ड को "जैन" घोषित कर रहे हैं, वे शोचनीय है "जैन" की गाथा ८६५ में आया है। वहाँ "जैनों के वचन" जैसे व्याख्या में कहा गया है -
कथन से अरहंत व निग्रंन्य मुनियों के "जैन" होने "जधजाद रूवजादं उप्पाडित केसमंसुगं सुद्ध की पुष्टि होती है, क्योंकि धर्म का विवेचन उन्हीं के रहिवं हिंसादीदो अप्पटिकम्म हवदि लिंग द्वारा हुआ है। इसी प्रकार जैन-गय, बैन-वर्शन, अंग-पत्र मुच्छारंभविमुक्कं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहिं सभी में "जैन" शब्द अपरिग्रही पंचपरमेष्ठियों को लिंग ण परावेक्खं अपुणम्भव कारणं हं।"
इंगित करता है, किन्हीं परिग्रहियों को नहीं । तथाहि-प्रवचनसार ३/५-६ "भेवं भूरि विकल्पजालकलितं नान्नयात् नैगमात् ।" . जेण्ड-"जिनस्यसंबंधीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् ।"
-आचारसार १०/२ -वही, तात्पर्य वृ. "दर्शनमेकमेवशरणं" जम्माटवी संकटे।" "सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो
याचारसारक बना-गणवरदेवावयः इत्यर्थः ।
"दूरासन्यसम विस्म सवः पातु वः।" -नियमसार ता.व. ना.१३९