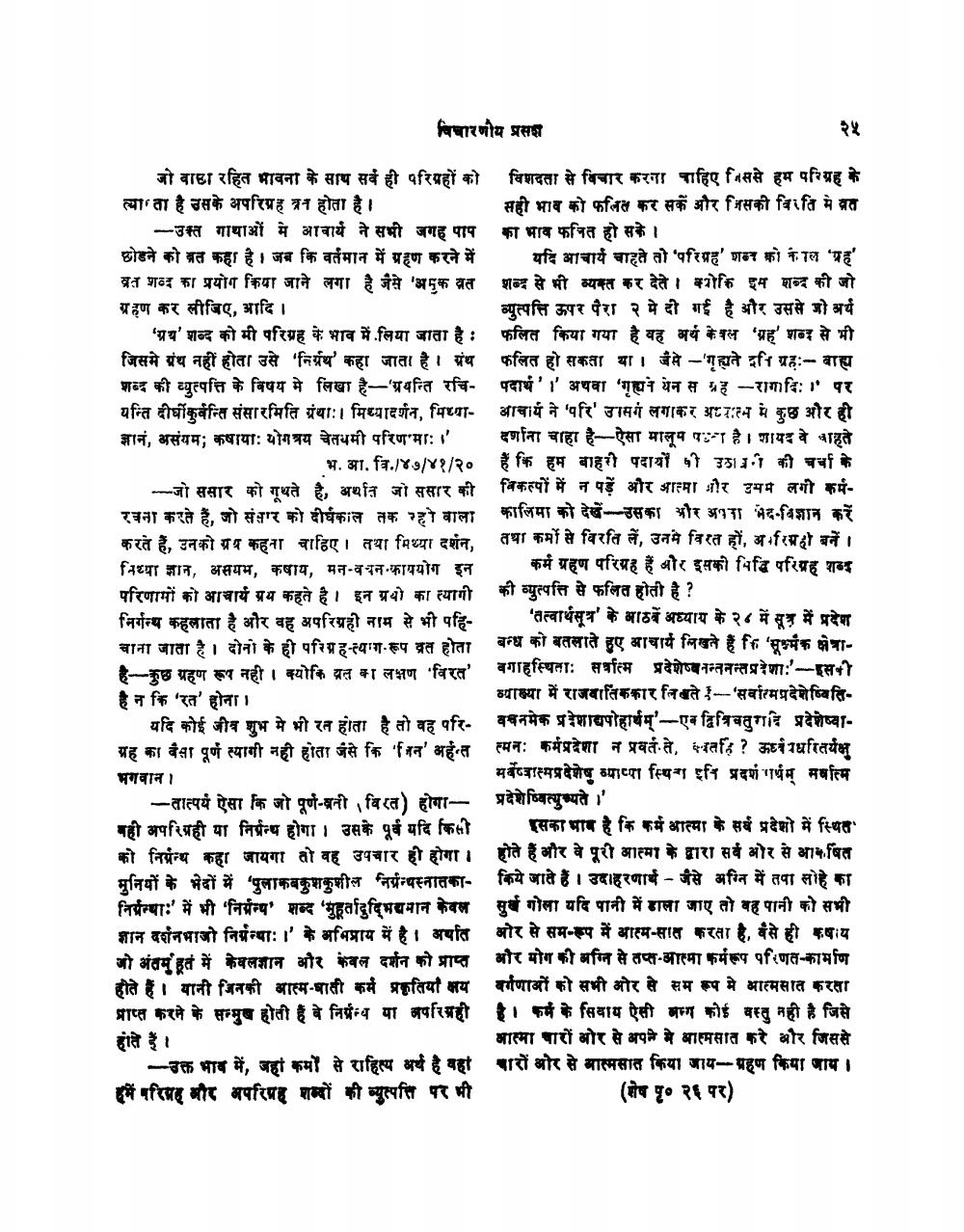________________
विचारणीय प्रस
जो वाछा रहित भावना के साथ सर्व ही परिग्रहों को वाता है उसके अपरिग्रह व्रत होता है।
- उक्त गाथाओं में आचार्य ने सभी जगह पाप छोडने को व्रत कहा है। जब कि वर्तमान में ग्रहण करने में व्रत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है जैसे 'अमुक व्रत ग्रहण कर लीजिए, आदि ।
'प्र' शब्द को भी परिग्रह के भाव में लिया जाता है: जिसमे ग्रंथ नहीं होता उसे 'निर्भय' कहा जाता है। ग्रंथ शब्द की व्युत्पत्ति के विषय मे लिखा है - 'ग्रयन्ति रचियन्ति दीर्घीकुर्वन्ति संसारमिति ग्रंथाः । मिथ्यादर्शन, मिध्याज्ञानं, असंयम; कषायाः योगत्रय चेतथमी परिणामाः ।' भ. आ. वि. / ४७/४१/२० ---जो ससार को गूथते है, अर्थात जो ससार की रचना करते हैं, जो संसार को दीर्घकाल तक रहो वाला करते हैं, उनको अब कहना चाहिए तथा मिथ्या दर्शन निथ्या ज्ञान, असयम, कषाय, मन-वचन-काययोग इन परिणामों को आचार्य प्रथ कहते है । इन ग्रथो का त्यागी निर्गन्ध कहलाता है और वह अपरिग्रही नाम से भी पहिचाना जाता है। दोनों के ही परिग्रह त्याग-रूप व्रत होता -कुछ पण रूप नहीं क्योकि प्रत का लक्षण 'विरत' है न कि 'रत' होना ।
यदि कोई जीव शुभ मे भी रत होता है तो वह परि ग्रह का बैना पूर्ण स्थानी नही होता जैसे कि 'जिन' अर्हत
भगवान ।
- तात्पर्य ऐसा कि जो पूर्ण बनी बिरल) होगा नही अपरिग्रही या निर्धन्य होगा उसके पूर्व यदि किसी को निर्ग्रन्थ कहा जायगा तो वह उपचार ही होगा । मुनियों के भेदों में 'पुलाकबकुशकुशील निर्ग्रन्थस्नातकानिर्मन्थाः' में भी 'निर्मन्थ' शब्द 'महद्यमान केवल ज्ञान दर्शनभाजो निर्ग्रन्थाः ।' के अभिप्राय में है । अर्थात जो अंतर्मुहूर्त में केवलज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त होते हैं। यानी जिनकी आत्म-भाती कर्म प्रकृतियाँ क्षय प्राप्त करने के सम्मुख होती हैं वे निर्ग्रन्थ या अपरिग्रही होते हैं।
उक्त भाव में, जहां कमों से राहित्य अर्थ है यहां हमें परिग्रह और अपरिग्रह शब्दों की व्युत्पत्ति पर भी
विशदता से विचार करना चाहिए जिससे हम परिग्रह के सही भाव को फलित कर सकें और जिसकी विरति मे व्रत का भाव फत्रित हो सके ।
२५
यदि आचार्य चाहते तो 'परिग्रह' शब्द को केवल 'ग्रह' शब्द से भी व्यक्त कर देते। क्योकि इस शब्द की जो व्युत्पत्ति ऊपर पैरा २ मे दी गई है और उससे जो अर्थ फलित किया गया है यह अर्थ केवल 'ग्रह' शब्द से भी फलित हो सकता था जैसे मुह्यते इनि बाह्य पदार्थ ' ' अथवा 'गृह्यने येन स ग्रह - रागादिः " पर आचार्य ने 'परि' उपसर्ग लगाकर अध्यन मे कुछ और ही दर्गांना पाहा है ऐसा मालूम पन है। शायद वे चाहते हैं कि हम बाहरी पदार्थों की उठाने की चर्चा के विकल्पों में न पड़ें और आत्मा और उसमें लगी कर्मकालिमा को देखें उसका और अपना मंद-विज्ञान करें तथा कर्मों से विरति में, उनमें विश्त हों, अबिने
-
कर्म ग्रहण परिग्रह हैं और इसकी सिद्धि परिग्रह शब्द की व्युत्पत्ति से फलित होती है ?
'तत्वार्थसूत्र' के आठवें अध्याय के २४ में सूत्र में प्रदेश बन्ध को बतलाते हुए आचार्य लिखते है कि 'सूर्मक क्षेत्रा वगाहस्थिताः सर्वात्म प्रवेशेष्यनतनन्तप्रदेश: इस व्याकया में राजवातिककार लिखते - 'सर्वात्मप्रदेष्वति
-
वचनमेक प्रदेशाद्यपहार्यम् एवं द्विचितिप्रदेशेष्यत्मनः कर्मप्रदेशा न प्रवर्तते स्वत? arren देशेषु व्याप्या स्थित इनि प्रदर्श गर्थम् मर्षात्म प्रदेशेध्वित्युच्यते ।'
इसका भाव है कि कर्म आत्मा के सर्व प्रदेशों में स्थित ' होते हैं और वे पूरी आत्मा के द्वारा सर्व ओर से आकर्षित किये जाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे अग्नि में तपा लोहे का सुखं गोला यदि पानी में डाला जाए तो वह पानी को सभी ओर से सम-रूप में आत्मसात करता है, वैसे ही कषाय और योग की अग्नि से तप्त आत्मा कर्मरूप परिणत कामण वर्गगाओं को सभी ओर से सम रूप मे आत्मसात करता है। कर्म के सिवाय ऐसी अन्य कोई वस्तु नही है जिसे आत्मा चारों ओर से अपने मे आत्मसात करे और जिससे चारों ओर से आत्मसात किया जाय ग्रहण किया जाय। (सेच पृ० २६ पर)