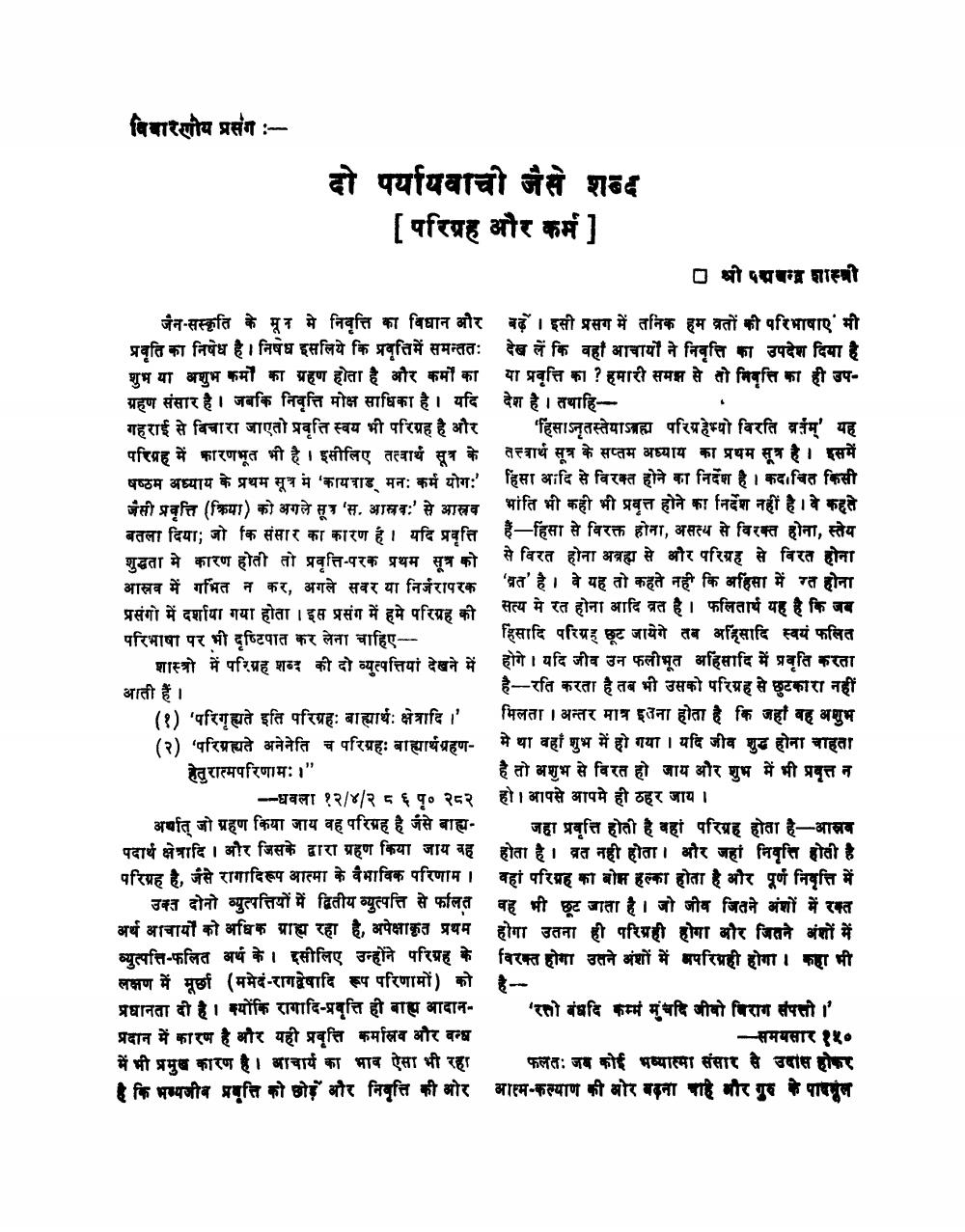________________
विचारणीय प्रसंग :
दो पर्यायवाची जैसे शब्द
[परिग्रह और कर्म]
श्री पप्रचन्द्र शास्त्री
जैन-सस्कृति के मून मे निवृत्ति का विधान और बढ़े। इसी प्रसग में तनिक हम व्रतों की परिभाषाए मी प्रवृति का निषेध है। निषेध इसलिये कि प्रवृत्तिमें समन्ततः देख लें कि वहाँ आचार्यों ने निवृत्ति का उपदेश दिया है शुभ या अशुभ कर्मों का ग्रहण होता है और कर्मों का या प्रवृत्ति का ? हमारी समझ से तो निवृत्ति का ही उपग्रहण संसार है। जबकि निवृत्ति मोक्ष साधिका है। यदि देश है । तथाहि-
. गहराई से विचारा जाएतो प्रवृत्ति स्वय भी परिग्रह है और हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति वर्तम्' यह परिग्रह में कारणभूत भी है । इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के तत्त्वार्थ सूत्र के सप्तम अध्याय का प्रथम सूत्र है। इसमें षष्ठम अध्याय के प्रथम सूत्र में 'कायराइ मनः कर्म योगः' हिंसा आदि से विरक्त होने का निर्देश है। कदाचित किसी जैसी प्रवृत्ति (क्रिया) को अगले सूत्र 'स. आस्रवः' से आस्रव भांति भी कही भी प्रवृत्त होने का निर्देश नहीं है। वे कहते बतलाया जो कि संसार का कारण है। यदि प्रवत्ति हैं-हिंसा से विरक्त होना, असत्य से विरक्त होना, स्तेय शुद्धता मे कारण होती तो प्रवृत्ति-परक प्रथम सत्र को से विरत होना अब्रह्म से और परिग्रह से विरत होना आस्रव में गभित न कर, अगले सवर या निर्जरापरक व्रत है। वे यह तो कहते नह' कि अहिसा में रत होना प्रसंगो में दर्शाया गया होता । इस प्रसंग में हमे परिग्रह की सत्य म रत होना आदि व्रत है। फालताये यह ह कि जब परिभाषा पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए---
हिसादि परिग्रह छूट जायेगे तब अहिंसादि स्वयं फलित शास्त्रो में परिग्रह शब्द की दो व्युत्पत्तियां देखने में होगे। यदि जीव उन फलीभूत अहिंसादि में प्रवृति करता आती हैं।
है-रति करता है तब भी उसको परिग्रह से छुटकारा नहीं (१) 'परिगृह्यते इति परिग्रहः बाह्यार्थः क्षेत्रादि ।' मिलता । अन्तर मात्र इतना होता है कि जहां वह अशुभ (२) 'परिग्रह्यते अनेनेति च परिग्रहः बाह्यार्थग्रहण- मे था वहाँ शुभ में हो गया । यदि जीव शुद्ध होना चाहता हेतुरात्मपरिणामः।"
है तो अशुभ से विरत हो जाय और शुभ में भी प्रवृत्त न -धवला १२/४/२८ ६ पृ० २८२ हो। आपसे आपमे ही ठहर जाय। अर्थात् जो ग्रहण किया जाय वह परिग्रह है जैसे बाह्य- जहा प्रवृत्ति होती है वहां परिग्रह होता है-आनव पदार्थ क्षेत्रादि । और जिसके द्वारा ग्रहण किया जाय वह होता है। व्रत नहीं होता। और जहां निवृत्ति होती है परिग्रह है, जैसे रागादिरूप आत्मा के वैभाविक परिणाम। वहां परिग्रह का बोझ हल्का होता है और पूर्ण निवृत्ति में
उक्त दोनो व्युत्पत्तियों में द्वितीय व्युत्पत्ति से फलित वह भी छट जाता है। जो जीव जितने अंशों में रक्त अर्थ आचार्यों को अधिक ग्राह्य रहा है, अपेक्षाकृत प्रथम होगा उतना ही परिग्रही होगा और जितने अंशों में व्युत्पत्ति-फलित अर्थ के। इसीलिए उन्होंने परिग्रह के विरक्त होगा उतने अंशों में अपरिग्रही होगा। कहा भी लक्षण में मूर्छा (ममेवं-रागद्वेषादि रूप परिणामों) को हैप्रधानता दी है। क्योंकि रागादि-प्रवृत्ति ही बाह्य आदान- 'रतो बंधदि कम्म मुंचदि जीवो विराग संपत्तो।' प्रदान में कारण है और यही प्रवृत्ति कर्मानव और बन्ध
-समयसार १५० में भी प्रमुख कारण है। आचार्य का भाव ऐसा भी रहा फलतः जब कोई भव्यास्मा संसार से उदास होकर हैकि भन्यजीव प्रवृत्ति को छोड़ें और निवृत्ति की ओर आत्म-कल्याण की ओर बढ़ना चाह और गुरु के पारमूल