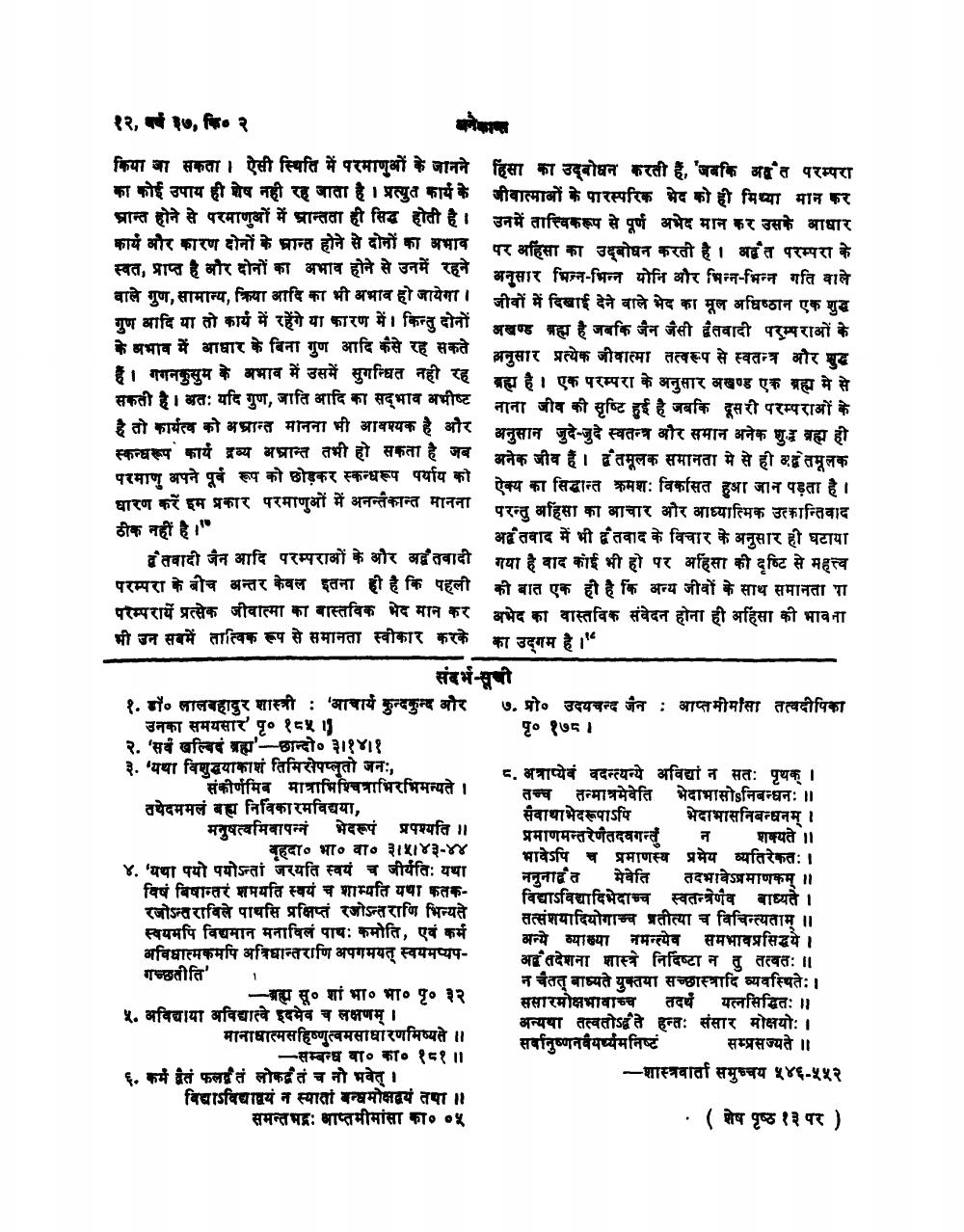________________
१२,३०२
बनेका
किया जा सकता। ऐसी स्थिति में परमाणुओं के जानने का कोई उपाय ही शेष नहीं रह जाता है। प्रत्युत कार्य के भ्रान्त होने से परमाणुओं में प्रान्तता ही सिद्ध होती है । कार्य और कारण दोनों के भ्रान्त होने से दोनों का अभाव
हिंसा का उद्बोधन करती है, जबकि त परम्परा जीवात्माओं के पारस्परिक भेद को ही मिथ्या मान कर उनमें तात्त्विक रूप से पूर्ण अभेद मान कर उसके आधार
स्वत प्राप्त है और दोनों का अभाव होने से उनमें रहने वाले गुण, सामान्य किया आदि का भी अभाव हो जायेगा । गुण आदि या तो कार्य में रहेंगे या कारण में किन्तु दोनों के अभाव में आधार के बिना गुण आदि कैसे रह सकते हैं। गगनकुसुम के अभाव में उसमें सुगन्धित नही रह सकती है। अतः यदि गुण, जाति आदि का सद्भाव अभीष्ट है तो कार्य को मत मानना भी आवश्यक है और अप्रान्त स्कन्धरूप कार्य द्रव्य अत्रान्त तभी हो सकता है जब परमाणु अपने पूर्व रूप को छोड़कर स्कन्धरूप पर्याय की धारण करें इस प्रकार परमाणुओं में अनन्तकान्त मानना ठीक नहीं है। "
पर अहिंसा का उद्बोधन करती है। मई व परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न योनि और गति वाले भिन्न-भिन्न जीवों में दिखाई देने वाले भेद का मूल अधिष्ठान एक शुद्ध अखण्ड ब्रह्म है जबकि जैन जैसी द्वैतवादी परम्पराओं के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा तत्वरूप से स्वतन्त्र और बुद्ध ब्रह्म है । एक परम्परा के अनुसार अखण्ड एक ब्रह्म मे से नाना जीव की सृष्टि हुई है जबकि दूसरी परम्पराओं के अनुसान जुदे-जुदे स्वतन्त्र और समान अनेक शुद्ध ब्रह्म ही अनेक जीव है। द्वंतमूलक समानता मे से ही कई मूलक ऐक्य का सिद्धान्त क्रमशः विकसित हुआ जान पड़ता है। परन्तु अहिंसा का आचार और आध्यात्मिक उत्क्रान्तिवाद अतवाद में भी ईतवाद के विचार के अनुसार ही घटाया गया है बाद कोई भी हो पर अहिंसा की दृष्टि से महत्त्व की बात एक ही है कि अन्य जीवों के साथ समानता पा अभेद का वास्तविक संवेदन होना ही अहिंसा की भावना का उद्गम है।"
द्वैतवादी जैन आदि परम्पराओं के और अद्वैतवादी परम्परा के बीच अन्तर केवल इतना ही है कि पहली परम्परायें प्रत्येक जीवात्मा का वास्तविक भेद मान कर भी उन सबमें तात्विक रूप से समानता स्वीकार करके
संदर्भ-सूची
:
१. डॉ० लालबहादुर शास्त्री 'आचार्य कुन्दकुन्द और उनका समयसार पृ० १८५
२. 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म छान्दो० ३११४११
३. 'यथा विशुद्धयाकाशं तिमिसेपप्लुतो जनः,
संकीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते । तयेदममलं बह्म निविकारमविद्यया,
मनुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति ।। वृहदा० भा० वा० ३१५१४३-४४ ४. 'यथा पयो पयोऽन्तां जरयति स्वयं च जीर्यतिः यथा विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति यथा कतकरजोऽन्तराविले पाथसि प्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि भिन्यते स्वयमपि विद्यमान मनाविलं पाय: कमोति एवं कर्म अविद्यात्मकमपि अविधान्तराणि अपगमयत् स्वयंमध्यप गच्छतीति'
- ब्रह्म सु० शां भा० भा० पृ० ३२ ५. अविद्याया विद्यारवे इदमेव च लक्षणम् । मानाधात्मसहिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते ॥ -सम्बन्ध वा० का० १५१ ।।
६. कर्म फलई लोकतं च नो भवेत् । विद्याविद्यrai न स्यातां बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥ समन्तभद्रः आप्तमीमांसा का० ०५
७. प्रो० उदयचन्द जैन आप्तमीमांसा तत्वदीपिका पृ० १७५।
।
८. अत्राप्येवं वदन्त्यन्ये अविद्यां न सतः पृथक् । तच्च तन्मात्रमेवेति भेदाभासोऽनिबन्धनः ॥ संवाषाभेदरूपाऽपि भेदाभासनिबन्धनम् । प्रमाणमन्तरेणैतदवगन्तु न शक्यते ॥ भावेऽपि च प्रमाणस्य प्रमेय व्यतिरेकतः । ननुनाई व मेवेति तदभावेप्रमाणकम् ॥ विद्याऽविद्याविभेदाच्च स्वतन्त्रेव बाध्यते । सत्संशयादियोगाच्च प्रतीत्या च विचिन्त्यताम् ॥ अन्ये व्याख्या नमन्त्येव समभावप्रसिद्धये । अतदेशना शास्त्रे निर्दिष्टा न तु तत्वतः ॥ न चैतत् बाध्यते युक्तया सच्छास्त्रादि व्यवस्थितेः ॥ ससारमोक्षभावाच्च तदर्थं यत्नसिद्धितः ॥ अन्यथा तत्वतोऽद्वैते हन्तः संसार मोक्षयोः । सर्वानुष्णनवैयर्थ्यमनिष्टं सम्प्रसज्यते ॥
- शास्त्रवार्ता समुच्चय ५४६-५५२
•
( शेष पृष्ठ १३ पर )