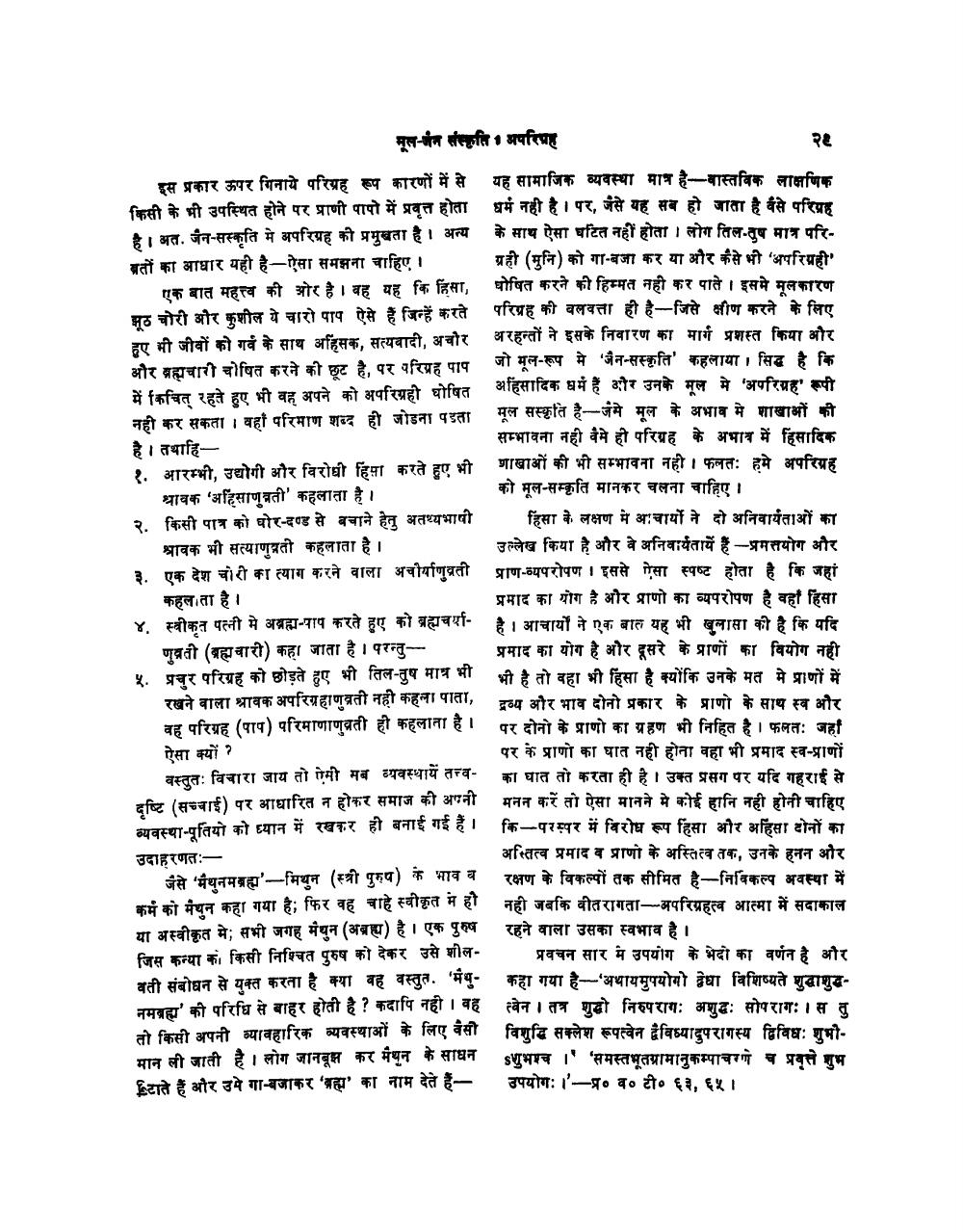________________
मूल-न संस्कृति
इस प्रकार ऊपर गिनाये परिग्रह रूप कारणों में से किसी के भी उपस्थित होने पर प्राणी पायो में प्रवृत्त होता है । अत. जैन संस्कृति मे अपरिग्रह की प्रमुखता है । अन्य व्रतों का आधार यही है - ऐसा समझना चाहिए ।
एक बात महत्त्व की ओर है। वह यह कि हिंसा, झूठ चोरी और कुशील ये चारो पाप ऐसे हैं जिन्हें करते हुए भी जीवों को गर्व के साथ अहिंसक, सत्यवादी अचोर और ब्रह्मचारी चोषित करने की छूट है, पर परिग्रह पाप में किचित् रहते हुए भी वह अपने को अपरिग्रही घोषित नही कर सकता । वहाँ परिमाण शब्द ही जोडना पडता है । तथाहि
१. आरम्भी, उद्योगी और विरोधी हिंसा करते हुए भी पावक 'अहिंसावती' कहलाता है।
२. किसी पात्र को पोरन से बचाने हेतु अतय्यभाषी श्रावक भी सत्याणुव्रती कहलाता है ।
३. एक देश चोरी का त्याग करने वाला अचौर्याणुव्रती कहलाता है ।
४. स्वीकृत पत्नी मे अब्रह्मन्याप करते हुए को ब्रह्मचर्या ती (बाबा) कहा जाता है। परन्तु
५. प्रचुर परिग्रह को छोड़ते हुए भी तिल-तुप मात्र भी रखने वाला श्रावक अपरिग्रहाणुव्रती नहीं कहला पाता, वह परिग्रह (पाप) परिमाणाणुव्रती ही कहलाता है । ऐसा क्यों? वस्तुतः विचारा जाय तो ऐसी मब व्यवस्थायें तत्त्वदृष्टि ( सच्चाई) पर आधारित न होकर समाज की अपनी व्यवस्था - पूर्तियो को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं । उदाहरणत:
जैसे 'मैथुनमा मिथुन (स्त्री पुरुष) के भाव कर्म को मैथुन कहा गया है; फिर वह चाहे स्वीकृत मे हो या अस्वीकृत मे सभी जगह मैथुन (अवहा है। एक पुरुष जिस कन्या को किसी निश्चित पुरुष को देकर उसे बती संबोधन से युक्त करता है क्या वह वस्तुत नमब्रह्म की परिधि से बाहर होती है ? कदापि नहीं तो किसी अपनी व्यावहारिक व्यवस्थाओं के लिए वैसी मानली जाती है । लोग जानबूझ कर मैथुन के साधन हटाते हैं और उमेगा-बजाकर 'ब्रह्म' का नाम देते हैं
वह
-
मैथु
अपरिग्रह
२८
यह सामाजिक व्यवस्था मात्र है— वास्तविक लाक्षणिक धर्म नहीं है। पर जैसे यह सब हो जाता है वैसे परिग्रह के साथ ऐसा घटित नहीं होता। लोग तिल-तुष मात्र परिग्रही ( मुनि) को गायजा कर या और कैसे भी 'अपरिग्रही" घोषित करने की हिम्मत नही कर पाते। इसमे मूलकारण परिग्रह की बलवत्ता ही है- जिसे क्षीण करने के लिए अरहन्तों ने इसके निवारण का मार्ग प्रशस्त किया और जो मूल रूप मे 'जैन संस्कृति' कहलाया। सिद्ध है कि अहिंसादिक धर्म हैं और उनके मूल मे 'अपरिग्रह' रूपी मूल संस्कृति है-जंमे मूल के अभाव मे शाखाओं की सम्भावना नहीं वैसे ही परिग्रह के अभाव में हिसादिक शाखाओं की भी सम्भावना नही । फलतः हमे अपरिग्रह को मूल सस्कृति मानकर चलना चाहिए।
।
हिंसा के लक्षण में अचार्यों ने दो अनिवार्यताओं का उल्लेख किया है और वे अनिवार्यतायें है-प्रमतयोग और प्राण-व्यपरोपण । इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि जहां प्रसाद का योग है और प्राणो का व्यपरोपण है यहाँ हिंसा है। आचार्यों ने एक बात यह भी खुलासा की है कि यदि प्रमाद का योग है और दूसरे के प्राणों का वियोग नही भी है तो वहा भी हिंसा है क्योंकि उनके मत मे प्राणों में द्रव्य और भाव दोनो प्रकार के प्राणो के साथ स्व और पर दोनो के प्राणो का ग्रहण भी निहित है। फलतः जहाँ पर के प्राणों का घात नहीं होता वहा भी प्रमाद स्व-प्राणों का घात तो करता ही है। उक्त प्रसग पर यदि गहराई से मनन करें तो ऐसा मानने में कोई हानि नही होनी चाहिए कि- परस्पर में विरोध रूप हिंसा और अहिंसा दोनों का अस्तित्व प्रमाद व प्राणी के अस्तित्व तक, उनके हनन और रक्षण के विकल्पों तक सीमित है - निर्विकल्प अवस्था में नही जबकि बीतरागता अपरिग्रहत्व आत्मा में सदाकाल रहने वाला उसका स्वभाव है ।
।
प्रवचन सार मे उपयोग के भेदो का वर्णन है और कहा गया है- 'अथायमुपयोगो द्या विशिष्यते शुद्धाशुद्धस्वेन तत्र शुद्धो निरुपरागः अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धि सक्लेश रूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभsere ।' 'समस्तभूतग्रामानुकम्पायरये च प्रवृते शुम उपयोगः । - प्र० व० टी० ६३, ६५ ।