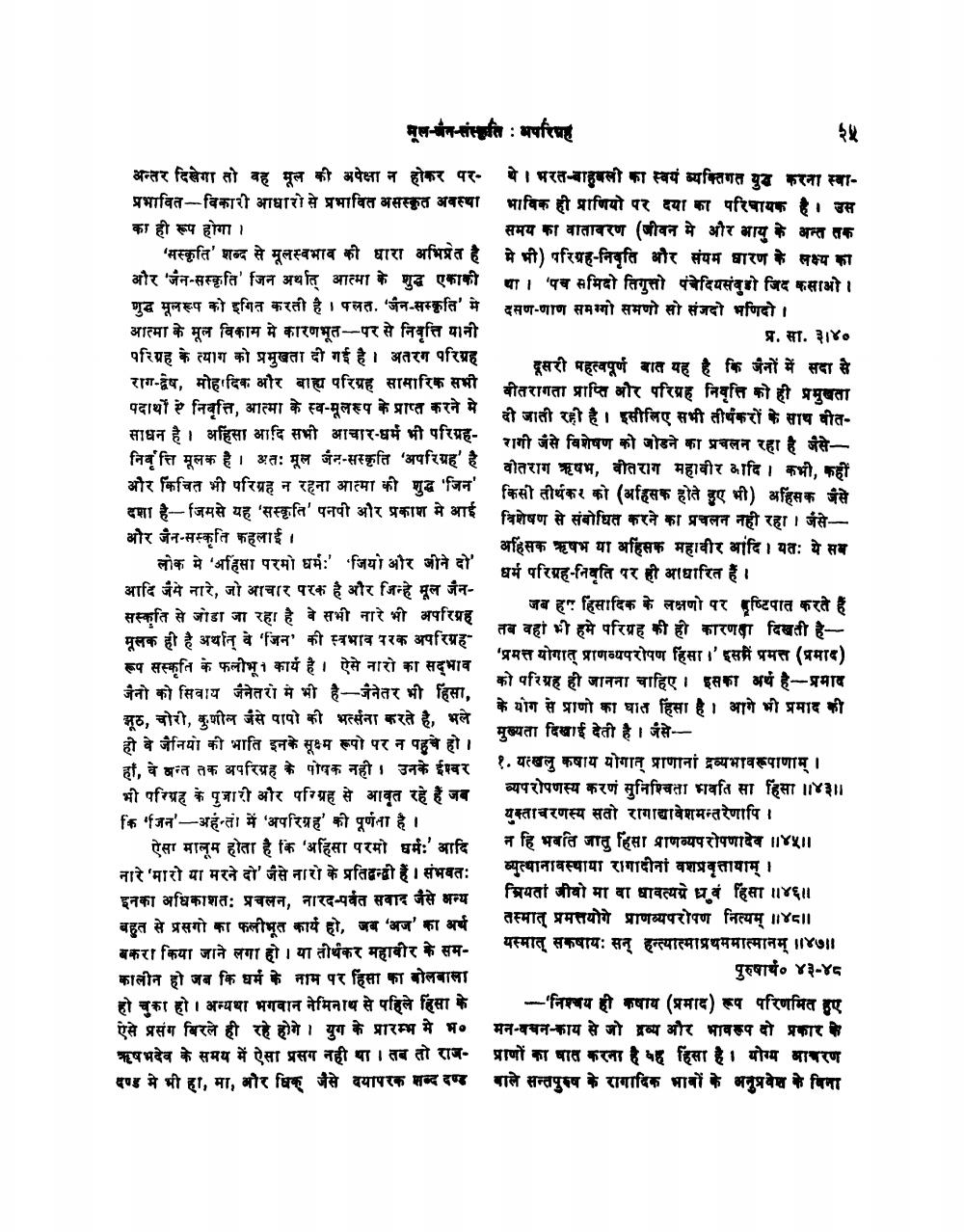________________
मूल-जैन-संसाति : अपरिह
अन्तर दिखेगा तो वह मूल की अपेक्षा न होकर पर. थे। भरत-बाहुबली का स्वयं व्यक्तिगत युद्ध करना स्वाप्रभावित-विकारी आधारो से प्रभावित असस्कृत अवस्था भाविक ही प्राणियो पर दया का परिचायक है। उस का ही रूप होगा।
समय का वातावरण (जीवन मे और आयु के अन्त तक ___मस्कृति' शब्द से मूलस्वभाव की धारा अभिप्रेत है मे भी) परिग्रह-निवृति और संयम धारण के लक्ष्य का और 'जन-सस्कृति' जिन अर्थात् आत्मा के शुद्ध एकाकी था। 'पच समिदो तिगुत्तो पंचेदियसंवुडो जिद कसाओ। शुद्ध मूलरूप को इगित करती है । पलत. 'जैन-सस्कृति' मे दसण-णाण समग्गो समणो सो संजदो भणिदो। आत्मा के मूल विकाम मे कारणभूत-पर से निवृत्ति यानी
प्र. सा. ३४० परिग्रह के त्याग को प्रमुखता दी गई है। अतरग परिग्रह
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनों में सदा से राग-द्वेष, मोहादिक और बाह्य परिग्रह सामारिक सभी
वीतरागता प्राप्ति और परिग्रह निवृत्ति को ही प्रमुखता पदार्थों से निवृत्ति, आत्मा के स्व-मूलरूप के प्राप्त करने मे हर
दी जाती रही है। इसीलिए सभी तीर्थंकरों के साथ वीतसाधन है। अहिंसा आदि सभी आचार-धर्म भी परिग्रह
रागी जैसे विशेषण को जोड़ने का प्रचलन रहा है जैसेनिर्वृत्ति मूलक है। अत: मूल जन-सस्कृति 'अपरिग्रह' है
वीतराग ऋषभ, वीतराग महावीर आदि। कभी, कहीं और किंचित भी परिग्रह न रहना आत्मा की शुद्ध "जिन' किसी तीर्थकर को (अहिसक होते हुए भी) अहिंसक जैसे दशा है-जिमसे यह 'सस्कृति' पनपी और प्रकाश में आई
विशेषण से संबोधित करने का प्रचलन नही रहा । जैसेऔर जन-सस्कृति कहलाई।
अहिंसक ऋषभ या अहिंसक महावीर आदि। यत: ये सब लोक मे 'अहिंसा परमो धर्मः' 'जियो और जीने दो'
धर्म परिग्रह-निवृति पर ही आधारित हैं। आदि जैसे नारे, जो आचार परक है और जिन्हे मूल जैन
जब हा हिंसादिक के लक्षणो पर दृष्टिपात करते हैं सस्कृति से जोडा जा रहा है वे सभी नारे भी अपरिग्रह
तब वहां भी हमे परिग्रह की ही कारणवा दिखती हैमूलक ही है अर्थात् वे 'जिन' की स्वभाव परक अपरिग्रह
'प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा।' इसमें प्रमत्त (प्रमाव) रूप सस्कृति के फलीभू। कार्य है। ऐसे नारो का सद्भाव
को परिग्रह ही जानना चाहिए। इसका अर्थ है-प्रमाव जैनो को सिवाय जनेतरो मे भी है-जनेतर भी हिंसा,
के योग से प्राणो का घात हिंसा है। आगे भी प्रमाद की झूठ, चोरी, कुशील जैसे पापो की भर्त्सना करते है, भले
मुख्यता दिखाई देती है। जैसे-- हो वे जैनियो की भाति इनके सूक्ष्म रूपो पर न पहुचे हो। हाँ, वे अन्त तक अपरिग्रह के पोषक नही। उनके ईश्वर
१. यत्खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् । भी परिग्रह के पुजारी और परिग्रह से आवृत रहे हैं जब
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४॥ कि 'जिन'-अहंतो में 'अपरिग्रह' को पूर्णता है।
युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । ऐसा मालूम होता है कि 'अहिंसा परमो धर्मः' आदि
न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥४५।। नारे 'मारो या मरने दो' जैसे नारो के प्रतिद्वन्द्वी हैं । संभवतः
व्युत्थानावस्थाया रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् । इनका अधिकाशत: प्रचलन, नारद-पर्वत सवाद जैसे अन्य
प्रियतां जीवो मा वा धावत्यने ध्रव हिंसा ॥४६॥ बहुत से प्रसगो का फलीभूत कार्य हो, जब 'अज' का अर्थ
तस्मात् प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम् ॥४८॥ बकरा किया जाने लगा हो । या तीर्थकर महावीर के सम
यस्मात् सकषायः सन् हन्त्यात्माप्रथममात्मानम् ।।४७॥ कालीन हो जब कि धर्म के नाम पर हिंसा का बोलबाला
पुरुषार्थ० ४३-४८ हो चुका हो । अन्यथा भगवान नेमिनाथ से पहिले हिंसा के -निश्चय ही कषाय (प्रमाद) रूप परिणमित हुए ऐसे प्रसंग बिरले ही रहे होगे। युग के प्रारम्भ मे भ. मन-वचन-काय से जो द्रव्य और भावरूप दो प्रकार के ऋषभदेव के समय में ऐसा प्रसग नही था । तब तो राज- प्राणों का बात करना है वह हिंसा है। योग्य बाबरण दण्ड मे भी हा, मा, और धिक् जैसे बयापरक शब्द दम बाले सन्तपुरुष के रागादिक भावों के अनुप्रवेश के बिना