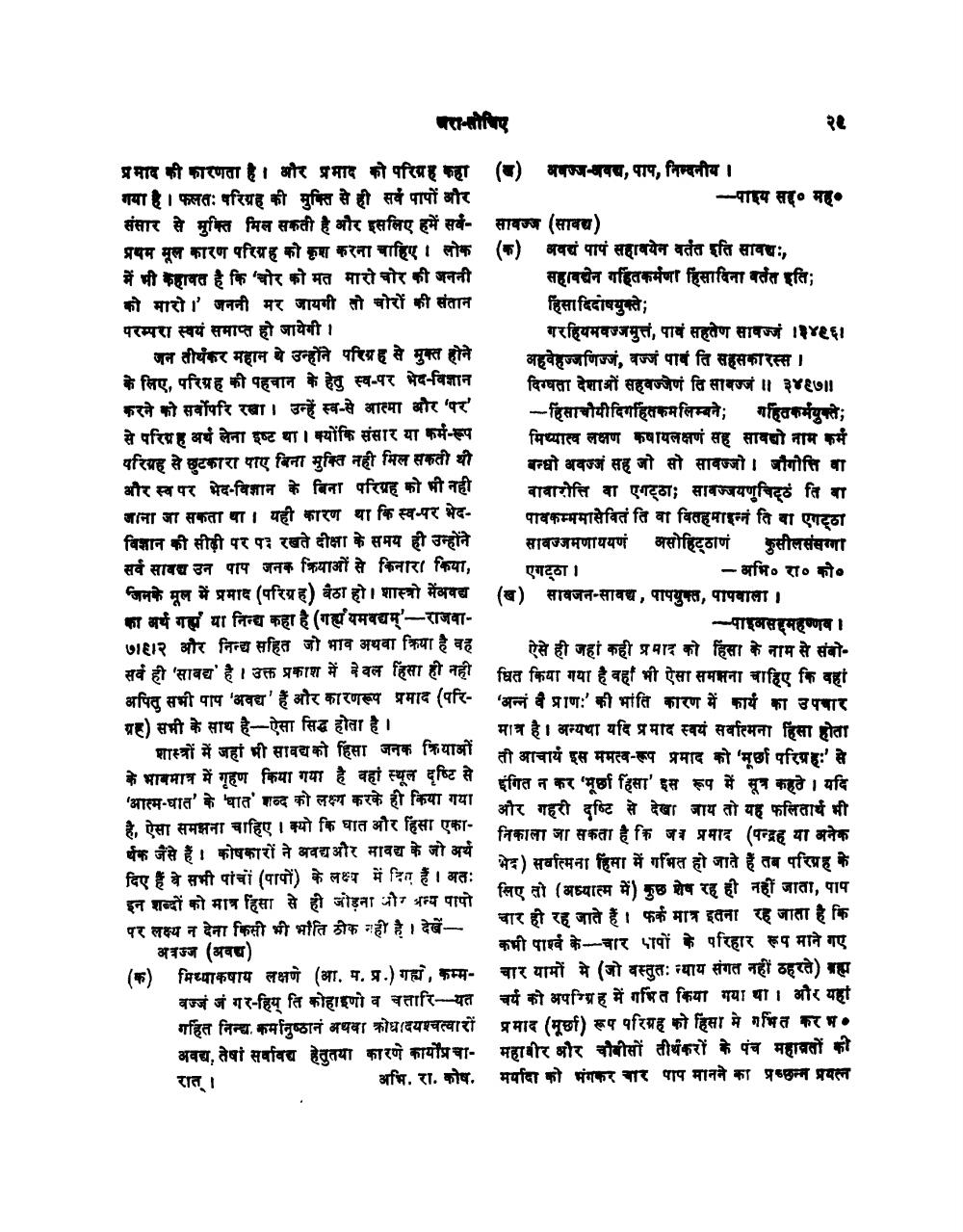________________
परा-सोधिए
प्रमाद की कारणता है। और प्रमाद को परिग्रह कहा (ब) अपज्ज-बवब, पाप, निन्दनीय । गया है। फलतः परिग्रह की मुक्ति से ही सर्व पापों और
-पाइय सह मह. संसार से मुक्ति मिल सकती है और इसलिए हमें सर्व- सावज्ज (सावद्य) प्रथम मूल कारण परिग्रह को कृश करना चाहिए। लोक (क) अवचं पापं सहावयेन वर्तत इति सावधः, में भी कहावत है कि 'चोर को मत मारो चोर की जननी सहावोन गहितकर्मणा हिंसाविना वर्तत इति; को मारो।' जननी मर जायगी तो चोरों की संतान हिंसादिदोषयुक्त; परम्परा स्वयं समाप्त हो जायेगी।
गरहियमवज्जमुत्तं, पावं सहतेण सावजं Irel जन तीर्थंकर महान थे उन्होंने परिग्रह से मुक्त होने
अहवेहज्जणिज्जं, वज्ज पावं ति सहसकारस्स । के लिए, परिग्रह की पहचान के हेतु स्व-पर भेद-विज्ञान
दिग्षता देशाओं सहवज्जेणं ति सावज्जं ॥ ३४१७॥ करने को सर्वोपरि रखा। उन्हें स्व-से आत्मा और 'पर'
-हिंसाचोयीदिहितकमलिम्बने; गहितकर्मयुक्त से परिग्रह अर्थ लेना इष्ट था। क्योंकि संसार या कर्म-रूप
मिथ्यात्व लक्षण कषायलक्षणं सह सावधो नाम कर्म परिग्रह से छुटकारा पाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती थी
बन्धो अवज्ज सह जो सो सावज्जो। जौगोत्ति वा और स्व पर भेद-विज्ञान के बिना परिग्रह को भी नहीं
बावारोत्ति वा एगट्ठा; सावज्जयणुचिट्ठ तिवा जाना जा सकता था। यही कारण था कि स्व-पर भेद
पावकम्ममासेवितं ति वा वितहमाइन्नं ति वा एगट्ठा विज्ञान की सीढ़ी पर पर रखते दीक्षा के समय ही उन्होंने सावज्जमणाययणं असोहिट्ठाणं कुसीलसंसग्गा सर्व सावध उन पाप जनक क्रियाओं से किनारा किया,
एगट्ठा।
-अभि० रा.को. जिनके मूल में प्रमाद (परिग्रह) बैठा हो। शास्त्रो मेंअवद्य (ख) सावजन-सावध, पापयुक्त, पापवाला। का अर्थ गर्दा या निन्द्य कहा है (गा यमवद्यम्'-राजवा
पाइनसहमहण्णव। पार और निन्द्य सहित जो भाव अथवा क्रिया है वह ऐसे ही जहां कही प्रमाद को हिंसा के नाम से संबोसर्व ही 'सावद्य' है। उक्त प्रकाश में वेवल हिसा ही नहीं धित किया गया है वहाँ भी ऐसा समझना चाहिए कि वहां अपितु सभी पाप 'अवद्य' हैं और कारणरूप प्रमाद (परि- 'अन्नं वै प्राणः' की भांति कारण में कार्य का उपचार ग्रह) सभी के साथ है-ऐसा सिद्ध होता है।
मात्र है। अन्यथा यदि प्रमाद स्वयं सर्वात्मना हिंसा होता शास्त्रों में जहां भी सावध को हिंसा जनक क्रियाओं
ती आचार्य इस ममत्व-रूप प्रमाद को 'मूर्छ परिग्रहः' से के भावमात्र में ग्रहण किया गया है वहां स्थूल दृष्टि से
इंगित न कर 'मूळ हिंसा' इस रूप में सूत्र कहते । यदि 'आत्म-घात' के 'घात' शब्द को लक्ष्य करके ही किया गया
और गहरी दृष्टि से देखा जाय तो यह फलितार्थ भी है, ऐसा समझना चाहिए । क्यो कि घात और हिंसा एका
निकाला जा सकता है कि जब प्रमाद (पन्द्रह या अनेक र्थक जैसे हैं। कोषकारों ने अवद्य और मावद्य के जो अर्थ
भेद) सर्वात्मना हिंसा में गभित हो जाते हैं तब परिग्रह के दिए हैं वे सभी पांचों (पापों) के लक्ष्य में दिया हैं । अतः इन शब्दों को मात्र हिंसा से ही जोड़ना और अन्य पापो
लिए तो (अध्यात्म में कुछ शेष रह ही नहीं जाता, पाप पर लक्ष्य न देना किसी भी भौति ठीक नहीं है। देखें- चार हा रह जात
चार ही रह जाते हैं। फर्क मात्र इतना रह जाता है कि अवज्ज (अवध)
कभी पार्श्व के-चार पापों के परिहार रूप माने गए (क) मिथ्याकषाय लक्षणे (आ. म.प्र.) गा, कम्म- चार यामों मे (जो वस्तुत: न्याय संगत नहीं ठहरते) ब्रह्म
वज्जं जंगर-हिय् ति कोहाइणो व चतारियत चर्य को अपरिग्रह में गमित किया गया था। और यहां गहित निन्द्य कर्मानुष्ठानं अथवा क्रोधादयश्चत्वारों प्रमाद (मूळ) रूप परिग्रह को हिंसा मे गमित करम. अवद्य, तेषां सर्वावध हेतुतया कारणे कार्योप्रचा- महावीर और चौबीसों तीर्थंकरों के पंच महावतों की
अभि. रा. कोष, मर्यादा को मंगकर चार पाप मानने का प्रच्छन्न प्रयत्न
रात् ।