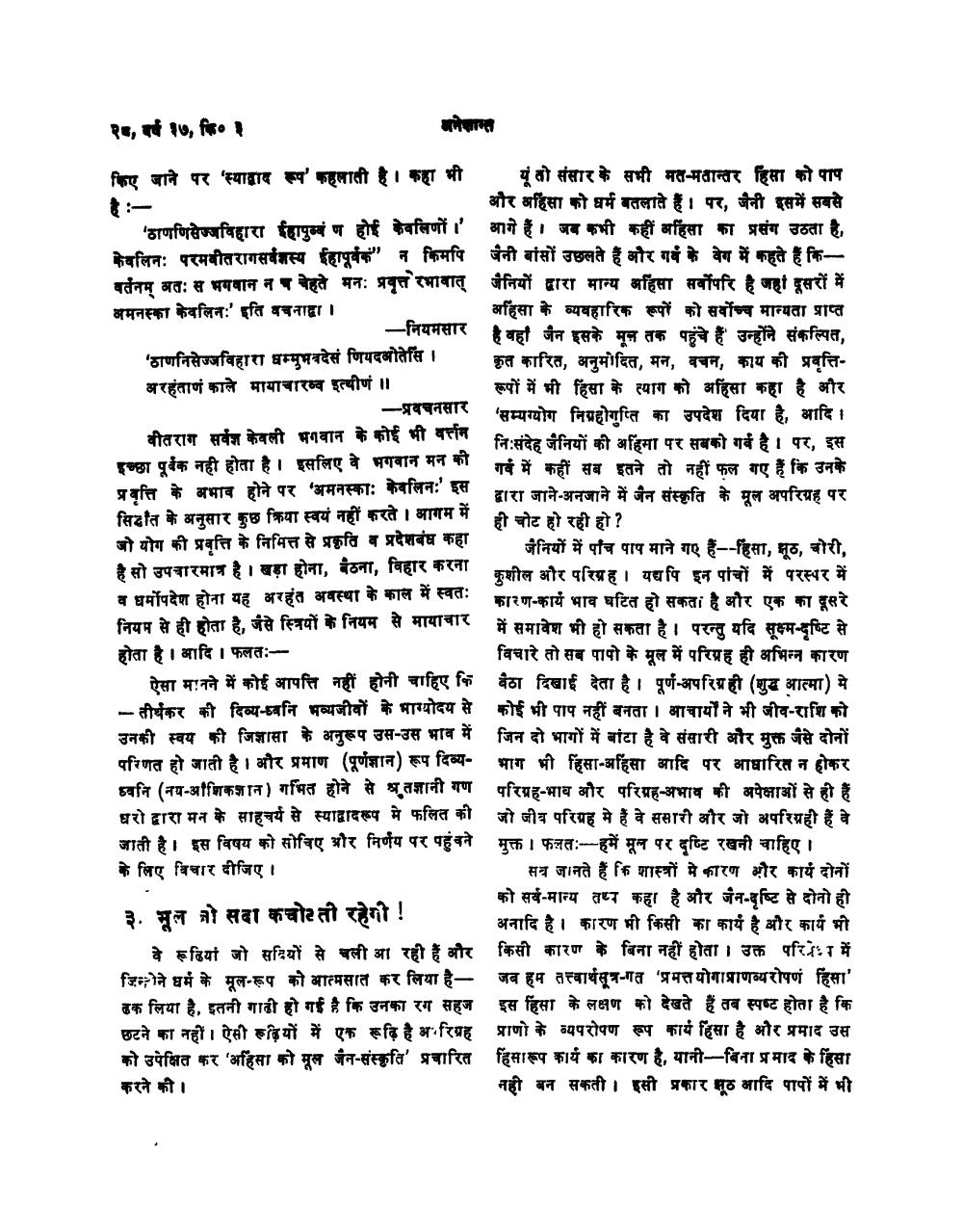________________
२० वर्ष ३७ कि.. किए जाने पर 'स्थाद्वाद रूप' कहलाती है। कहा भी यूं तो संसार के सभी मत-मतान्तर हिंसा को पाप
और अहिंसा को धर्म बतलाते हैं। पर, जैनी इसमें सबसे 'ठाणणिसेज्जविहारा ईहापुवं ण होई केवलिणों।' आगे हैं। जब कभी कहीं अहिंसा का प्रसंग उठता है, केवलिनः परमवीतरागसर्वशस्य ईहापूर्वक" न किमपि जैनी बांसों उछलते हैं और गर्व के वेग में कहते हैं किवर्तनम् अतः स भगवान न पहते मनः प्रवृत्त रभावात् जैनियों द्वारा मान्य अहिंसा सर्वोपरि है जहां दूसरों में अमनस्का केवलिनः' इति वचनाद्वा।
अहिंसा के व्यवहारिक रूपों को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त
-नियमसार है वहाँ जैन इसके मूल तक पहुंचे हैं उन्होंने संकल्पित, 'ठाणनिसेज्जविहारा धम्मुभवदेस णियदबोतेसि ।
कृत कारित, अनुमोदित, मन, वचन, काय की प्रवृत्तिअरहताणं काले मायाचारव्व इत्थीणं ॥
रूपों में भी हिंसा के त्याग को अहिंसा कहा है और -प्रवचनसार
'सम्यग्योग निग्रहोगुप्ति का उपदेश दिया है, आदि। वीतराग सर्वज्ञ केवली भगवान के कोई भी वर्तन
नि:संदेह जैनियों की अहिंमा पर सबको गर्व है। पर, इस इच्छा पूर्वक नही होता है। इसलिए वे भगवान मन की
गर्व में कहीं सब इतने तो नहीं फल गए हैं कि उनके प्रवृत्ति के अभाव होने पर 'अमनस्काः केवलिनः' इस
द्वारा जाने-अनजाने में जैन संस्कृति के मूल अपरिग्रह पर सिद्धांत के अनुसार कुछ क्रिया स्वयं नहीं करते । आगम में
ही चोट हो रही हो? जो योग की प्रवृत्ति के निमित्त से प्रकृति व प्रदेशबंध कहा
जैनियों में पांच पाप माने गए हैं--हिंसा, झूठ, चोरी, है सो उपचारमात्र है। खड़ा होना, बैठना, विहार करना
कुशील और परिग्रह । यद्यपि इन पांचों में परस्पर में व धर्मोपदेश होना यह अरहंत अवस्था के काल में स्वतः
कारण-कार्य भाव घटित हो सकता है और एक का दूसरे नियम से ही होता है, जैसे स्त्रियों के नियम से मायाचार
में समावेश भी हो सकता है। परन्तु यदि सूक्ष्म-दृष्टि से होता है । आदि । फलतः
विचारे तो सब पापो के मूल में परिग्रह ही अभिन्न कारण ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बैठा दिखाई देता है। पूर्ण-अपरिग्रही (शुद्ध आत्मा) मे -तीर्थकर की दिव्य-ध्वनि भव्यजीवों के भाग्योदय से कोई भी पाप नहीं बनता। आचार्यों ने भी जीव-राशि को उनकी स्वय की जिज्ञासा के अनुरूप उस-उस भाव में जिन दो भागों में बांटा है वे संसारी और मुक्त जैसे दोनों परिणत हो जाती है। और प्रमाण (पूर्णज्ञान) रूप दिव्य- भाग भी हिंसा-अहिंसा आदि पर आधारित न होकर ध्वनि (नय-आशिकज्ञान) गभित होने से अतज्ञानी गण परिग्रह-भाव और परिग्रह-अभाव की अपेक्षाओं से ही हैं घरो द्वारा मन के साहचर्य से स्याद्वादरूप मे फलित की जो जीव परिग्रह मे हैं वे ससारी और जो अपरिग्रही हैं वे जाती है। इस विषय को सोचिए और निर्णय पर पहुंचने मुक्त । फलतः हमें मूल पर दृष्टि रखनी चाहिए। के लिए विचार दीजिए।
सब जानते हैं कि शास्त्रों मे कारण और कार्य दोनों
को सर्व-मान्य तय कहा है और जैन-दृष्टि से दोनो ही ३. मूल जो सदा कचोटती रहेगी!
अनादि है। कारण भी किसी का कार्य है और कार्य भी कलियां जो सदियों से चली आ रही हैं और किसी कारण के बिना नहीं होता। उक्त परिम में जिन्नोने धर्म के मूल-रूप को आत्मसात कर लिया है- जब हम तत्त्वार्थसूत्र-गत 'प्रमत्तयोगाप्राणव्यरोपणं हिंसा' ढक लिया है, इतनी गाढी हो गई है कि उनका रग सहज इस हिंसा के लक्षण को देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि छटने का नहीं। ऐसी रूढ़ियों में एक रूढ़ि है अरिग्रह प्राणो के व्यपरोपण रूप कार्य हिंसा है और प्रमाद उस को उपेक्षित कर 'अहिंसा को मूल जैन-संस्कृति' प्रचारित हिंसारूप कार्य का कारण है, यानी-बिना प्रमाद के हिंसा करने की।
नही बन सकती। इसी प्रकार मूठ आदि पापों में भी