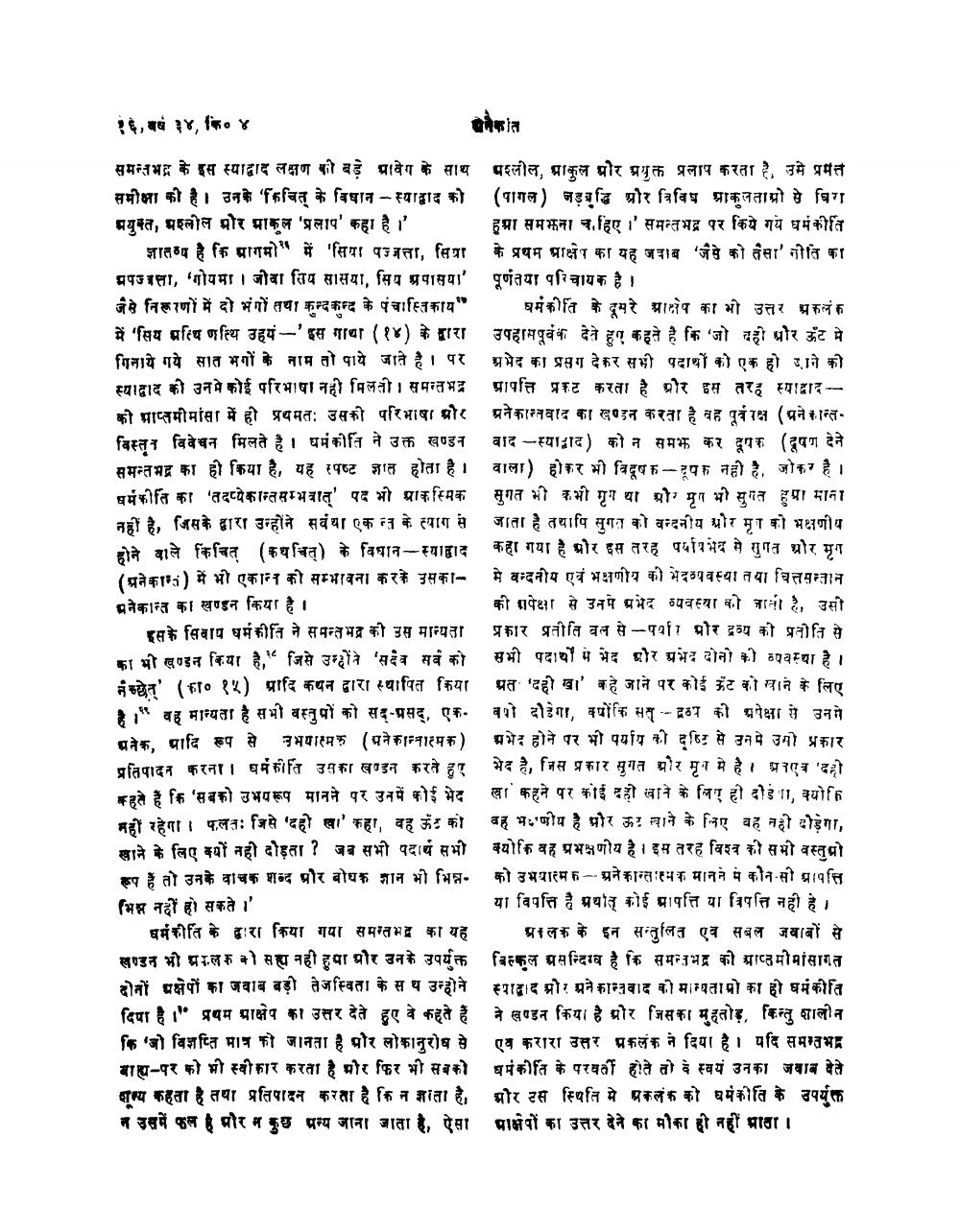________________
१६ वर्ष ३४, कि० ४
समन्तभद्र के इस स्याद्वाद लक्षण को बड़े प्रावेग के साथ पश्लील, प्राकुल पोर प्रयुक्त प्रलाप करता है, उसे प्रमत्त समीक्षा की है। उनके किचित् के विधान - स्याद्वाद को (पागल) नड़बद्धि और विविध प्राकुलतानो से घिग प्रयुक्त, मश्लील पोर माकुल 'प्रलाप' कहा है।' हुमा समझना चाहिए।' समन्तभद्र पर किये गये धर्म कीति
ज्ञातव्य है कि मागमो" में "सिया पज्जत्ता, सिया के प्रथम प्राक्षेप का यह जवाब 'जैसे को तैसा' नीति का अपनत्ता, 'गोयमा । जीवा सिय सासया, सिय प्रपासया' पूर्णतया परिचायक है। जैसे निरूरणों में दो भंगों तथा कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय" धर्मकीति के दूसरे प्राक्षेप का भी उत्तर प्रकलंक में सिय प्रत्थि पत्थि उहयं-' इस गाथा (१४) के द्वारा उपहासपूर्वक देते हुए कहते है कि 'जो वही और ऊँट मे गिनाये गये सात भगों के नाम तो पाये जाते है । पर अभेद का प्रसग देकर सभी पदार्थों को एक हो जाने को स्याद्वाद को उनमे कोई परिभाषा नहीं मिलती। समन्तभद्र प्रापत्ति प्रकट करता है और इस तरह स्याद्वाद -- को प्राप्तमीमांसा में ही प्रथमत: उसको परिभाषा और अनेकान्लवाद का खण्डन करता है वह पूर्व पक्ष (प्रने कान्तविस्तन विवेचन मिलते है। धर्मकीति ने उक्त खण्डन वाद -स्याद्वाद) को न समझ कर दूपक (दूषण देने समन्तभद्र का ही किया है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है। वाला) होकर भी विदूषक-दूपक नही है, जोकर है । धर्मकीति का 'तदप्येकान्तसम्भवात्' पद भी प्राकस्मिक सुगत भी कभी गृग था और मृग भी सुगत हुप्रा माना नहीं है, जिसके द्वारा उन्होंने सर्वथा एकल के त्याग से जाता है तथापि सुगत को वन्दनीय और मृा को भक्षणीय होने वाले किचित् (कथचित्) के विधान-स्याद्वाद कहा गया है और इस तरह पर्याप भव मे सुगत प्रौर मृग (अनेकार) में भी एकान की सम्भावना करके उसका- मे बन्दनीय एवं भक्षणीय को भेदव्यवस्था तया चित्तसम्मान अनेकान्त का खण्डन किया है।
की पेक्षा से उनमे प्रभेद व्यवस्था को जाती है, उसी इसके सिवाय धर्मकीति ने समन्तभद्र की उस मान्यता प्रकार प्रतीति बल से -पर्यार और द्रव्य को प्रतीति से का भी खण्डन किया है, जिसे उन्होंने 'सदेव सर्व को सभी पदार्थों में भेद और प्रभेद दोनो की व्यवस्था है। नन्छेत' (का० १५) प्रादि कथन द्वारा स्थापित किया प्रत दही खा' कहे जाने पर कोई ऊँट को खाने के लिए है। वह मान्यता है सभी वस्तुपों को सद्-प्रसद्, एक. वो दौडेगा, क्योंकि सत् -- द्रव्य की अपेक्षा से उनमें प्रतेक प्रादि रूप से भयात्मक (पने कानात्मक) प्रभेद होने पर भी पर्याय को दृष्टि से उनमे उमो प्रकार प्रतिपादन करना। धर्मकीति उसका खण्डन करते हुए भेद है, जिस प्रकार सुगत पौर मृग में है। प्रतएव 'दी कहते हैं कि 'सबको उभय रूप मानने पर उनमें कोई भेद खा कहने पर कोई दही खाने के लिए ही दोगा क्योकि महीं रहेगा। फलतः जिसे 'दही खा' कहा, वह ऊंट को वह भणीय है और ऊरवाने के लिए वह नही दौडगा, खाने के लिए क्यों नही दौड़ता? जब सभी पदार्थ सभी क्योकि वह प्रभक्षणीय है। इस तरह विश्व की सभी वस्तम्रो रूप हैं तो उनके वाचक शब्द और बोधक ज्ञान भी भिन्न- को उभयात्म :-- अनेकान्तात्मक मानने में कौन-सी प्रापत्ति भिन्न नहीं हो सकते।'
या विपत्ति है अर्थात् कोई प्रापत्ति या विपत्ति नही है। धर्मकीर्ति के द्वारा किया गया समन्तभद्र का यह मालक के इन सन्तुलित एवं सबल जवाबों से खण्डन भी प्रा.लक को सह्य नही हुपा और उनके उपर्युक्त बिल्कुल प्रसन्दिग्व है कि समन्तभद्र को प्राप्त मीमांसागत दोनों प्रक्षेपों का जवाब बड़ी तेजस्विता के स थ उन्होंने स्माद्वाद और प्रने कान्तवाद की मान्यतापो का ही घमंकीति दिया है। प्रथम प्राक्षेप का उत्सर देते हुए वे कहते हैं ने खण्डन किया है और जिसका मुहतोड़, किन्तु शालीन कि 'जो विज्ञप्ति मात्र को जानता है और लोकानुरोध से एक करारा उसर प्रकलंक ने दिया है। यदि समन्तभद्र बाध-पर को भी स्वीकार करता है और फिर भी सबको धमकीति के परवर्ती होते तो वे स्वयं उनका जवाब देते शुन्य कहता है तथा प्रतिपादन करता है कि न ज्ञाता है, और उस स्थिति में प्रकलंक को धर्मकीति के उपर्युक्त न उसमें फल मोर म कुछ अन्य जाना जाता है, ऐसा पापों का उत्तर देने का मौका ही नहीं पाता ।