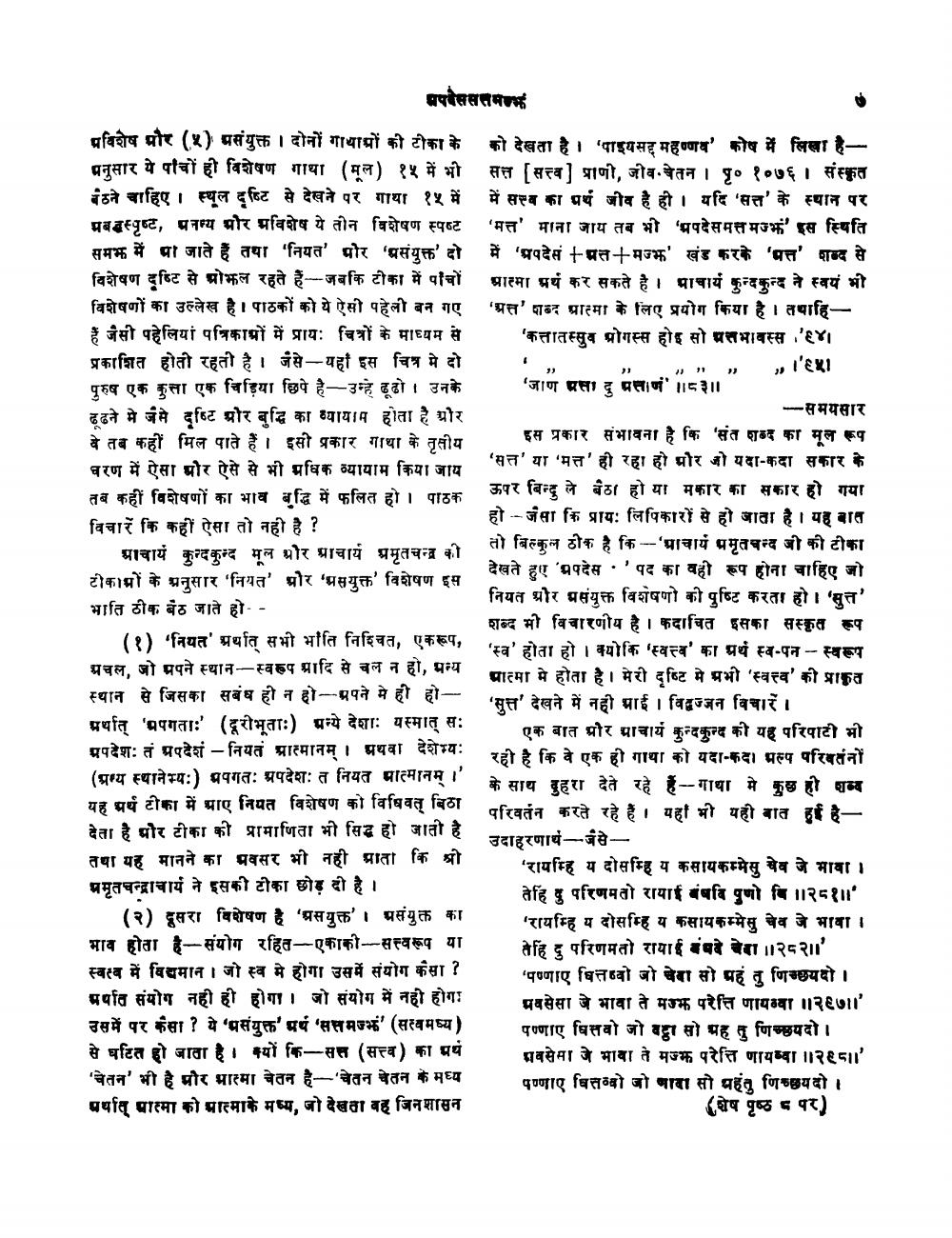________________
प्रवेस सलम
प्रविशेष धौर (५) संयुक्त दोनों गाथाओं की टीका के अनुसार ये पाँचों ही विशेषण गाथा (मूल) १५ में भी बंठने चाहिए। स्थूल दृष्टि से देखने पर गाथा १५ में प्रबद्धस्पृष्ट, अनम्य भोर भविशेष ये तीन विशेषण स्पष्ट समझ में पा जाते हैं तथा 'नियत' मोर 'प्रसंयुक्त' दो विशेषण दृष्टि से श्रोत रहते हैं जबकि टीका में पाँचों विशेषणों का उल्लेख है। पाठकों को ये ऐसी पहेली बन गए हैं जैसी पहेलियां पत्रिकायों में प्रायः चित्रों के माध्यम से प्रकाशित होती रहती है। जैसे यहाँ इस चित्र मे दो पुरुष एक कुला एक चिड़िया छिपे है - उन्हें ढूढो । उनके ढूंढने मे मे दृष्टि घोर बुद्धि का व्यायाम होता है और वे तब कहीं मिल पाते हैं । इसी प्रकार गाथा के तृतीय चरण में ऐसा धौर ऐसे से भी अधिक व्यायाम किया जाय तब कहीं विशेषणों का भाव बुद्धि में फलित हो । पाठक विचारों कि कहीं ऐसा तो नही है ?
प्राचार्य कुन्दकुन्द मूल और प्राचार्य प्रमृतचन्द्र की टीकाओं के अनुसार 'नियत' और 'प्रसयुक्त' विशेषण इस भाति ठीक बैठ जाते हो -
(१) 'नियत' अर्थात् सभी भाँति निश्चित, एकरूप, अचल, जो अपने स्थान - स्वरूप प्रादि से चल न हो, भन्य स्थान से जिसका संबंध ही न हो - प्रपने मे ही होप्रर्थात् 'भपगता:' ( दूरीभूताः ) धन्ये देशाः यस्मात् सः पदेशः तं देशं नियतं म्रात्मानम् अथवा देवेभ्यः ( श्रभ्य स्थानेभ्यः) प्रपगतः अपदेशः त नियत मात्मानम् ।' यह अर्थ टीका में धाए नियत विशेषण को विधिवत् बिठा देता है घोर टीका की प्रामाणिता भी सिद्ध हो जाती है तथा यह मानने का अवसर भी नही प्राता कि श्री प्रमृतचन्द्राचार्य ने इसकी टीका छोड़ दी है।
—
(२) दुसरा विशेषण है 'प्रसयुक्त' । प्रसंयुक्त का भाव होता है - संयोग रहित - एकाकी - सत्वरूप या स्वत्व में विद्यमान जो स्व मे होगा उसमें संयोग कैसा ? अर्थात संयोग नहीं ही होगा जो संयोग में नहीं होगा उसमें पर कैसा ? ये 'संयुक्त' पर्थ 'सत्तमम् (सत्यमध्य) से घटित हो जाता है। क्योंकि -सत ( सत्त्व) का अर्थ 'चेतन' भी है और मारमा चेतन है-चेतन चेतन के मध्य अर्थात् म्रात्मा को म्रात्माके मध्य, जो देखता वह जिनशासन
को देखता है। 'पाइयसद महण्णव' कोष में लिखा हैसत [ सत्व] प्राणी, जीव-चेतन पृ० १०७६ संस्कृत में सत्य का पर्थ जीव है ही। यदि 'सल' के स्थान पर 'मत्त' माना जाय तब भी 'अपदेसमसमभं इस स्थिति में 'प्रपदे + प्रत + मज्भ' खंड करके 'मत्त' शब्द से आत्मा अर्थ कर सकते है । प्राचार्य कुन्दकुन्द ने स्वयं भी 'स' शब्दात्मा के लिए प्रयोग किया है। तथाहि'कत्तातस्तुव भोगस्स होइ सो प्रभावस्स २४|
,, l'εx!
4
33
'जाण प्रसादु
----
"
.
"3
115311
-समयसार
3
इस प्रकार संभावना है कि 'संत शब्द का मूल रूप 'सत्त' या 'मत्त' ही रहा हो भौर जो यदा-कदा सकार के ऊपर बिन्दु ले बैठा हो या मकार का सकार हो गया हो जैसा कि प्रायः लिपिकारों से हो जाता है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि प्राचार्य प्रमृतन्य जी की टीका देखते हुए 'अपदेस पद का यही रूप होना चाहिए जो नियत और संयुक्त विशेषणों की पुष्टि करता हो। 'सुत्त' शब्द मी विचारणीय है । कदाचित इसका संस्कृत रूप 'स्व' होता हो। क्योंकि 'स्वत्व' का अर्थ स्वपन स्वरूप प्रात्मा मे होता है । मेरी दृष्टि मे प्रभी 'स्वत्त्व' की प्राकृत 'सुत' देखने में नहीं भाई । विद्वज्जन विचारें ।
एक बात और प्राचार्य कुन्दकुन्द की यह परिपाटी भी रही है कि वे एक ही गाथा को यदा-कदा भल्प परिवर्तनों के साथ दुहरा देते रहे हैं-गाथा मे कुछ ही शब्द परिवर्तन करते रहे है। यहाँ भी यही बात हुई हैउदाहरणार्थ जैसे
"
'यहि व दोसवि कसायकम्मे चैव जे माया । तेहि परिणमतो शयाई बंधदि पुणो वि ।। २६१ ।। * 3 'रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चैव जे भावा । तेहि परिणमतो शयाई बंदे देवा ।। २६२ ।' 'पण्णाए बिल जो बेवा सो यहं तु णिडयो। प्रवसेसा जे भावा ते मज्झ परेति णायग्वा ॥ २६७॥ पाए घितवो जो बहुत सो मह तु पिच्छयदो ।
दु
बसेमा जे भाषा ते मम परेति णावया ॥२९८॥ पण्णाए घिसन्बो जो जावा सो महंतु णिच्छय दो । (शेष पृष्ठ ८ पर)