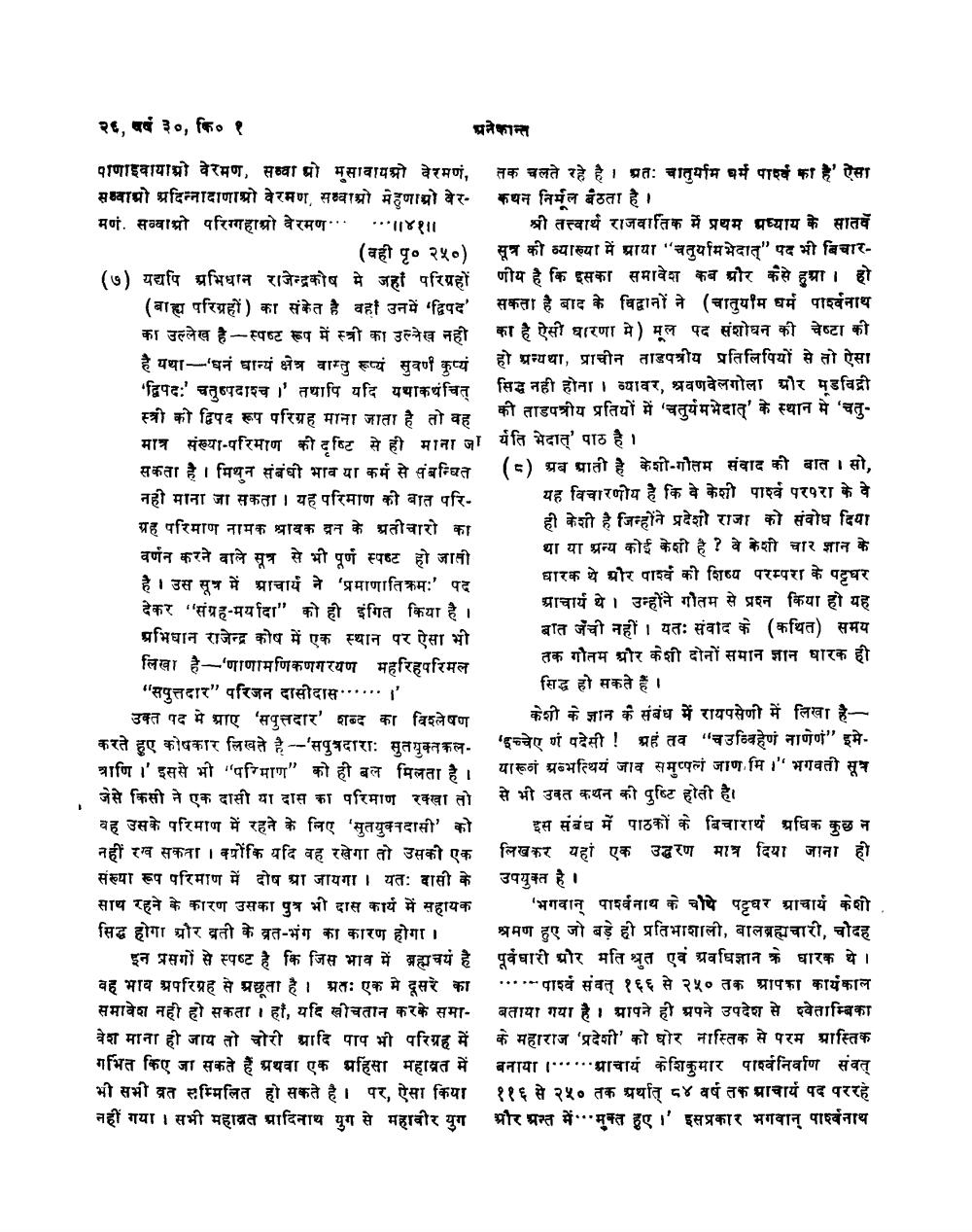________________
२३०० १
पाणावायाश्रो वेरमण, सब्वा प्रो मुसावायनो वेरमणं, सवा दिन्नादाणाश्रो वेरमण, सध्वाश्रो मेहुणाम्रो वेरमणं सन्याची परिगहाथो वेरमण 1118811
( वही पृ० २५० ) मे जहाँ परिग्रहों
( ७ ) यद्यपि अभिधान राजेन्द्रकोष
( बाह्य परिग्रहों का संकेत है वहाँ उनमें 'द्विपद' का उल्लेख है - स्पष्ट रूप में स्त्री का उल्लेख नही है यथा - 'धनं धान्यं क्षेत्र वास्तु रूप्यं सुवर्ण कुप्यं 'द्विपद:' चतुष्पदाश्च तथापि यदि यथाकथंचित् स्त्री को द्विपद रूप परिग्रह माना जाता है तो वह मात्र संख्या - परिमाण की दृष्टि से ही माना जा सकता है। मिथुन संबंधी भाव या कर्म से संबन्धित नही माना जा सकता। यह परिमाण की बात परिग्रह परिमाण नामक श्रावक व्रत के श्रतीचारो का वर्णन करने वाले सूत्र से भी पूर्ण स्पष्ट हो जाती है उस सूत्र में प्राचार्य ने 'प्रमाणातिक्रमः' पद देकर "संग्रह-मर्यादा" को हो इंगित किया है । अभिधान राजेन्द्र कोष में एक स्थान पर ऐसा भी लिखा है 'णाणामणिकणगरवण महरिहरिमल "सपुतदार" परिजन दासीदास ...... ।' उक्त पद मे प्राए 'सपुत्तदार' शब्द का विश्लेषण करते हुए कोचकार लिखते है 'सपुत्रदाराः गुलपुतल त्राणि । इससे भी "परिमाण" को ही बल मिलता है। जैसे किसी ने एक दासी या दास का परिमाण रक्खा तो वह उसके परिमाण में रहने के लिए 'सुतयुक्नदासी' को नहीं रख सकता । क्योंकि यदि वह रखेगा तो उसकी एक संख्या रूप परिमाण में दोष श्रा जायगा । यतः दासी के साथ रहने के कारण उसका पुत्र भी दास कार्य में सहायक सिद्ध होगा और व्रती के व्रत भंग का कारण होगा ।
इन प्रसगों से स्पष्ट है कि जिस भाव में ब्रह्मवयं है वह भाव अपरिग्रह से अछूता है । अतः एक मे दूसरे का समावेश नही हो सकता । हाँ, यदि खीचतान करके समादेश माना ही जाय तो चोरी आदि पाप भी परिग्रह में गर्भित किए जा सकते है अथवा एक महिसा महाव्रत में भी सभी व्रत सम्मिलित हो सकते है पर ऐसा किया नहीं गया। सभी महावत भादिनाथ युग से महावीर युग
धनेशान्त
तक चलते रहे है । भ्रतः चातुर्याम धर्म पार्श्व का है' ऐसा कथन निर्मन बैठता है।
श्री तत्त्वार्थं राजवार्तिक में प्रथम अध्याय के सातवें सूत्र की व्याख्या में श्राया "चतुर्यामभेदात् " पद भी बिचारणीय है कि इसका समावेश कब और कैसे हुआ । हो सकता है बाद के विद्वानों ने (चातुर्याम धर्म पार्श्वनाथ का है ऐसी धारणा मे ) मूल पद संशोधन की चेष्टा की हो अन्यथा, प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिलिपियों से तो ऐसा सिद्ध नहीं होता। व्यावर वणवेनगोला पौर मूडबिद्री की ताडपत्रीय प्रतियों में 'चतुर्यमभेदात्' के स्थान मे 'चतु र्यति भेदात्' पाठ है ।
(८) अब प्राती है केशी- गौतम संवाद की बात । सो,
यह विचारणीय है कि वे केशी पाप परपरा के वे ही बेशी है जिन्होंने प्रदेशी राजा को संवोध दिया था या अन्य कोई केशी है ? वे केशी चार ज्ञान के धारक थे और पार्श्व की शिष्य परम्परा के पट्टधर आचार्य थे । उन्होंने गौतम से प्रश्न किया हो यह बात जेंची नहीं । यतः संवाद के ( कथित) समय तक गौतम और केशी दोनों समान ज्ञान धारक ही सिद्ध हो सकते हैं।
केशी के ज्ञान के संबंध में रायपसेणी में लिया है 'इच्चे णं पदेसी ! श्रहं तव "चउब्विणं नाणेणं" इमे या समत्थियं जाव समुप्पन जाण. मि" भगवती सूष से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है।
इस संबंध में पाठकों के विचारार्थं श्रधिक कुछ न लिखकर यहां एक उद्धरण मात्र दिया जाना ही उपयुक्त है ।
'भगवान् पार्श्वनाथ के पौधे पर प्राचार्य केशी श्रमण हुए जो बड़े ही प्रतिभाशाली बालब्रह्मचारी, चौदह पूर्वधारी और मति श्रुत एवं अवधिज्ञान के धारक थे। - पार्श्व संवत् १६६ से २५० तक प्रापका कार्यकाल बताया गया है। आपने ही अपने उपदेश से श्वेताम्बिका के महाराज 'प्रदेशी' को घोर नास्तिक से परम श्रास्तिक बनाया । ...... आचार्य केशिकुमार पार्श्वनिर्वाण संवत् ११६ से २५० तक र्थात् ८४ वर्ष तक प्राचार्य पद पर रहे और अन्त में मुक्त हुए।' इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथ
....N