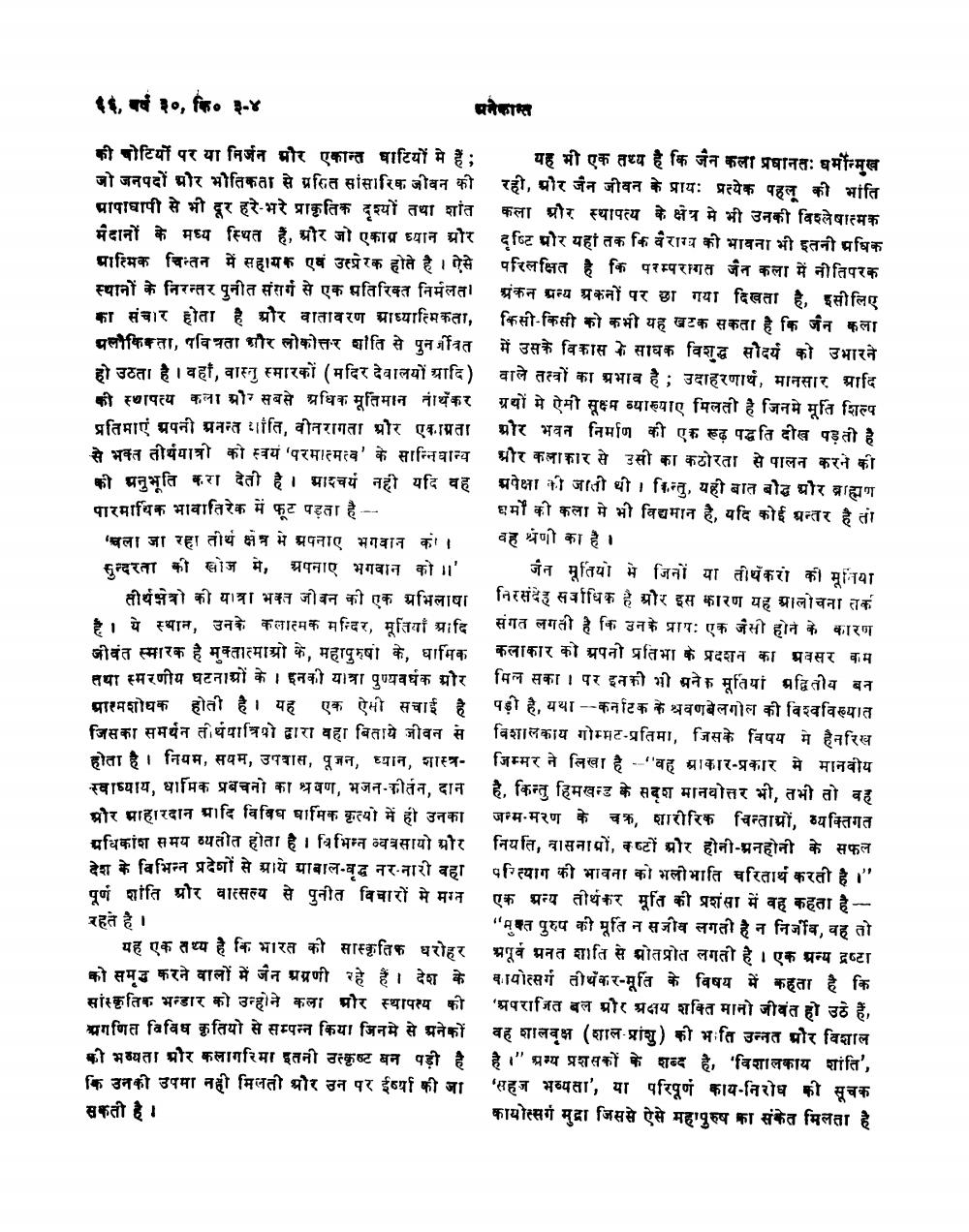________________
१६ बर्ष ३०, कि० ३-४
अनेकान्त
की चोटियों पर या निर्जन भौर एकान्त घाटियों मे हैं; यह भी एक तथ्य है कि जैन कला प्रधानतः घोन्मुख जो जनपदों और भौतिकता से ग्रसित सांसारिक जीवन की रही, और जैन जीवन के प्रायः प्रत्येक पहल की भांति प्रापाघापी से भी दूर हरे-भरे प्राकृतिक दृश्यों तथा शांत कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी उनकी विश्लेषात्मक मैदानों के मध्य स्थित हैं, और जो एकाग्र ध्यान और दृष्टि और यहां तक कि वैराग्य की भावना भी इतनी अधिक मात्मिक चिन्तन में सहायक एवं उत्प्रेरक होते है । ऐसे परिलक्षित है कि परम्परागत जैन कला में नीतिपरक स्थानों के निरन्तर पुनीत संसर्ग से एक अतिरिक्त निर्मलता अंकन अन्य प्रकनों पर छा गया दिखता है, इसीलिए का संचार होता है और वातावरण प्राध्यात्मिकता, किसी-किसी को कभी यह खटक सकता है कि जन कला मलौकिक्ता, पवित्रता और लोकोत्तर शांति से पुनर्जीवत में उसके विकास के साधक विशुद्ध सौदर्य को उभारने हो उठता है । वहाँ, वास्तु स्मारकों (मदिर देवालयों ग्रादि) वाले तत्वों का प्रभाव है ; उदाहरणार्थ, मानसार आदि की स्थापत्य कला और सबसे अधिक मूर्तिमान नार्थंकर ग्रयों मे ऐमी सूक्ष्म व्याख्याए मिलती है जिनमे मूर्ति शिल्प प्रतिमाएं अपनी अनन्त गांति, वीतरागता और एकाग्रता और भवन निर्माण की एक रूढ़ पद्धति दीख पड़ती है से भक्त तीर्थयात्री को स्वयं 'परमात्मत्व' के सान्निधान्य और कलाकार से उसी का कठोरता से पालन करने की की अनुभति करा देती है। मादचर्य नहीं यदि वह अपेक्षा की जाती थी। किन्तु, यही बात बौद्ध पौर ब्राह्मण पारमार्थिक भावातिरेक में फूट पड़ता है -
घमों की कला मे भी विद्यमान है, यदि कोई अन्तर है तो 'चला जा रहा तीर्थ क्षेत्र में अपनाए भगवान का। वह धणी का है। सन्दरता की खोज में, अपनाए भगवान को॥' जन मूर्तियो मे जिनों या तीर्थंकरों की मूनिया
तीर्थक्षेत्रो की यात्रा भक्त जोबन की एक अभिलाषा निरसंदेह सर्वाधिक है और इस कारण यह मालोचना तर्क है। ये स्थान, उनके कलात्मक मन्दिर, मूतियाँ प्रादि संगत लगती है कि उनके प्रायः एक जैसी होने के कारण जीवंत स्मारक है मक्तात्माग्रो के, महापुरुषो के, घामिक कलाकार को अपनी प्रतिभा के प्रदशन का अवसर कम तथा स्मरणीय घटनामों के । इनकी यात्रा पुण्यवर्धक पोर मिल सका । पर इनकी भी अनेक मूर्तियां अद्वितीय बन प्रारमशोधक होती है। यह एक ऐसी सचाई है पड़ी है, यथा--कर्नाटक के श्रवणबेलगोल की विश्वविख्यात जिसका समर्थन तीर्थयात्रियो द्वारा वहा बिताये जीवन से विशालकाय गोम्मट-प्रतिमा, जिसके विषय मे हैनरिख होता है। नियम, सयम, उपवास, पूजन, ध्यान, शास्त्र- जिम्मर ने लिखा है . 'वह प्राकार-प्रकार मे मानवीय स्वाध्याय, धामिक प्रबचनो का श्रवण, भजन-कीर्तन, दान है, किन्तु हिमखन्ड के सदश मानवोत्तर भी, तभी तो वह और माहारदान प्रादि विविध धार्मिक कृत्यो में ही उनका जन्म-मरण के चक्र, शारीरिक चिन्तामों, व्यक्तिगत अधिकांश समय व्यतीत होता है । विभिन्न व्यवसायो पौर नियति, वासनाप्रों, कष्टों और होनी-अनहोनी के सफल देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राये पाबाल-वृद्ध नर-नारी वहा परित्याग की भावना को भलीभाति चरितार्थ करती है।" पूर्ण शांति और वात्सल्य से पुनीत विचारों मे मग्न एक अन्य तीर्थकर मूर्ति की प्रशंसा में वह कहता हैरहते है।
__ "मुक्त पुरुष की मूर्ति न सजीव लगती है न निर्जीव, वह तो यह एक तथ्य है कि भारत को सास्कृतिक धरोहर अपूर्व मनत शाति से मोतप्रोत लगती है। एक अन्य द्रष्टा को समद्ध करने वालों में जैन प्रग्रणी रहे हैं। देश के वायोत्सर्ग तीर्थंकर-मूर्ति के विषय में कहता है कि सांस्कृतिक भन्डार को उन्होंने कला पौर स्थापत्य को 'अपराजित बल और अक्षय शक्ति मानो जीवंत हो उठे हैं, अगणित विविध कृतियो से सम्पन्न किया जिनमे से अनेकों वह शालवृक्ष (शाल-प्रांशु) की भाति उन्नत प्रौर विशाल की भव्यता और कलागरिमा इतनी उत्कृष्ट बन पड़ी है है।" अन्य प्रशसकों के शब्द है, "विशालकाय शांति', कि उनकी उपमा नहीं मिलती और उन पर ईष्या की जा 'सहज भव्यता', या परिपूर्ण काय-निरोध की सूचक सकती है।
कायोत्सर्ग मुद्रा जिससे ऐसे महापुरुष का संकेत मिलता है