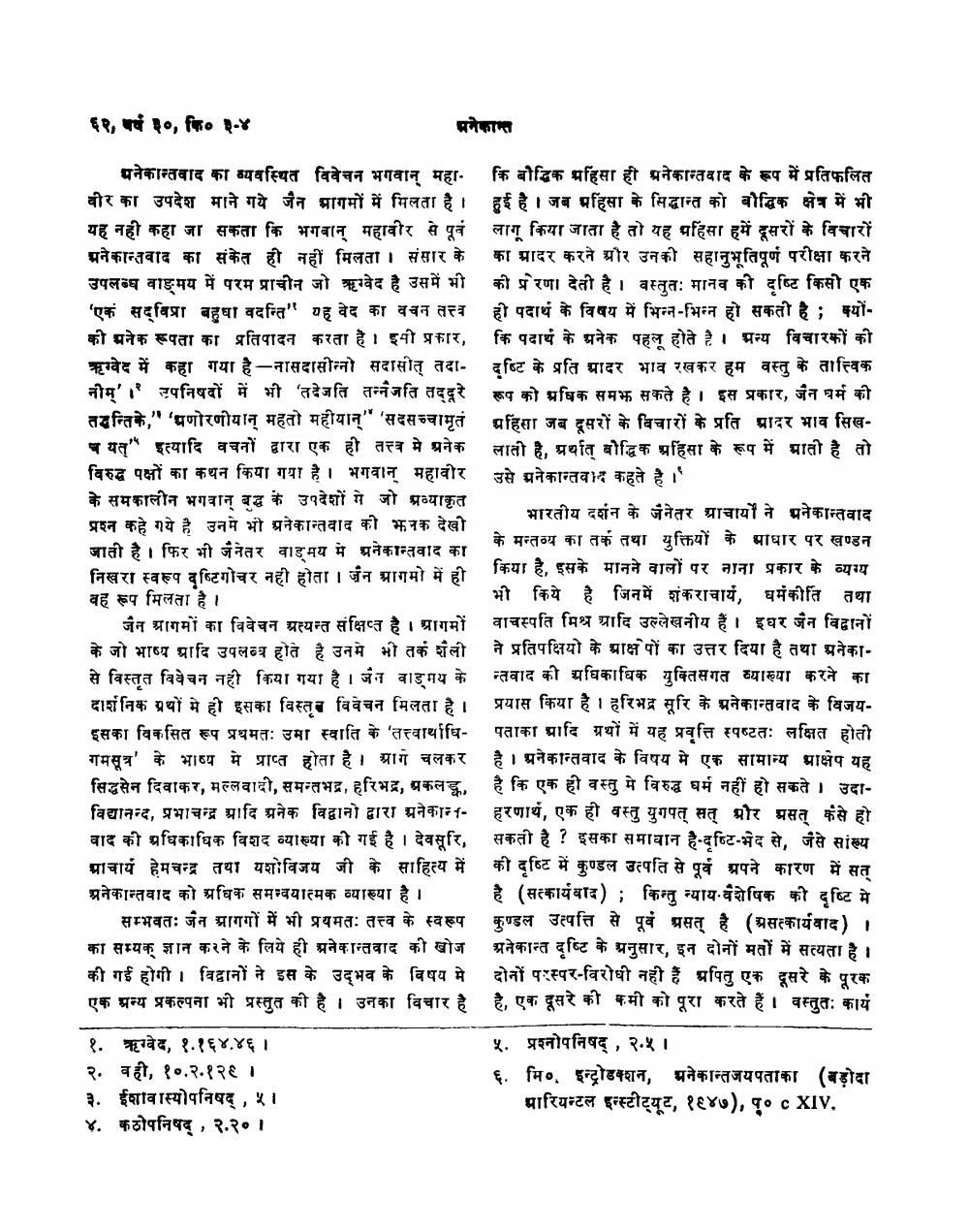________________
६२,
३०, कि०३.४
अनेकान्त
भनेकान्तवाद का व्यवस्थित विवेचन भगवान महा. कि बौद्धिक अहिंसा ही अनेकान्तवाद के रूप में प्रतिफलित वीर का उपदेश माने गये जैन मागमों में मिलता है। हुई है । जब महिंसा के सिद्धान्त को बौद्धिक क्षेत्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान महावीर से पूर्व लागू किया जाता है तो यह अहिंसा हमें दूसरों के विचारों भनेकान्तवाद का संकेत ही नहीं मिलता। संसार के का मादर करने और उनकी सहानुभूतिपूर्ण परीक्षा करने उपलब्ध वाङ्मय में परम प्राचीन जो ऋग्वेद है उसमें भी की प्रेरणा देती है। वस्तुत: मानव की दृष्टि किसी एक 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" यह वेद का वचन तत्त्व ही पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न हो सकती है; क्योंकी अनेक रूपता का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार, कि पदार्थ के अनेक पहल होते है। अन्य विचारकों की ऋग्वेद में कहा गया है-नासदासीनो सदासीत् तदा- दष्टि के प्रति आदर भाव रखकर हम वस्तु के तात्त्विक नीम'। उपनिषदों में भी 'तदे जति तन्नजति तद्दूरे रूप को अधिक समझ सकते है। इस प्रकार, जैन धर्म की तलन्तिके," 'प्रणोरणीयान् महतो महीयान्" 'सदसच्चामृतं अहिंसा जब दूसरों के विचारों के प्रति प्रादर भाव सिखच यत" इत्यादि वचनों द्वारा एक ही तत्व मे अनेक लाती है. अर्थात बौद्धिक अहिंसा के रूप में भाती है तो विरुद्ध पक्षों का कथन किया गया है। भगवान महावीर उसे अनेकान्तवाद कहते है। के समकालीन भगवान बद्ध के उपदेशों में जो अव्याकृत
भारतीय दर्शन के जैनेतर प्राचार्यों ने अनेकान्तवाद प्रश्न कहे गये है उनमे भी अनेकान्तवाद की झनक देखी
के मन्तव्य का तर्क तथा युक्तियों के माधार पर खण्डन जाती है। फिर भी जेनेतर वाड्मय में अनेकान्तवाद का निखरा स्वरूप दष्टिगोचर नही होता। जन भागमो में ही
किया है, इसके मानने वालों पर नाना प्रकार के व्यग्य वह रूप मिलता है।
भी किये है जिनमें शंकराचार्य, धर्मकीर्ति तथा जैन आगमों का विवेचन अत्यन्त संक्षिप्त है । प्रागमों वाचस्पति मिश्र आदि उल्लेखनीय हैं। इधर जैन विद्वानों के जो भाष्य प्रादि उपलब्ध होते है उनमे भी तक शैली ने प्रतिपक्षियो के प्राक्ष पों का उत्तर दिया है तथा अनेकासे विस्तृत विवेचन नही किया गया है । जैन वाड़मय के न्तवाद की अधिकाधिक युक्तिसगत व्याख्या करने का दार्शनिक प्रथों में ही इसका विस्तृत विवेचन मिलता है। प्रयास किया है । हरिभद्र सूरि के भनेकान्तवाद के विजयइसका विकसित रूप प्रथमतः उमा स्वाति के 'तत्त्वार्थाधि- पताका प्रादि ग्रथों में यह प्रवृत्ति स्पष्टतः लक्षित होती गमसूत्र' के भाष्य में प्राप्त होता है। आगे चलकर है। अनेकान्तवाद के विषय मे एक सामान्य माप यह सिद्धसेन दिवाकर, मल्लवादी, समन्तभद्र, हरिभद्र, प्रकलङ्क, है कि एक ही वस्तु मे विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते । उदाविद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि अनेक विद्वानो द्वारा अनेकानन- हरणार्थ, एक ही वस्तु युगपत् सत् और प्रसत कसे हो वाद की अधिकाधिक विशद व्याख्या की गई है । देवसूरि, सकती है ? इसका समाधान है-दृष्टि-भेद से, जैसे सांख्य प्राचार्य हेमचन्द्र तथा यशोविजय जी के साहित्य में की दृष्टि में कुण्डल उत्पति से पूर्व अपने कारण में सत अनेकान्तवाद को अधिक समन्वयात्मक व्याख्या है। है (सत्कार्यवाद); किन्तु न्याय वैशेषिक की दृष्टि मे
सम्भवतः जन प्रागगों में भी प्रयमतः तत्त्व के स्वरूप कुण्डल उत्पत्ति से पूर्व प्रसत् है (असत्कार्यवाद) । का सम्यक् ज्ञान करने के लिये ही अनेकान्तवाद की खोज अनेकान्त दृष्टि के अनुसार, इन दोनों मतों में सत्यता है। की गई होगी। विद्वानों ने इस के उद्भव के विषय मे दोनों परस्पर-विरोधी नही हैं अपितु एक दूसरे के पूरक एक अन्य प्रकल्पना भी प्रस्तुत की है । उनका विचार है है, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। वस्तुत: कार्य १. ऋग्वेद, १.१६४.४६ ।
५. प्रश्नोपनिषद् , २.५। २. वही, १०.२.१२६ ।
६. मि०, इन्ट्रोडक्शन, अनेकान्तजयपताका (बड़ोदा ३. ईशावास्योपनिषद् , ५।
मारियन्टल इन्स्टीट्यूट, १९४७), पृ.cXIV. ४. कठोपनिषद् , २.२० ।