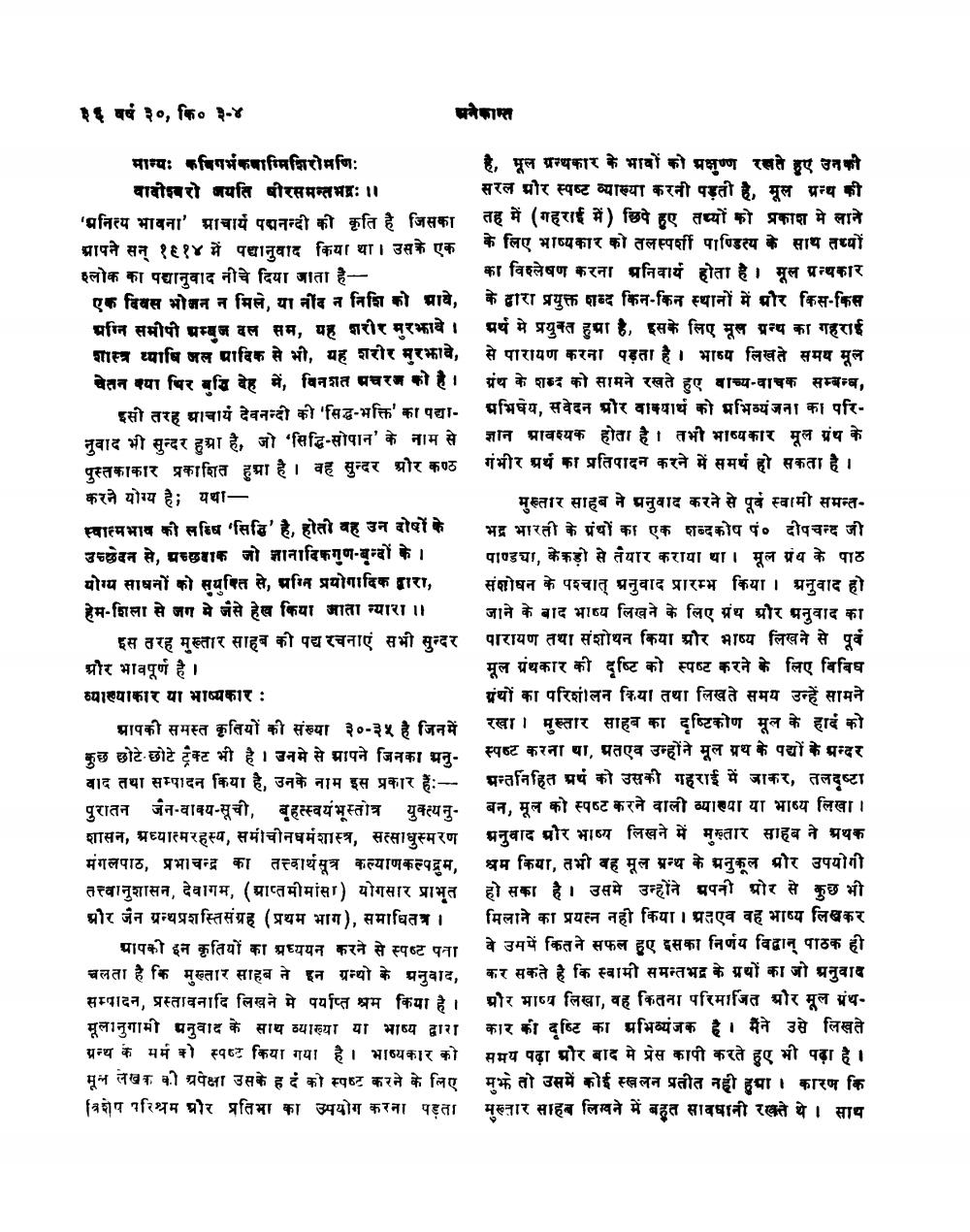________________
३६ वर्ष ३०, कि० ३-४
भनेकान्त
मान्यः कषिगर्भकवाग्मिशिरोमणिः
है, मूल ग्रन्थकार के भावों को प्रक्षुण्ण रखते हुए उनको वावीश्वरो जयति बीरसमन्तभद्रः॥
सरल और स्पष्ट व्याख्या करनी पड़ती है, मूल अन्य की 'भनित्य भावना' माचार्य पद्मनन्दी की कृति है जिसका तह में (गहराई में) छिपे हुए तथ्यों को प्रकाश मे लाने मापने सन् १९१४ में पद्यानुवाद किया था। उसके एक के लिए भाष्यकार को तलस्पर्शी पाण्डित्य के साथ तथ्यों श्लोक का पद्यानुवाद नीचे दिया जाता है-
का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है। मूल प्रन्थकार एक दिवस भोजन न मिले, या नींद न निशि को प्रावे, के द्वारा प्रयुक्त शब्द किन-किन स्थानों में और किस-किस अग्नि समीपी अम्बुज बल सम, यह शरीर मुरझावे। मर्थ मे प्रयुक्त हुप्रा है, इसके लिए मूल ग्रन्थ का गहराई शास्त्र च्याधि जल प्रादिक से भी, यह शरीर मुरझावे, से पारायण करना पड़ता है। भाष्य लिखते समय मूल चेतन क्या घिर बतिदेह में, विनशत प्रचरज को है। ग्रंथ के शब्द को सामने रखते हुए वाच्य-वाचक सम्बन्ध,
इसी तरह प्राचार्य देवनन्दी की 'सिद्ध-भक्ति' का पद्या- अभिधेय, सवेदन और वाक्यार्थ को भभिव्यंजना का परिनुवाद भी सुन्दर हया है, जो 'सिद्धि-सोपान' के नाम से ज्ञान प्रावश्यक होता है। तभी भाष्यकार मुल ग्रंथ के पुस्तकाकार प्रकाशित हुमा है। वह सुन्दर और कण्ठ गंभीर प्रर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ हो सकता है। करने योग्य है। यथा
मुख्तार साहब ने अनुवाद करने से पूर्व स्वामी समन्त. स्वात्मभाव की लम्धि सिद्धि' है, होती वह उन दोषों के भद्र भारती के ग्रंथों का एक शब्दकोष पं. दीपचन्द जी उच्छेदन से, अच्छवाक जो ज्ञानादिकगुण-वृन्दों के। पाण्डया, केकड़ो से तैयार कराया था। मूल ग्रंथ के पाठ योग्य साधनों को सयुक्ति से, अग्नि प्रयोगादिक द्वारा, संशोधन के पश्चात् अनुवाद प्रारम्भ किया। अनुवाद हो हेम-शिला से जग मे जैसे हेख किया जाता न्यारा ।। जाने के बाद भाष्य लिखने के लिए ग्रंथ और अनुवाद का ___इस तरह मुख्तार साहब को पद्य रचनाएं सभी सुन्दर पारायण तथा संशोथन किया और भाष्य लिखने से पूर्व और भावपूर्ण है।
मूल ग्रंथकार की दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए विविध व्याख्याकार या भाष्यकार:
ग्रंथों का परिशीलन किया तथा लिखते समय उन्हें सामने मापकी समस्त कृतियों की संख्या ३०-३५ है जिनमें रखा। मुख्तार साहब का दृष्टिकोण मूल के हाई को कुछ छोटे छोटे ट्रेक्ट भी है। उनमे से मापने जिनका मनु
स्पष्ट करना था, प्रतएव उन्होंने मूल अथ के पद्यों के अन्दर वाद तथा सम्पादन किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:- अन्तनिहित प्रथं को उसकी गहराई में जाकर, तलदृष्टा पुरातन जैन-वाक्य-सूची, बृहत्स्वयंभस्तोत्र युक्त्यन- बन, मूल को स्पष्ट करने वाली व्याख्या या भाष्य लिखा। शासन, अध्यात्मरहस्य, समीचीनधर्मशास्त्र, सत्साधुस्मरण अनुवाद और भाष्य लिखने में मुख्तार साहब ने प्रथक मंगलपाठ, प्रभाचन्द्र का तत्त्वार्थ सूत्र कल्याणकल्पद्रुम, श्रम किया, तभी वह मूल ग्रन्थ के अनुकूल और उपयोगी तत्त्वानुशासन, देवागम, (माप्तमीमांसा) योगसार प्राभूत हो सका है। उसमे उन्होंने अपनी प्रोर से कुछ भी पौर जैन ग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह (प्रथम भाग), समाधितत्र। मिलाने का प्रयत्न नही किया। प्रतएव वह भाष्य लिखकर
पापको इन कृतियों का अध्ययन करने से स्पष्ट पता वे उममें कितने सफल हुए इसका निर्णय विद्वान् पाठक ही चलता है कि मुख्तार साहब ने इन ग्रन्थो के अनुवाद, कर सकते है कि स्वामी समन्तभद्र के प्रथों का जो अनुवाद सम्पादन, प्रस्तावनादि लिखने में पर्याप्त श्रम किया है। और भाष्य लिखा, वह कितना परिमार्जित और मूल ग्रंथमूलानुगामी पनुवाद के साथ व्याख्या या भाष्य द्वारा कार की दृष्टि का अभिव्यंजक है। मैंने उसे लिखते ग्रन्थ के मर्म को स्पष्ट किया गया है। भाष्यकार को समय पढ़ा और बाद मे प्रेस कापी करते हुए भी पढ़ा है। मूल लेखक की अपेक्षा उसके हदं को स्पष्ट करने के लिए मुझे तो उसमें कोई स्खलन प्रतीत नही हुपा। कारण कि विशेष परिश्रम और प्रतिभा का उपयोग करना पड़ता महतार साहब लिम्वने में बहुत सावधानी रखते थे। साथ