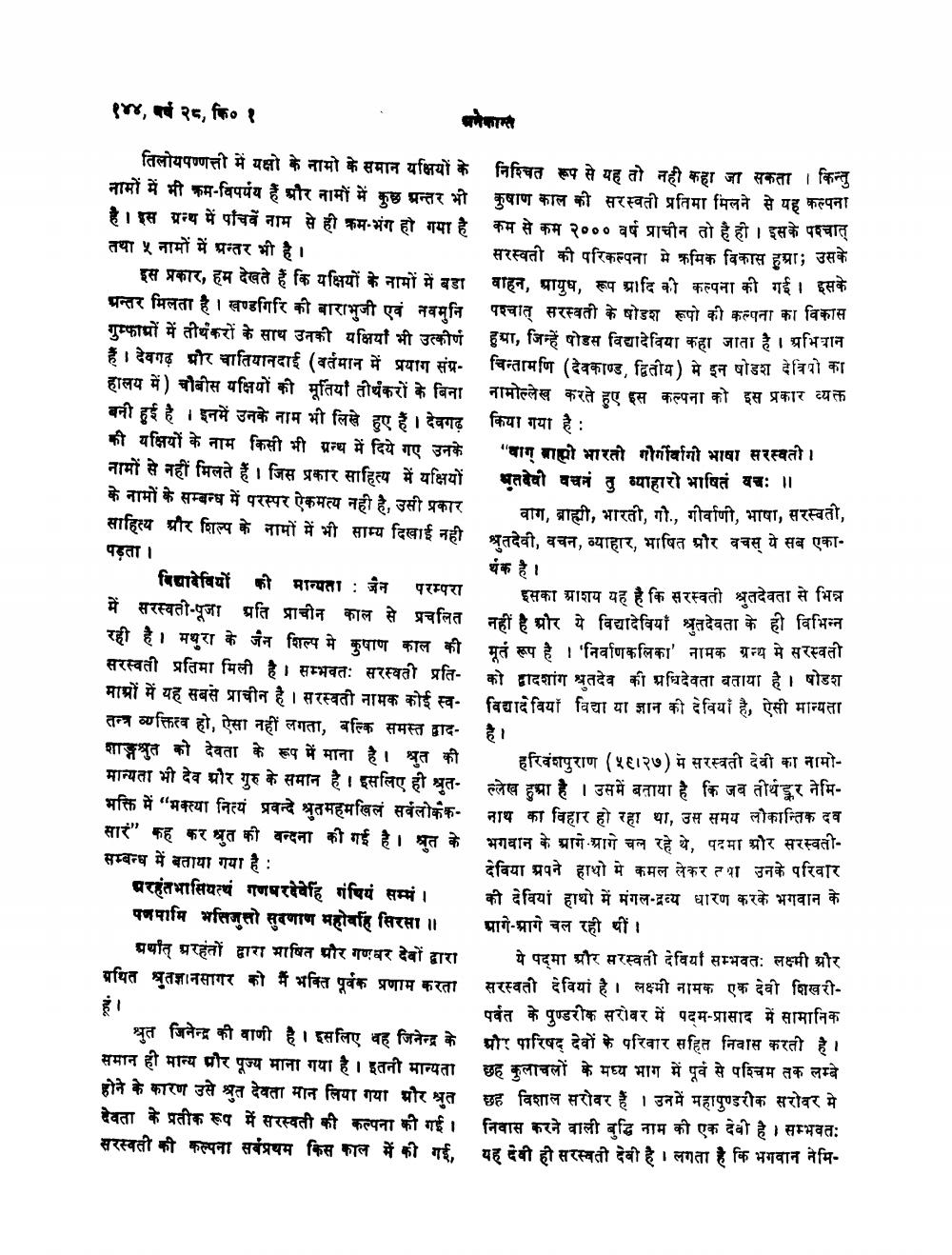________________
१४,
२८, कि.१
तिलोयपण्णत्ती में यक्षो के नामो के समान यक्षियों के निश्चित रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता । किन्तु नामों में भी क्रम-विपर्यय हैं और नामों में कुछ अन्तर भी कुषाण काल की सरस्वती प्रतिमा मिलने से यह कल्पना है। इस ग्रन्थ में पांचवें नाम से ही क्रम-भंग हो गया है कम से कम २००० वर्ष प्राचीन तो है ही। इसके पश्चात् तथा ५ नामों में अन्तर भी है।
सरस्वती की परिकल्पना में क्रमिक विकास हुप्रा; उसके इस प्रकार, हम देखते हैं कि यक्षियों के नामों में बड़ा वाहन, प्रायूध, रूप प्रादि की कल्पना की गई। इसके अन्तर मिलता है । खण्डगिरि की बाराभुजी एवं नवनि पश्चात् सरस्वती के षोडश रूपो की कल्पना का विकास गुम्फामों में तीर्थंकरों के साथ उनकी यक्षियां भी उत्कीर्ण हुमा, जिन्हें षोडस विद्यादेविया कहा जाता है । अभियान हैं । देवगढ़ और चातियानदाई (वर्तमान में प्रयाग संग्र- चिन्तामणि (देवकाण्ड, द्वितीय) मे इन षोडश देवियो का हालय में ) चौबीस यक्षियों की मूर्तियां तीर्थंकरों के बिना नामोल्लेख करते हुए इस कल्पना को इस प्रकार व्यक्त बनी हुई है । इनमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं । देवगढ़ किया गया है : की यक्षियों के नाम किसी भी अन्य में दिये गए उनके ___ "वाग् ब्राह्मो भारती गोर्गीर्वागी भाषा सरस्वती। नामों से नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार साहित्य में यक्षियों
मलत ह । जिस प्रकार साहित्य में यक्षियों भूतदेवी वचनं तु व्याहारो भाषितं वचः ॥ के नामों के सम्बन्ध में परस्पर ऐकमत्य नही है, उसी प्रकार वाग. ब्राझी. भारती, गो., गीर्वाणी, भाषा, सरस्वता, साहित्य और शिल्प के नामों में भी साम्य दिखाई नही तदेवी. बचन, व्याहार, भाषित और वचस् ये सब एकापड़ता।
र्थक है। विद्यादेवियों की मान्यता : जैन परम्परा
इसका आशय यह है कि सरस्वती श्रुतदेवता से भिन्न में सरस्वती-पूजा प्रति प्राचीन काल से प्रचलित नहीं है और ये विद्यादेवियाँ श्रुतदेवता के हो विभिन्न रही है। मथुरा के जैन शिल्प मे कुषाण काल की मतं रूप है । 'निर्वाणकलिका' नामक ग्रन्थ में सरस्वता सरस्वती प्रतिमा मिली है। सम्भवतः सरस्वती प्रति- को द्वादशांग श्रतदेव की अधिदेवता बताया है। षोडश मानों में यह सबसे प्राचीन है। सरस्वती नामक कोई स्व. विद्यादेवियाँ विद्या या ज्ञान की देवियाँ है, ऐसी मान्यता तन्त्र व्यक्तित्व हो, ऐसा नहीं लगता, बल्कि समस्त द्वाद- है। शानश्रुत को देवता के रूप में माना है। श्रत की
ना है। श्रुत की हरिवंशपुराण (५६।२७) में सरस्वती देवी का नामोमान्यता भी देव और गुरु के समान है। इसलिए ही श्रुत- लेख हा है । उसमें बताया है कि जब तीर्थङ्कर नेमिभक्ति में "भक्त्या नित्यं प्रवन्दे श्रुतमहमखिलं सर्वलोकक- नाथ का विहार हो रहा था, उस समय लोकान्तिक दव सारं" कह कर श्रुत की बन्दना की गई है। श्रत के भगवान के प्रागे पागे चल रहे थे, पदमा और सरस्वतीसम्बन्ध में बताया गया है :
देविया अपने हाथो मे कमल लेकर तथा उनके परिवार परहंतभासियत्थं गणपरदेवेहि गंपियं सम्म। की देवियां हाथो में मंगल-द्रव्य धारण करके भगवान के पणमामि भतिजुत्तो सुदणाण महोवहि सिरसा ॥ प्रागे-मागे चल रही थीं।
अर्थात् प्ररहंतों द्वारा भाषित पौर गण वर देवों द्वारा ये पदमा और सरस्वती देवियाँ सम्भवत: लक्ष्मी और अथित श्रुतज्ञानसागर को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता सरस्वती देवियां है। लक्ष्मी नामक एक देवी शिखरी
पर्वत के पुण्डरीक सरोवर में पद्म-प्रासाद में सामानिक श्रुत जिनेन्द्र की वाणी है। इसलिए वह जिनेन्द्र के और पारिषद देवों के परिवार सहित निवास करती है। समान ही मान्य प्रौर पूज्य माना गया है । इतनी मान्यता छह कुलाचलों के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तक लम्बे होने के कारण उसे श्रुत देवता मान लिया गया और श्रुत छह विशाल सरोवर हैं । उनमें महापुण्डरीक सरोवर मे देवता के प्रतीक रूप में सरस्वती की कल्पना की गई। निवास करने वाली बुद्धि नाम की एक देवी है । सम्भवत: सरस्वती की कल्पना सर्वप्रथम किस काल में की गई, यह देवी ही सरस्वती देवी है। लगता है कि भगवान नेमि