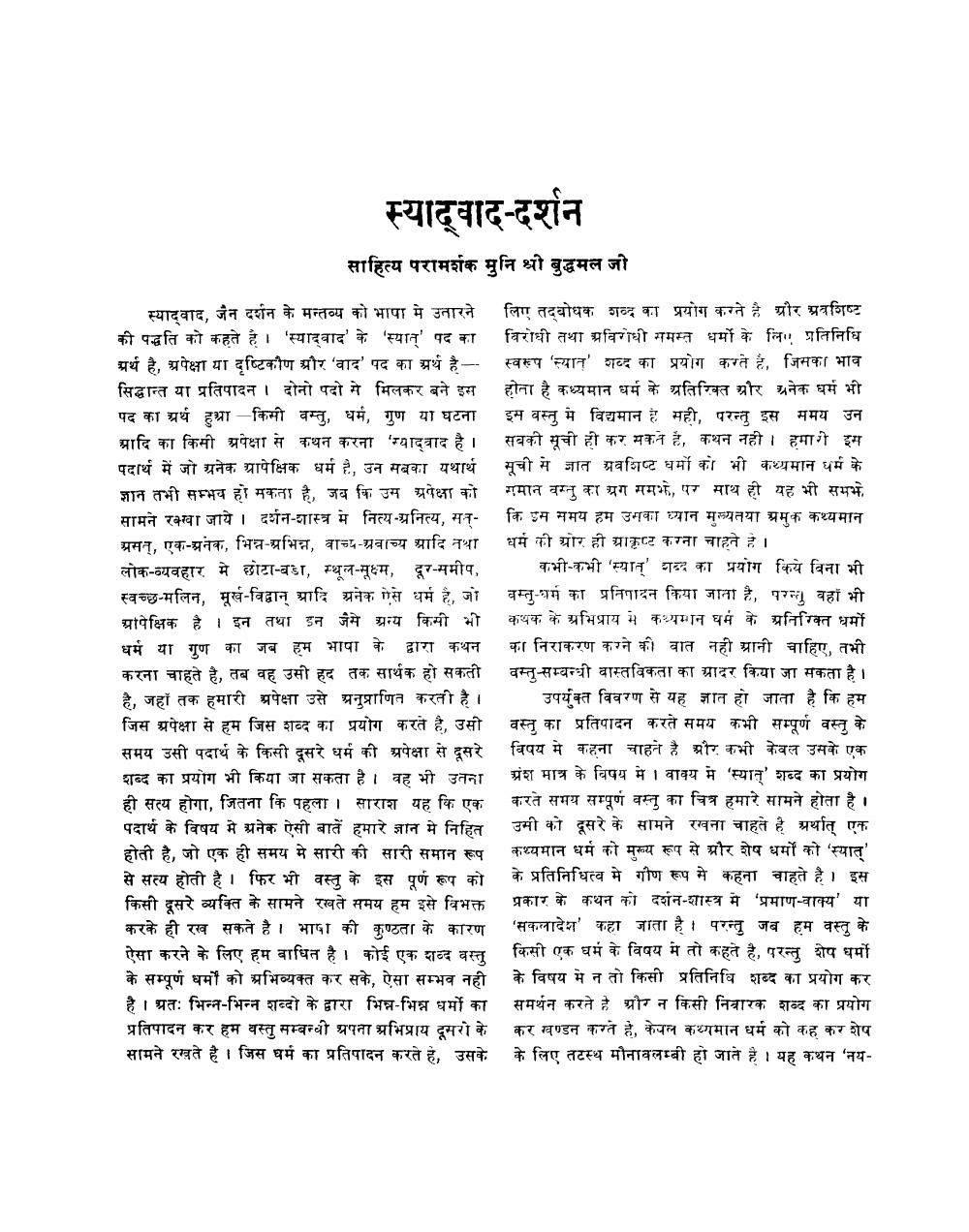________________
स्याद्वाद-दर्शन
साहित्य परामर्शक मुनि श्री बुद्धमल जी स्याद्वाद, जैन दर्शन के मन्तव्य को भापा मे उतारने लिए तद्बोधक शब्द का प्रयोग करते है और प्रवशिष्ट की पद्धति को कहते है। 'स्याद्वाद' के 'स्यान्' पद का विरोधी तथा अविगेधी समस्त धर्मों के लिए प्रतिनिधि अर्थ है, अपेक्षा या दृष्टिकोण और 'वाद' पद का अर्थ है- स्वरूप 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करते है, जिसका भाव सिद्धान्त या प्रतिपादन । दोनो पदो मे मिलकर बने इस होता है कथ्यमान धर्म के अतिरिक्त और अनेक धर्म भी पद का अर्थ हुश्रा –किमी वस्तु, धर्म, गुण या घटना इम वस्तु में विद्यमान है मही, परन्तु इस ममय उन
आदि का किमी अपेक्षा से कथन करना 'ग्यावाद है। सबकी सूची ही कर सकते है, कथन नही। हमारी इम पदार्थ में जो अनेक प्रापेक्षिक धर्म है, उन सबका यथार्थ मूची मे ज्ञात अवशिष्ट धर्मों को भी कथ्यमान धर्म के ज्ञान तभी सम्भव हो मकता है, जब कि उम अपेक्षा को समान वस्तु का अग समझे, पर साथ ही यह भी समझे सामने रखा जाये । दर्शन-शास्त्र मे नित्य-अनित्य, मन्- कि इस समय हम उसका ध्यान मुख्यतया अमुक कथ्यमान असन, एक-अनक, भिन्न-भिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि नथा धर्म की योर ही याकृष्ट करना चाहते है। लोक-व्यवहार मे छोटा-बड़ा, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-ममीप, कभी-कभी 'स्यान्' शब्द का प्रयोग किये बिना भी स्वच्छ-मलिन, मूर्ख-विद्वान् आदि अनेक ऐसे धर्म है, जो वस्तु-धर्म का प्रतिपादन किया जाना है, परन्तु वहाँ भी प्रापेक्षिक है । इन तथा इन जैसे अन्य किसी भी कथक के अभिप्राय में कथ्यमान धर्म के अतिरिक्त धर्मो धर्म या गुण का जब हम भाषा के द्वारा कथन का निराकरण करने की बात नही पानी चाहिए, तभी करना चाहते है, तब वह उसी हद तक सार्थक हो सकती वस्तु-सम्बन्धी वास्तविकता का प्रादर किया जा सकता है। है, जहाँ तक हमारी अपेक्षा उसे अनुप्राणित करती है। उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि हम जिस अपेक्षा से हम जिस शब्द का प्रयोग करते है, उसी वस्तु का प्रतिपादन करते समय कभी सम्पूर्ण वस्तु के समय उसी पदार्थ के किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा से दूसरे विषय मे कहना चाहते है और कभी केवल उसके एक शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह भी उतना अंश मात्र के विषय मे । वाक्य में 'स्यात्' शब्द का प्रयोग ही सत्य होगा, जितना कि पहला। साराश यह कि एक करते समय सम्पूर्ण वस्तु का चित्र हमारे सामने होता है। पदार्थ के विषय मे अनेक ऐसी बातें हमारे ज्ञान में निहित उमी को दूसरे के सामने रखना चाहते है अर्थात् एक होती है, जो एक ही समय मे सारी की सारी समान रूप कथ्यमान धर्म को मुख्य रूप से और शेष धर्मों को 'स्यात' से सत्य होती है। फिर भी वस्तु के इस पूर्ण रूप को के प्रतिनिधित्व मे गीण रूप से कहना चाहते है। इस किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते समय हम इसे विभक्त प्रकार के कथन को दर्शन-शास्त्र में 'प्रमाण-वाक्य' या करके ही रख सकते है। भाषा की कुण्ठता के कारण 'सकलादेश' कहा जाता है। परन्तु जब हम वस्तु के ऐसा करने के लिए हम बाधित है। कोई एक शब्द वस्तु किसी एक धर्म के विषय में तो कहते है, परन्तु शेष धर्मो के सम्पूर्ण धर्मों को अभिव्यक्त कर सके, ऐसा सम्भव नही के विषय मे न तो किसी प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग कर है । अत: भिन्न-भिन्न शब्दो के द्वारा भिन्न-भिन्न धर्मों का समर्थन करते है और न किसी निवारक शब्द का प्रयोग प्रतिपादन कर हम वस्तु सम्बन्धी अपना अभिप्राय दूमरी के कर खण्डन करते हैं, केवल कथ्यमान धर्म को कह कर शेष सामने रखते है । जिस धर्म का प्रतिपादन करते है, उसके के लिए तटस्थ मौनावलम्बी हो जाते है । यह कथन 'नय