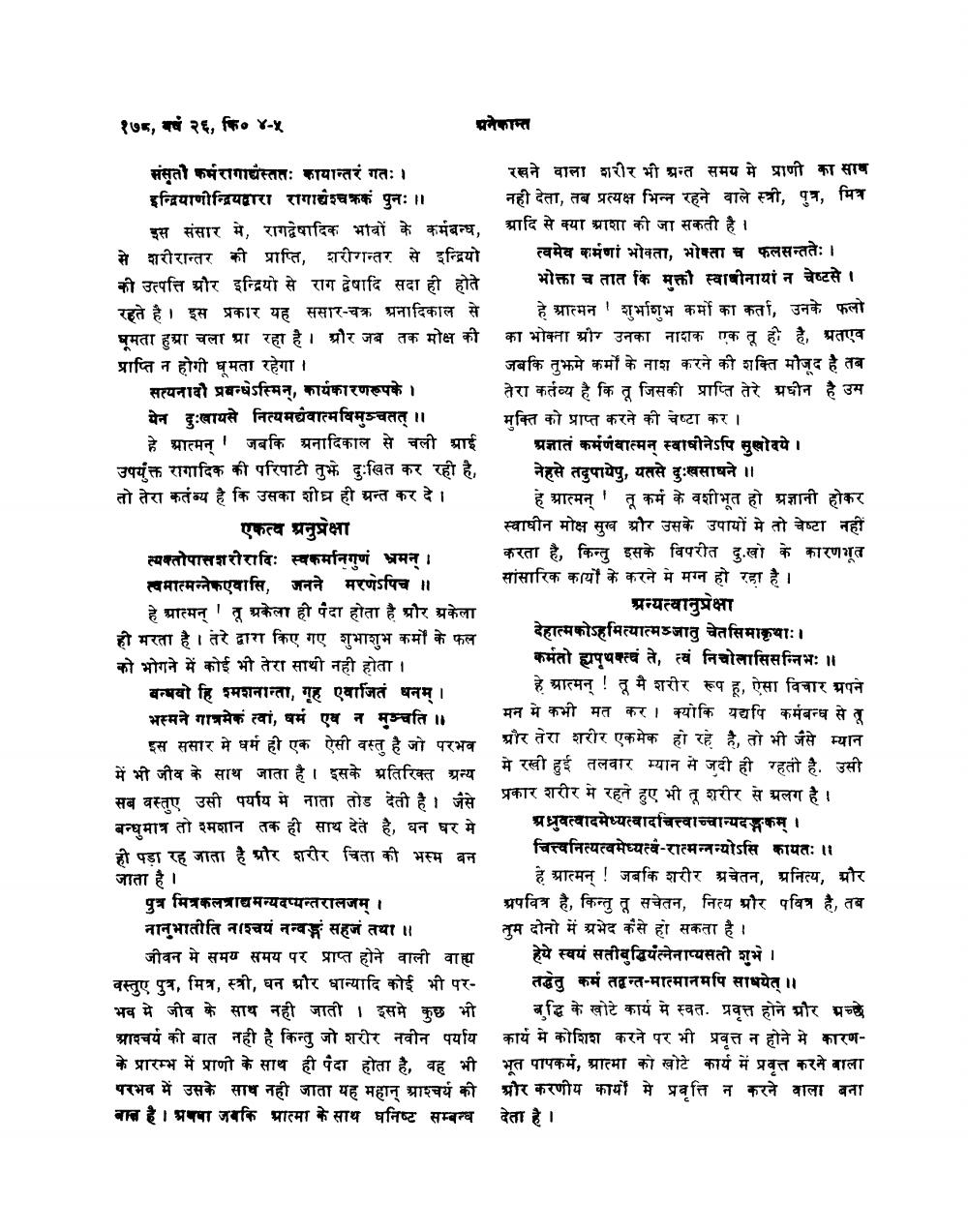________________
१७५, वर्ष २६, कि० ४-५
अनेकान्त
मंसृती कर्मरागाद्यस्ततः कायान्तरं गतः।
रखने वाला शरीर भी अन्त समय मे प्राणी का साथ इन्द्रियाणीन्द्रियद्वारा रागाद्यश्चक्रकं पुनः॥ नही देता, तब प्रत्यक्ष भिन्न रहने वाले स्त्री, पुत्र, मित्र
इस संसार मे, रागद्वेषादिक भावों के कर्मबन्ध, आदि से क्या प्राशा की जा सकती है। से शरीरान्तर की प्राप्ति, शरीगन्तर से इन्द्रियो
त्वमेव कर्मणां भोक्ता, भोक्ता च फलसन्ततेः । की उत्पत्ति और इन्द्रियो से राग द्वेषादि सदा ही होते भोक्ता च तात कि मुक्ती स्वाधीनायां न चेष्टसे । रहते है। इस प्रकार यह ससार-चक्र अनादिकाल से हे आत्मन । शुर्भाशुभ कर्मो का कर्ता, उनके फलो घूमता हुआ चला पा रहा है। और जब तक मोक्ष की का भोक्ना और उनका नाशक एक तू ही है, अतएव प्राप्ति न होगी धूमता रहेगा।
जबकि तुझमे कर्मों के नाश करने की शक्ति मौजद है तब सत्यनादौ प्रबन्धेऽस्मिन्, कार्यकारणरूपके। तेरा कर्तव्य है कि तू जिसकी प्राप्ति तेरे अधीन है उम मेन दुःखायसे नित्यमद्यवात्मविमुञ्चतत् ॥ मुक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा कर।
हे पात्मन् । जबकि अनादिकाल से चली आई प्रज्ञातं कर्मणवात्मन् स्वाधीनेऽपि सुखोदये। उपर्युक्त रागादिक की परिपाटी तुझे दुःखित कर रही है, नेहसे तदुपायेपु, यससे दुःखसाधने । तो तेरा कर्तव्य है कि उसका शीघ्र ही अन्त कर दे।
हे आत्मन् । तू कर्म के वशीभूत हो अज्ञानी होकर एकत्व अनुप्रेक्षा
स्वाधीन मोक्ष सुख और उसके उपायों मे तो चेष्टा नहीं त्यक्तोपासशरीरादिः स्वकर्मानगुणं भ्रमन् ।
करता है, किन्तु इसके विपरीत दु.खो के कारणभूत त्वमात्मन्नेकएवासि, जनने मरणेऽपिच ॥
सांसारिक कार्यों के करने मे मग्न हो रहा है। हे पात्मन् । तू अकेला ही पैदा होता है और अकेला
अन्यत्वानुप्रेक्षा ही मरता है । तेरे द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल
देहात्मकोऽहमित्यात्मजातु चेतसिमाकृथाः। को भोगने में कोई भी तेरा साथी नही होता।
कर्मतो ह्यपृथक्त्वं ते, त्वं निचोलासिसन्निभः ॥ बन्धवो हि श्मशनान्ता, गृह एवाजितं धनम् ।
हे आत्मन् ! तू मै शरीर रूप हू, ऐसा विचार अपने भस्मने गात्रमेकं त्वां, धर्म एव न मुञ्चति ॥
मन मे कभी मत कर। क्योकि यद्यपि कर्मबन्ध से तू इस ससार मे धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो परभव
और तेरा शरीर एकमेक हो रहे है, तो भी जैसे म्यान में भी जीव के साथ जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य
मे रखी हुई तलवार म्यान में जदी ही रहती है. उसी सब वस्तुए उसी पर्याय मे नाता तोड देती है। जैसे
प्रकार शरीर में रहते हुए भी तू शरीर से अलग है। बन्धुमात्र तो श्मशान तक ही साथ देते है, धन घर मे
अध्रुवत्वादमेध्यत्वादचित्त्वाच्चान्यदङ्गकम् । ही पड़ा रह जाता है और शरीर चिता की भस्म बन
चित्त्वनित्यत्वमेध्यत्व-रात्मन्नन्योऽसि कायतः ।। जाता है।
हे आत्मन् ! जबकि शरीर अचेतन, अनित्य, और पुत्र मित्रकलत्राधमन्यदप्यन्तरालजम् ।
अपवित्र है, किन्तु तू सचेतन, नित्य और पवित्र है, तब नानुभातीति नाश्चयं नन्वङ्ग सहजं तथा । तुम दोनो में अभेद कैसे हो सकता है।
जीवन मे समय समय पर प्राप्त होने वाली वाह्य हेये स्वयं सतीवुद्धियंत्नेनाप्यसती शुभे । वस्तुए पुत्र, मित्र, स्त्री, धन और धान्यादि कोई भी पर- तद्धेतु कर्म तद्वन्त-मात्मानमपि साधयेत् ॥ भव मे जीव के साथ नही जाती । इसमे कुछ भी बुद्धि के खोटे कार्य मे स्वत. प्रवृत्त होने और अच्छे आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु जो शरीर नवीन पर्याय कार्य मे कोशिश करने पर भी प्रवृत्त न होने के कारणके प्रारम्भ में प्राणी के साथ ही पैदा होता है, वह भी भूत पापकर्म, प्रात्मा को खोटे कार्य में प्रवृत्त करने वाला परभव में उसके साथ नहीं जाता यह महान् आश्चर्य की और करणीय कार्यों मे प्रवृत्ति न करने वाला बना बान है। अबषा जबकि मात्मा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध देता है।