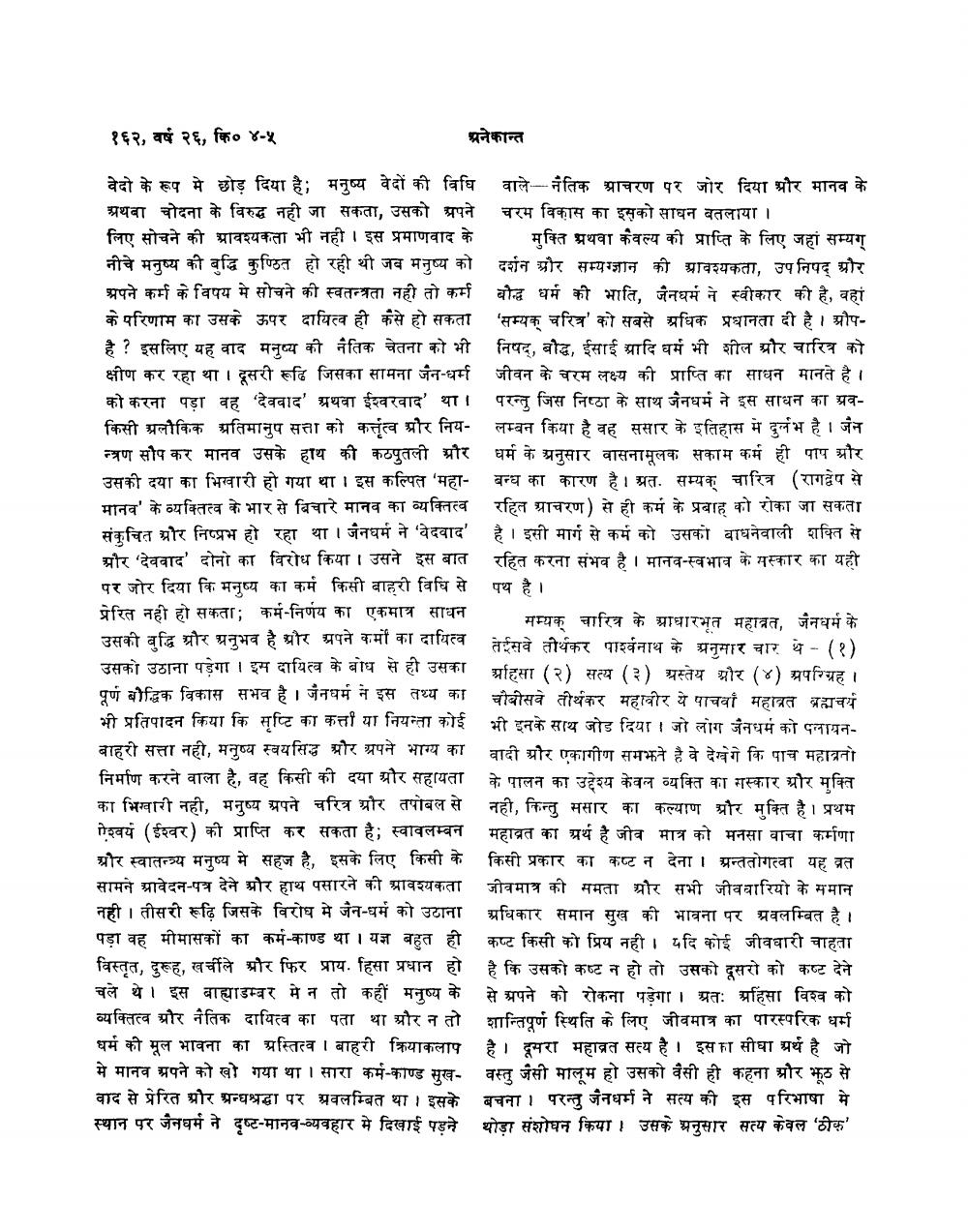________________
१६२, वर्ष २६, कि० ४-५
अनेकान्त
वेदो के रूप मे छोड़ दिया है। मनुष्य वेदों की विधि वाले-नैतिक आचरण पर जोर दिया और मानव के अथबा चोदना के विरुद्ध नही जा सकता, उसको अपने चरम विकास का इसको साधन बतलाया । लिए सोचने की आवश्यकता भी नहीं । इस प्रमाणवाद के मुक्ति अथवा कैवल्य की प्राप्ति के लिए जहां सम्यग् नीचे मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हो रही थी जब मनुष्य को दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्रावश्यकता, उपनिषद् और अपने कर्म के विषय मे सोचने की स्वतन्त्रता नहीं तो कर्म बौद्ध धर्म की भाति, जैनधर्म ने स्वीकार की है, वहां के परिणाम का उसके ऊपर दायित्व ही कैसे हो सकता 'सम्यक् चरित्र' को सबसे अधिक प्रधानता दी है । औपहै ? इसलिए यह वाद मनुष्य की नैतिक चेतना को भी निषद्, बौद्ध, ईसाई आदि धर्म भी शील और चारित्र को क्षीण कर रहा था । दूसरी रूढि जिसका सामना जन-धर्म जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मानते है । को करना पड़ा वह 'देववाद' अथवा ईश्वरवाद' था। परन्तु जिस निष्ठा के साथ जैनधर्म ने इस साधन का अवकिसी अलौकिक अतिमानुष सत्ता को कर्तृत्व और निय- लम्बन किया है वह ससार के इतिहास में दुर्लभ है । जैन न्त्रण सौप कर मानव उसके हाथ की कठपुतली और धर्म के अनुसार वासनामूलक सकाम कर्म ही पाप और उसकी दया का भिखारी हो गया था। इस कल्पित 'महा- बन्ध का कारण है। अत. सम्यक् चारित्र (रागद्वेष से मानव' के व्यक्तित्व के भार से बिचारे मानव का व्यक्तित्व रहित प्राचरण) से ही कर्म के प्रबाह को रोका जा सकता संकुचित और निष्प्रभ हो रहा था । जैनधर्म ने 'वेदवाद' है। इसी मार्ग से कर्म को उसको बाधनेवाली शक्ति से
और 'देववाद' दोनो का विरोध किया। उसने इस बात रहित करना संभव है। मानव-स्वभाव के मस्कार का यही पर जोर दिया कि मनुष्य का कर्म किसी बाहरी विधि से पथ है। प्रेरित नही हो सकता; कर्म-निर्णय का एकमात्र साधन
मम्यक् चारित्र के आधारभूत महाव्रत, जैनधर्म के उसकी बुद्धि और अनुभव है और अपने कर्मों का दायित्व
तेईसवे तीर्थकर पार्श्वनाथ के अनुसार चार थे - (१) उसको उठाना पड़ेगा । इस दायित्व के बोध से ही उसका ।
अहिसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । पूर्ण बौद्धिक विकास सभव है । जैनधर्म ने इस तथ्य का ।
चौबीसवे तीर्थकर महावीर ये पाचौं महाव्रत ब्रह्मचर्य भी प्रतिपादन किया कि सृष्टि का कत्ती या नियन्ता कोई भी इनके साथ जोड दिया। जो लोग जैनधर्म को पलायनबाहरी सत्ता नही, मनुष्य स्वयसिद्ध और अपने भाग्य का वादी और एकागीण समझते है वे देखेंगे कि पाच महाव्रतो निर्माण करने वाला है, वह किसी की दया और सहायता के पालन का उद्देश्य केवल व्यक्ति का मस्कार और मुक्ति का भिग्वारी नही, मनुष्य अपने चरित्र और तपोबल से नही, किन्तु मसार का कल्याण और मुक्ति है। प्रथम ऐश्वर्य (ईश्वर) की प्राप्ति कर सकता है। स्वावलम्बन महाव्रत का अर्थ है जीव मात्र को मनसा वाचा कर्मणा
और स्वातन्त्र्य मनुष्य मे सहज है, इसके लिए किसी के किसी प्रकार का कष्ट न देना। अन्ततोगत्वा यह व्रत सामने आवेदन-पत्र देने और हाथ पसारने की आवश्यकता जीवमात्र की ममता और सभी जीवधारियो के ममान नही । तीसरी रूढ़ि जिसके विरोध मे जैन-धर्म को उठाना अधिकार समान सुख की भावना पर अवलम्बित है। पड़ा वह मीमासकों का कर्म-काण्ड था। यज्ञ बहुत ही कष्ट किसी को प्रिय नही। यदि कोई जीवधारी चाहता विस्तृत, दुरूह, खर्चीले और फिर प्राय. हिसा प्रधान हो है कि उसको कष्ट न हो तो उसको दूसरो को कष्ट देने चले थे। इस बाह्याडम्बर में न तो कहीं मनुष्य के से अपने को रोकना पड़ेगा। अतः अहिंसा विश्व को व्यक्तित्व और नैतिक दायित्व का पता था और न तो शान्तिपूर्ण स्थिति के लिए जीवमात्र का पारस्परिक धर्म धर्म की मूल भावना का अस्तित्व । बाहरी क्रियाकलाप है। दूसरा महाव्रत सत्य है। इसका सीधा अर्थ है जो मे मानव अपने को खो गया था। सारा कर्म-काण्ड सुख- वस्तु जैसी मालूम हो उसको वैसी ही कहना और झूठ से वाद से प्रेरित और अन्धश्रद्धा पर अवलम्बित था। इसके बचना । परन्तु जैनधर्म ने सत्य की इस परिभाषा मे स्थान पर जैनधर्म ने दृष्ट-मानव-व्यवहार मे दिखाई पड़ने थोड़ा संशोधन किया। उसके अनुसार सत्य केवल 'ठीक'