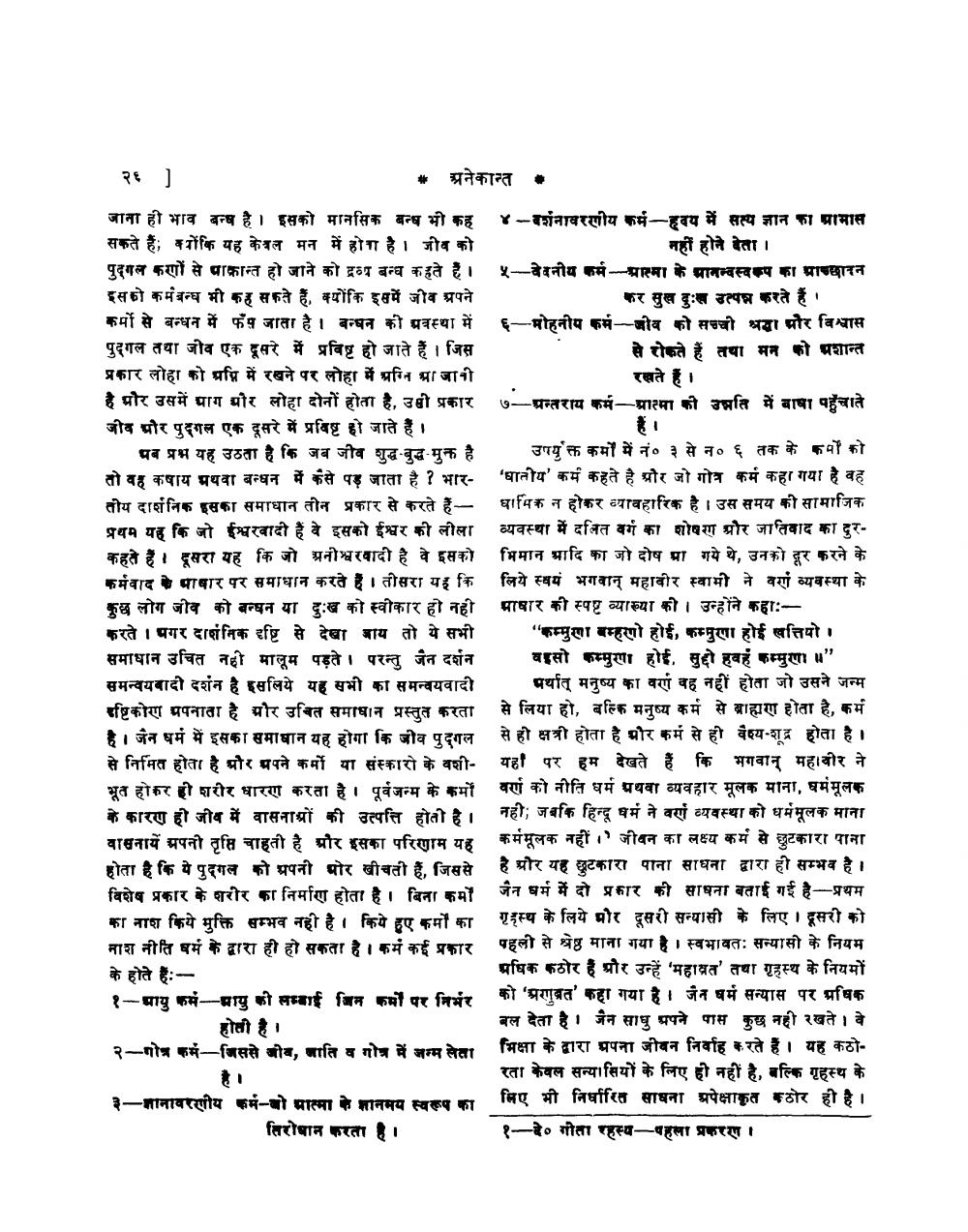________________
२६
]
* अनेकान्त .
जाना ही भाव बन्ध है। इसको मानसिक बन्ध भी कह ४-वर्शनावरणीय कर्म-हृदय में सत्य ज्ञान का प्रामास सकते हैं; क्योंकि यह केवल मन में होता है। जीव को
नहीं होने देता। पुद्गल कणों से पाक्रान्त हो जाने को द्रव्य बन्ध कहते हैं। ५–वेदनीय कर्म-प्रात्मा के मानन्दस्वरूप का प्राच्छानन इसको कर्मबन्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जीव अपने
कर सुख दुःख उत्पन्न करते हैं । कर्मो से बन्धन में फंप जाता है। बन्धन की अवस्था में ६-मोहनीय कर्म-जीव को सच्ची श्रया और विश्वास पुद्गल तथा जीव एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं । जिस
से रोकते हैं तथा मन को प्रशान्त प्रकार लोहा को अग्नि में रखने पर लोहा में अग्नि पाजानी
रखते हैं। है और उसमें प्राग और लोहा दोनों होता है, उसी प्रकार ७-अन्तराय कर्म-प्रात्मा की उन्नति में बाधा पहुंचाते जीव और पुद्गल एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं ।
अब प्रभ यह उठता है कि जब जीव शुद्ध-बुद्ध-मुक्क है उपयुक्त कर्मों में नं० ३ से न० ६ तक के कर्मों को तो वह कषाय अथवा बन्धन में कैसे पड़ जाता है ? भार- 'धातीय' कर्म कहते है और जो गोत्र कर्म कहा गया है वह तोय दार्शनिक इसका समाधान तीन प्रकार से करते हैं- धामिक न होकर व्यावहारिक है। उस समय की सामाजिक प्रथम यह कि जो ईश्वरवादी हैं वे इसको ईश्वर की लीला व्यवस्था में दलित वर्ग का शोषण और जातिवाद का दुरकहते हैं। दूसरा यह कि जो अनीश्वरवादी है वे इसको भिमान भादि का जो दोष मा गये थे, उनको दूर करने के कर्मवादमापार पर समाधान करते हैं। तीसरा यह कि लिये स्वयं भगवान् महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था के कुछ लोग जीव को बन्धन या दुःख को स्वीकार हो नही माघार की स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने कहा:करते । प्रगर दार्शनिक दृष्टि से देखा जाय तो ये सभी "कम्मुरणा बम्हणो होई, कम्मुरणा होई खत्तियो। समाधान उचित नहीं मालूम पड़ते। परन्तु जैन दर्शन वासो कम्मरणा होई, सुद्दो हवहं कम्मुणा ।" समन्वयवादी दर्शन है इसलिये यह सभी का समन्वयवादी पर्थात् मनुष्य का वर्ण वह नहीं होता जो उसने जन्म रष्टिकोण अपनाता है और उचित समाधान प्रस्तुत करता से लिया हो, बल्कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म है। जैन धर्म में इसका समाधान यह होगा कि जीव दगल से ही क्षत्री होता है और कर्म से ही वैश्य-शूद्र होता है। से निर्मित होता है और अपने कर्मों या संस्कारो के वशी- यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान् महावीर ने भूत होकर ही शरीर धारण करता है। पूर्वजन्म के कर्मों वर्ण को नीति धर्म अथवा व्यवहार मूलक माना, धर्ममूलक के कारण ही जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। नही; जबकि हिन्दू धर्म ने वर्ण व्यवस्था को धर्ममूलक माना वासनायें अपनी तृप्ति चाहती है और इसका परिणाम यह कर्ममूलक नहीं।' जीवन का लक्ष्य कर्म से छुटकारा पाना होता है कि ये पुद्गल को अपनी पोर खीचती हैं, जिससे है और यह छुटकारा पाना साधना द्वारा ही सम्भव है। विशेष प्रकार के शरीर का निर्माण होता है। बिना को जैन धर्म में दो प्रकार की साधना बताई गई है-प्रथम का नाश किये मुक्ति सम्भव नही है। किये हुए कर्मों का गृहस्थ के लिये और दूसरी सन्यासी के लिए । दूसरी को माश नीति धर्म के द्वारा ही हो सकता है। कर्म कई प्रकार पहली से श्रेष्ठ माना गया है। स्वभावतः सन्यासी के नियम के होते हैं:
अधिक कठोर हैं और उन्हें 'महावत' तथा गृहस्थ के नियमों १-मायु कर्म-मायु की लम्बाई जिन कर्मों पर निर्भर
को 'अणुव्रत' कहा गया है। जैन धर्म सन्यास पर अधिक होती है।
बल देता है। जैन साधु अपने पास कुछ नहीं रखते। वे २-गोत्र कर्म-जिससे जीव, जाति व गोत्र में जन्म लेता
मिक्षा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह कठो
रता केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं है, बल्कि गृहस्थ के ३-शानावरणीय कर्म-जो मात्मा के शानमय स्वरूप का
लिए भी निर्धारित साधना अपेक्षाकृत कठोर ही है। तिरोधान करता।
१-० गीता रहस्य-पहला प्रकरण ।