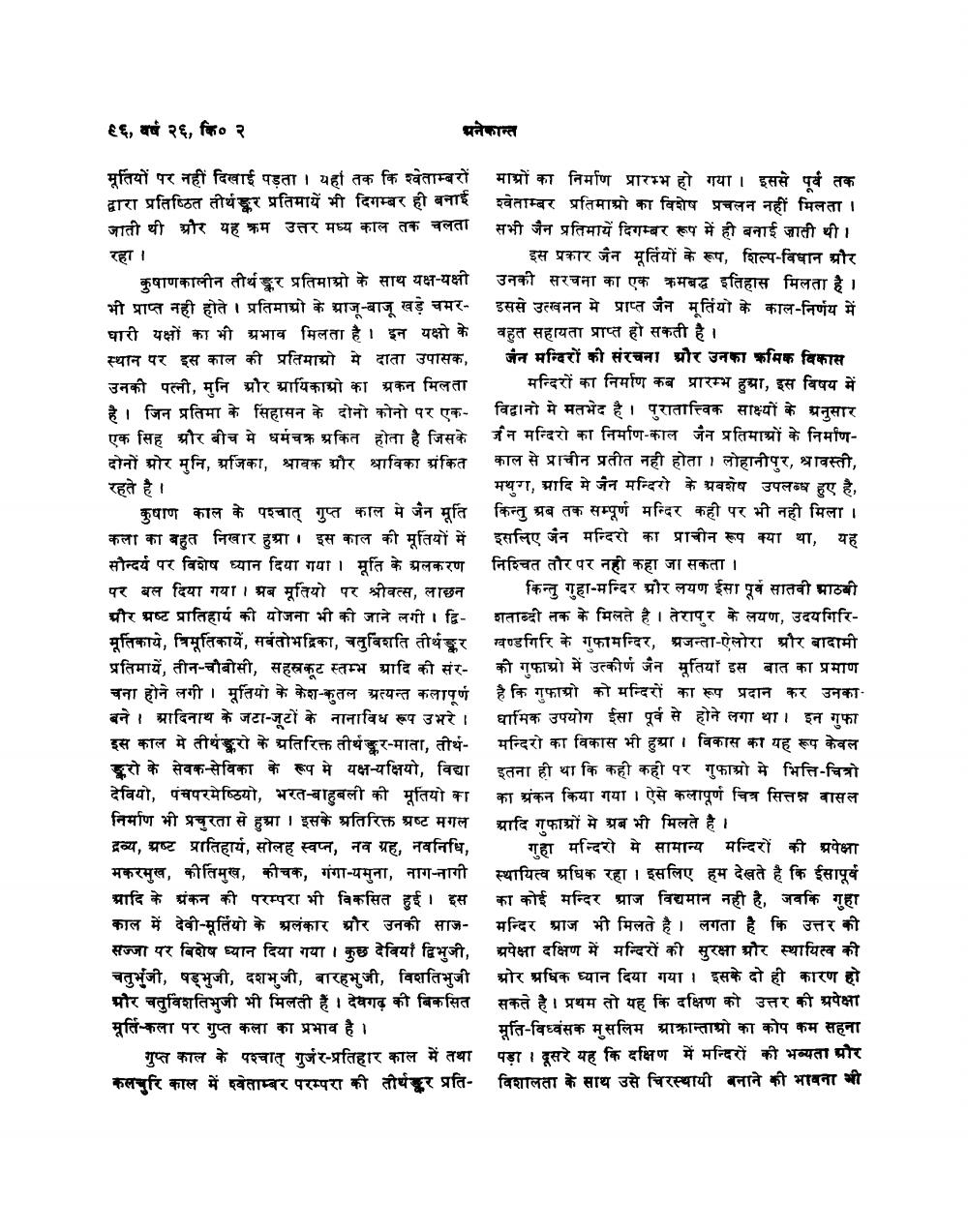________________
९६, वर्ष २६, कि०२
अनेकान्त
मूर्तियों पर नहीं दिखाई पड़ता। यहां तक कि श्वेताम्बरों माओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया। इससे पूर्व तक द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थङ्कर प्रतिमायें भी दिगम्बर ही बनाई श्वेताम्बर प्रतिमानो का विशेष प्रचलन नहीं मिलता । जाती थी और यह क्रम उत्तर मध्य काल तक चलता सभी जैन प्रतिमायें दिगम्बर रूप में ही बनाई जाती थी। रहा।
इस प्रकार जैन मूर्तियों के रूप, शिल्प-विधान और कुषाणकालीन तीर्थङ्कर प्रतिमानो के साथ यक्ष-यक्षी उनकी सरचना का एक कमबद्ध इतिहास मिलता है। भी प्राप्त नही होते । प्रतिमानो के पाजू-बाजू खड़े चमर- इससे उत्खनन मे प्राप्त जैन मूर्तियो के काल-निर्णय में घारी यक्षों का भी प्रभाव मिलता है। इन यक्षो के बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है। स्थान पर इस काल की प्रतिमानो मे दाता उपासक, जैन मन्दिरों की संरचना और उनका क्रमिक विकास उनकी पत्नी, मुनि और आर्यिकापो का अकन मिलता __मन्दिरों का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, इस विषय में है। जिन प्रतिमा के सिंहासन के दोनो कोनो पर एक- विद्वानो मे मतभेद है। पुरातात्त्विक साक्ष्यों के अनुसार एक सिह और बीच मे धर्मचक्र अकित होता है जिसके जैन मन्दिरो का निर्माण-काल जैन प्रतिमाओं के निर्माणदोनों ओर मुनि, अजिका, श्रावक और श्राविका अंकित काल से प्राचीन प्रतीत नहीं होता। लोहानीपुर, श्रावस्ती, रहते है।
मथुग, मादि मे जैन मन्दिरो के अवशेष उपलब्ध हए है, कुषाण काल के पश्चात् गुप्त काल मे जैन मूर्ति किन्तु अब तक सम्पूर्ण मन्दिर कही पर भी नही मिला। कला का बहुत निखार हुआ। इस काल की मूर्तियों में इसलिए जैन मन्दिरो का प्राचीन रूप क्या था, यह सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया। मूर्ति के अलकरण निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। पर बल दिया गया। अब मूतियो पर श्रीवत्स, लाछन किन्तु गुहा-मन्दिर और लयण ईसा पूर्व सातवी पाठबी पौर प्रष्ट प्रातिहार्य की योजना भी की जाने लगी। द्वि- शताब्दी तक के मिलते है । तेरापुर के लयण, उदयगिरिमूर्तिकाये, त्रिमूर्तिकायें, सर्वतोभद्रिका, चतुर्विशति तीर्थङ्कर खण्डगिरि के गुफामन्दिर, अजन्ता-ऐलोरा और बादामी प्रतिमायें, तीन-चौबीसी, सहस्रकुट स्तम्भ आदि की संर- की गुफानो में उत्कीर्ण जैन मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण चना होने लगी। मूर्तियो के केश-कुतल अत्यन्त कलापूर्ण है कि गुफापो को मन्दिरों का रूप प्रदान कर उनका बने। आदिनाथ के जटा-जूटों के नानाविध रूप उभरे। धार्मिक उपयोग ईसा पूर्व से होने लगा था। इन गुफा इस काल मे तीर्थङ्करो के अतिरिक्त तीर्थङ्कर-माता, तीर्थ- मन्दिरो का विकास भी हुआ। विकास का यह रूप केवल करो के सेवक-सेविका के रूप मे यक्ष-यक्षियो, विद्या इतना ही था कि कहीं कही पर गुफाप्रो मे भित्ति-चित्रो देवियो, पंचपरमेष्ठियो, भरत-बाहुबली की मूर्तियो का का अंकन किया गया । ऐसे कलापूर्ण चित्र सित्तन्न वासल निर्माण भी प्रचुरता से हुआ । इसके अतिरिक्त प्रष्ट मगल आदि गफाओं में अब भी मिलते है। द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, सोलह स्वप्न, नव ग्रह, नवनिधि, गहा मन्दिरो मे सामान्य मन्दिरों की अपेक्षा मकरमुख, कीर्तिमुख, कीचक, गंगा-यमुना, नाग-नागी स्थायित्व अधिक रहा । इसलिए हम देखते है कि ईसापूर्व आदि के अंकन की परम्परा भी विकसित हुई। इस का कोई मन्दिर प्राज विद्यमान नही है, जबकि गुहा काल में देवी-मूर्तियो के अलंकार और उनकी साज- मन्दिर आज भी मिलते है। लगता है कि उत्तर की सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछ देवियाँ द्विभुजी, अपेक्षा दक्षिण में मन्दिरों की सुरक्षा और स्थायित्व की चतुर्भुजी, षड्भुजी, दशभुजी, बारहभुजी, विशतिभुजी ओर अधिक ध्यान दिया गया। इसके दो ही कारण हो पौर चतुर्विशतिभुजी भी मिलती हैं । देवगढ़ की बिकसित सकते है। प्रथम तो यह कि दक्षिण को उत्तर की अपेक्षा मूर्ति-कला पर गुप्त कला का प्रभाव है।
मूर्ति-विध्वंसक मुसलिम आक्रान्तामो का कोप कम सहना गुप्त काल के पश्चात् गुर्जर-प्रतिहार काल में तथा पड़ा। दूसरे यह कि दक्षिण में मन्दिरों की भव्यता और कलचुरि काल में श्वेताम्बर परम्परा की तीर्थकर प्रति- विशालता के साथ उसे चिरस्थायी बनाने की भावना भी