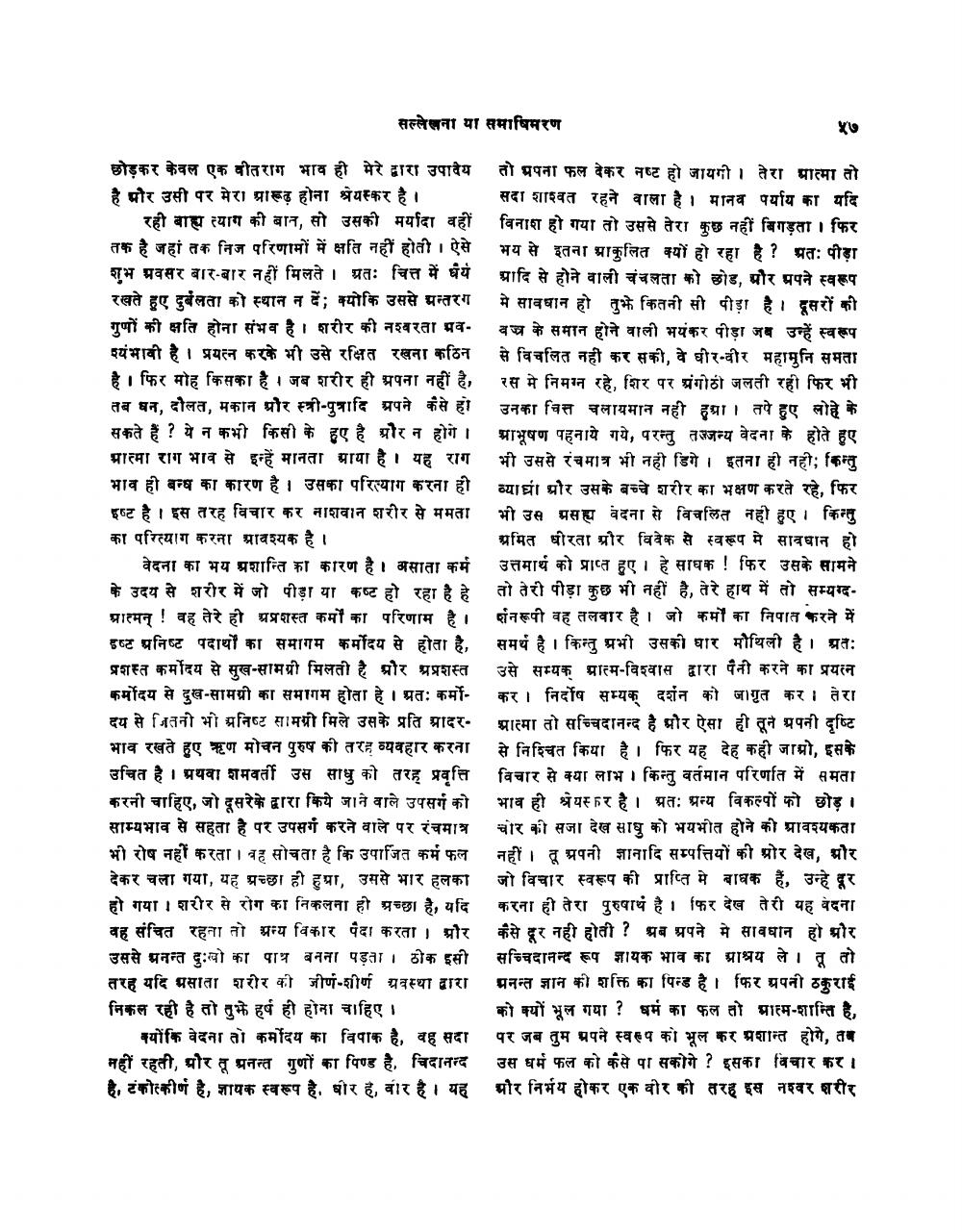________________
सल्लेखना या समाधिमरण
छोड़कर केवल एक वीतराग भाव ही मेरे द्वारा उपादेय तो अपना फल देकर नष्ट हो जायगी। तेरा मात्मा तो है और उसी पर मेरा प्रारूढ़ होना श्रेयस्कर है। सदा शाश्वत रहने वाला है। मानव पर्याय का यदि
रही बाह्य त्याग की बात, सो उसकी मर्यादा वहीं विनाश हो गया तो उससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। फिर तक है जहां तक निज परिणामों में क्षति नहीं होती। ऐसे भय से इतना पाकुलित क्यों हो रहा है? प्रतः पीड़ा शुभ अवसर बार-बार नहीं मिलते । प्रतः चित्त में धैर्य प्रादि से होने वाली चंचलता को छोड, और अपने स्वरूप रखते हुए दुर्बलता को स्थान न दें; क्योकि उससे अन्तरग मे सावधान हो तुझे कितनी सी पीड़ा है। दूसरों की गुणों की क्षति होना संभव है। शरीर की नश्वरता भव- वज्र के समान होने वाली भयंकर पीड़ा जब उन्हें स्वरूप श्यंभावी है। प्रयत्न करके भी उसे रक्षित रखना कठिन से विचलित नहीं कर सकी, वे धीर-वीर महामुनि समता है। फिर मोह किसका है । जब शरीर ही अपना नहीं है, रस मे निमग्न रहे, शिर पर अंगोठी जलती रही फिर भी तब धन, दौलत, मकान और स्त्री-पुत्रादि अपने कैसे हो उनका चित्त चलायमान नही हमा। तपे हुए लोहे के सकते हैं ? ये न कभी किसी के हुए है और न होगे। माभूषण पहनाये गये, परन्तु तज्जन्य वेदना के होते हुए मात्मा राग भाव से इन्हें मानता पाया है। यह राग भी उससे रंचमात्र भी नही डिगे। इतना ही नही; किन्तु भाव ही बन्ध का कारण है। उसका परित्याग करना ही व्याघ्री और उसके बच्चे शरीर का भक्षण करते रहे, फिर इष्ट है। इस तरह विचार कर नाशवान शरीर से ममता भी उस प्रसह्य वंदना से विचलित नही हुए। किन्तु का परित्याग करना आवश्यक है।
अमित धीरता और विवेक से स्वरूप में सावधान हो वेदना का भय प्रशान्ति का कारण है। असाता कर्म उत्तमार्थ को प्राप्त हुए। हे साधक ! फिर उसके सामने के उदय से शरीर में जो पीड़ा या कष्ट हो रहा है हे तो तेरी पीड़ा कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में तो सम्यग्दप्रात्मन् ! वह तेरे ही अप्रशस्त कर्मों का परिणाम है। निरूपी वह तलवार है। जो कर्मों का निपात करने में इष्ट अनिष्ट पदार्थों का समागम कर्मोदय से होता है, समर्थ है । किन्तु अभी उसकी धार मौथिली है। अतः प्रशस्त कर्मोदय से सुख-सामग्री मिलती है और अप्रशस्त उसे सम्यक प्रात्म-विश्वास द्वारा पैनी करने का प्रयत्न कर्मोदय से दुख-सामग्री का समागम होता है । अतः कर्मो- कर। निर्दोष सम्यक् दर्शन को जागृत कर । तेरा दय से जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिले उसके प्रति प्रादर- प्रात्मा तो सच्चिदानन्द है और ऐसा ही तूने अपनी दृष्टि भाव रखते हुए ऋण मोचन पुरुष की तरह व्यवहार करना से निश्चित किया है। फिर यह देह कही जामो, इसके उचित है । प्रथवा शमवर्ती उस साधु को तरह प्रवृत्ति विचार से क्या लाभ । किन्तु वर्तमान परिणति में समता करनी चाहिए, जो दूसरेके द्वारा किये जाने वाले उपसर्ग को भाव ही श्रेयस्कर है। अत: अन्य विकल्पों को छोड़। साम्यभाव से सहता है पर उपसर्ग करने वाले पर रंचमात्र चोर की सजा देख साधु को भयभीत होने को प्रावश्यकता भी रोष नहीं करता। वह सोचता है कि उपाजित कर्म फल नहीं। तू अपनी ज्ञानादि सम्पत्तियों की ओर देख, और देकर चला गया, यह अच्छा ही हुआ, उससे भार हलका जो विचार स्वरूप की प्राप्ति मे बाधक हैं, उन्हें दूर हो गया। शरीर से रोग का निकलना ही अच्छा है, यदि करना ही तेरा पुरुषार्थ है। फिर देख तेरी यह वेदना वह संचित रहता तो अन्य विकार पैदा करता । और कैसे दूर नही होती? अब अपने में सावधान हो और उससे अनन्त दुःखो का पात्र बनना पड़ता। ठीक इसी सच्चिदानन्द रूप ज्ञायक भाव का आश्रय ले । तू तो तरह यदि मसाता शरीर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था द्वारा मनन्त ज्ञान की शक्ति का पिन्ड है। फिर अपनी ठकुराई निकल रही है तो तुझे हर्ष ही होना चाहिए।
को क्यों भूल गया ? धर्म का फल तो मात्म-शान्ति है, क्योंकि वेदना तो कर्मोदय का विपाक है, वह सदा पर जब तुम अपने स्वरूप को भूल कर प्रशान्त होगे, तब नहीं रहती, और तू अनन्त गुणों का पिण्ड है, चिदानन्द उस धर्म फल को कैसे पा सकोगे? इसका विचार कर । है, टंकोत्कीर्ण है, ज्ञायक स्वरूप है. धीर है, वीर है। यह मौर निर्भय होकर एक वीर की तरह इस नश्वर शरीर