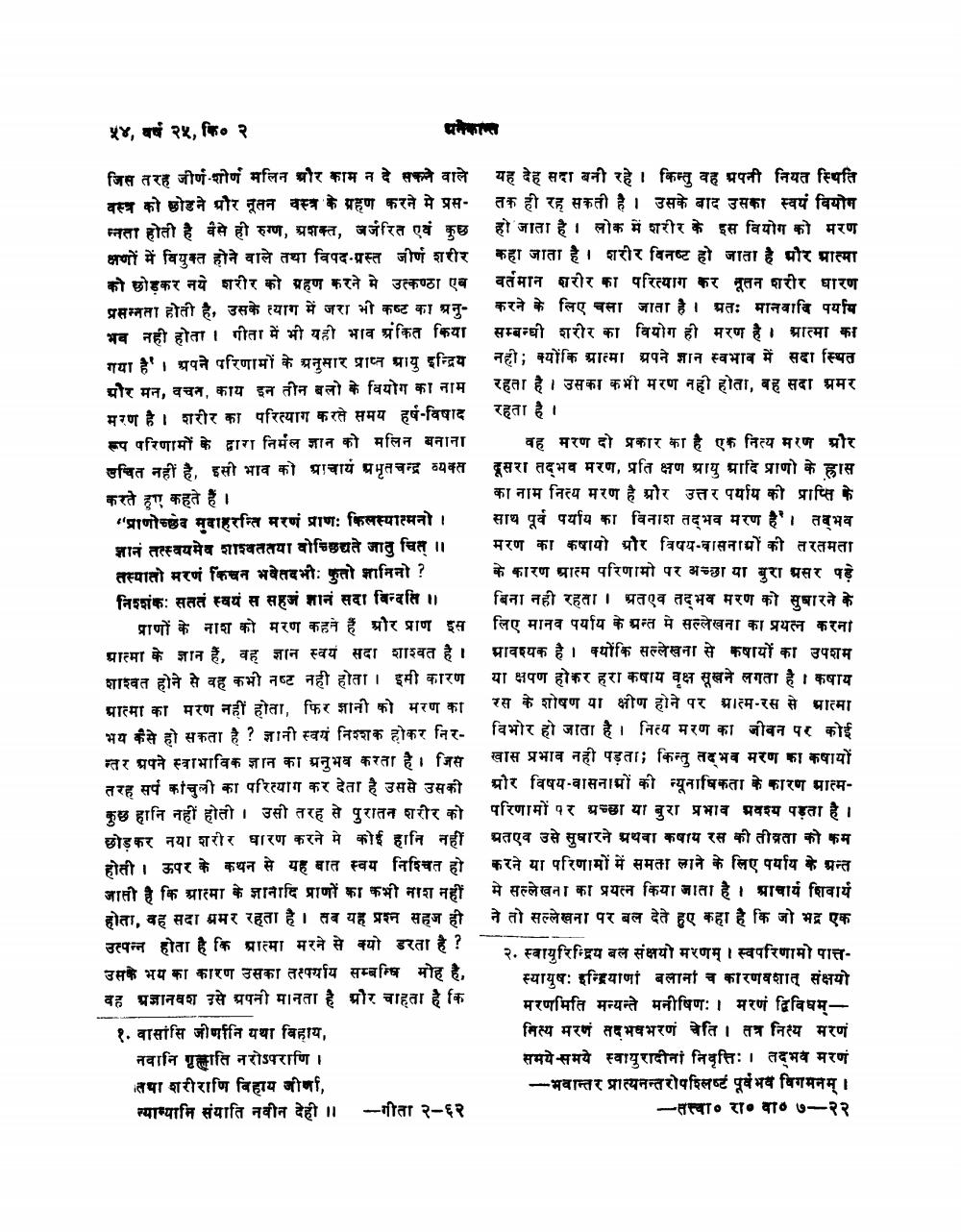________________
५४, वर्ष २५, कि० २
अनेकान्त
जिस तरह जीर्ण-शोर्ण मलिन और काम न दे सकने वाले यह देह सदा बनी रहे। किन्तु वह अपनी नियत स्थिति वस्त्र को छोड़ने और नूतन वस्त्र के ग्रहण करने मे प्रस- तक ही रह सकती है। उसके बाद उसका स्वयं वियोग ग्नता होती है वैसे ही रुग्ण, अशक्त, जर्जरित एवं कुछ हो जाता है। लोक में शरीर के इस वियोग को मरण क्षणों में वियुक्त होने वाले तथा विपद-ग्रस्त जीर्ण शरीर कहा जाता है। शरीर विनष्ट हो जाता है भोर मात्मा को छोड़कर नये शरीर को ग्रहण करने मे उत्कण्ठा एव वर्तमान शरीर का परित्याग कर नूतन शरीर धारण प्रसन्नता होती है, उसके त्याग में जरा भी कष्ट का अनु- करने के लिए चला जाता है। अतः मानवादि पर्याय भब नही होता। गीता में भी यही भाव अंकित किया सम्बन्धी शरीर का वियोग ही मरण है। प्रात्मा का गया है। अपने परिणामों के अनुसार प्राप्त प्रायु इन्द्रिय नही; क्योंकि प्रात्मा अपने ज्ञान स्वभाव में सदा स्थित पौर मन, वचन, काय इन तीन बलो के वियोग का नाम रहता है। उसका कभी मरण नही होता, वह सदा अमर मरण है। शरीर का परित्याग करते समय हर्ष-विषाद रहता है। रूप परिणामों के द्वारा निर्मल ज्ञान को मलिन बनाना वह मरण दो प्रकार का है एक नित्य मरण और खचित नहीं है, इसी भाव को प्राचार्य प्रभृतचन्द्र व्यक्त दूसरा तद्भव मरण, प्रति क्षण प्रायु प्रादि प्राणो के ह्रास करते हुए कहते हैं।
का नाम नित्य मरण है और उत्तर पर्याय की प्राप्ति के "प्राणोच्छेद मुवाहरन्ति मरणं प्राणः किलस्यात्मनो। साथ पूर्व पर्याय का विनाश तद्भव मरण है। तभव जानं तत्स्वयमेव शाश्वततया वोच्छिद्यते जातु चित् ।। मरण का कषायो पौर विषय-वासनामों की तरतमता तस्यातो मरणं किंचन भवेतदभीः कुतो शामिनो? के कारण प्रात्म परिणामो पर अच्छा या बुरा असर पड़े निश्शंकः सततं स्वयं स सहजंशानं सदा विन्दति । बिना नही रहता । प्रतएव तद्भव मरण को सुधारने के
प्राणों के नाश को मरण कहते हैं और प्राण इस लिए मानव पर्याय के अन्त मे सल्लेखना का प्रथल करना मात्मा के ज्ञान हैं, वह ज्ञान स्वयं सदा शाश्वत है। मावश्यक है। क्योंकि सल्लेखना से कषायों का उपशम शाश्वत होने से वह कभी नष्ट नहीं होता। इसी कारण या क्षपण होकर हरा कषाय वृक्ष सूखने लगता है। कषाय मात्मा का मरण नहीं होता, फिर ज्ञानी को मरण का रस के शोषण या क्षीण होने पर प्रात्म-रस से प्रात्मा भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी स्वयं निश्शक होकर निर. विभोर हो जाता है। नित्य मरण का जीवन पर कोई तर अपने स्वाभाविक ज्ञान का अनुभव करता है। जिस खास प्रभाव नहीं पड़ता; किन्तु तदभव मरण का कषायों तरह सर्प काचुली का परित्याग कर देता है उससे उसकी और विषय-वासनामों की न्यूनाधिकता के कारण मात्मकुछ हानि नहीं होती। उसी तरह से पुरातन शरीर को परिणामों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। छोड़ कर नया शरीर धारण करने मे कोई हानि नहीं प्रतएव उसे सुधारने अथवा कषाय रस की तीव्रता को कम होती। ऊपर के कथन से यह बात स्वय निश्चित हो करने या परिणामों में समता लाने के लिए पर्याय के अन्त जाती है कि प्रात्मा के ज्ञानादि प्राणों का कभी नाश नहीं मे सल्लेखना का प्रयत्न किया जाता है। प्राचार्य शिवार्य होता, वह सदा अमर रहता है। तब यह प्रश्न सहज ही ने तो सल्लेखना पर बल देते हुए कहा है कि जो भद्र एक उत्पन्न होता है कि प्रात्मा मरने से क्यो डरता है ?
२. स्वायुरिन्द्रिय बल संक्षयो मरणम् । स्वपरिणामो पात्तउसके भय का कारण उसका तत्पर्याय सम्बन्धि मोह है,
स्यायुषः इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात् संक्षयो वह प्रजानवश उसे अपनी मानता है और चाहता है कि
मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः । मरणं द्विविधम्१. वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय,
मित्य मरणं सदभषभरणं चेति । तत्र नित्य मरणं नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
समये-समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः। तद्भव मरणं तथा शरीराणि विहाय जी ,
-भवान्तर प्रात्यनन्तरोपश्लिष्टं पूर्वभव विगमनम् । न्यान्यानि संयाति नवीन देही ॥ -गीता २-६२
-तत्त्वा० रा.वा०७-२२