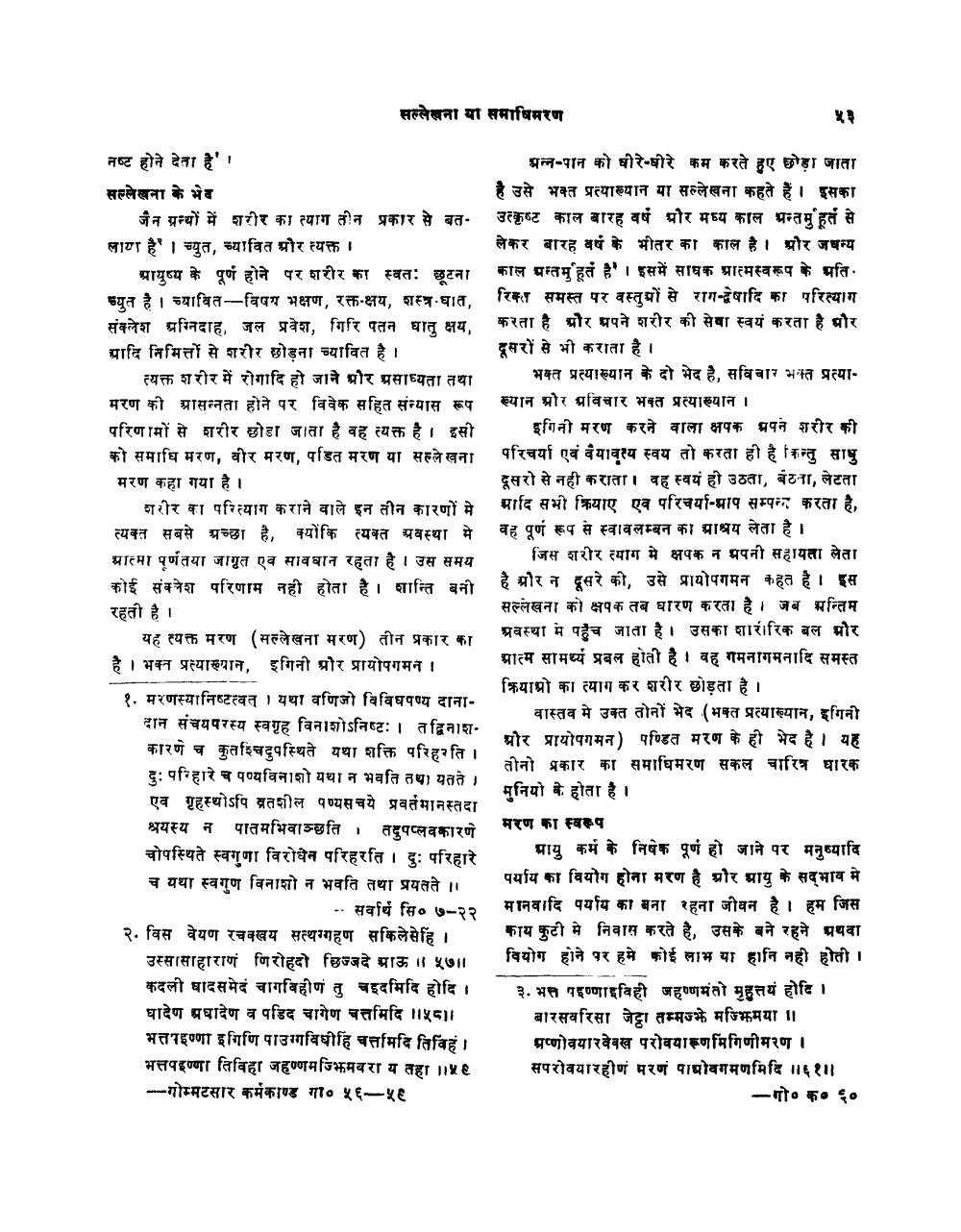________________
सल्लेखना या समाधिमरण
५३
नष्ट होने देता है।
अन्न-पान को धीरे-धीरे कम करते हुए छोड़ा जाता सल्लेखना के भेद
है उसे भक्त प्रत्याख्यान या सल्लेखना कहते हैं। इसका जैन ग्रन्थों में शरीर का त्याग तीन प्रकार से बत- उत्कृष्ट काल बारह वर्ष और मध्य काल अन्तमुहर्त से लाण है । च्युत, च्यावित और त्यक्त ।
लेकर बारह वर्ष के भीतर का काल है। और जघन्य आयुष्य के पूर्ण होने पर शरीर का स्वतः छूटना काल मन्तमहतं है। इसमें साधक प्रात्मस्वरूप के भति. ध्यूत है। च्यावित-विषय भक्षण, रक्त-क्षय, शस्त्र-घात,
रिक्त समस्त पर वस्तुमों से राग-द्वेषादि का परित्याग संक्लेश अग्निदाह, जल प्रवेश, गिरि पतन घात क्षय करता है और अपने शरीर की सेवा स्वयं करता है और पादि मिमित्तों से शरीर छोड़ना च्यावित है।
दूसरों से भी कराता है। त्यक्त शरीर में रोगादि हो जाने और प्रसाध्यता तथा
भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद है, सविचार भक्त प्रत्यामरण की प्रसन्नता होने पर विवेक सहित संन्यास रूप ख्यान और अविचार भक्त प्रत्याख्यान । परिणामों से शरीर छोडा जाता है वह त्यक्त है। इसी इगिनी मरण करने वाला क्षपक अपने शरीर की को समाधि मरण, वीर मरण, पडित मरण या सहले खना परिचर्या एवं वैयावृत्य स्वय तो करता ही है किन्तु साधु मरण कहा गया है।
दूसरो से नही कराता। वह स्वयं ही उठता, बैठना, लेटता शरीर का परित्याग कराने वाले इन तीन कारणों मे मादि सभी क्रियाए एव परिचर्या-पाप सम्पक करता है, त्यक्त सबसे अच्छा है, क्योंकि त्यक्त अवस्था मे वह पूर्ण रूप से स्वावलम्बन का प्राश्रय लेता है। मात्मा पूर्णतया जागृत एव सावधान रहता है । उस समय
जिस शरीर त्याग मे क्षपक न अपनी सहायता लेता कोई संक्लेश परिणाम नही होता है। शान्ति बनी
है और न दूसरे की, उसे प्रायोपगमन कहत है। इस रहती है।
सल्लेखना को क्षपक तब धारण करता है। जब मन्तिम यह त्यक्त मरण (मल्लेखना मरण) तीन प्रकार का
अवस्था में पहुँच जाता है। उसका शारीरिक बल मौर है । भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन ।
मात्म सामर्थ्य प्रबल होती है । वह गमनागमनादि समस्त
क्रियानो का त्याग कर शरीर छोड़ता है। १. मरणस्यानिष्टत्वत । यथा वणिजो विविधपण्य दानादान संचयपरस्य स्वगृह विनाशोऽनिष्टः । तद्विनाश
वास्तव में उक्त तोनों भेद (भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी कारणे च कुतश्चिदुपस्थिते यथा शक्ति परिहरति ।
और प्रायोपगमन) पण्डित मरण के ही भेद है। यह दुः पनिहारे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यतते ।
तीनो प्रकार का समाधिमरण सकल चारित्र धारक एव गृहस्थोऽपि व्रतशील पण्यसचये प्रवर्तमानस्तदा
मुनियो के होता है। श्रयस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपप्लवकारणे
मरण का स्वरूप चोपस्थिते स्वगुणा विरोधेन परिहरति । दु: परिहारे
मायु कर्म के निषेक पूर्ण हो जाने पर मनुष्यादि च यथा स्वगुण विनाशो न भवति तथा प्रयतते ॥
पर्याय का वियोग होना मरण है और प्रायु के सद्भाव मे
.. सर्वार्थ सि०७-२२ मानवादि पयाय का बना रहना जीवन है। हम २. विस वेयण रचक्खय सत्थग्रहण सकिलेसेहिं ।।
काय कुटी मे निवास करते है, उसके बने रहने अथवा उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जदे पाऊ ।। ५७।। वियोग होने पर हमे कोई लाभ या हानि नहीं होती। कदली घादसमेदं चागविहीणं तु चइदमिदि होदि । ३. भत्त पइण्णाइविही जहण्णमंतो महत्तयं होदि । घादेण प्रधादेण व पडिद चागेण चत्तमिदि ॥५॥ बारसवरिसा जेट्टा तम्मज्झे मज्झिमया ॥ भत्तपइण्णा इगिणि पाउग्गविधीहिं चमिदि तिविहं । प्रणोवयारवेवख परोवयारूणमिगिणीमरण । भत्तपदण्णा तिविहा जहण्णमझिमवरा य तहा ॥५६ सपरोवयारहीणं मरणं पापोवगमणमिदि ॥११॥ -गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा०५६-५६
-गो.क.६०