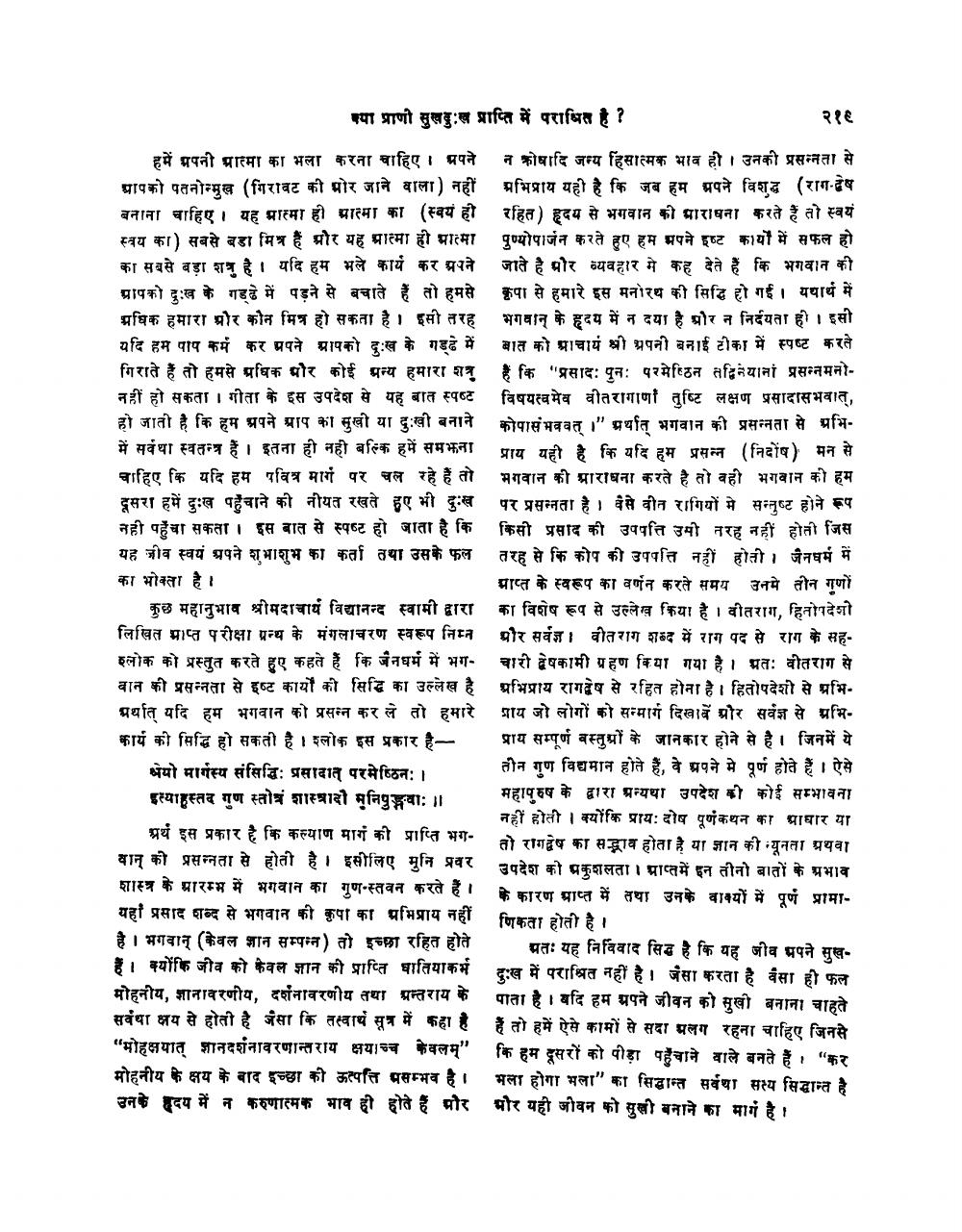________________
क्या प्राणी सुखदुःख प्राप्ति में पराधित है ?
२१९ हमें अपनी प्रात्मा का भला करना चाहिए। अपने न क्रोधादि जन्य हिंसात्मक भाव हो । उनकी प्रसन्नता से पापको पतनोन्मुख (गिरावट की भोर जाने वाला) नहीं अभिप्राय यही है कि जब हम अपने विशुद्ध (राग-द्वेष बनाना चाहिए। यह मात्मा ही पात्मा का (स्वयं ही रहित) हृदय से भगवान की भाराधना करते हैं तो स्वयं स्वय का) सबसे बड़ा मित्र हैं और यह पात्मा ही मात्मा पुण्योपार्जन करते हुए हम अपने इष्ट कार्यों में सफल हो का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम भले कार्य कर अपने जाते है और व्यवहार मे कह देते हैं कि भगवान की प्रापको दुःख के गड्ढे में पड़ने से बचाते हैं तो हमसे कृपा से हमारे इस मनोरथ की सिद्धि हो गई। यथार्थ में अधिक हमारा और कौन मित्र हो सकता है। इसी तरह भगवान् के हृदय में न दया है और न निर्दयता ही । इसी यदि हम पाप कर्म कर अपने प्रापको दुःख के गड्ढे में बात को प्राचार्य श्री अपनी बनाई टीका में स्पष्ट करते गिराते हैं तो हमसे अधिक भोर कोई अन्य हमारा शत्रु हैं कि "प्रसादः पुनः परमेष्ठिन तद्विनेयानां प्रसन्नमनोनहीं हो सकता । गीता के इस उपदेश से यह बात स्पष्ट विषयत्वमेव वीतरागाणां तुष्टि लक्षण प्रसादासभवात्, हो जाती है कि हम अपने पाप का सुखी या दुःखी बनाने कोपासंभववत् ।" अर्थात् भगवान की प्रसन्नता से अभिमें सर्वथा स्वतन्त्र हैं। इतना ही नही बल्कि हमें समझना प्राय यही है कि यदि हम प्रसन्न (निदोष) मन से चाहिए कि यदि हम पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं तो भगवान की प्राराधना करते है तो वही भगवान को हम दूसरा हमें दुःख पहुँचाने की नीयत रखते हुए भी दुःख पर प्रसन्नता है। वैसे वीत रागियों मे सन्तुष्ट होने रूप नही पहुँचा सकता। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रसाद की उपपत्ति उसी तरह नहीं होती जिस यह जीव स्वयं अपने शुभाशुभ का कर्ता तथा उसके फल तरह से कि कोप की उपपत्ति नहीं होती। जैनधर्म में का भोक्ता है।
प्राप्त के स्वरूप का वर्णन करते समय उनमे तीन गुणों __कुछ महानुभाव श्रीमदाचार्य विद्यानन्द स्वामी द्वारा का विशेष रूप से उल्लेख किया है । वीतराग, हितोपदेशो लिखित प्राप्त परीक्षा प्रन्थ के मंगलाचरण स्वरूप निम्न और सर्वज्ञ। वीतराग शब्द में राग पद से राग के सहश्लोक को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जैनधर्म में भग- चारी देषकामी ग्रहण किया गया है। प्रतः वीतराग से वान की प्रसन्नता से इष्ट कार्यों को सिद्धि का उल्लेख है अभिप्राय रागद्वेष से रहित होना है। हितोपदेशी से अभिअर्थात् यदि हम भगवान को प्रसन्न कर ले तो हमारे प्राय जो लोगों को सन्मार्ग दिखावें और सर्वज्ञ से अभिकार्य की सिद्धि हो सकती है । श्लोक इस प्रकार है- प्राय सम्पूर्ण वस्तुओं के जानकार होने से है। जिनमें ये श्रेयो मार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात परमेष्ठिनः।
तीन गुण विद्यमान होते हैं, वे अपने मे पूर्ण होते हैं । ऐसे इत्याहस्तव गुण स्तोत्रं शास्त्रादौ मनिपुङ्गवाः ।।
महापुरुष के द्वारा अन्यथा उपदेश की कोई सम्भावना
नहीं होती । क्योंकि प्राय: दोष पूर्णकथन का प्राधार या अर्थ इस प्रकार है कि कल्याण माग को प्राप्ति भग- तो रागद्वेष का सद्भाव होता है या ज्ञान की न्यूनता अथवा वान् का प्रसन्नता स हाता है। इसलिए मुनि प्रवर उपदेश को प्रकुशलता। प्राप्तमें इन तीनो बातों के प्रभाव शास्त्र के प्रारम्भ में भगवान का गुण-स्तवन करते हैं। के कारण प्राप्त में तथा उनके वाक्यों में पूर्ण प्रामायहाँ प्रसाद शब्द से भगवान की कृपा का अभिप्राय नहीं णिकता होती है। है । भगवान् (केवल ज्ञान सम्पन्न) तो इच्छा रहित होते अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि यह जीव अपने सुखहैं। क्योंकि जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति घातियाकर्भ दुःख में पराश्रित नहीं है। जैसा करता है वैसा ही फल मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय तथा अन्तराय के पाता है। यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते सर्वथा क्षय से होती है जैसा कि तस्वार्थ सूत्र में कहा है हैं तो हमें ऐसे कामों से सदा अलग रहना चाहिए जिनसे "मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्त राय क्षयाच्च केवलम्" कि हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले बनते हैं। "कर मोहनीय के क्षय के बाद इच्छा की उत्पत्ति असम्भव है। भला होगा भला" का सिद्धान्त सर्वथा सत्य सिद्धान्त है उनके हृदय में न करुणात्मक भाव ही होते हैं और भौर यही जीवन को सुखी बनाने का मार्ग है।