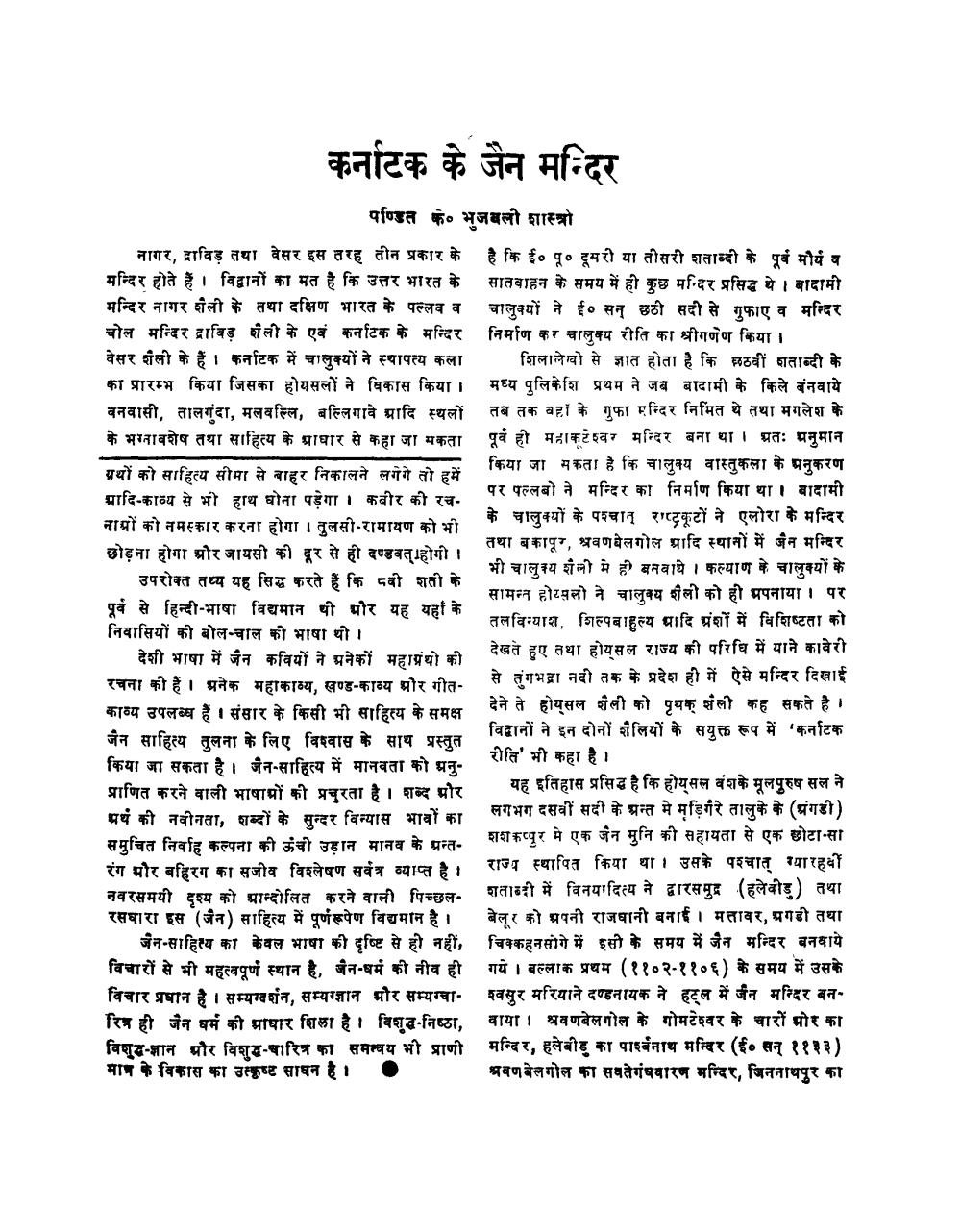________________
कर्नाटक के जैन मन्दिर
पण्डित के० भुजबलो शास्त्रो नागर, द्राविड़ तथा वेसर इस तरह तीन प्रकार के है कि ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी के पूर्व मौर्य व मन्दिर होते हैं। विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत के सातवाहन के समय में ही कुछ मन्दिर प्रसिद्ध थे। बादामी मन्दिर नागर शैली के तथा दक्षिण भारत के पल्लव व चालुक्यों ने ई० सन् छठी सदी से गुफाए व मन्दिर चोल मन्दिर द्राविड़ शैली के एवं कर्नाटक के मन्दिर निर्माण कर चालुक्य रीति का श्रीगणेण किया। वेसर शैली के हैं । कर्नाटक में चालुक्यों ने स्थापत्य कला शिलालेखो से ज्ञात होता है कि छठवीं शताब्दी के का प्रारम्भ किया जिसका होयसलों ने विकास किया। मध्य पुलिकेशि प्रथम ने जब बादामी के किले बनवाये वनवासी, तालगुंदा, मलवल्लि, बल्लिगावे प्रादि स्थलों तब तक वहाँ के गुफा मन्दिर निर्मित थे तथा मगलेश के के भग्नावशेष तथा साहित्य के प्राधार से कहा जा सकता पूर्व ही महाकटेश्वर मन्दिर बना था। प्रतः अनुमान प्रथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेगे तो हमें
किया जा सकता है कि चालुक्य वास्तुकला के अनुकरण मादि-काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। कबीर की रच
पर पल्लबो ने मन्दिर का निर्माण किया था। बादामी नामों को नमस्कार करना होगा । तुलसी-रामायण को भी
के चालुक्यों के पश्चात् राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मन्दिर छोड़ना होगा और जायसी की दूर से ही दण्डवत्।होगी।
तथा बकापूर, श्रवणबेलगोल प्रादि स्थानों में जैन मन्दिर
भी चालुक्य शैली में ही बनवाये । कल्याण के चालुक्यों के उपरोक्त तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि ८वी शती के
सामन्त होसलो ने चालुक्य शैली को ही अपनाया। पर पूर्व से हिन्दी-भाषा विद्यमान थी और यह यहाँ के निवासियों की बोल-चाल की भाषा थी।
तलविन्याश, शिल्प बाहुल्य प्रादि ग्रंशों में विशिष्टता को देशी भाषा में जैन कवियों ने अनेकों महाग्रंथो की
देखते हुए तथा होयसल राज्य की परिधि में याने कावेरी रचना की हैं। अनेक महाकाव्य, खण्ड-काव्य और गीत
से तुंगभद्रा नदी तक के प्रदेश ही में ऐसे मन्दिर दिखाई काव्य उपलब्ध हैं । संसार के किसी भी साहित्य के समक्ष
देने ते होयसल शैली को पृथक् शैली कह सकते है । जैन साहित्य तुलना के लिए विश्वास के साथ प्रस्तुत
विद्वानों ने इन दोनों शैलियों के सयुक्त रूप में कर्नाटक किया जा सकता है। जैन-साहित्य में मानवता को अनु
रीति' भी कहा है। प्राणित करने वाली भाषामों की प्रचुरता है । शब्द मोर
यह इतिहास प्रसिद्ध है कि होयसल वंशके मूलपुरुष सल ने मथं की नवीनता, शब्दों के सुन्दर विन्यास भावों का
लगभग दसवीं सदी के अन्त मे मड़िगैरे तालुके के (अंगडी) समुचित निर्वाह कल्पना की ऊंची उड़ान मानव के अन्त
शशाप्पुर मे एक जैन मुनि की सहायता से एक छोटा-सा रंग और बहिरग का सजीव विश्लेषण सर्वत्र व्याप्त है।
राज्य स्थापित किया था। उसके पश्चात् ग्यारहवीं नवरसमयी दृश्य को प्रान्दोलित करने वाली पिच्छल शताब्दी में विनयादित्य ने द्वारसमुद्र (हलेवीड) तथा रसधारा इस (जैन) साहित्य में पूर्णरूपेण विद्यमान है। बेलर को अपनी राजधानी बनाई। मत्तावर, अगडी तथा
जैन-साहित्य का केवल भाषा की दृष्टि से ही नहीं, चिक्कहनसांगे में इसी के समय में जैन मन्दिर बनवाये विचारों से भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैन-धर्म की नीव ही गये । बल्लाक प्रथम (११०२-११०६) के समय में उसके विचार प्रधान है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चा- श्वसुर मरियाने दण्डनायक ने हल में जैन मन्दिर बनरित्र ही जैन धर्म की प्राधार शिला है। विशुद्ध-निष्ठा, वाया। श्रवणबेलगोल के गोमटेश्वर के चारों मोर का विशुद्ध-ज्ञान पौर विशुद्ध-चारित्र का समन्वय भी प्राणी मन्दिर, हलेबीडु का पार्श्वनाथ मन्दिर (ई.सन् ११३३) मात्र के विकास का उत्कृष्ट साधन है।
श्रवणबेलगोल का सबतेगंधवारण मन्दिर, जिननाथपुर का