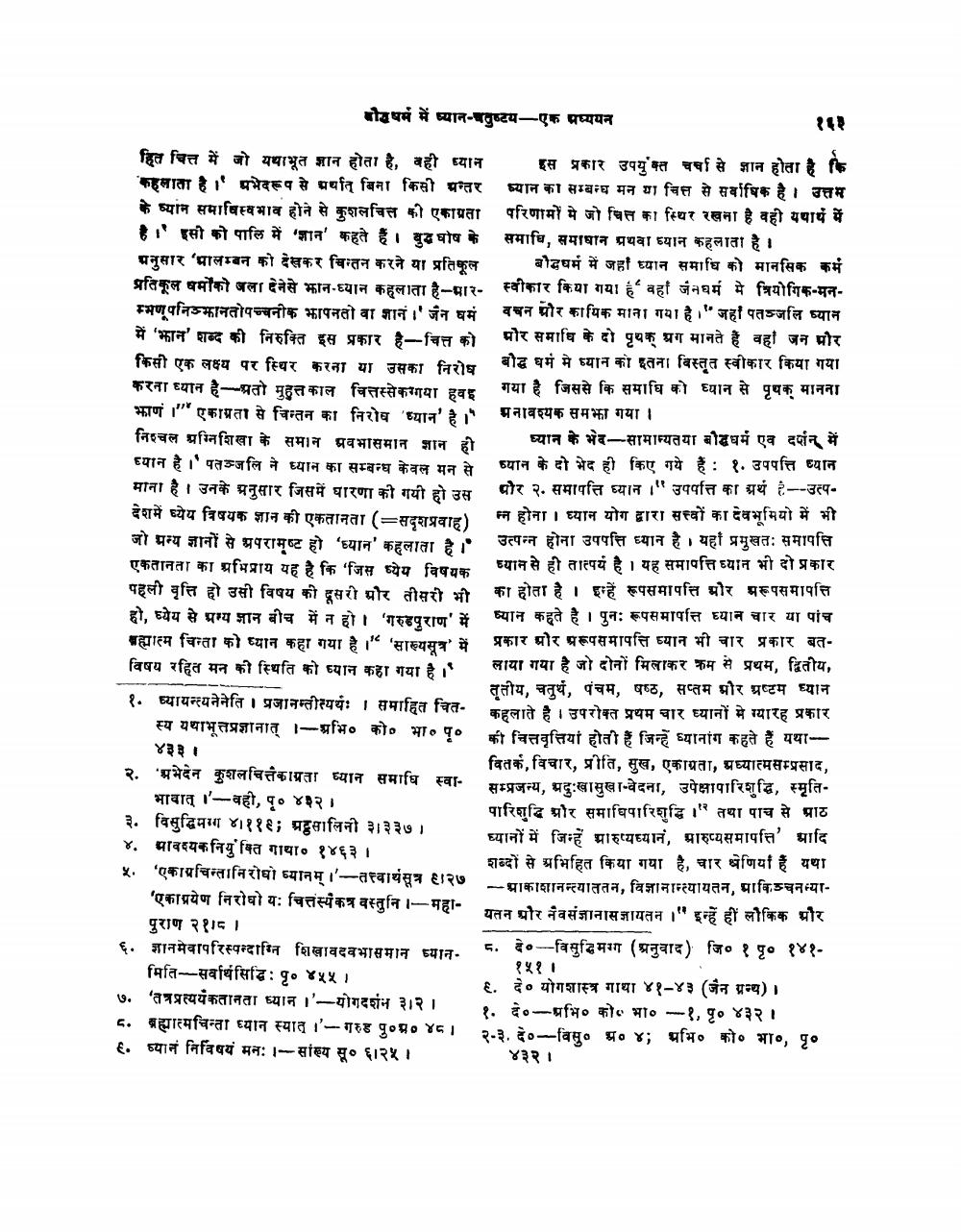________________
बौधर्म में ध्यान-चतुष्टय-एक अध्ययन
हित चित्त में जो यथाभूत ज्ञान होता है, वही ध्यान इस प्रकार उपयुक्त चर्चा से ज्ञान होता है कि कहलाता है। प्रभेदरूप से अर्थात् बिना किसी अन्तर ध्यान का सम्बन्ध मन या चित्त से सर्वाधिक है। उत्तम के ध्यान समाधिस्वभाव होने से कुशलचित्त की एकाग्रता परिणामों मे जो चित्त का स्थिर रखना है वही यथार्थ में है। इसी को पालि में 'शान' कहते हैं। बुद्धघोष के समाधि, समाधान प्रथवा ध्यान कहलाता है। अनुसार 'मालम्बन को देखकर चिन्तन करने या प्रतिकूल बौद्धधर्म में जहां ध्यान समाधि को मानसिक कर्म प्रतिकूल धोको जला देनेसे झान-ध्यान कहलाता है-मार- स्वीकार किया गया है वहाँ जनधर्म मे त्रियोगिक-मनम्भणपनिझानतोपच्चनीक झापनतो वा ज्ञानं । जैन धर्म वचन पौर कायिक माना गया है। "जहाँ पतञ्जलि ध्यान में 'झान' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है-चित्त को मोर समाधि के दो पृथक प्रग मानते हैं वहाँ जन पौर किसी एक लक्ष्य पर स्थिर करना या उसका निरोष चा
बौद्ध धर्म मे ध्यान को इतना विस्तृत स्वीकार किया गया करना ध्यान है-प्रतो मुहत्त काल चित्तस्सेकग्गया हवह गया है जिससे कि समाधि को ध्यान से पृथक मानना झाणं ।"" एकाग्रता से चिन्तन का निरोष 'ध्यान' है। अनावश्यक समझा गया। निश्चल अग्निशिखा के समान प्रवभासमान ज्ञान ही
ध्यान के भेद-सामान्यतया बौद्धधर्म एव दर्शन में ध्यान है ।' पतञ्जलि ने ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ध्यान कदा भद हा । माना है। उनके अनुसार जिसमें धारणा की गयी हो उस पोर २. समापत्ति ध्यान ।" उपपत्ति का अर्थ है--उत्पदेशमें ध्येय विषयक ज्ञान की एकतानता (=सदृशप्रवाह)
न होना । ध्यान योग द्वारा सत्त्वों का देवभूमियो में भी जो अन्य ज्ञानों से अपरामष्ट हो 'ध्यान' कहलाता है।'
उत्पन्न होना उपपत्ति ध्यान है। यहाँ प्रमुखतः समापत्ति एकतानता का अभिप्राय यह है कि 'जिस ध्येय विषयक
ध्यान से ही तात्पर्य है । यह समापत्ति ध्यान भी दो प्रकार पहली वृत्ति हो उसी विषय की दूसरी और तीसरी भी का होता है । इन्हें रूपसमापत्ति मौर मरूपसमापत्ति हो, ध्येय से प्रम्य ज्ञान बीच में न हो। 'गरुडपुराण' में
ध्यान कहते है । पुनः रूपसमापत्ति ध्यान चार या पांच ब्रह्मात्म चिन्ता को ध्यान कहा गया है ।" 'साख्यसूत्र' में प्रकार पोर प्ररूपसमापत्ति ध्यान भा चार प्रकार बतविषय रहित मन की स्थिति को ध्यान कहा गया है।
लाया गया है जो दोनों मिलाकर कम से प्रथम, द्वितीय,
तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम ध्यान १. घ्यायन्स्यनेनेति । प्रजानन्तीत्यर्थः । समाहित चित
कहलाते है । उपरोक्त प्रथम चार ध्यानों में ग्यारह प्रकार स्य यथाभूत्तप्रज्ञानात् ।-अभि० को भा०पू० को चित्तवत्तियां होती हैं जिन्हें ध्यानांग कहते हैं यथा
वितर्क,विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, अध्यात्मसम्प्रसाद, २. 'मभेदेन कुशलचित्तकाग्रता ध्यान समाधि स्वा
सम्प्रजन्य, प्रदुःखासुखा-वेदना, उपेक्षापारिशुद्धि, स्मृतिभावात् ।'-वही, पृ० ४३२।
पारिशुद्धि और समाधिपारिशुद्धि । २ तथा पाच से पाठ ३. विसुद्धिमग्ग ४।११६, अट्टसालिनी ३१३३७ ।
ध्यानों में जिन्हें मारुप्यध्यानं, प्रारुप्यसमापत्ति' आदि ४. मावश्यक नियुक्ति गाथा० १४६३ । ५. 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्।'-तत्त्वार्थसूत्र ६२७
शब्दों से अभिहित किया गया है, चार श्रेणियाँ हैं यथा
-माकाशानन्त्याततन, विज्ञानान्त्यायतन, माकिञ्चनन्या'एकाग्रयेण निरोधो यः चित्तस्यैकत्र वस्तुनि ।-महा
यतन पोर नवसंज्ञानासज्ञायतन ।" इन्हें ही लौकिक और पुराण २१८ । ६. ज्ञानमेवापरिस्पन्दाग्नि शिखावदवभासमान ध्यान. ८. दे०-विसुद्धिमग्ग (अनुवाद) जि०१ पृ० १४१. मिति-सर्वार्थसिद्धिः पृ० ४५५ ।
६. दे. योगशास्त्र गाथा ४१-४३ (जैन ग्रन्थ)। ७. 'तत्रप्रत्ययंकतानता ध्यान ।'-योगदर्शन ३।२। १. दे०-अभि० को भा० -१, पृ० ४३२ । ८. ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्यात् ।'-गरुड पु०म०४८। २-३. दे०-विम० अ०४; भभि० को० भा०, पृ० ६. ध्यानं निविषयं मनः । -सांख्य सू० ६२५ ।
४३२।