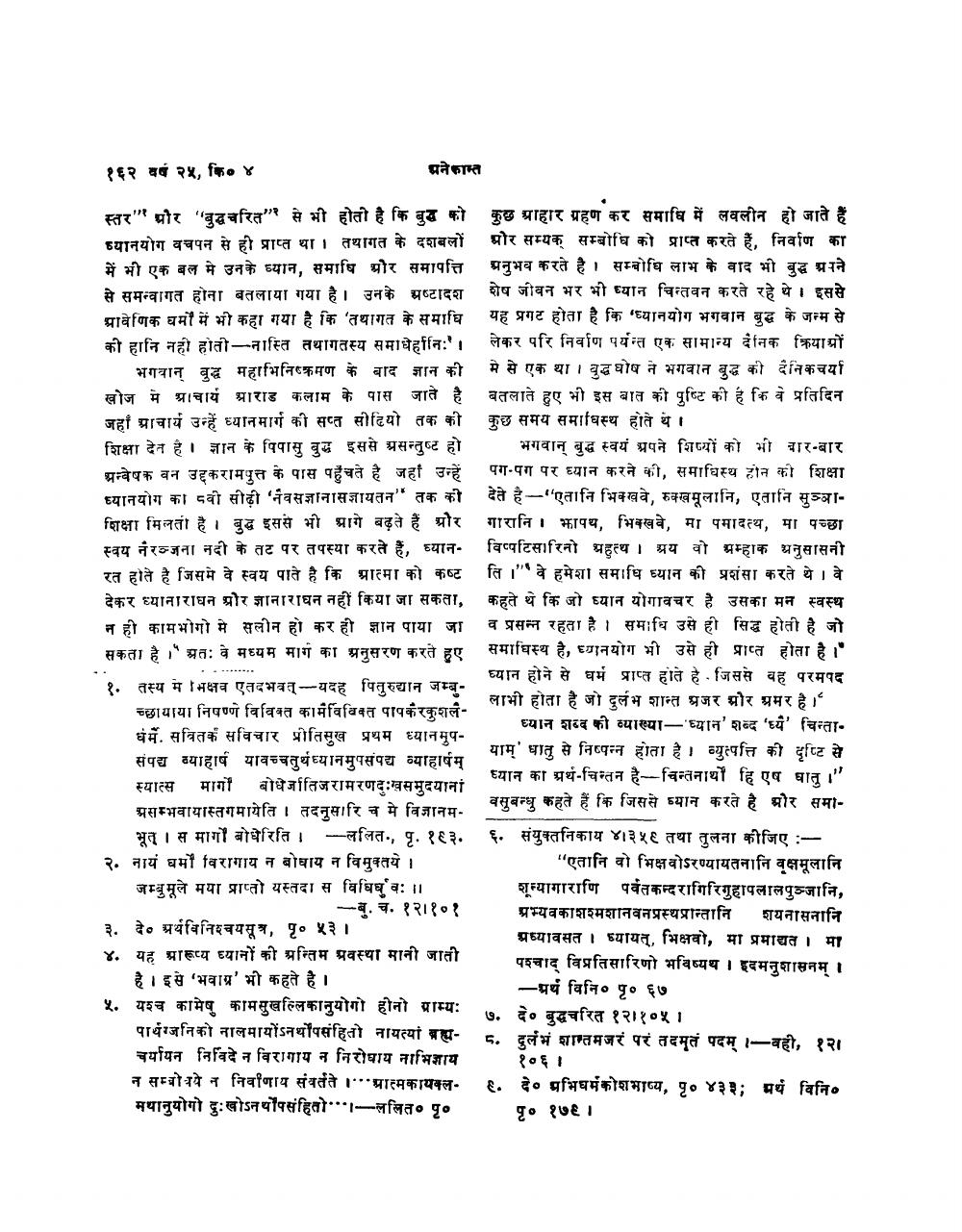________________
१६२ वर्ष २५, कि० ४
अनेकान्त
स्तर"" मोर "बुद्धचरित"" से भी होती है कि बुद्ध को ध्यानयोग वचपन से ही प्राप्त था । तथागत के दशबलों में भी एक बल मे उनके ध्यान, समाधि और समापत्ति से समन्वागत होना बतलाया गया है। उनके अष्टादश श्रावेणिक धर्मों में भी कहा गया है कि 'तथागत के समाधि की हानि नही होती नास्ति तथागतस्य समानः ।
भगवान् बुद्ध महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज मे श्राचार्य श्राराड कलाम के पास जाते है जहाँ प्राचार्य उन्हें ध्यानमार्ग की सप्त सीढ़ियों तक की शिक्षा देत है। ज्ञान के पिपासु बुद्ध इससे प्रसन्तुष्ट हो अन्वेषक बन उकरामत के पास पहुंचते है जहाँ उन्हें ध्यानयोग का वो सोढी 'नवज्ञानासहायतन" तक की शिक्षा मिलती है। बुद्ध इससे भी आगे बढ़ते हैं और स्वय नरञ्जना नदी के तट पर तपस्या करते हैं, ध्यानरत होते है जिसमे वे स्वयं पाते है कि श्रात्मा को कष्ट देकर ध्यानाराधन और ज्ञानाराघन नहीं किया जा सकता, न ही कामभोगो मे सलीन हो कर ही ज्ञान पाया जा सकता है ।" अतः वे मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए १ तस्य मे शिव एतदभवत्यदह पितुरुद्यान जम्बुछायाया निषण्णे विविश्व कामविति पापककुम
सवितर्क विचार प्रीतिमुख प्रथम ध्यानमुपसंपद्य व्याहार्ष यावच्चतुर्थध्यानमुपसंपद्य व्याहार्षम् स्यात्स मार्गो बोधेजतिजरामरणदुःखसमुदयानां असम्भवायास्तगमायेति तदनुसारि च मे विज्ञानम भूस मार्गों बोचेरिति जति पृ. १९३. २. नायं घर्मो विरागाय न बोघाय न विमुक्तये । जम्बुले मया प्राप्तो यस्तदा स विधिवः ।। - बु. च. १२१०१
।
,
३. दे० अर्थविनिश्चयसूत्र, पृ० ५३ । ४. यह श्ररूप्य ध्यानों की अन्तिम अवस्था मानी जाती है। इसे 'भवान' भी कहते है।
५. यश्च कामेषु कामसुखल्लिकानुयोगो होनो ग्राम्य: पार्थग्जनको नालमायोंऽनर्थोपसंहितो नायत्यां ब्रह्मचर्यायन निविदेन विरागाय न निरोघाय नाभिज्ञाय न सम्बोधन निर्वाणाय संवर्तते । श्रात्मकायक्ल मयानुयोगो दुःखोपसंहितो-ललित० पृ०
कुछ श्राहार ग्रहण कर समाधि में लवलीन हो जाते हैं और सम्यक् सम्बोधि को प्राप्त करते हैं, निर्वाण का अनुभव करते है । सम्बोधि लाभ के बाद भी बुद्ध अपने शेष जीवन भर भी ध्यान चिन्तवन करते रहे थे । इससे यह प्रगट होता है कि 'ध्यानयोग भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर परिनिर्वाण पर्यन्त एक सामान्य दैनिक क्रियाओं मे से एक था। बुद्धघोष ने भगवान बुद्ध की दैनिकचर्या बतलाते हुए भी इस बात की पुष्टि की है कि वे प्रतिदिन कुछ समय समाधिस्थ होते थे ।
भगवान् बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों को भी बार-बार पग-पग पर ध्यान करने की, समाधिस्थ होन की शिक्षा देते है एतानि भिख मूलानि एतानि सुब्बागारानि । झापथ, भिक्खवे, मा पमादत्य, मा पच्छा विपसारिनो अहुत्थ । श्रय वो अम्हाक अनुसासनी ति ।"" वे हमेशा समाधि ध्यान की प्रशंसा करते थे । वे कहते थे कि जो ध्यान योगावचर है उसका मन स्वस्थ व प्रसन्न रहता है । समाधि उसे ही सिद्ध होती है जो समाधिस्य है, योग भी उसे ही प्राप्त होता है। ध्यान होने से धर्म प्राप्त होते है जिससे वह परमपद लाभी होता है जो दुर्लभ शान्त अजर और अमर है ।"
"
ध्यान शब्द की व्याख्या- 'ध्यान' शब्द 'ध्ये' चिन्तायाम्' धातु से निष्पन्न होता है । व्युत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान का अर्थ-पितन हैन्तिनाय हि एवं धातु " वसुबन्धु कहते हैं कि जिससे ध्यान करते है और समा६. संयुक्तनिका ४२५६ तथा तुलना कीजिए :
"एतानि वो भिक्षवोऽरण्यायतनानि वृक्षमूलानि शुभ्यागाराणि पर्वतकन्दरागिरिगुहापलालजानि, अभ्यवकाशश्मशानवनप्रस्थ प्रान्तानि शयनासनानि अध्यावसत। ध्यायत्, भिक्षवो, मा प्रमाद्यत । मा पश्चाद् विप्रतिसारिणो भविष्यथ । इदमनुशासनम् ॥ -अर्थं विनि० पृ० ६७
दे० बुद्धचरित १२ १०५ ।
दुर्लभ शान्तमजरं परं तदमृतं पदम् । वही, १२॥
१०६ ।
९.
दे० श्रभिधर्मकोशभाष्य, पृ० ४३३; मर्थं विनि० पृ० १७६ ।
७.
८.
,