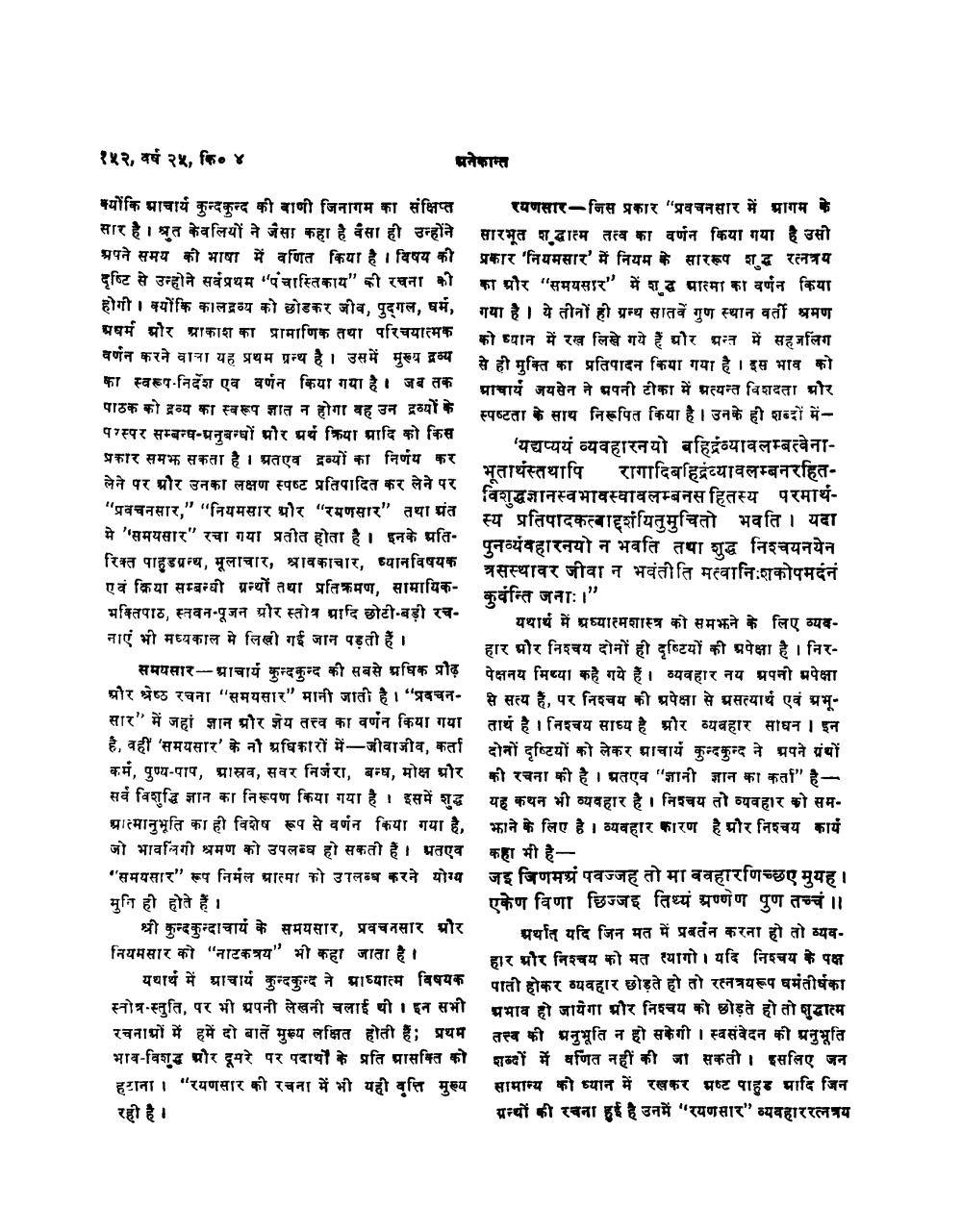________________
१५२, वर्ष २५, कि० ४
क्योंकि प्राचार्य कुन्दकुन्द की बाणी जिनागम का संक्षिप्त सार है। केवलियों ने जैसा कहा है वैसा ही उन्होंने अपने समय की भाषा में वर्णित किया है । विषय की दृष्टि से उन्होंने सर्वप्रथम "पंचास्तिकाय" की रचना की होगी। क्योंकि कालद्रव्य को छोड़कर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और प्रकाश का प्रामाणिक तथा परिचयात्मक वर्णन करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ है । उसमें मुख्य द्रव्य का स्वरूप निर्देश एव वर्णन किया गया है। जब तक पाठक को द्रव्य का स्वरूप ज्ञात न होगा वह उन द्रव्यों के परस्पर सम्बन्धधनुबन्धों और पर्व क्रिया मादि को किस प्रकार समझ सकता है । अतएव द्रव्यों का निर्णय कर लेने पर प्रौर उनका लक्षण स्पष्ट प्रतिपादित कर लेने पर "प्रवचनसार," "नियमसार पोर "रमणसार" तथा मंत मे "समयसार" रचा गया प्रतीत होता है। इनके प्रति रिक्त पाहुडग्रन्थ, मूलाचार, श्रावकाचार, ध्यानविषयक एवं क्रिया सम्बन्धी ग्रन्थों तथा प्रतिक्रमण, सामायिकभक्तिपाठ, स्तवन-पूजन प्रोर स्तोष यादि छोटी-बड़ी रचनाएं भी मध्यकाल मे लिखी गई जान पड़ती हैं ।
अनेकान्त
समयसार - प्राचार्य कुन्दकुन्द की सबसे अधिक प्रौढ़ श्रीर श्रेष्ठ रचना "समयसार" मानी जाती है । "प्रवचनसार" में जहां ज्ञान और ज्ञेय तत्त्व का वर्णन किया गया है, वहीं 'समयसार' के नौ अधिकारों में- जीवाजीव, कर्ता कर्म, पुण्य-याच घास, सवर निर्जरा, बन्ध, मोल भौर सर्व विशुद्धि ज्ञान का निरूपण किया गया है । इसमें शुद्ध श्रात्मानुभूति का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जो भावलिंगी श्रमण को उपलब्ध हो सकती हैं। अतएव "समयसार" रूप निर्मल आत्मा को उपलब्ध करने योग्य मुनि ही होते हैं।
श्री कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार, प्रवचनसार और नियमसार को "नाटकत्रय" भी कहा जाता है । यथार्थ में प्राचार्य कुन्दकुन्द ने प्राध्यात्म विषयक स्तोत्र स्तुति पर भी अपनी लेखनी चलाई थी। इन सभी रचनाओं में हमें दो बातें मुख्य लक्षित होती हैं प्रथम भाव-विशुद्ध और दूसरे पर पदार्थों के प्रति प्रासक्ति को हटाना। " रयणसार की रचना में भी यही वृत्ति मुख्य रही है।
रयणसार - जिस प्रकार " प्रवचनसार में आगम के सारभूत द्वारम तत्व का वर्णन किया गया है उसी प्रकार 'नियमसार' में नियम के साररूप शुद्ध रत्नत्रय का और "समयसार" में शुद्ध मात्मा का वर्णन किया गया है। ये तीनों ही ग्रन्थ सातवें गुण स्थान वर्ती श्रमण को ध्यान में रख लिखे गये हैं और अन्त में सहजलिंग से ही मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इस भाव को प्राचार्य जयसेन ने अपनी टीका में अत्यन्त विशदता और स्पष्टता के साथ निरूपित किया है। उनके ही शब्दों में
'यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिग्यावलम्बत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिद्रिव्यावलम्बनरहितविशुद्धज्ञानस्वभावस्वावलम्बनस हितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्दर्शयितुमुचितो भवति । यदा पुनव्यवहारनयो न भवति तथा शुद्ध निश्चयनयेन त्रसस्थावर जीवा न भवतीति मत्वा निःशकोपमदंनं कुर्वन्ति जनाः । "
यथार्थ में अध्यात्मशास्त्र को समझने के लिए व्यव हार और निश्चय दोनों ही दृष्टियों की अपेक्षा है । निरपेक्षनय मिथ्या कहे गये हैं । व्यवहार नय प्रपनी मपेक्षा से सत्य है, पर निश्चय की अपेक्षा से प्रसत्यार्थ एवं प्रभूतार्थ है । निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन । इन दोनों दृष्टियों को लेकर प्राचार्य कुन्दकुन्द ने अपने ग्रंथों की रचना की है । प्रतएव "ज्ञानी ज्ञान का कर्ता" है - यह कथन भी व्यवहार है। निश्चय तो व्यवहार को सम झाने के लिए है। व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य कहा भी है
जई जिणमश्रं पवज्जह तो मा बवहारणिच्छए मुयह । एकेण विणा छिज्जद्द तिथ्यं प्रण्णेण पुण तभ्वं ॥
अर्थात् यदि जिन मत में प्रवर्तन करना हो तो व्यव हार और निश्चय को मत त्यागो। यदि निश्चय के पक्ष पाती होकर व्यवहार छोड़ते हो तो रत्नत्रयरूप घर्मतीर्धका प्रभाव हो जायेगा और निश्चय को छोड़ते हो तो शुद्धात्म तत्व की धनुभूति न हो सकेगी। स्वसंवेदन की अनुभूति शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। इसलिए जन सामान्य को ध्यान में रखकर भ्रष्ट पाहुड भादि जिन ग्रन्थों की रचना हुई है उनमें "रयणसार" व्यवहाररत्नत्रय