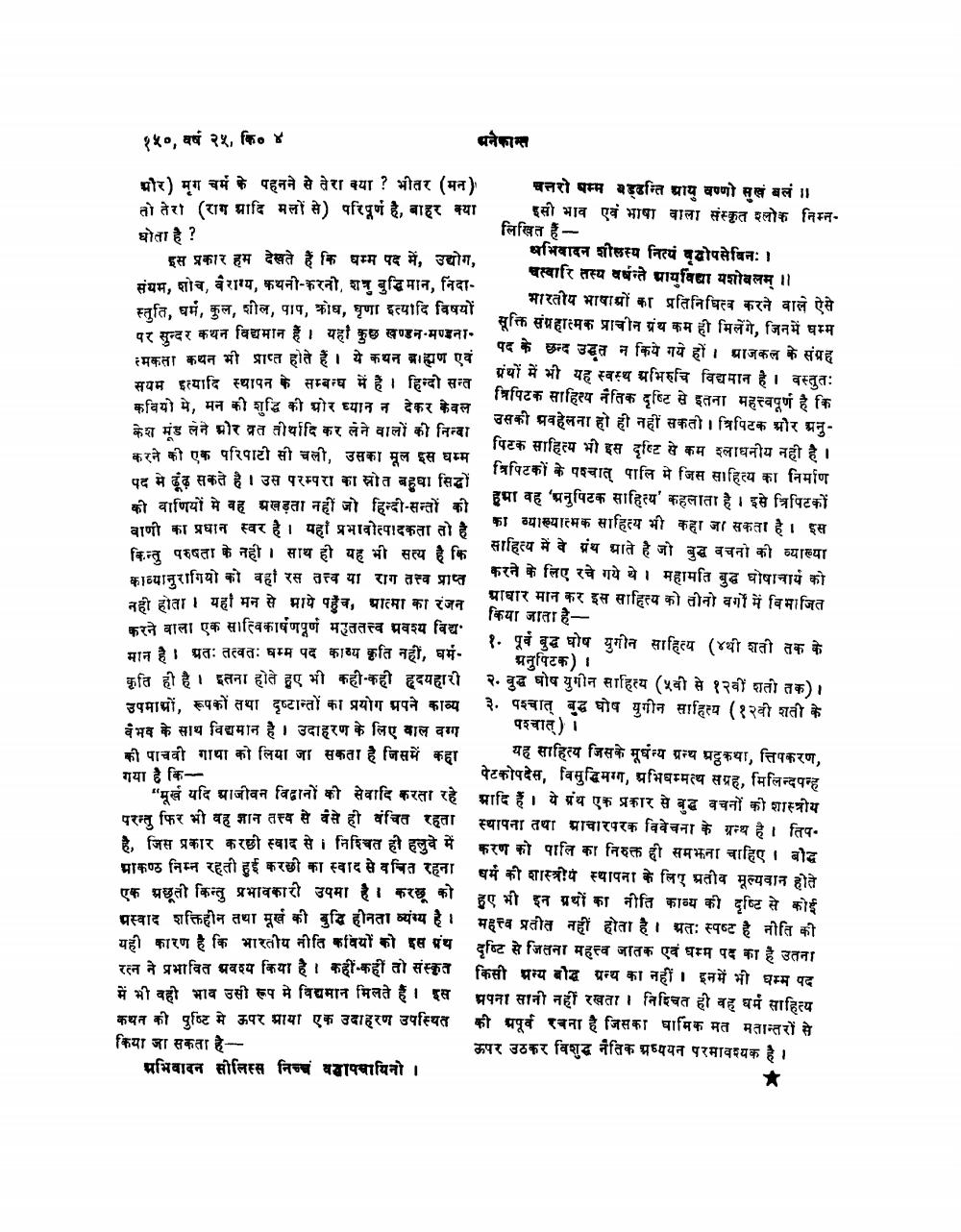________________
१५०, वर्ष २५, कि.४
अनेकान्त
प्रौर) मग चर्म के पहनने से तेरा क्या ? भीतर (मन) उत्तरो पम्म बड्ढन्ति प्रायु वण्णो सुखं बलं ॥ तो तेरी (राग मादि मलों से) परिपूर्ण है, बाहर क्या इसी भाव एवं भाषा वाला संस्कृत श्लोक निम्नधोता है ?
लिखित है
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। इस प्रकार हम देखते हैं कि धम्म पद में, उद्योग,
चत्वारि तस्य वर्षन्ते प्रायविद्या यशोवलम् ॥ संयम, शोच, वैराग्य, कथनी-करनी, शत्रु बुद्धिमान, निंदा
भारतीय भाषामों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे स्तुति, धर्म, कुल, शील, पाप, क्रोध, घृणा इत्यादि विषयों
सूक्ति संग्रहात्मक प्राचीन ग्रंथ कम ही मिलेंगे, जिनमें धम्म पर सुन्दर कथन विद्यमान हैं। यहाँ कुछ खण्डन-मण्डना.
पद के छन्द उद्धृत न किये गये हों। प्राजकल के संग्रह स्मकता कथन भी प्राप्त होते हैं। ये कथन ब्राह्मण एवं
ग्रंथों में भी यह स्वस्थ अभिरुचि विद्यमान है। वस्तुतः सयम इत्यादि स्थापन के सम्बन्ध में हैं। हिन्दी सन्त
त्रिपिटक साहित्य नैतिक दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण है कि कवियो मे, मन की शुद्धि की भोर ध्यान न देकर केवल
उसकी अवहेलना हो ही नहीं सकती। त्रिपिटक और अनुकेश मुंड लेने मोर व्रत तीर्थादि कर लेने वालों की निन्दा
पिटक साहित्य भी इस दृष्टि से कम इलाधनीय नही है। करने की एक परिपाटी सी चली, उसका मूल इस धम्म
त्रिपिटकों के पश्चात् पालि मे जिस साहित्य का निर्माण पद मे ढूंढ़ सकते है । उस परम्परा का स्रोत बहुधा सिद्धों
हुमा वह 'अनुपिटक साहित्य' कहलाता है । इसे त्रिपिटकों की वाणियों में वह प्रखड़ता नहीं जो हिन्दी-सन्तों की
का व्याख्यात्मक साहित्य भी कहा जा सकता है। इस वाणी का प्रधान स्वर है। यहाँ प्रभावोत्पादकता तो है
साहित्य में वे ग्रंथ माते है जो बुद्ध वचनो की व्याख्या किन्तु परुषता के नही। साथ ही यह भी सत्य है कि
करने के लिए रचे गये थे। महामति बुद्ध घोषाचार्य को काव्यानुरागियो को वहाँ रस तत्त्व या राग तत्त्व प्राप्त
प्राधार मान कर इस साहित्य को तीनो वर्गों में विभाजित नही होता। यहाँ मन से माये पहुँच, पात्मा का रंजन
किया जाता हैकरने वाला एक सात्विकार्षणपूर्ण मस्ततत्त्व अवश्य विद्या
१. पूर्व बुद्ध घोष युगीन साहित्य (४थी शती तक के मान है। प्रतः तत्वतः धम्म पद काव्य कृति नहीं, धर्म
अनुपिटक)। कृति ही है। इतना होते हुए भी कही कही हृदयहारी २. बुद्ध घोष युगीन साहित्य (५वी से १२वीं शती तक)। उपमानों, रूपकों तथा दृष्टान्तों का प्रयोग अपने काव्य ३. पश्चात् बुद्ध घोष युगीन साहित्य (१२वी शती के वैभव के साथ विद्यमान है। उदाहरण के लिए वाल वग्ग पश्चात्)। की पाचवी गाथा को लिया जा सकता है जिसमें कहा यह साहित्य जिसके मूर्धन्य ग्रन्थ प्रकथा, तिपकरण, गया है कि
पेटकोपदेस, विसुद्धिमग्ग, अभिधम्मत्थ सग्रह, मिलिन्दपन्ह मख यदि माजीवन विद्वानों की सेवादि करता रहे मादि हैं। ये ग्रंथ एक प्रकार से बद्ध वचनों की शास्त्रीय पर फिर भी वह ज्ञान तत्व से वैसे ही वंचित रहता स्थापना तथा प्राचारपरक विवेचना के ग्रन्थ है। तिप. है. जिस प्रकार करछी स्वाद से। निश्चित ही हलुवे में करण को पालि का निरुक्त ही समझना चाहिए । बौद्ध
कण्ठ निम्न रहती हई करछी का स्वाद से वचित रहना धर्म की शास्त्रीय स्थापना के लिए प्रतीव मूल्यवान होते एक अछुती किन्तु प्रभावकारी उपमा है। करछू को भी न पचों का, प्रस्वाद शक्तिहीन तथा मूर्ख की बुद्धि हीनता व्यंग्य है। महत्त्व प्रतीत नहीं होता है। अतः स्पष्ट है नीति की यही कारण है कि भारतीय नीति कवियों को इस प्रथ दृष्टि से जितना महत्त्व जातक एवं धम्म पद का है उतना रत्न ने प्रभावित अवश्य किया है। कहीं-कहीं तो संस्कृत किसी अन्य बौद्ध ग्रन्थ का नहीं। इनमें भी धम्म पद में भी वही भाव उसी रूप में विद्यमान मिलते हैं। इस प्रपना सानी नहीं रखता। निश्चित ही वह धर्म साहित्य कथन की पुष्टि मे ऊपर माया एक उदाहरण उपस्थित की अपूर्व रचना है जिसका पामिक मत मतान्तरों से किया जा सकता है
ऊपर उठकर विशुद्ध नैतिक अध्ययन परमावश्यक है। मभिवादन सीलिस्स निच्च वडापचायिनो ।