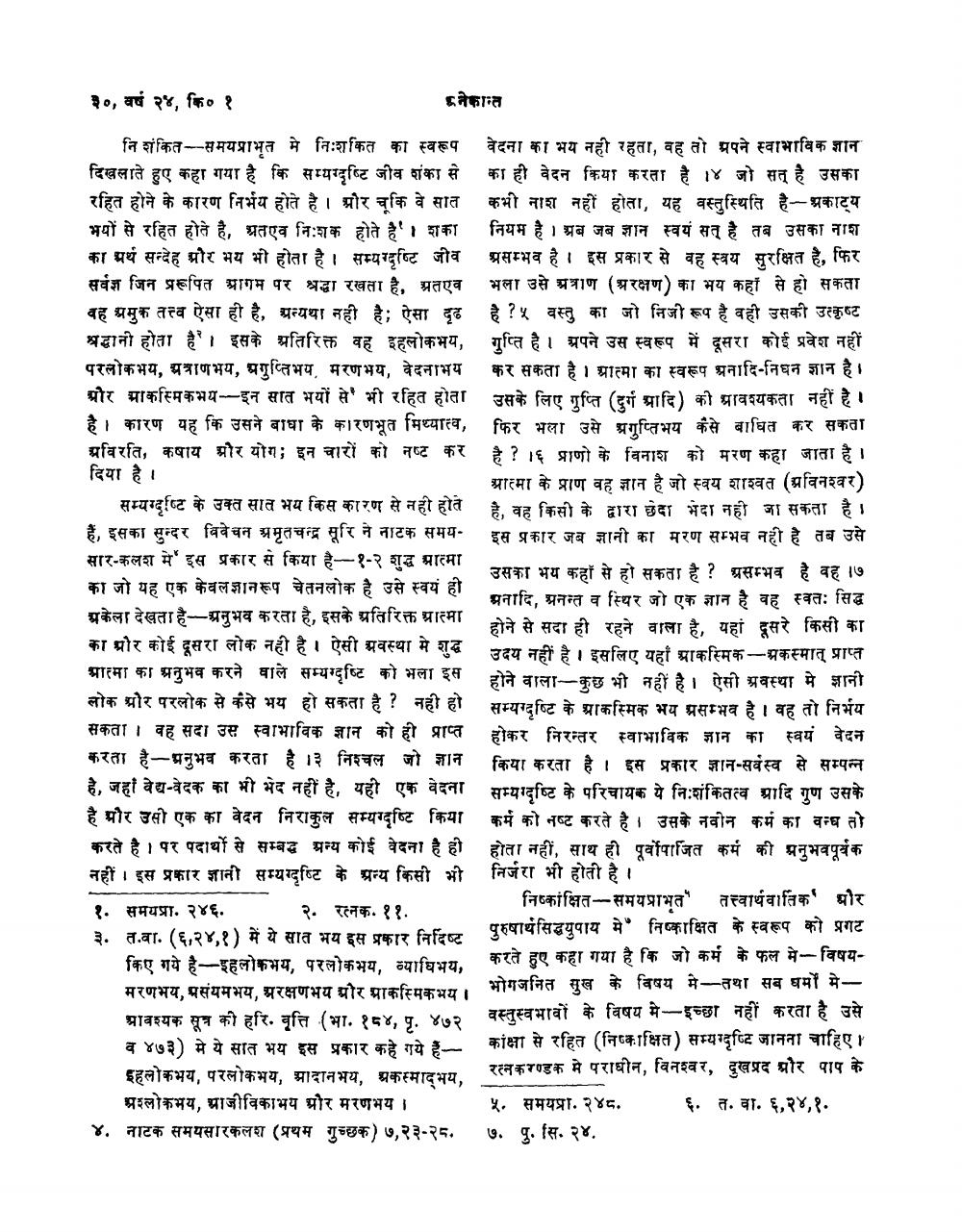________________
३०, वर्ष २४, कि०१
बनेकान्त
निशंकित-समयप्राभूत मे निःशकित का स्वरूप वेदना का भय नहीं रहता, वह तो अपने स्वाभाविक ज्ञान दिखलाते हुए कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि जीव शंका से काही वेदन किया करता है ।४ जो सत् है उसका रहित होने के कारण निर्भय होते है। और कि वे सात कभी नाश नहीं होता, यह वस्तुस्थिति है-अकाट्य भयों से रहित होते है, अतएव निःशक होते है। शका नियम है । अब जब ज्ञान स्वयं सत् है तब उसका नाश का अर्थ सन्देह और भय भी होता है। सम्यग्दृष्टि जीव असम्भव है। इस प्रकार से वह स्वय सुरक्षित है, फिर सर्वज्ञ जिन प्ररूपित आगम पर श्रद्धा रखता है, अतएव भला उसे प्रत्राण (अरक्षण) का भय कहाँ से हो सकता वह अमुक तत्त्व ऐसा ही है, अन्यथा नही है। ऐसा दृढ है ? ५ वस्तु का जो निजी रूप है वही उसकी उत्कृष्ट श्रद्धानी होता है। इसके अतिरिक्त वह इहलोकभय, गुप्ति है। अपने उस स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं परलोकभय, अत्राणभय, अगुप्तिभय, मरणभय, वेदनाभय कर सकता है। प्रात्मा का स्वरूप अनादि-निधन ज्ञान है। और माकस्मिकभय--इन सात भयों से भी रहित होता उसके लिए गप्ति (दुर्ग प्रादि) की अावश्यकता नहीं है । है। कारण यह कि उसने बाधा के कारणभूत मिथ्यात्व, फिर भला उसे अप्तिभय कैसे बाधित कर सकता अविरति, कषाय और योग; इन चारों को नष्ट कर है? ६ प्राणो के विनाश को मरण कहा जाता है। दिया है।
आत्मा के प्राण वह ज्ञान है जो स्वय शाश्वत (अविनश्वर) सम्यग्दृष्टि के उक्त सात भय किस कारण से नही होते
है, वह किसी के द्वारा छेदा भेदा नहीं जा सकता है। हैं, इसका सुन्दर विवेचन अमृतचन्द्र सूरि ने नाटक समय- इस प्रकार जब ज्ञानी का मरण सम्भव नहीं है तब उसे सार-कलश में इस प्रकार से किया है-१-२ शुद्ध प्रात्मा
उसका भय कहाँ से हो सकता है ? असम्भव है वह 1७ का जो यह एक केवलज्ञानरूप चेतनलोक है उसे स्वयं ही
अनादि, अनन्त व स्थिर जो एक ज्ञान है वह स्वतः सिद्ध अकेला देखता है-अनुभव करता है, इसके अतिरिक्त प्रात्मा
होने से सदा ही रहने वाला है, यहां दूसरे किसी का का और कोई दूसरा लोक नही है। ऐसी अवस्था मे शुद्ध
उदय नहीं है । इसलिए यहाँ आकस्मिक-अकस्मात् प्राप्त मात्मा का अनुभव करने वाले सम्यग्दृष्टि को भला इस
होने वाला-कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था मे ज्ञानी लोक और परलोक से कैसे भय हो सकता है ? नही हो सम्यग्दष्टि के प्राकस्मिक भय असम्भव है। वह तो निर्भय सकता। वह सदा उस स्वाभाविक ज्ञान को ही प्राप्त होकर निरन्तर स्वाभाविक ज्ञान का स्वयं वेदन करता है-अनुभव करता है ।३ निश्चल जो ज्ञान किया करता है। इस प्रकार ज्ञान-सर्वस्व से सम्पन्न है, जहाँ वेद्य-वेदक का भी भेद नहीं है, यही एक वेदना सम्यग्दष्टि के परिचायक ये निःशंकितत्व प्रादि गुण उसके है और उसी एक का वेदन निराकुल सम्यग्दृष्टि किया कर्म को नष्ट करते है। उसके नवीन कर्म का वन्ध तो करते है। पर पदार्थों से सम्बद्ध अन्य कोई वेदना है ही होता नहीं, साथ ही पूर्वोपाजित कर्म की अनुभवपूर्वक नहीं। इस प्रकार ज्ञानी सम्यग्दृष्टि के अन्य किसी भी निर्जरा भी होती है। १. समयप्रा. २४६.
तत्त्वार्थवातिक' और निष्कांक्षित-समयप्राभत २. रत्नक. ११. ३. त.वा. (६,२४,१) में ये सात भय इस प्रकार निर्दिष्ट पुरुषायात
पुरुषार्थसिद्धयुपाय मे निष्काक्षित के स्वरूप को प्रगट किए गये है-इहलोकभय, परलोकभय, व्याधिभय,
करते हुए कहा गया है कि जो कर्म के फल मे-विषयमरणभय, पसंयमभय, अरक्षणभय और माकस्मिकभय ।
भोगजनित सुख के विषय मे-तथा सब धर्मों मेआवश्यक सूत्र की हरि. वृत्ति (भा. १५४, पृ. ४७२ वस्तुस्वभावों के विषय मे-इच्छा नहीं करता है उसे व ४७३) मे ये सात भय इस प्रकार कहे गये हैं
कांक्षा से रहित (निष्काक्षित) सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। इहलोकभय, परलोकभय, आदान भय, अकस्माद्भय,
रत्नकरण्डक मे पराधीन, विनश्वर, दुखप्रद और पाप के अश्लोकभय, आजीविकाभय और मरणभय । ५. समयप्रा. २४८. ६. त. वा. ६,२४,१. ४. नाटक समयसारकलश (प्रथम गुच्छक) ७,२३-२८. ७. पु. सि. २४.