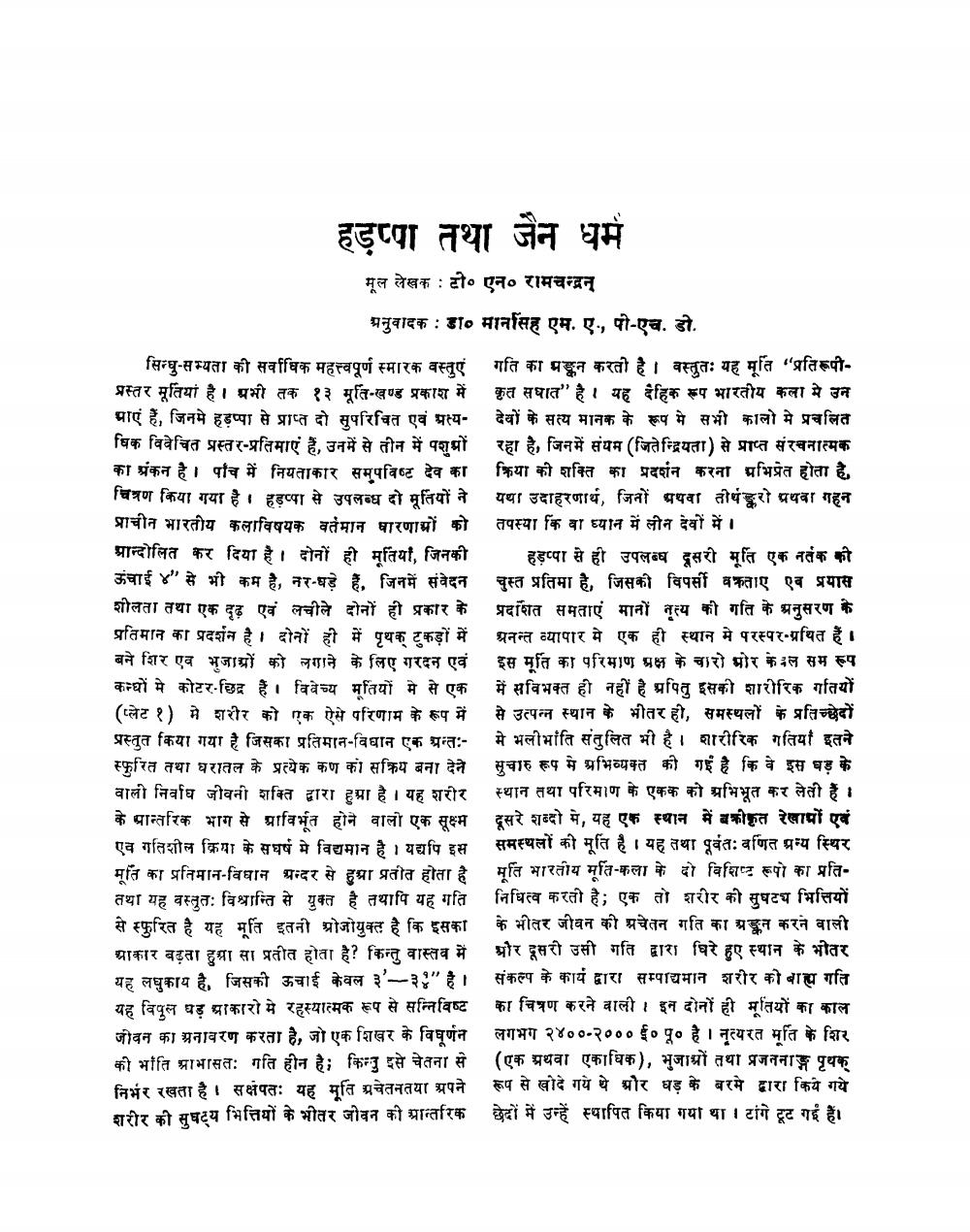________________
हड़प्पा तथा जैन धर्म
मूल लेखक डी० एन० रामचन्द्रन्
:
अनुवादक डा०
सिन्धु सभ्यता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्मारक वस्तुएं प्रस्तर मूर्तियां है। धभी तक १२ मूर्तिखण्ड प्रकाश में माएं हैं, जिनमे हड़प्पा से प्राप्त दो सुपरिचित एवं प्रत्य विक विवेचित प्रस्तर प्रतिमाएं हैं, उनमें से तीन में पशुओंों का अंकन है । पाँच में नियताकार समुपविष्ट देव का चित्रण किया गया है। हडप्पा से उपलब्ध दो मूर्तियों ने प्राचीन भारतीय कलाविषयक वर्तमान धारणाओं को प्रान्दोलित कर दिया है। दोनों ही मूर्तियों, जिनकी ऊंचाई ४" से भी कम है, नर घड़े है, जिनमें संवेदन शीलता तथा एक दृढ़ एवं लचीले दोनों ही प्रकार के प्रतिमान का प्रदर्शन है। दोनों ही में पृथ टुकड़ों में बने शिर एवं भुजाओं को लगाने के लिए गरदन एवं कम्पों में कोटर छिद्र है। विवेच्य मूर्तियों में से एक (प्लेट १ ) मे शरीर को एक ऐसे परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रतिमान विधान एक अन्त:स्फुरित तथा घरातल के प्रत्येक कण को सक्रिय बना देने वाली निर्वाध जीवनी शक्ति द्वारा हुआ है। यह शरीर के धान्तरिक भाग से प्राविर्भूत होने वाली एक सूक्ष्म एव गतिशील क्रिया के संघर्ष मे विद्यमान है । यद्यपि इस मूर्ति का प्रतिमान विधान चन्दर से हुआ प्रतीत होता है तथा यह वस्तुतः विश्रान्ति से युक्त है तथापि यह गति से स्फुरित है यह मूर्ति इतनी भोजोयुक्त है कि इसका आकार बढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है ? किन्तु वास्तव में यह लघुका है, जिसकी ऊचाई केवल ३ - ३१ है । यह विपुल घड़ ग्राकारो मे रहस्यात्मक रूप से सन्निविष्ट जीवन का अनावरण करता है, जो एक शिखर के विपूर्णन की भाँति श्राभासतः गति हीन है; किन्तु इसे चेतना से निर्भर रखता है। संक्षेपतः यह मूर्ति प्रचेतनतया अपने शरीर की सुध भित्तियों के भीतर जीवन की धान्तरिक
मानसह एम. ए., पीएच. डी.
गति का मन करती है। वस्तुतः यह मूर्ति "प्रतिरूपीकृत सघात" है । यह दैहिक रूप भारतीय कला मे उन देवों के सत्य मानक के रूप मे सभी कालो मे प्रचलित रहा है, जिनमें संयम (जितेन्द्रियता) से प्राप्त संरचनात्मक किया की शक्ति का प्रदर्शन करना प्रभिप्रेत होता है, यथा उदाहरणार्थ, जिनों अथवा तीर्थङ्करो प्रथवा गहन तपस्या किं वा ध्यान में लीन देवों में ।
1
हडप्पा से ही उपलब्ध दूसरी मूर्ति एक नर्तक की चुस्त प्रतिमा है, जिसकी विपर्सी वक्रताए एव प्रयास प्रदक्षित समताएं मानों नृत्य की गति के अनुसरण के श्रनन्त व्यापार मे एक ही स्थान में परस्पर-ग्रथित हैं । इस मूर्ति का परिमाण प्रक्ष के चारो मोर केवल सम रूप मैं सविभक्त ही नहीं है अपितु इसको शारीरिक गतियों से उत्पन्न स्थान के भीतर ही समस्थलों के प्रतिच्छेदों मे भलीभाँति संतुलित भी है। शारीरिक गतियाँ इतने सुचारु रूप मे अभिव्यक्त की गई है कि वे इस घड़ के स्थान तथा परिमाण के एकक को अभिभूत कर लेती हैं । दूसरे शब्दों में यह एक स्थान में बीकृत रेखाओं एवं समस्थलों को मूर्ति है। यह तथा पूर्वतः वर्णित धन्य स्थिर मूर्ति भारतीय मूर्ति कला के दो विशिष्ट रूपो का प्रतिनिधित्व करती है; एक तो शरीर की सुघट भित्तियों के भीतर जीवन की अचेतन गति का प्रङ्कन करने वाली और दूसरी उसी गति द्वारा घिरे हुए स्थान के भीतर संकल्प के कार्य द्वारा सम्पाद्यमान शरीर को बाह्य गति का चित्रण करने वाली । इन दोनों ही मूर्तियों का काल लगभग २४००-२००० ई० पू० है । नृत्यरत मूर्ति के शिर ( एक अथवा एकाधिक ), भुजाओं तथा प्रजननाङ्ग पृथ रूप से खोदे गये थे घोर पढ़ के बरमे द्वारा किये गये छेदों में उन्हें स्थापित किया गया था। टांग टूट गई हैं।