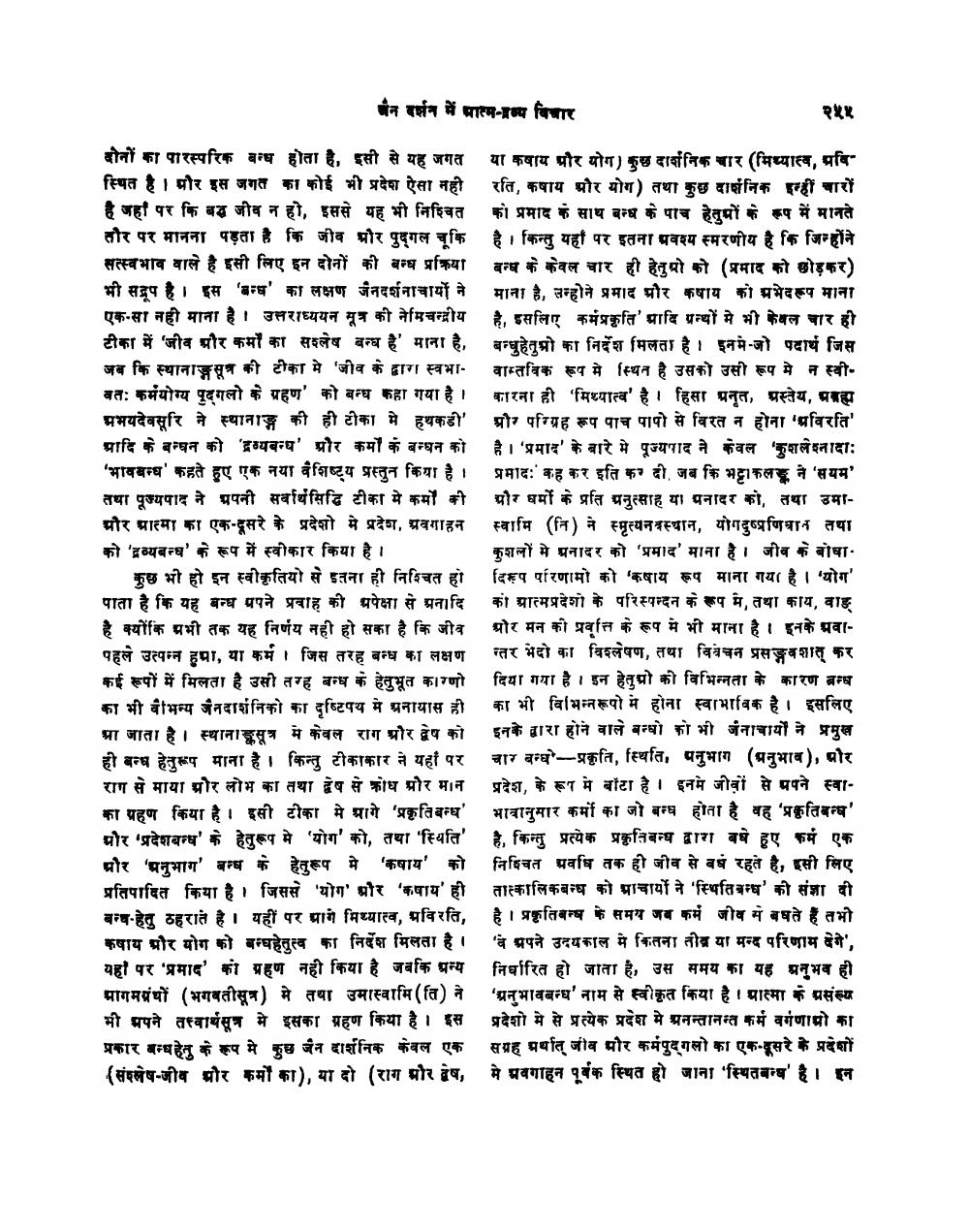________________
चन वर्शन में प्रात्म-व्य विचार
२५५
दोनों का पारस्परिक बन्ध होता है, इसी से यह जगत या कषाय और योग) कुछ दार्शनिक चार (मिथ्यात्व, प्रवि स्थित है। और इस जगत का कोई भी प्रदेश ऐसा नही रति, कषाय और योग) तथा कुछ दार्शनिक इन्हीं चारों है जहां पर कि बढ जीव न हो, इससे यह भी निश्चित को प्रमाद के साथ बन्ध के पाच हेतुमों के रूप में मानते तौर पर मानना पड़ता है कि जीव और पुद्गल चूकि है। किन्तु यहाँ पर इतना अवश्य स्मरणीय है कि जिन्होंने सत्स्वभाव वाले है इसी लिए इन दोनों की बन्ध प्रक्रिया बन्ध के केवल चार ही हेतुपो को (प्रमाद को छोड़कर) भी सद्रूप है। इस 'बन्ध' का लक्षण जैनदर्शनाचार्यों ने माना है, उन्होने प्रमाद और कषाय को प्रभेदरूप माना एक-सा नही माना है। उत्तराध्ययन मूत्र की नेमिचन्द्रीय है, इसलिए कर्मप्रकृति' प्रादि ग्रन्थों मे भी केवल चार ही टीका में 'जीव और कर्मों का सश्लेष बन्ध है' माना है, बन्धहेतप्रो का निर्देश मिलता है। इनमे-जो पदार्थ जिस जब कि स्थानाङ्गसूत्र की टीका मे 'जीव के द्वारा स्वभा- वास्तविक रूप में स्थित है उसको उसी रूप मे न स्वीवत: कर्मयोग्य पुदगलो के ग्रहण' को बन्ध कहा गया है। कारना ही 'मिथ्यात्व' है। हिसा अनूत, अस्तेय, प्रब्रह्म मभयदेवसूरि ने स्थानाङ्ग की ही टीका मे हथकडी' और परिग्रह रूप पाच पापो से विरत न होना 'अविरति' प्रादि के बन्धन को 'द्रव्यबन्ध' और कर्मों के बन्धन को है। 'प्रमाद' के बारे मे पूज्यपाद ने केवल 'कुशलेश्नादा: 'भावबन्ध' कहते हुए एक नया वैशिष्ट्य प्रस्तुत किया है। प्रमाद: कह कर इति कर दी, जब कि भट्टाकलङ्क ने 'सयम' तथा पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थ सिद्धि टीका मे कर्मों की और धर्मों के प्रति अनुत्साह या अनादर को, तथा उमापौर प्रात्मा का एक-दूसरे के प्रदेशो मे प्रदेश, अवगाहन स्वामि (ति) ने स्मृत्यनवस्थान, योगदुष्प्रणिधान तथा को 'द्रव्यबन्ध' के रूप में स्वीकार किया है।
कुशलों मे अनादर को 'प्रमाद' माना है। जीव के बोषा. ___ कुछ भी हो इन स्वीकृतियो से इतना ही निश्चित हो दिरूप परिणामो को 'कषाय रूप माना गया है । 'योग' पाता है कि यह बन्ध अपने प्रवाह की अपेक्षा से अनादि को प्रात्मप्रदेशो के परिस्पन्दन के रूप में, तथा काय, वाङ् है क्योंकि अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका है कि जीव और मन की प्रवृत्ति के रूप में भी माना है। इनके प्रवापहले उत्पन्न हुमा, या कर्म। जिस तरह बन्ध का लक्षण तर भेदो का विश्लेषण, तथा विवेचन प्रसङ्गवशात् कर कई रूपों में मिलता है उसी तरह बन्ध के हेतुभूत कारणो। दिया गया है । इन हेतुप्रो को विभिन्नता के कारण बन्ध का भी वीभन्य जैनदार्शनिको का दृष्टिपथ मे अनायास ही का भी विभिन्न रूपो में होना स्वाभाविक है। इसलिए पा जाता है। स्थानाङ्कसूत्र में केवल राग और द्वेष को इनके द्वारा होने वाले बन्धो को भी जैनाचार्यों ने प्रमुख ही बन्ध हेतुरूप माना है। किन्तु टीकाकार ने यहां पर चार बन्ध-प्रकृति, स्थिति, पनुभाग (अनुभाव), और राग से माया पोर लोभ का तथा द्वेष से क्रोध और मान प्रदेश, के रूप में बाँटा है। इनमे जीवों से अपने स्वाका ग्रहण किया है। इसी टीका मे मागे 'प्रकृतिबन्ध' भावानुमार कर्मो का जो बन्ध होता है वह 'प्रकृतिबन्ध' पौर 'प्रदेशबन्ध' के हेतुरूप मे 'योग' को, तथा 'स्थिति' है, किन्तु प्रत्येक प्रकृतिबन्ध द्वारा बधे हुए कर्म एक और 'मनुभाग' बन्ध के हेतुरूप मे 'कषाय' को निश्चित अवधि तक ही जीव से बधं रहते है, इसी लिए प्रतिपादित किया है। जिससे 'योग' और 'कषाय' ही तात्कालिकबन्ध को प्राचार्यों ने 'स्थितिबन्ध' की संज्ञा दी बन्ध-हेतु ठहराते है। यहीं पर पागे मिथ्यात्व, अविरति, है। प्रकृतिबन्ध के समय जब कर्म जीव में बषते हैं तभी कषाय और योग को बन्धहेतुत्व का निर्देश मिलता है। वे अपने उदयकाल में कितना तीव्र या मन्द परिणाम देगे', यहाँ पर 'प्रमाद' को ग्रहण नही किया है जबकि अन्य निर्धारित हो जाता है, उस समय का यह अनुभव ही मागमयंघों (भगवतीसूत्र) मे तथा उमास्वामि (ति) ने 'अनुभावबन्ध' नाम से स्वीकृत किया है । मात्मा के असंख्य भी अपने तत्वार्थसूत्र मे इसका ग्रहण किया है। इस प्रदेशो में से प्रत्येक प्रदेश मे अनन्तानन्त कर्म वर्गणामो का प्रकार बन्ध हेतु के रूप मे कुछ जैन दार्शनिक केवल एक सग्रह अर्थात् जीव भोर कर्मपुद्गलो का एक-दूसरे के प्रदेशों (संश्लेष-जीव और कर्मों का), या दो (राग मोर वेष, मे अवगाहन पूर्वक स्थित हो जाना 'स्थितबन्ध' है। इन