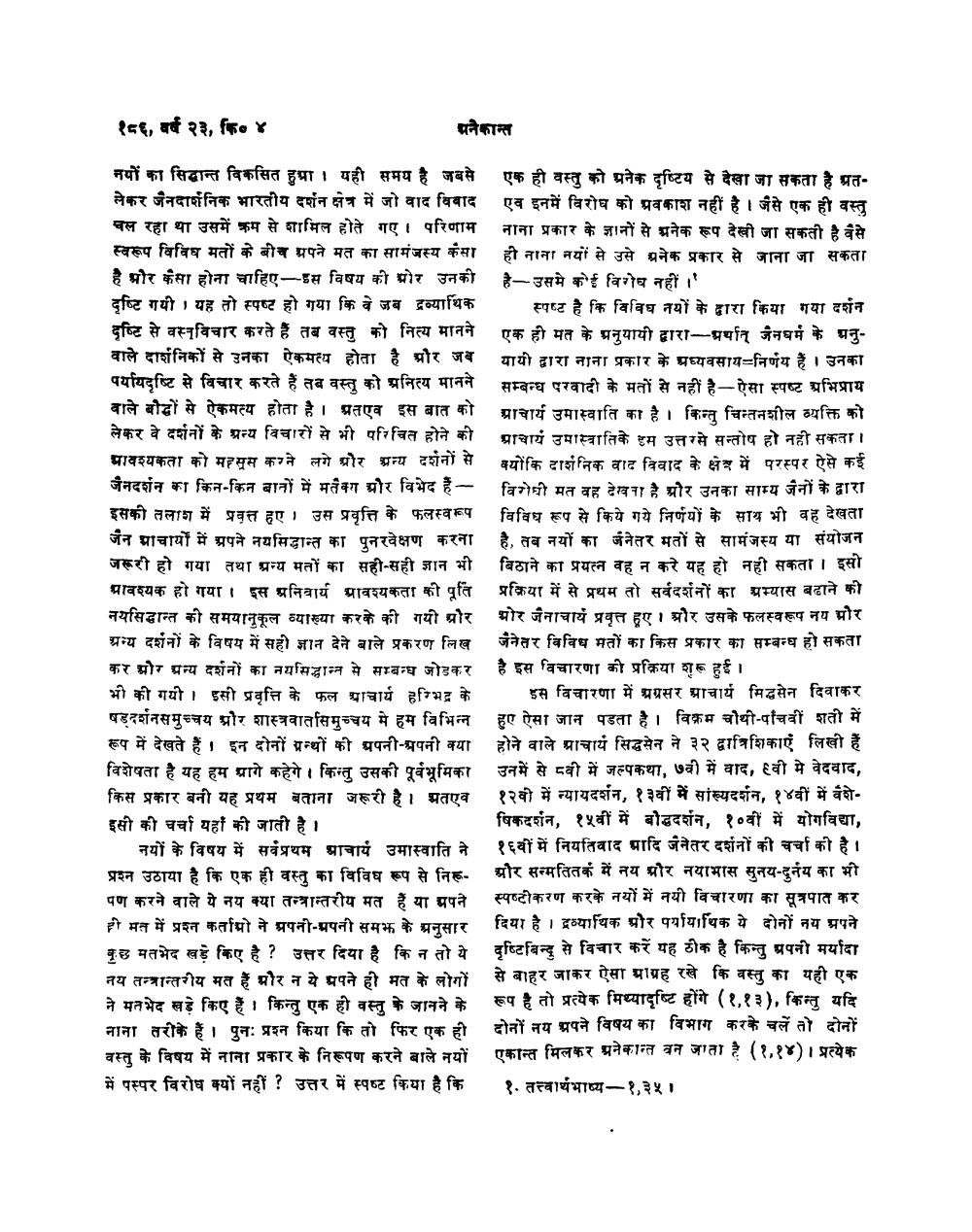________________
१९६, वर्ष २३, कि०४
मनैकान्त
नयों का सिद्धान्त विकसित हुप्रा । यही समय है जबसे एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिय से देखा जा सकता है प्रतलेकर जैनदार्शनिक भारतीय दर्शन क्षेत्र में जो वाद विवाद एव इनमें विरोध को प्रवकाश नहीं है । जैसे एक ही वस्तु चल रहा था उसमें क्रम से शामिल होते गए। परिणाम नाना प्रकार के ज्ञानों से अनेक रूप देखी जा सकती है वैसे स्वरूप विविध मतों के बीच अपने मत का सामंजस्य कैसा ही नाना मयों से उसे अनेक प्रकार से जाना जा सकता है और कैसा होना चाहिए-इस विषय की पोर उनकी है-उसमे कोई विरोध नहीं।' दृष्टि गयी। यह तो स्पष्ट हो गया कि वे जब द्रव्यार्थिक स्पष्ट है कि विविध नयों के द्वारा किया गया दर्शन दृष्टि से वस्तुविचार करते हैं तब वस्तु को नित्य मानने एक ही मत के अनुयायी द्वारा-प्रर्थात् जैनधर्म के अनुवाले दार्शनिकों से उनका ऐकमत्य होता है और जब यायो द्वारा नाना प्रकार के प्रध्यवसाय-निर्णय हैं । उनका पर्यायदृष्टि से विचार करते हैं तब वस्तु को प्रनित्य मानने सम्बन्ध परवादी के मतों से नहीं है-ऐसा स्पष्ट अभिप्राय वाले बौद्धों से ऐकमत्य होता है। प्रतएव इस बात को प्राचार्य उमास्वाति का है। किन्तु चिन्तनशील व्यक्ति को लेकर वे दर्शनों के अन्य विचारों से भी परिचित होने की प्राचार्य उमास्वातिके हम उत्तरसे सन्तोष हो नहीं सकता। पावश्यकता को महसस करने लगे और अन्य दर्शनों से क्योंकि दार्शनिक वाद विवाद के क्षेत्र में परस्पर ऐसे कई जैनदर्शन का किन-किन बातों में मतैक्ग और विभेद है - विरोधी मत वह देखना है और उनका साम्य जनों के द्वारा इसकी तलाश में प्रवृत्त हए। उस प्रवृत्ति के फलस्वरूप विविध रूप से किये गये निर्णयों के साथ भी वह देखता जन प्राचार्यों में अपने नय सिद्धान्त का पुनरवेक्षण करना है, तब नयों का नेतर मतों से सामंजस्य या संयोजन जरूरी हो गया तथा अन्य मतों का सही-सही ज्ञान भी बिठाने का प्रयत्न वह न करे यह हो नहीं सकता। इसी पावश्यक हो गया। इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया में से प्रथम तो सर्वदर्शनों का अभ्यास बढाने की नयसिद्धान्त की समयानुकूल व्याख्या करके की गयी और भोर जैनाचार्य प्रवृत्त हुए। और उसके फलस्वरूप नय मौर अन्य दर्शनों के विषय में सही ज्ञान देने बाले प्रकरण लिख जनेतर विविध मतों का किस प्रकार का सम्बन्ध हो सकता कर और अन्य दर्शनों का नयसिद्धान्त से सम्बन्ध जोडकर है इस विचारणा की प्रक्रिया शुरू हुई। भी की गयी। इसी प्रवृत्ति के फल प्राचार्य हरिभद्र के इस विचारणा में अग्रसर प्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर षड्दर्शनसमुच्चय और शास्त्रवासिमुच्चय मे हम विभिन्न हुए ऐसा जान पडता है। विक्रम चौथी-पांचवीं शती में रूप में देखते हैं । इन दोनों ग्रन्थों की अपनी-अपनी क्या होने वाले प्राचार्य सिद्धसेन ने ३२ द्वात्रिशिकाएं लिखी हैं विशेषता है यह हम प्रागे कहेगे। किन्तु उसकी पूर्वभूमिका उनमें से ८वी में जल्पकथा, ७वी में वाद, हवी मे वेदवाद, किस प्रकार बनी यह प्रथम बताना जरूरी है। प्रतएव १२वी में न्यायदर्शन, १३वीं में सांख्यदर्शन, १४वीं में वैशेइसी की चर्चा यहाँ की जाती है।
षिकदर्शन, १५वीं में बौद्धदर्शन, १०वीं में योगविद्या, नयों के विषय में सर्वप्रथम प्राचार्य उमास्वाति ने १६वीं में नियतिवाद प्रादि जैनेतर दर्शनों की चर्चा की है। प्रश्न उठाया है कि एक ही वस्तु का विविध रूप से निरू. और सन्मतितर्क में नय और नयाभास सुनय-दुनय का भी पण करने वाले ये नय क्या तन्त्रान्तरीय मत हैं या अपने स्पष्टीकरण करके नयों में नयी विचारणा का सूत्रपात कर ही मत में प्रश्न कर्तामो ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार दिया है । द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये दोनों नय अपने कृछ मतभेद खड़े किए है ? उत्तर दिया है कि न तो ये दृष्टिबिन्दु से विचार करें यह ठीक है किन्तु अपनी मर्यादा नय तन्त्रान्तरीय मत हैं और न ये अपने ही मत के लोगों से बाहर जाकर ऐसा माग्रह रखे कि वस्तु का यही एक ने मतभेद खड़े किए हैं। किन्तु एक ही वस्तु के जानने के रूप है तो प्रत्येक मिथ्यादृष्टि होंगे (१.१३), किन्त यदि नाना तरीके हैं। पुनः प्रश्न किया कि तो फिर एक ही दोनों नय अपने विषय का विभाग करके चलें तो दोनों वस्तु के विषय में नाना प्रकार के निरूपण करने बाले नयों एकान्त मिलकर अनेकान्त बन जाता है (१,१४)। प्रत्येक में पस्पर विरोध क्यों नहीं ? उत्तर में स्पष्ट किया है कि १. तत्त्वार्थभाष्य-१,३५।